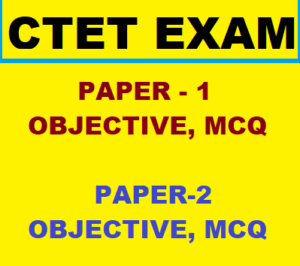ज्ञान एवं पाठ्यक्रम
| विश्वविद्यालय | महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बी.एड तृतीय सेमेस्टर |
| विषय | 303- ज्ञान एवं पाठ्यक्रम सिलेबस , नोट्स , क्वेश्चन पेपर |
| सेमेस्टर | तृतीय सेमेस्टर |
| कोर्स | बी.एड |
| lnfo | इस पेज में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बी.एड तृतीय सेमेस्टर के ज्ञान एवं पाठ्यक्रम सिलेबस नोट्स क्वेश्चन पेपर दिया गया है | |
VVI NOTES .IN के ईस में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ बीएड के सेमेस्टर -३ के ज्ञान एवं पाठ्यक्रम सिलेबस , ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के नोट्स , ज्ञान एवं पाठ्यक्रम क्वेश्चन पेपर , दिया गया है |
MGKVP B.Ed 3rd SEMESTER ALL SUBJENT NAME
-
- विषय शिक्षण प्रथम
- विषय शिक्षण द्वितीय
- ज्ञान एवं पाठ्यक्रम
- समावेशी शिक्षा
ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नोट्स
| विषय | ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नोट्स
Knowledge and Curriculum |
| पेपर | 303 |
| विश्वविद्यालय | महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बी.एड तृतीय सेमेस्टर के नोट्स |
| सेमेस्टर | तृतीय सेमेस्टर |
| lnfo | यहा महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बी.एड तृतीय सेमेस्टर के नोट्स के पेपर -303 विषय शिक्षण प्रथम नोट्स दिया गया है | यह विषय सभी स्टूडेंट्स का समान होता है | |
लघु उत्तरीय प्रश्न
(Short Answer Type Questions)
नोट : प्रश्न संख्या 1 (a से j) लघु उत्तरीय प्रश्न है। परीक्षार्थियों को सभी दस प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं।
निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए- 10 x 2 = 20 अंक)
प्रश्न ‘a (i) ज्ञान का अर्थ बताइए।
उत्तर – शिक्षा का आधार ज्ञान ही होता है परन्तु ज्ञान का स्वरूप व्यवस्थित नहीं होता है बल्कि यह अनुभवों एवं प्रत्यक्षीकरण पर आधारित होता है। हमारे जीवन में हमें विभिन्न प्रकार के अच्छे तथा बुरे अनुभव होते हैं जो हमारे मन-मस्तिष्क पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। ज्ञान इन्हीं अनुभवों से सम्बन्धित होता है। अनुभव हमें यह भी बताते हैं कि कौन-सी चीज जीवन तथा समाज के लिए उपयोगी है और कौन-सी नहीं। यह अनुभव जब हम दूसरों को बाँटने का प्रयास करते हैं तो यह दूसरों के लिए ज्ञान बन जाता है। इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि ज्ञान केवल एक व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण समाज के लिए उपयोगी होता है।
ज्ञान का अर्थ स्पष्ट तौर पर उन सूचनाओं का संग्रह माना जाता है जो किसी वस्तु, परिस्थिति और अनुभवों की समझ को विकसित करने में सहायक होते हैं। ज्ञान समस्त शिक्षा का आधार है। शिक्षा किसी भी प्रकार की हो, चाहे विद्यालयीय औपचारिक या अनौपचारिक ज्ञान एक साधन एवं साध्य दोनों ही रूपों में पाया जाता है। ज्ञान किसी परिस्थिति एवं प्रक्रिया से सम्बन्धित तथ्य और सत्य है। यह हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों तथा वातावरण से सम्बन्धित कई तरह के लक्ष्य होते हैं जो सत्य पर आधारित होते हैं। इन परिस्थितियों और वातावरण की लक्ष्यपूर्ण जानकारी ज्ञान कहलाती है जो वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमेशा परिमार्जित तथा परिशोधित रूप में हस्तान्तरित होता रहता है। ज्ञान अनुभवों की समझ पर आधारित सूचनाएँ हैं सभी व्यक्तियों को जीवन में अनुभव होते रहते हैं और इन अनुभवों का जब हम सामान्यीकरण कर लेते हैं और इन्हें एक सिद्धान्त तथा नियम के रूप में विकसित कर लेते हैं तो यह ज्ञान बन जाता है। यही ज्ञान सम्पूर्ण समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो जाता है।
प्रश्न a (ii) विश्वास और सत्य के बीच अन्तर लिखिए।
उत्तर-विश्वास और सत्य संबंधित अवधारणाएँ हैं, लेकिन वे अलग-अलग चीजों को संदर्भित करते हैं। विश्वास और सत्य में अंतर है। विश्वास एक मानसिक दृष्टिकोण या दृढ़ विश्वास है कि कोई चीज सत्य या वास्तविक है, बिना इसके समर्थन में सबूत या प्रमाण के। विश्वास व्यक्तिगत अनुभव, अंतर्ज्ञान, अधिकार या सांस्कृतिक और धार्मिक शिक्षाओं पर आधारित हो सकते हैं।
दूसरी ओर, सत्य, मामलों की वास्तविक स्थिति या जिस तरह से चीजें हैं, उसे संदर्भित करता है। यह व्यक्तिगत विश्वासों या राय से स्वतंत्र है और इसे साक्ष्य या अवलोकन के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। सत्य वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक है, जिसका अर्थ है कि यह सभी पर लागू होता है, चाहे उनकी मान्यताएँ या दृष्टिकोण कुछ भी हों।
संक्षेप में, विश्वास एक व्यक्तिपरक दृढ़ विश्वास या किसी चीज को सत्य के रूप में स्वीकार करना है, जबकि सत्य एक वस्तुनिष्ठ तथ्य या वास्तविकता है जो व्यक्तिगत विश्वासों या विचारों से स्वतंत्र रूप में मौजूद है।
प्रश्न a (iii) ज्ञान बनाम विश्वास ।
उत्तर-ज्ञान और विश्वास दो ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ के मामले में अक्सर भ्रम हो जाता है, जबकि कड़ाई से बोलने पर उनके बीच कुछ अंतर होता है। ज्ञान पूरी तरह से जानकारी के बारे में है ज्ञान वह है जो हम अनुभव और प्रयोग के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यह हमारे चारों ओर की दुनिया की वास्तविकताओं से उत्पन्न होता है। जैसे-जैसे दुनिया आगे बढ़ी, ज्ञान के विभिन्न स्रोतों का भी विस्तार हुआ है। दूसरी ओर, विश्वास पूरी तरह से दृढ़ विश्वास पर आधारित है। यह अधिकतर धार्मिक परिवेश में दिखाई देता है, जहाँ आदर्शों का परीक्षण नहीं किया जाता बल्कि केवल विश्वास किया जाता है। यह दोनों शब्दों के बीच मुख्य अंतर है। यह लेख अंतरों को उजागर करते हुए दो शब्दों के बीच के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास करता है।
विश्वास एक दृढ़तापूर्वक रखी गई राय है। इसके लिए किसी जानकारी की आवश्यकता नहीं होती जैसा कि ज्ञान के मामले में होता है। विश्वास कुछ सिद्धांतों के इर्द-गिर्द घूमता है। इसमें विश्वास एक ऐसे कारक के रूप में है जो शासन करता है। आत्म-अनुभव पर निर्भर ज्ञान के विपरीत, विश्वास व्यक्ति के शुद्ध विश्वास से उत्पन्न होता है। व्यक्ति को विश्वास करने के लिए घटना का अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। यह उसके आंतरिक विश्वास से आता है। अधिकांश धर्मों में विश्वास एक मूल सिद्धांत है। यही विश्वास लोगों को उस धर्म विशेष का सच्चा अनुयायी बनाता है। मानव बुद्धि द्वारा निर्देशित ज्ञान के विपरीत, विश्वास नहीं है। विश्वास धार्मिक विश्वासों पर आधारित है। यह सच है कि आस्था और विश्वास एक साथ चलते हैं। विश्वास की परिणति विश्वास में होती है। हो सकता हैं कि इसका उलटा सच न हो।
प्रश्न a (iv) ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए।
अथवा
ज्ञान निर्माण से आप क्या समझते हैं?
उत्तर-
किसी वस्तु के सम्बन्ध में जानकारी को ज्ञान कहते हैं। वह वस्तु कुछ भी हो सकती है जैसे- बैंक द्वारा दिया हुआ कर्ज या गणित की समस्या इत्यादि । ज्ञान का उद्देश्य किसी वस्तु के सम्बन्ध में जैसी वह है वैसी ही उसकी जानकारी होना है। हमारी इस बात की चिन्ता कि हम ठीक से जान जायें, कि यह वस्तु यथार्थ में वैसी ही है जैसा उसका ज्ञान यह जाहिर कर देता है कि इस बात की सम्भावना है कि हम धोखा खा रहे हों और हमारे कुछ निर्णय उस वस्तु के सम्बन्ध में गलत भी हो सकते हैं। एक गलत निर्णय हमें इस बात से अवगत न कराकर कि वस्तु यथार्थ में कैसी है इस बात का ज्ञान हमें करायेगी कि वस्तु हमें ऐसी प्रतीत होती है। अतएव यदि हम उन दशाओं के सम्बन्ध में जानकारी रखें सकते हैं जिनमें हमारे निर्णय सत्य हैं तब हम उसके साथ-साथ ऐसे स्तर निर्धारित कर सकते हैं जिनके द्वारा हम कृत्रिम का यथार्थता से विभेद कर सकते हैं।
किसी वस्तु के सम्बन्ध में जब हम यह कहते हैं कि हमें उसकी जानकारी है तो हम यह मान कर चलते हैं कि यह जानकारी सत्य है। अतएव ज्ञान की धारणा में पहली बात तो यह निहित है कि ज्ञान को अवश्य सत्य होना चाहिए। जैसे जब हम कहते हैं कि सोहन को हम जानते हैं तो सोहन से हमारा परिचय सत्य होना चाहिए। दूसरी बात यह कि ज्ञाता को उस बात की सत्यता में विश्वास होना चाहिए। हम सोहन को जानते हैं तथा तीसरी बात यह कि ज्ञाता के पास इस बात के पर्याप्त प्रमाण होने चाहिए कि यह बात सत्य है। हमारे पास इस बात के प्रमाण होने चाहिए कि हम सोहन को जानते हैं जैसे हम सोहन से कई बार मिल चुके हैं या हम और सोहन साथ-साथ पढ़े हैं इत्यादि। इस प्रकार ज्ञान के अर्थ में तीन बातें आती हैं-सत्यता, सत्यता में विश्वास तथा सत्यता के लिए पर्याप्त प्रमाण ।
•
प्रश्न a (v) अन्तर्ज्ञान ज्ञान का स्त्रोत ।
उत्तर-
हमें अपनी स्वतंत्रता का आभास अन्तर्ज्ञान से होता है। एक दार्शनिक का दिमाग संसार की विभिन्न समस्याओं के बारे में सोचता है और वह एक आधारभूत सिद्धांत विकसित कर लेता है वास्तविकता का ज्ञान वैज्ञानिक विधि से नहीं हो सकता। इसके लिए अन्तर्ज्ञान की आवश्यकता होती हैं प्राकृतिक विज्ञान और कॉमनसेंस वस्तुओं की बाहरी रूप से व्याख्या करते हैं। हमें उनकी वास्तविकता को जानने के लिए उनके अन्दर घुसना पड़ता है। इसके लिए अंतर्ज्ञान की आवश्यकता होती है।
उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि अन्तर्ज्ञान ज्ञान का महत्त्वपूर्ण स्रोत है। पर इसे बुद्धि से अलग नहीं किया जा सकता। अन्तर्ज्ञान तथा बुद्धि दोनों चित्त के व्यापार हैं। चित्त की पहली अवस्था का नाम है बुद्धि तथा दूसरी का अन्तर्ज्ञान। दोनों परस्पर सहयोगी व सहगामी हैं। बुद्धि के अभाव में अन्तर्बोध असहाय है। इस प्रकार अन्तर्ज्ञान व बुद्धि दोनों ही प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।
इनके अतिरिक्त ज्ञान के स्रोत के रूप में निम्नलिखित को भी शामिल किया जा सकता है-
1. श्रुति-
इस शब्द का अर्थ है-सुनना या प्रकट होना। विभिन्न धर्म ग्रन्थों की प्रामाणिकता के सिद्ध करने के लिए प्रायः यह कहा जाता है कि उस धर्म के प्रर्वतकों ने अपने दिव्य नेत्रों के द्वारा वचने को प्रत्यक्ष किया है। अर्थात् श्रुति का सम्बन्ध ज्ञान से होता है। धार्मिक ज्ञान के लिए यह महत्त्वपूर्ण है भारत सहित दूसरे देशों के धार्मिक ग्रन्थों का आधार श्रुति है। इस प्रकार प्राप्त ज्ञान देश व काल की सीमाओं से परे अतः सार्वभौमिक होता है। हमारे ऋषि-मुनियों तथा गुरुओं को दिव्य व अलौकिक शक्तियों का ज्ञान प्राप्त होता है जो बाहरी कानों से सुना नहीं जा सकता, अपितु अपनी अन्दर की आवाज से सुना जाता है। लेकिन श्रुति को प्रामाणिक मानने में अनेक कठिनाइयाँ सामने आती हैं। क्योंकि विभिन्न श्रुतियाँ एक-दूसरे की विरोधी बातें कहती हैं। ऐसी स्थिति में उनकी सत्यता की जाँच के लिए हमें अनुभव व तर्क की सहायता लेने में संकोच नहीं करना चाहिए।
2. आस्था-
आस्था शब्द का अर्थ-लगाव अथवा विश्वास। हमारी विरासत में ऐसी कई बातें चली आ रही हैं जिनका तार्किक आधार नहीं होता है। परन्तु उन बातों को सिरे से नहीं नकारा जा सकता है
वास्तव में ज्ञान के ये सभी स्रोत एक-दूसरे के पूरक हैं। इस संदर्भ में प्रो० मोण्टेन का यह कथन ध्यान देने योग्य है कि “ज्ञान के स्रोतों का वास्तव में एक संघ है।”
प्रश्न a (vi) प्राधिकार : ज्ञान का स्रोत ।
उत्तर-
प्राधिकार भी ज्ञान प्राप्ति का एक स्रोत है। कुछ लोग अपने क्षेत्र में पारंगत होते हैं, जैसे अर्थशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, गणितज्ञ आदि विभिन्न लोग अपने प्रयोगों और ज्ञान के आधार पर कुछ नियमों के ऊपर प्राधिकार रखते हैं। हम उनके ज्ञान को चुनौती नहीं दे सकते और उनकी बातों को बिना संदेह के सच मानते हैं। इसको दूसरे शब्दों में हम आप्तवचन भी कह सकते हैं। इसका अर्थ है- दूसरे के वचन पर विश्वास करके प्राप्त किया गया ज्ञान। हमारे ज्ञान का एक बड़ा भाग वह होता जिसे न तो हम ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त करते हैं और न ही बुद्धि अथवा तर्क से। इसे हम दूसरों के वचनों पर विश्वास करके प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आप्तवचन भी ज्ञान का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है।
प्रश्न a (vii) ज्ञान व सूचना में समानता बताइए।
उत्तर-
यदि हम ज्ञान व सूचना से सम्बन्धित विभिन्न परिभाषाओं का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि दोनों प्रत्ययों में सम्बन्ध है। उदाहरणार्थ-सूचना का निष्कर्षण मूल आँकड़ों में होता है और ज्ञान का उद्भव भी मूल आँकड़ों से होता है। इस प्रकार दोनों ही प्रत्यय हेतु मूल स्रोत आँकड़े ही हैं। नितेकी (Nitecki) ने दोनों प्रत्ययों की व्याख्या निम्न वाक्यों द्वारा की, Information is knowledge affects 3 “Knowledge is information processed with a point of nice through reprentation”, जिससे पता चलता है कि ज्ञान व सूचना एक ही है परन्तु ज्ञान सूचना का अधिक विकसित रूप है। इसका यह तथ्य है कि ज्ञान व सूचना दोनों की पहचान अवलोकन (Observation) में ही होती है, इसके द्वारा भी ज्ञान व सूचना को समान माना जा सकता है।
ओटन (Otten) ने इन दोनों सम्प्रत्ययों का वर्णन इसकी प्रक्रियाओं के आधार पर इस प्रकार किया है “सूचना के अर्जन की प्रक्रिया में इसका हस्तान्तरण ज्ञान में होता है व ज्ञान का सम्मिलित (assimilation) एक सामान्य समझ में व अंतः बुद्धि (Wisdom) में होता है।”
इस समाज में दो प्रकार के बुद्धिजीवी (Intellectuals) होते हैं, लोक बुद्धिजीवी और नीति बुद्धिजीवी । हमें यह समझना होगा कि दोनों के कार्यक्षेत्र पृथक् न होकर एक है। लोकनीति एक सम्पूर्ण विषय-वस्तु है जहाँ नीति बुद्धिजीवी अपने ज्ञान को केवल एक लिखित और सैद्धान्तिक वस्तु मानकर रूपरेखा तैयार कर देते हैं वहीं लोक बुद्धिजीवी किसी तथ्य को गहराई से समझने का प्रयत्न करते हैं ये नीतियों के सूक्ष्म तथ्यों और नैतिकता के सापेक्ष रखते हैं। समस्या यह है कि 90 के दशक के बाद से भारत में लोक बुद्धिजीवियों की अपेक्षा नीति बुद्धिजीवियों का आधिक्य हो गया है जिसके कारण आज भारत ज्ञान का उपभोक्ता मात्र बनकर रह गया है। यह केवल ज्ञान को आत्मसात करने की चेष्टा करता है, स्वयं इसकी व्याख्या या नए खोज में रुचि नहीं रखता और यही कारण है कि भारत अन्य देशों की अपेक्षा काफी पीछे रह गया है।
प्रश्न a (viii) सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञान में अन्तर बताइए ।
उत्तर-
सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञान में निम्न अन्तर है-
सैद्धान्तिक ज्ञान (Theoretical Knowledge) स्वयं प्रत्यक्ष की भाँति समझा जाता है। सिद्धान्त जब समझ लिए जाते हैं, सत्य पहचान लिए जाते हैं फिर उन्हें निरीक्षण, अनुभव या प्रयोग द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से ज्ञान को स्वतः सिद्ध या प्रमाणित मान लिया जाता है। इस प्रकार के ज्ञान में तर्क द्वारा तथ्यों को संगठित कर दिया जाता है तथा बुद्धि इसे बिना अनुभव की सहायता से प्राप्त कर लेती है।
व्यावहारिक ज्ञान (Practical Knowledge) प्रयोग द्वारा प्राप्त होता है। डीवी के अनुसार, ज्ञान की प्रक्रिया एक प्रयास एवं समझ (Trying and Undergoing) की प्रक्रिया है—एक विचार का अभ्यास में प्रयास करना एवं ऐसे प्रयास के परिणामस्वरूप जो फल प्राप्त होते हैं उनसे सीखता है। एक धारणा के अनुसार ज्ञान कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे अनुभव द्वारा सक्रिय रूप में न लाया जा सके। व्यावहारिक ज्ञान स्वयमेव उद्भासित होता है इसमें किसी पूर्व धारणा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि हम शतरंज के खिलाड़ी का उदाहरण लें तो उसके लिए शतरंज का ज्ञान सैद्धान्तिक ज्ञान होगा अर्थात् खेलने के क्या नियम हैं आदि। परन्तु इस खेल में वह कैसे महारत हासिल करे या प्रतिद्वन्द्वी की दी हुई चुनौती का मुकाबला कैसे कर सकता है, यह सब व्यावहारिक ज्ञान है। व्यावहारिक ज्ञान (Practical Knowledge) हेतु नियमों की पाबन्दी नहीं होती है। यह ज्ञान कौशल पर आधारित ज्ञान होता है। अतः व्यावहारिक ज्ञान प्रयोग द्वारा प्राप्त होता है। एक विचार को अभ्यास में परिवर्तित करने का प्रयास करना एवं ऐसे प्रयास के परिणामस्वरूप जो फल प्राप्त होते हैं वह व्यावहारिक ज्ञान है। व्यावहारिक ज्ञान हेतु आगमन विधि (Inductive Method) का प्रयोग किया जाता है।
प्रश्न b (i) विद्यालयी ज्ञान व बाह्य विद्यालयी ज्ञान में अन्तर बताइए।
उत्तर-
छात्र द्वारा औपचारिक रूप से प्राप्त ज्ञान को विद्यालयी ज्ञान (School Knowledge) कहा जाता है जिसे छात्र एक निश्चित समय सीमा में निश्चित प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। परन्तु केवल विद्यालय की परिधि के अन्दर प्राप्त ज्ञान ही वास्तविक नहीं होता। विद्यालय की परिधि के बाहर भी ज्ञान प्राप्ति के अनेकों अवसर उपलब्ध हैं जैसे दूरस्थ शिक्षा व मुक्त विद्यालय या विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त ज्ञान, किसी ज्ञानी श्रेष्ठ पुरुष की संगति में प्राप्त ज्ञान, विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा प्राप्त ज्ञान आदि। इस सन्दर्भ में एकलव्य का उदाहरण द्रष्टव्य है जिसने औपचारिक रूप में गुरुकुल में ज्ञान प्राप्ति की अनुमति न मिलने पर गुरु की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उससे ही श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लिया था। मूसा को दस महत्त्वपूर्ण ईश्वरीय सूत्रों का ज्ञान एक पर्वत पर बैठकर मिला था। आज गुरु का स्थान दूरस्थ शिक्षा ने लेना शुरू कर दिया है।
इसी सन्दर्भ में ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान को भी अनौपचारिक विधि से प्राप्त ज्ञान या बहिर्विद्यालयी ज्ञान कहा जा सकता है। ऋषियों के मन में ज्ञान अपने आप उपजा उसे उन्होंने मन्त्र के रूप में बनाया। इसी प्रकार बहुत से महापुरुष सन्त व धर्म प्रवर्तक हुए जिन्होंने पहले शिक्षा नहीं प्राप्त की, परन्तु उनके मन में ज्ञान उत्पन्न हुआ और फिर उन्होंने दूसरों को शिक्षा दी। अतः इसी आधार पर प्राप्त ज्ञान का सन्दर्भ लेते हुए इवान इलिच द्वारा निर्विद्यालयीकरण (Deschooling) की संकल्पना को भी प्रस्तुत किया गया था।
प्रश्न b (ii) ज्ञान-प्राप्ति की विधियाँ बताइए।
उत्तर-
ज्ञान-प्राप्ति की विधियाँ-विश्लेषणात्मक दर्शन ज्ञान की वैयक्तिक विधि, ज्ञान की अधिकारिता विधि-ज्ञान की निगमन तर्कविधि एवं ज्ञान की आगमन तर्क विधि आदि ।
(i) ज्ञान की निगमन तर्क विधि-
इस विधि के विकास में प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक सुकरात व उसके सहयोगियों का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। यह विधि तर्क के रूप में ज्ञान से अज्ञान की ओर ले जाकर ज्ञान प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है। इस विधि को निरपेक्ष न्याय वाक्य नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें प्रतिज्ञप्तियों (Preserve) के आधार पर न्याय वाक्यों (Syllogism) को चार वर्गों अर्थात् निरपेक्ष न्याय वाक्य (Categorical Syllogism), वैकल्पिक न्याय वाक्य (Alternative Syllogism), परिकल्पित न्याय वाक्य (Hypothesis Syllogism) एवं नियोजक न्याय वाक्य (Disjunctives Syllogism) में विभक्त किया जा सकता है।
(ii) ज्ञान की आगमन तर्क विधि-
ज्ञानार्जन की इस विधि के प्रणेता फ्रांसिस बेकन (Francis Bacon ) थे। इसलिए इसे बेकोनियन विधि के नाम से भी जाना जाता है। निगमन तर्क के विपरीत आगमन तर्क विशिष्ट से सामान्य की ओर प्रवृत्त होता है। इस विधि के अन्तर्गत व्यक्ति एक विशिष्ट प्रकार के अनेक दृष्टान्तों का संकलन करके उनमें निहित समानता को पहचानने का प्रयास करता है और इस प्रक्रिया में वह नवीन ज्ञान के अर्जन की ओर अग्रसर होता है। जहाँ एक ओर इस विधि को निगमन विधि की विपरीत विधि कहा जाता है तो वहीं दूसरी ओर इसे निगमन विधि की पूरक विधि भी कहा जा सकता है। आगमन तर्क विधि के दो प्रकार पूर्ण आगमन (Perfect Induction) तथा अपूर्ण (Imperfect Induction) भी हो सकते हैं। पूर्ण आगमन विधि में जहाँ अध्ययन क्षेत्र के सभी दृष्टान्तों के अवलोकन के आधार पर सामान्यीकृत निष्कर्ष निकाले जाते हैं वहीं अपूर्ण आगमन में कुछ चुने दृष्टान्तों के आधार पर प्रायिकता निष्कर्ष निकाले जाते हैं। परन्तु दोनों ही प्रकार की विधियों में निःसन्देह विशिष्ट स्थितियों के सामान्यीकरण द्वारा ही निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है।
प्रश्न b (iii) ज्ञान ज्ञान के प्रमुख स्रोत बताइए।
उत्तर-
ज्ञान प्राप्ति के मूल रूप से निम्नलिखित स्रोत हैं-
(i) इन्द्रिय अनुभव –
ज्ञान का एक प्रमुख साधन इन्द्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव का प्रत्यक्षीकरण है। मनुष्य की पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा उसे क्रमशः देखकर, सुनकर, सूँघकर, स्वाद लेकर तथा स्पर्श करके सांसारिक वस्तुओं के बारे में तरह-तरह का ज्ञान प्रदान करती हैं। ऐसे ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार से मनुष्य ज्ञानेन्द्रियों द्वारा ही संसार की वस्तुओं के सम्पर्क में आता है तो एक प्रकार की संवेदना उत्पन्न होती है, यह सब देना ज्ञानेन्द्रियों को प्राप्त उत्तेजना में ही होती है तथा वस्तु का ज्ञान प्रदान करती है। इसे प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। यह प्रत्यक्षीकरण ही हमें उस वस्तु की जानकारी देता है।
प्रत्यक्षीकरण द्वारा चेतन मन में अवधारणायें उत्पन्न होती हैं जिन पर हमारा ज्ञान निर्भर होता है । इन्द्रिय अनुभव दक्ष ज्ञान प्राप्ति की इस क्रिया को सभी दार्शनिकों द्वारा ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत माना गया है। इन्द्रियों द्वारा प्राप्त इस ज्ञान की विश्वसनीयता का आंकलन तो किया जा सकता है परन्तु उस ज्ञान की वैधता ज्ञात करना कठिन होता है अर्थात् सत्यता की दृष्टि में कठिनाई आती है।
(ii) साक्ष्य –
जब हम दूसरों के अनुभव तथा निरीक्षण पर आधारित ज्ञान को मान्यता देते हैं तो इसे साक्ष्य कहा जाता है, साक्ष्य में व्यक्ति स्वयं निरीक्षण नहीं करता। वह दूसरों के निरीक्षण पर ही तथ्य का ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार साक्ष्य दूसरों के अनुभव पर आधारित ज्ञान है। हम प्रायः अपने जीवन में साक्ष्य का बहुत उपयोग करते हैं। हमने स्वयं बहुत से स्थानों को नहीं देखा है किन्तु जब दूसरे उनका वर्णन करते हैं तो हम उन स्थानों के अस्तित्व में विश्वास करने लगते हैं।
प्रश्न b (iv) सूचना तथा ज्ञान में अन्तर बताइए।
उत्तर-
प्रत्येक ज्ञान के सत्य एक ज्ञाता व एक ज्ञेय जुड़ा होता है और जब ज्ञाता का ज्ञेय के साथ इन्द्रियों के माध्यम से सम्पर्क होता है तो ज्ञेय को पदार्थ के सम्बन्ध में एक चेतना होती है जिसे ज्ञान की संज्ञा दी जा सकती है। इसी प्रकार ज्ञानेन्द्रियों से जो प्रत्यक्षीकरण तथा अनुभव होता है, उसे भी ज्ञान कहते हैं। ज्ञान इन्द्रियों तक ही सीमित नहीं होता अपितु इन्द्रियों से परे भी जो अनुभूतियाँ होती हैं उसे भी ज्ञान कहा जाता है।
ज्ञान को समझने हेतु ‘ज्ञान के स्वरूप’ (Nature of Knowledge) पर प्रकाश डालना आवश्यक है। ज्ञान का स्वरूप किसी वस्तु के सम्बन्ध में जानकारी है जिसे सूचना भी कहा जा सकता है। जब हम किसी वस्तु के सम्बन्ध में यह कहते हैं कि हमें उसकी जानकारी है तो हम यह मानकर चलते हैं कि यह जानकारी सत्य है। अतएव ज्ञान की धारणा में पहले तो यह बात निहित है कि ज्ञान को अवश्य सत्य होना चाहिये। इसी प्रकार ज्ञान के अर्थ में तीन बातें आती हैं-सत्यता, सत्यता में विश्वास तथा सत्यता के लिये पर्याप्त प्रमाण आदि । प्रायः ज्ञान के स्वरूप को मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक क्रिया, जैसे—जानना, करना और अनुभूति करना माना जाता है। यही तीन तत्त्व मनुष्य ● के व्यवहार में भी दृष्टिगत होते हैं तथा यह कहा जा सकता है कि अमुक व्यक्ति को इस कार्य का अच्छा ज्ञान है। इसी प्रकार ज्ञान का पक्ष वस्तु के गुणों में भी सम्बन्धित होता है जो इस बात का प्रतीक है कि जब व्यक्ति किसी वस्तु के गुणों को वास्तविक रूप से देख लें तभी उसे उस वस्तु का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है।
प्रायः ‘ज्ञान’ जिसका अंग्रेजी रूपान्तर नॉलेज है, को समानार्थी ही प्रयुक्त किया जाता है परन्तु पाश्चात्य मत में मिली ‘नॉलेज’ शब्द की विवेचना तथा ‘भारतीय मतानुसार’ ‘ज्ञान’ शब्द की दार्शनिक विवेचना में अन्तर है। ‘नॉलेज’ सिर्फ सत्य होता है जबकि ‘ज्ञान’ का सत्य व असत्य दोनों ही रूपों में पाया जाना नियत है। पाश्चात्य तर्कनिष्ठ अनुभववादी परम्परा में ‘असत्य ज्ञान’ (False Knowl- edge) एक स्वतोव्याघाती पद और ‘सत्य ज्ञान’ (True Knowledge) एक पुनरुक्ति है जबकि भारतीय परम्परा व पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा में आधारभूत भेद हैं। अतः दोनों शब्दों को एक-दूसरे की भाषा में अनूदित या रूपान्तरित नहीं किया जा सकता।
प्रश्न b (v) ‘ज्ञान’ और ‘नॉलेज’।
उत्तर-
‘ज्ञान’ और ‘नॉलेज’- प्रायः इन दोनों शब्दों को समानार्थी, ही प्रयुक्त किया जाता है परन्तु ‘पाश्चात्य मत’ में मिली ‘नॉलेज’ शब्द की विवेचना तथा ‘भारतीय मतानुसार’ ‘ज्ञान’ शब्द की दार्शनिक विवेचना में अन्तर है। ‘नॉलेज’ सिर्फ सत्य होता है जबकि ‘ज्ञान’ का सत्य व असत्य दोनों ही रूपों में पाया जाना नियत है। पाश्चात्य तर्कनिष्ठ अनुभववादी परम्परा में ‘असत्य ज्ञान’ एक स्वतोव्याघाती पद और ‘सत्य ज्ञान’ एक पुनरुक्ति है जबकि भारतीय परम्परा में न तो ‘असत्य ज्ञान’ स्वतोव्याघातक है व ‘सत्य ज्ञान’ ‘पुनरुक्ति’ है।
साधारण शब्दकोष में ‘ज्ञान’ पद का अनुवाद ‘नॉलेज’ पद से किया जाता है किन्तु दार्शनिक दृष्टि में यह उचित नहीं है। भारतीय और पाश्चात्य ज्ञानमीमांसा में आधारभूत भेद है। अतः दोनों शब्दों को एक-दूसरे की भाषा में अनूदित या रूपान्तरित नहीं किया जा सकता।
भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ-भारतीय दर्शन के अनुसार ‘ज्ञान का अर्थ ‘ समझने से पूर्व सत्य की वस्तुनिष्ठता, ज्ञान की सार्थकता, ज्ञान की सत्यता तथा तार्किक प्रतिज्ञप्ति सत्यता पर विचार करना आवश्यक है। अर्थात्-
(i) ज्ञान की सत्यता हेतु उसकी वस्तुनिष्ठता का आंकलन किया जाना आवश्यक है।
(ii) ज्ञान के अस्तित्व में कोई संशय नहीं होना चाहिए।
(iii) ज्ञान की सत्यता की पुष्टि भी सन्देहरहित होनी चाहिए।
(iv) तार्किक प्रतिज्ञप्ति भी सत्य होनी चाहिए।
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि शिक्षा केवल एक साधन है, लक्ष्य नहीं, ज्ञान शिक्षा से हमें सूचना मिलती है और उस सूचना में व्यावहारिकता अनुभव परिमार्जित आदि का समावेश करने के पश्चात् सूचना का अन्तर ज्ञान से होता है।
प्रश्न b (vi) ज्ञान के प्रकार बताइए।
उत्तर- ज्ञान के निम्नलिखित प्रकार हैं-
(i) आगमनात्मक ज्ञान-
इस प्रकार का ज्ञान हमारे अनुभव तथा निरीक्षण पर आधारित है। जॉन लॉक (John Locke) इस प्रकार के ज्ञान के प्रवर्तक हैं। उनके अनुसार बालक का मन जन्म के समय कोरी पटिया के समान (Tabular rasa) होता है। जैसे-जैसे अनुभव मिलते जाते हैं, इस पटिया पर लेखन होने लगता है। इससे तात्पर्य है कि ज्ञान अनुभवों द्वारा वृद्धि करता रहता है। शिक्षा में इस प्रकार के ज्ञान को प्रवर्तक कहते हैं कि सीखने के लिए समग्र अनुभव प्रदान करने चाहिए। इस प्रकार के ज्ञान में अलौकिक का कोई स्थान नहीं है।
(ii) प्रयोगमूलक ज्ञान-
ज्ञान प्रयोग द्वारा प्राप्त होता है, ऐसा प्रयोजनवादियों की धारणा है। ड्यूवी (Dewey) का कहना है कि ज्ञान की प्रक्रिया ‘एक प्रयास एवं सहन’ (Trying and undergoing) की प्रक्रिया है-एक विचार का अभ्यास में प्रयास करना एवं ऐसे प्रयास के परिणाम से जो फल प्राप्त होते हैं उनसे सीखना। इस धारणा के अनुसार ज्ञान कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे हम समझें कि वह अनुभव या निरीक्षण से अन्तिम रूप से समझी जा सकती है जबकि हम ऐसी विधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे आगमन। यह तो कुछ ऐसी वस्तु है जो अनुभव में सक्रिय होती है। एक कृत्य की भाँति जो अनुभव को सन्तोषपूर्ण ढंग से आगे की ओर ले जाती है
(iii) प्रागनुभव ज्ञान-ज्ञान स्वयं-
प्रत्यक्ष की भाँति समझा जाता है (Knowledge is self- evident)। सिद्धान्त जब समझ लिए जाते हैं, सत्य पहचान लिए जाते हैं फिर उन्हें निरीक्षण, या प्रयोग द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती।
प्रश्न b (vii) वर्गीकरण (टैक्सोनॉमी) किसे कहते हैं?
उत्तर-
अंग्रेजी में Taxonomy शब्द का अर्थ होता है-वर्गीकरण अर्थात् स्तरीकरण। जब इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है तो इसका तात्पर्य ‘शैक्षिक उद्देश्यों के एक व्यवस्थित क्रम (Systematic Classification of Educational Objectives) से होता है। इस प्रकार का वर्गीकरण सर्वप्रथम बेंजामिन बी. ब्लूम ने किया था। बाद में, आर.एफ. मेगर (Meger), डी.आर. कैथवाल (Krathwohl ), एन. ई. ग्रीनलैण्ड (N.E. Gronland) तथा मैसिया (B.B. Massia) आदि ने भी इस क्षेत्र में कार्य किया।
इस वर्गीकरण को मानसिक जीवन के तीन पक्षों-ज्ञान, भावना और कर्म के आधार पर विकसित किया गया है जिन्हें क्रमशः ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक क्षेत्रों की संज्ञा प्रदान की गई है। टैक्सोनॉमी शब्द जीवविज्ञान से सम्बन्धित है जिसके अन्तर्गत प्राणियों एवं पौधों को क्रमिक रूप में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि वे सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हुए अधिक-से-अधिक स्पष्ट होते जायें।
ब्लूम तथा उसके सहयोगियों ने शिकागो विश्वविद्यालय में ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक तीनों पक्षों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। 1956 ई. में ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का, 1964 में ब्लूम, कैथवाल तथा मैसिया ने भावात्मक पक्ष का तथा 1969 में सिम्पसन ने क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। यह टैक्सोनॉमी शैक्षिक, तार्किक तथा मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण का एक न्यायोचित एवं सन्तुलित एकीकरण है। इसमें विभिन्न वर्गों का भेद शैक्षिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इसमें शब्दावली को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि उनके अर्थ तार्किक दृष्टि से सही मालूम पड़ते हैं। यह वर्गीकरण आधुनिकतम मनोवैज्ञानिक खोजों पर आधारित है।
प्रश्न b (viii) ज्ञानात्मक क्षेत्र को बताइए।
उत्तर-
ज्ञानात्मक क्षेत्र के अन्तर्गत बौद्धिक पक्ष आता है जिसका शैक्षिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्व है। पूर्वकाल में तो औपचारिक शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य मस्तिष्क का प्रशिक्षण ही माना जाता रहा है। इस बात से सभी सहमत होंगे कि विद्यालयों में इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि विद्यार्थी अपने वातावरण से कैसे सीखते हैं, अवधारणाएँ कैसे बनती और विकसित होती हैं। इसके साथ ही इस पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है कि बालक की अभिरुचि क्या है, वह दूसरे व्यक्तियों से तथा दूसरे व्यक्ति उससे कैसे व्यवहार करते हैं, वह तर्क को क्या महत्त्व देता है तथा कारण एवं परिणाम में कैसे सम्बन्ध स्थापित करता है, निर्णय किस प्रकार लेता है तथा समस्याओं का समाधान कैसे करता है, तार्किक चिन्तन की योग्यता एवं आदत का विकास कैसे करता है? विद्यालयों में बालकों की भाषा सम्बन्धी, वैज्ञानिक, सौन्दर्यबोधात्मक, ऐतिहासिक, तकनीकी, चिन्तन की मानसिक प्रक्रियाओं, विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं, अभिमुखी (Convergent) एवं अपसारी (Divergent) बौद्धिक प्रक्रियाओं के अन्तर को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है।
ज्ञानात्मक क्षेत्र को छः वर्गों में विभाजित किया गया है-ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन ।
प्रश्न c (i) ज्ञान का संवाद सिद्धान्त क्या है?
उत्तर-
संवाद सिद्धान्त-इस सिद्धान्त के अनुसार सत्य विचार तथा उस वस्तु में जिसका वह विचार है उनके आपसी संवाद पर निर्भर है तथ्यों को हम सत्य या असत्य नहीं कहते क्योंकि तथ्य तो जैसे हैं वैसे हैं ही। सत्य या असत्य तो उन तथ्यों के सम्बन्ध में कथन हैं। यदि तथ्य और कथन में भेद नहीं है तो वह सत्य है। यदि कथन तथा तथ्य एक-दूसरे के प्रतिकूल हैं तो वह असत्य है। इस प्रकार तथ्य की अनुकूलता ही उसकी सत्यता का प्रमाण है। जैसे, जब हम कहते हैं कि स्टेशन से कॉलेज चार किलोमीटर है तो इसकी परीक्षा हम स्टेशन से कॉलेज की दूरी माप कर, कर सकते हैं। यदि यह तथ्य ठीक हुआ, दूरी चार किलोमीटर ही हुई तो तथ्य का प्रमाण मिल गया और इसकी सत्यता स्थापित हो गई, किन्तु इस प्रकार के परीक्षण में दो बातें आवश्यक हैं। एक तो यह कि तथ्य वास्तविक हैं तथा स्वतन्त्र रूप से स्थित है और दूसरे यह कि अनुभव द्वारा उसका सत्यापन किया जा सकता है। यह सिद्धान्त यथार्थवादियों द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। यथार्थवाद यह मानता है कि ज्ञान तथा ज्ञान की वस्तु का सम्बन्ध बाहरी होता है, तथ्य प्रस्तुत होते हैं। आदर्शवाद इस सम्बन्ध को आन्तरिक मानता है और इस कारण दोनों में एकत्व समझता है। इस सिद्धान्त में तथ्य ही मुख्य आधार है और कथन को सत्य होने के वास्ते तथ्य के साथ संवाद आवश्यक है। इस सिद्धान्त की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि हम कैसे जान सकते हैं कि तथ्य क्या हैं और किस प्रकार तथ्य के ज्ञान की कथन से अनुकूलता परखी जा सकती है।
प्रश्न c (ii) ज्ञान के संसक्तता सिद्धान्त से आप क्या समझते हैं?
उत्तर-
संसक्तता सिद्धान्त-इस सिद्धान्त का आधार यह है कि यदि मनुष्य का ज्ञान उसके प्रत्ययों तक ही सीमित है और हम उनकी तथ्यों के साथ अनुरूपता की परीक्षा नहीं कर सकते तो सत्यता को परखने के लिए हमें यह देखना होगा कि तथ्यों के सम्बन्ध में जो एक कथन है वह दूसरे कथन जिसकों हम सत्य मानते हैं उससे संगति रखता है। जैसे जब हम दो स्थानों के बीच की दूरी 4 किलोमीटर कहते है तो यदि इस कथन में निहित है कि चार किलोमीटर में कितनी दूरी आती है तो चार किलोमीटर उतनी ही दूरी कहने में सत्यता होगी। इस प्रकार हम सत्य उस कथन को कहेंगे जिसमें दूसरे कथनों के साथ परस्पर संगति है और यदि ऐसा नहीं है जैसे कि एक किलोमीटर में जितनी दूरी आती है वह विभिन्न कथनों में विभिन्न है तो हमारा चार किलोमीटर दूरी का कथन भी असत्य होगा।
इस सिद्धान्त में हम यह मानकर चलते हैं कि मानव के समक्ष सत्यता की प्रणाली है जिसमें वह सब विचार विद्यमान हैं जिन्हें हम पहले मान चके हैं और जिनकी सत्यता पहले सिद्ध हो चुकी है। अब जब कोई एक नया निर्णय या कथन प्रस्तुत होता है तो हम उसका परीक्षण इस सत्य की प्रणाली के अनुसार करते हैं। जैसे जब यह कथन सत्यता की प्रणाली में आ चुका है कि एक किलोमीटर में कितनी दूरी आयेगी तो चार किलोमीटर में आने वाली दूरी में उस सत्यता से संगति होगी, किन्तु ऐसा नहीं है कि यदि कोई बात जो नयी हो और पुरानी ज्ञान प्रणाली से विभिन्न हो तो वह सत्य नहीं हो सकती। विज्ञान में पहले अणु को पदार्थ का सबसे छोटा भाग माना जाता था, किन्तु अब ऐसा नहीं है तो क्या यह नवीन मान्यता असत्य है। यदि हम ऐसा कहते हैं तो हम किसी भी नई धारणा को मानने से इन्कार करते हैं। वास्तव में यह गलत बात होगी। हमें नयी बात को सत्य मानना होगा। इसकी व्याख्या इस सिद्धान्त में यह है कि यदि नया सत्य पुरानी प्रणाली में एक नये ढंग के संगठन को बना सकता है और पिछली व्यवस्था से भी बड़ी ज्ञान-व्यवस्था कायम कर सकता है तो इसे सत्य मानना चाहिए। यह सिद्धान्त इस बात पर बल देता है कि ज्ञान की सत्यता उसकी आत्म संगति, संगठन तथा एकरूपता में होती है।
प्रश्न c (iii) ज्ञान का व्यवहारवादी सिद्धान्त।
उत्तर-
व्यवहारवादी सिद्धान्त-व्यवहारवादी तो सत्यता को परिवर्तनशील मानते हैं। सत्य समय तथा स्थान के साथ बदलता रहता है। वह कहते हैं कि सत्य हमारे व्यावहारिक जीवन से सम्बन्धित है और इसके लिए ही उपयोगी है। विलियम जेम्स के अनुसार कथन दो प्रकार के हो सकते हैं-सार्थक कथन तथा निरर्थक कथन । सार्थक कथन का गुण सत्यता होती है। जेम्स के अनुसार एक कथन जिसका परिणाम जीवन में उपयोगी, लाभकारी तथा सुखद आदि है वह कथन सत्य है। जो कथन के परिणाम जीवन को दुःखद बना देते हैं, उसके लिए हानिकारक हैं वह असत्य है। इस प्रकार सत्यता का परीक्षण हम उपयोगिता, कार्यक्षमता, सन्तोष, सुख इत्यादि के आधार पर करते हैं। जेम्स कहता है कि सत्य वह है जो सफल है।
इस सिद्धान्त में यह दोष है कि कथन की सत्यता देखने के लिए परिणाम देखने होते हैं, किन्तु परिणाम मिलने में बहुत समय लग सकता है और जब तक सब परिणाम नहीं मिल जाते हम सत्यता स्थापित नहीं कर सकते। परिणामों की प्रतीक्षा में बहुत देर हो सकती है और प्रतीक्षा करना स्वयं में एक निर्णय है जिसके बुरे परिणाम निकल सकते हैं। फिर यदि हम प्रतीक्षा करने का निर्णय ले भी लें तो पूर्ण परिणाम कभी-कभी प्राप्त नहीं हो सकते। इसका कारण यह है कि परिणामों के भी परिणाम निकलते हैं और इस प्रकार इस क्रिया का कोई अन्त नहीं है। हम सब कोई निर्णय सत्यता का नहीं ले पायेंगे तो अनावस्था के दोष से घिर जायेंगे। हमारे जीवन में कुछ बातों के सम्बन्ध में एक तथ्य अनुकूल हो सकता तो दूसरा प्रतिकूल तो व्यावहारिकतावादी उनमें से किसको सत्य कहेंगे, यदि उपयोगिता और सत्यता में अन्तर हो तो व्यवहारवादी उपयोगिता को ही देखेगा और इस प्रकार वह असत्य को सत्य भी मान सकता है|
प्रश्न c (iv) सूचना प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत बताइए ।
उत्तर-
सूचना प्राप्त करने के निम्नलिखित प्रमुख स्रोत व साधन हैं-
1. मुद्रित संचार साधन – पाठ्य-पुस्तकें, सन्दर्भ ग्रन्थों, पाठ्यक्रम से सम्बन्धित पुस्तकें पत्र- पत्रिकाएँ, वाचनालय तथा अन्य सार्वजनिक वाचनालय ।
2. प्रत्यक्ष जानकारी देने वाले साधन-बाग-बगीचे, नदी, पर्वत, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थान, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक अनुभव इत्यादि ।
3. दृश्य-श्रव्य साधन-चित्र, चार्ट, रेडियो, टेलीविजन आदि।
उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षकों, सहपाठियों, सहकर्मियों, अभिभावकों, परिजनों तथा समाज के सदस्यों द्वारा भी औपचारिक व अनौपचारिक रूप से सूचनाएँ प्राप्त होती हैं।
वर्तमान युग विज्ञान एवं तकनीकी का युग है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष एवं क्रिया को प्रभावित किया है। इसके प्रभाव से शिक्षा भी अछूती नहीं रही है। आज शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान की नित नवीन शाखाओं का विकास हो रहा है। इस ज्ञान को आत्मसात् करने, ज्ञान का संचय, प्रसार एवं वृद्धि एवं सम्प्रेषण के लिए विकसित तकनीकी के ज्ञान एवं उपयोग की आवश्यकता है, और इस आवश्यकता की पूर्ति केवल सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी द्वारा ही सम्भव है। सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी से अभिप्राय “यन्त्रों, उपकरणों एवं अनुप्रयोग आधार से युक्त एक ऐसी तकनीकी से है जो सूचना के एकत्रीकरण, भंडारण या संचयीकरण, पुनः प्रस्तुतीकरण, उपयोग, स्थानांतरण, संश्लेषण, विश्लेषण एवं आत्मसातीकरण के विश्वसनीय एवं यथार्थ संपादन में सहायक सिद्ध होते हुए उपयोगकर्ता को अपना ज्ञानवर्द्धन करने तथा उसके सम्प्रेषण को प्रभावी बनाने तथा निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान योग्यता में वृद्धि करने में यथासम्भव सहायक सिद्ध होती है।”
प्रश्न C (v) पाठ्यचर्या की अवधारणा बताइए ।
उत्तर-
पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में ‘Curriculum’ कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के ‘Curricere/Currere’ से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ है ‘दौड़ का मैदान’ (A Race Cource)। सीधे शब्दों में कहा जाये तो पाठ्यक्रम वह क्रम है जिसे व्यक्ति को अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचने के लिए पार करना होता है अर्थात् पाठ्यक्रम दौड़ के मैदान की तरह ही होता है जिसमें बालक को तब तक दौड़ना पड़ता है जब तक कि वह अपने लक्ष्य को न प्राप्त कर ले। विद्यालयों में शिक्षक और शिथार्थी द्वारा किए गए प्रयासों से किसी उद्देश्य की प्राप्ति होना है, पाठ्यक्रम कहलाता है। अतः पाठ्यचर्या वह. साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। यह अध्ययन का निश्चित व तर्कपूर्ण क्रम है जिसके माध्यम से शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का विकास होता है तथा वह नवीन ज्ञान तथा अनुभव ग्रहण करता है।
शिक्षा के अर्थ के बारे में दो धारणाएँ हैं – पहला प्रचलित अर्थ या संकुचित अर्थ व दूसरा वास्तविक या व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ में शिक्षा केवल स्कूली शिक्षा या पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित माना जाता है परन्तु विस्तृत अर्थ में पाठ्यक्रम के अन्तर्गत वे सभी अनुभव आ जाते हैं जिसे एक नई पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ियों से प्राप्त करती है। साथ ही विद्यालय में रहते हुए शिक्षक के संरक्षण में विद्यार्थी जो भी संक्रियाएँ करता है वह सभी पाठ्यक्रम के अन्तर्गत आती हैं तथा इसके अतिरिक्त विभिन्न पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाएँ भी पाठ्यक्रम के अन्तर्गत आती हैं तथा इसके अतिरिक्त विभिन्न पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाएँ भी पाठ्यक्रम का अंग होती हैं। अतः वर्तमान समय में ‘पाठ्यक्रम’ से तात्पर्य उसके विस्तृत रूप से है।
प्रश्न c (vi) पाठ्यचर्या की प्रकृति बताइए।
उत्तर-
शिक्षा जीवन-पर्यन्तं चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में निरन्तर परिवर्तन एवं परिमार्जन होता है। व्यक्ति के व्यवहार में यह परिवर्तन अनेक माध्यमों से होता है, किन्तु मुख्य रूप से इन माध्यमों को दो रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है- औपचारिक एवं अनौपचारिक । औपचारिक रूप के अन्तर्गत वे माध्यम आते हैं जिनका नियोजन कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यवस्थित ढंग से संस्थापित संस्थाओं में किया जाता है। इस प्रकार की संस्थाओं को विद्यालय कहा जाता है, किन्तु व्यक्ति के परिवर्तन की प्रक्रिया विद्यालय एवं विद्यालयी जीवन में ही पूर्ण नहीं हो पाती है, बल्कि वह विद्यालय से बाहर तथा जीवन भर चलती रहती है। अतः व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले अनेक परिवर्तन विद्यालय की सीमा से बाहर की परिस्थितियों के परिणामस्वरूप होते हैं। चूँकि ऐसी परिस्थितियाँ सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत नहीं की जाती हैं, अतः वे अनौपचारिक माध्यम के अन्तर्गत आती हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों को जो कुछ भी कक्षा एवं कक्षा के बाहर प्रदान किया जाता है, उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है एवं उसे किसी विशेष माध्यम से ही पूरा किया जाता है। हमारी कुछ संकल्पनायें होती हैं कि एक विशेष कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विद्यार्थी के व्यवहार में अमुक परिवर्तन आ जायेगा, परन्तु यह परिवर्तन किस प्रकार लाया जायेगा? किसके द्वारा लाया जायेगा? और कितना लाया जायेगा? आदि ऐसे अनेक प्रश्न हैं, जिनका समाधान पाठ्यक्रम जैसे साधन से प्राप्त होता है। अतः पाठ्यक्रम का सम्बन्ध शिक्षा के औपचारिक माध्यम से है।
प्रश्न c (vii) पाठ्यचर्या के क्षेत्र बताइए ।
उत्तर-
यदि हम पाठ्यक्रम के इतिहास पर एक दृष्टि डालें तो स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पाठ्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने वाले ज्ञान का स्वरूप एवं विस्तार अनिवार्य रूप से सम्बन्धित समाज द्वारा मान्य शैक्षिक उद्देश्यों पर निर्भर करता है। इसीलिए देश और काल की भिन्नता के अनुसार वहाँ के पाठ्यक्रमों में भिन्नता भी पायी जाती है। भारतीय सन्दर्भ में यदि हम वैदिक काल की शिक्षा पर दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि वैदिक काल में भारतीय शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य ईश्वर भक्ति एवं धार्मिक भावना को दृढ़ करना, बालकों का चरित्र निर्माण एवं उनके व्यक्तित्व का विकास करना तथा सामाजिक कुशलता में वृद्धि करना था। इस दृष्टि से उस समय का पाठ्यक्रम भी अत्यन्त विस्तृत था। उसमें परा विद्या अर्थात् धार्मिक साहित्य का अध्ययन तथा अपरा विद्या अर्थात् लौकिक एवं सांसारिक ज्ञान दोनों का ही समावेश था। उस समय शिक्षा कार्य गुरुकुलों में होता था तथा शिक्षार्थी पूरे शिक्षाकाल में गुरुकुल या गुरु-परिवार के सदस्य के रूप में रहता था। वह गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के साथ-साथ गुरु एवं गुरु-पत्नी की सेवा, आश्रम की सफाई, पशुओं की देखभाल तथा भिक्षाटन के माध्यम से कर्त्तव्यपालन, सेवाभाव, विनयशीलता तथा अन्य चारित्रिक गुणों की शिक्षा भी प्राप्त करता था। कभी-कभी शिक्षा प्राप्त करने हेतु शिष्यों को देशाटन पर भी जाना पड़ता था। इस प्रकार वैदिककालीन पाठ्यक्रम में पठन-पाठन के साथ-साथ विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के समुचित अवसर भी प्राप्त होते थे तथा उसका सम्पादन भी अध्ययन कक्षों और समय के घण्टों में सीमित नहीं था।
इसी प्रकार यदि हम यूरोप के इतिहास का अध्ययन करें तो वहाँ के पाठ्यक्रम के सीमा क्षेत्र का आभास मिलता है। प्राचीन यूनान के नगर राज्य स्पार्टा को प्रायः युद्धरत रहना पड़ता था, अतः वहाँ पर बालकों के शारीरिक विकास एवं शस्त्र विद्या पर अधिक ध्यान दिया जाता रहा, जबकि एथेन्स नगर राज्य में शान्ति एवं स्थायित्व होने से वहाँ पर साहित्य, दर्शन एवं ललित कलाओं को अधिक महत्त्व दिया जाता था। प्रारम्भ में यूरोप और अमेरिका में भी शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को पढ़ने, लिखने एवं सामान्य गणना कर सकने के योग्य बना देना मात्र था। अतः उस समय पाठ्यक्रम भी 3R’s तक सीमित था। यह स्थिति एक लम्बी अवधि तक बनी भी रही, क्योंकि पाश्चात्य देशों में भी पाठ्यक्रम के अन्तर्गत उन्हीं प्रवृत्तियों का समावेश किया जाता रहा जो कक्षा के अन्दर पाठ पढ़ाते समय आयोजित की जाती थीं। कालान्तर में भारत में भी अनेक राजनीतिक कारणों से पाठ्यक्रम का रूप, पश्चिमी देशों जैसा ही हो गया तथा गुरुकुलों एवं आश्रमों के स्थान पर पाठशालाओं का उदय हुआ, जिनका कार्य केवल पाठ पढ़ने-पढ़ाने तक ही सीमित रह गया। इस प्रकार पठन-पाठन से इतर प्रवृत्तियों को पाठशाला के क्षेत्र से बाहर की चीज माना जाने लगा।
प्रश्न d (i) पाठ्यचर्या की परिभाषा बताइए ।
उत्तर-
पाठ्यक्रम को विभिन्न विद्वानों द्वारा निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है-
पॉल हिरस्ट के अनुसार, “पाठ्यक्रम ऐसी गतिविधियों का समायोजन है जिनके द्वारा छात्र जहाँ तक सम्भव हो, निश्चित परिणामों व उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं।”
कनिंघम के अनुसार, “पाठ्यक्रम कलाकार (शिक्षक) के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपनी सामग्री (शिक्षार्थी) को अपने आदर्श, उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला (विद्यालय) में ढाल सकता है।”
मुनरो के अनुसार, “पाठ्यक्रम सारे अनुभवों को अपने में सम्मिलित करता है जिसका प्रयोग विद्यालय द्वारा बालक को शिक्षित करने के उद्देश्य से होता है।”
माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) “पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धान्तिक विषयों से नहीं है जो विद्यालयों में परम्परागत रूप से पढ़ाए जाते हैं बल्कि इसमें अनुभवों की वह सम्पूर्णता भी सम्मिलित होती है, जिनको विद्यार्थी विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, खेल के मैदान तथा शिक्षक एवं छात्रों के अनेक अनौपचारिक सम्पर्कों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का सम्पूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है और उनके सन्तुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है।”
होर्नी के शब्दों में, “पाठ्यक्रम वह है जो शिक्षार्थी को पढ़ाया जाता है। वह शक्तिपूर्ण पढ़ने या सीखने से अधिक है। इसमें उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास और क्रियाएँ शामिल हैं। ”
प्रश्न d (ii) शिक्षकों के अनुभव व चिन्त्य विषय के बारे में बताइए ।
उत्तर-
शिक्षकों के अनुभव एवं पाठ्यचर्या बालकों के लिए आवश्यक होते हैं। पाठ्यचर्या के विकास हेतु शिक्षकों के अनुभव व चिन्त्य विषय भी सकारात्मक योगदान देते हैं। यद्यपि पाठ्यचर्यां रचना में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले शिक्षकों की संख्या बहुत थोड़ी है जबकि पाठ्यचर्या को लागू करने वालों में शिक्षकों का योगदान शिक्षा प्रक्रिया में बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। शायद यही वजह है कि शिक्षकों को ‘पाठ्यचर्या रचनाकार’ की बजाए ‘पाठ्यचर्या का वाहक’ माना जाता है। विद्यालय आधारित पाठ्यचर्या विकास का विचार लोकप्रिय हो रहा है और जैसे-जैसे विकेन्द्रीकरण का विचार विद्यालयों में व्याप्त होगा वैसे-वैसे भविष्य में इस प्रक्रिया में शिक्षकों की भागीदारी बड़े पैमाने पर अपेक्षित होगी। यह तब तक सम्भव नहीं होगा जब तक शिक्षक इस परिवर्तित भूमिका के लिए वास्तव में सक्षम नहीं बनाए जाते। राष्ट्र को शिक्षकों के अनुभवों पर पाठ्यचर्या निर्माण के समय पूर्ण विश्वास करना चाहिए। सक्षम शिक्षक समुदाय की परिकल्पना ने शिक्षण को पुनर्व्याख्या की और प्रवृत्त किया है। इसके अनुसार शिक्षण कार्य अधिक चिन्तनशील और विचारशील व्यवसाय के रूप में उभरेगा।
पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया में चूँकि शिक्षक प्रभावशाली कार्यकर्त्ता है इसलिए उपयुक्त और पर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण जरूरी है, जो पूर्व-सेवाकालीन और सेवाकालीन दोनों ही कार्यक्रमों पर लागू होगा। सेवाकालीन प्रशिक्षण को तो पाठ्यचर्या विकास प्रक्रिया का आन्तरिक अंग बनना होगा और प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से दोनों तत्त्वों, शिक्षण प्रविधि और मूल्यांकन प्रक्रिया को शामिल करना होगा।
प्रश्न d (iii) आधुनिक समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं पाठ्यक्रम बताइए।
उत्तर-
आधुनिक समाज की बदलती हुई आवश्यकतायें, उसमें तीव्र गति से होने वाले परिवर्तनों की ही देन होती है। कोई भी समाज इन तीव्रगामी परिवर्तनों से तभी सही ढंग से अनुकूलन कर सकता है जब वह उन परिवर्तनों से उपजी वैयक्तिक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, तकनीकी एवं पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करे। इसके लिए शिक्षा के उद्देश्य निम्न प्रकार के होने चाहिए-
(i) व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक एवं सांस्कृतिक विकास करना ।
(ii) व्यक्ति में समुचित अभिरुचियों एवं आदतों का निर्माण करना।
(iii) समुचित अभिवृत्तियों एवं मूल्यों का प्रतिपादन करना तथा परम्परागत एवं नवीन मूल्यों में सामंजस्य स्थापित करना।
(iv) व्यक्ति तथा समाज के प्रति व्यक्तियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना।
(v) नागरिक कर्त्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित करना ।
(vi) विज्ञान एवं तकनीकी का विकास करना तथा व्यक्तियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना।
प्रश्न d (iv) पाठ्यक्रम में लैंगिक भेदभाव को बताइए।
अथवा
पाठ्यक्रम निर्धारण के रूप में वातावरण एवं लिंग कैसे प्रभाव डालता है?
उत्तर-
शैक्षिक क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव देखने को मिलता है। विद्यालय, जिसमें कई संस्कृति के विद्यार्थी होते हैं, ये भी लिंग आधारित भेद-भाव संस्थान की पाठ्य-पुस्तकों द्वारा, निष्पत्ति परीक्षणों द्वारा, खेलकूद के कार्यक्रमों द्वारा, व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा व लैंगिक विभेदीकृत पाठ्यक्रम द्वारा स्पष्ट दिखाई देता है। शिक्षक व्यक्तिगत तौर पर तो समाज में व्यक्ति लैंगिक भूमिकाओं के सापेक्ष सांस्कृतिक आकांक्षाओं के बोझ तले शिक्षित होते ही हैं, साथ ही जिन शैक्षिक संस्थाओं में उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया होता है, वहाँ भी लैंगिक पक्षपात का सामना करके आते हैं। ये दोनों ही स्थितियाँ उनकी सांस्कृतिक अपेक्षाओं को अनजाने ही लैंगिक भेद-भाव की ओर मोड़ देती हैं। और वे भी व्यक्तिगत तौर पर शैक्षिक प्रक्रियाओं में लिंग भूमिकाओं की तरफ पक्षपात का दृष्टिकोण अपना लेते हैं तथा छात्र व छात्राओं से विभिन्न शैक्षिक निष्पत्ति के स्तरों व क्षमताओं की उम्मीद करते हैं और पाठ्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों के सन्दर्भ में भी लिंग आधारित विचारों के सापेक्ष ही इसे तैयार करते हैं।
–
यही कारण है कि एक समान कक्षा में बैठकर एक समान पाठ्य पुस्तक को पढ़ते हुए, एक ही अध्यापक के व्याख्यान को सुनते हुए भी लड़के व लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। जहाँ तक हमारे विद्यालयों में छात्रों की संख्या का प्रश्न है, लड़के व लड़कियों की समान भागीदारी है। यहाँ तक कि कुछ विद्यालयों में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है फिर भी इन विद्यालयों में हमें पुरुष सापेक्ष वातावरण दिखाई देता है जहाँ बालिकाओं को बालकों की तरह स्वतन्त्र अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं मिलता है, न ही उनके बराबर शैक्षिक अवसर प्राप्त हो पाते हैं। सम्भवतः यह पुराने चले आ रहे रूढ़िवादी विश्वास का ही परिणाम है।
लिंग आधारित भेद-भाव युक्त विचार इन विद्यार्थियों का बहुत अहित करते हैं उदाहरणार्थ- कक्षा 9 के विद्यार्थी चूँकि इस समय किशोरावस्था की जटिल परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं। इस समय यदि वे भेद-भावपूर्ण व पक्षपातपूर्ण रवैये का सामना करते हैं तो उनके जीवन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। पाठ्य-पुस्तकों में दी गई लिंग आधारित पक्षपातपूर्ण अभिवृत्तियाँ भी बालक व बालिकाओं की अभिवृत्ति पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं तथा वे उसी के आधार पर अपने भविष्य की योजना बनाने लगते हैं तथा अपने प्रत्ययों को भी उसी तरफ मोड़ लेते हैं। जैसा दृष्टिकोण वे इन लिंग आधारित पाठ्य-पुस्तकों के आधार पर बना लेते हैं इसलिए वर्तमान पीढ़ी आज भी सदियों पुरानी इन परम्पराओं व लिंग आधारित धारणाओं से बाहर नहीं निकल पाई है। यह भेद-भाव विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि के साथ-साथ समाज में भी दिखाई देता है।
प्रश्न d (v) अनुभव केन्द्रित पाठ्यक्रम।
उत्तर-अनुभव केन्द्रित पाठ्यक्रम-अनुभव केन्द्रित पाठ्यक्रम का अभिप्रायः उस पाठ्यक्रम से है जिसमें मानव जाति के अनुभव सम्मिलित किये जाते हैं। दूसरे शब्दों में अनुभव केन्द्रित पाठ्यक्रम विषयों की अपेक्षा अनुभवों पर आधारित होता है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य बालकों को प्रेरणा प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवन को उपयोगी बना सकें। यह भौतिक तथा सामाजिक वातावरण का अधिक-से-अधिक प्रयोग करता है क्योंकि इसमें बालक को स्वाभाविक ढंग से ‘अनुभव’ प्राप्त करने को मिलते हैं। यही कारण है कि यह पूर्णतया मनोविज्ञान पर आधारित होता है अर्थात् इसका सम्बन्ध छात्रों की रुचियों, आवश्यकताओं तथा योग्यताओं से होता है।
प्रश्न d (vi) पाठ्यक्रम में लैंगिक भेदभाव मिटाने के उपाय बताइए।
उत्तर – पाठ्यक्रम में लैंगिक भेदभाव को मिटाने में शिक्षकों की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो सकती है। अक्सर यह सुना जाता है कि लड़कियाँ, विज्ञान, गणित, व्यावसायिक व गैर-पारम्परिक विषय चयनित नहीं करना चाहतीं, परन्तु इसके लिए भी विद्यालय स्तर पर Intervention Programmes किए जा सकते हैं जिससे संग्रहालय के पैर, विज्ञान मेले व विज्ञान केन्द्रों तक बालिकाओं को ले जाना व भौतिकी में पानी, हवा व ऊर्जा के प्रयोग कराना, इन बालिकाओं में भी आत्मविश्वास पैदा कर देते हैं। इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य बालिकाओं के विज्ञान, इंजीनियरिंग व तकनीकी सहभागिता में संकोच को दूर करना है जिससे एक सशक्त समाज का निर्माण हो सके व बालिकाओं को हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले। उनके लिए शिक्षण व्यवसाय जैसे पारम्परिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त भी रोजगार की नवीन सृजनाएँ सम्भव हैं।
प्रश्न d (vii) पाठ्यक्रम आधारित लिंग असमानता को दूर करने के उपाय बताइए।
उत्तर-
पाठ्यक्रमों के माध्यमों से छात्रों में लिंग समानता लाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किये जा सकते हैं-
(i) पाठ्यक्रम बनाते समय लैंगिक नीति-निर्माताओं को बालक या बालिका वर्ग समूह को अलग से प्रदर्शित नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें अपनी पाठ्यक्रम नीति में समजातीय समूह का समावेश करना चाहिए व एक दिशीय व समान कार्य-प्रणाली उपयोग में लानी चाहिए।
(ii) गणितीय, वैज्ञानिक तथा टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर बालक (नर) समूह का आधिपत्य है। बालिकाओं को पाठ्यक्रम के इन विषयों का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
(iii) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत शैक्षिक तथा सह-शैक्षिक सभी प्रकार की गतिविधियों में (बालिका वर्ग) के योगदान को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान हस्तान्तरण कार्यक्रम जो कि मुख्य रूप से बालिकाओं- को इन गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करे, उनका आयोजन।
(iv) विषय चयन में परिवार, अध्यापक, सहयोगी समूह द्वारा बालिकाओं में प्रेरणा उत्पन्न करना ।
(v) सभी प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक कोर्सों को अनिवार्य स्तर पर लागू किया जाना चाहिए।
(vi) नृत्य, गायन, अभिनय व कला जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
उपर्युक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम में विस्तार तथा विषय-प्रणाली में परिवर्तन करके लिंग-असमानता को कम किया जा सकता है।
प्रश्न e (i) पाठ्यक्रम में समावेशन को स्पष्ट कीजिए।
अथवा
पाठ्यक्रम निर्धारकों में समावेशी शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए।
उत्तर- 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) में बच्चों के अधिकार विषय पर सम्मेलन हुआ और उसमें निर्णय लिया गया कि किसी भी क्षेत्र में बच्चों के साथ किसी भी आधार पर चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र ही क्यों न हो, कोई भेदभाव नहीं होगा। सन् 2001 में विशिष्ट आवश्यकताओं की शिक्षा पर श्वेत-पत्र 61 समावेशी शिक्षा एवं प्रशिक्षण व्यवस्था का निर्माण, 2001 प्रसारित हुआ |इसमें समावेशी शिक्षा के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि समावेशी शिक्षा यह स्वीकार करती है कि सभी सीखने वाले किसी-न-किसी दृष्टि से भिन्न होते हैं तथा उनके सीखने से सम्बन्धित आवश्यकताएँ भी भिन्न होती हैं और ये भिन्नता हमारे लिए मूल्यवान हैं तथा मानवीय अनुभवों का एक सामान्य भाग है। अतः सीखने वालों के बीच अन्तर को स्वीकार करते हुए हम उसका आदर करते हैं, चाहे वह अन्तर आयु, लिंग, नास्तिकता, भाषा, वर्ग एवं अपंगता किसी भी कारण क्यों न हो। इससे समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं उसका स्वरूप निश्चित हुआ और यूनेस्को द्वारा सभी राज्यों से सभी स्तर पर समावेशी शिक्षा की व्यवस्था करने का आह्वान किया गया। यूनेस्को द्वारा समावेशी शिक्षा को बड़े व्यापक रूप से लिया गया है। उसके शब्दों में-
“व्यापक रूप से समावेशन को एक ऐसे सुधार के रूप में लिया जाता है जिसमें सीखने वालों की भिन्नता का आदर किया जाता है।”
प्रश्न e (ii) समावेशी स्कूलों की कार्य-प्रणाली का वर्णन कीजिए।
उत्तर- समावेशी स्कूलों की कार्य-प्रणाली निम्नलिखित दो रूपों में देखी जाती है—
(1) सम्पूर्ण समावेशन-
अर्थात् विद्यालय में सभी प्रकार के बच्चों का प्रवेश, सभी के लिए समान पाठ्यक्रम, सभी को एक ही विधि से एक साथ पढ़ना, लिखना, सभी की एक समान रूप से परीक्षा लेना और सभी का एक ही पैमाने पर मूल्यांकन करना और सभी को एक ही प्रकार के प्रमाण- पत्र देना आदि ।
(2) अल्प समावेशन- जो प्रायः दो रूपों में चलता है-
(i) कुछ विषयों, जैसे—संगीत, कला, स्वास्थ्य शिक्षा एक साथ और कुछ विषयों जैसे-भाषा, विज्ञान, गणित की शिक्षा अलग-अलग और सभी क्रियाओं-खेलकूद एवं समाज सेवा आदि एक साथ ।
(ii) सैद्धान्तिक कार्य अलग-अलग और क्रियात्मक कार्य एक साथ जहाँ तक समावेशन की नीति को पाठ्यचर्या के निर्धारक के रूप में अपनाने की बात है तो समावेशन की इस नीति को हर स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की जरूरत है। बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र से वह चाहे स्कूल में हो या बाहर, सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। स्कूलों को ऐसे केन्द्र बनाए जाने की जरूरत है जहाँ बच्चों को जीवन की तैयारी कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चों खासकर शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों, समाज के हाशिए पर जीने वाले बच्चों और कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों को शिक्षा के इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के सबसे ज्यादा फायदे मिले। अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के मौके और सहपाठियों के साथ बाँटने के मौके देना बच्चों में प्रोत्साहन और जुड़ाव को पोषण देने के शक्तिशाली तरीके हों, स्कूलों में अक्सर हम कुछ गिने-चुने बच्चों को ही बार-बार चुनते रहते हैं।
प्रश्न e (iii) पाठ्यक्रम के निर्धारक के रूप में मूल्य के महत्त्व की व्याख्या कीजिए।
उत्तर – शिक्षक खुद सुविचारित प्रयास कर सकते हैं कि पाठ्य सामग्री और बच्चों के विकास के स्तर के अनुरूप शान्ति से सम्बन्धित मूल्यों को पठन-पाठन में शामिल कर लें और उन पर लगातार बल दें। उदाहरण के लिए, शिक्षा का किसी पाठ में छिपे घटकों का उपयोग सकारात्मक भावों को जगाने के लिए अनुभवों आदि के आधार पर शान्ति के मूल्यों को स्थापित करने के लिए कर सकते हैं। प्रश्न किस्सा, कहानी, खेलकूद, व्यावहारिक चर्चा, उदाहरणों, रूपकों, मूल्य स्पष्टीकरण के माध्यम से शान्ति की शिक्षा दी जा सकती है। नैतिक शिक्षा और आचरण व्यक्तिगत, सामाजिक, सामुदायिक और वैश्विक आयामों से जोड़कर सिखाये जा सकते हैं। शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रमों में भी शान्ति की शिक्षा को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया जा सकता है।
इस सन्दर्भ में विद्यालयी शिक्षा के बहुत प्रारम्भिक चरण में ही मूल्य शिक्षा के प्रसार सम्बन्धी एक समग्र कार्यक्रम को विद्यालयी दिनचर्या के नियमित अंग के रूप में शुरू करना अनिवार्य है। सम्पूर्ण शिक्षा प्रक्रिया ऐसी हो कि बालक-बालिकाएँ इस योग्य बन जाएँ कि ये ‘उत्तम’ को जानें, ‘उत्तम’ से प्रेम करें और ‘उत्तम’ कार्य करने तथा एक-दूसरे के प्रति सहनशील नागरिकों के रूप में विकसित हों। इसके लिए प्रत्येक शिक्षक को मूल्य- शिक्षक बनाना होगा। प्रत्येक क्रिया-कलाप, इकाई और अन्तर्क्रिया का परीक्षण, मूल्य-पहचान, मूल्य-प्रसार, मूल्य-प्रबलन और इसके पश्चात् मूल्यों को अमलीजामा पहनाने के लिए सन्तुलित और समुचित कार्यनीति सम्बन्धी निर्णयों के आधार पर निर्णय लेने चाहिए। मूल्य निष्पादन के लिए दो पक्षीय संवाद, कल्याण सेवाएँ, जरूरतमन्द छात्रों की मदद, उपचारात्मक शिक्षण, पुनर्मूल्यांकन और कमतर उपलब्धियों वाले छात्रों को निरस्त न करने का भाव आवश्यक है। इसके लिए ऐसे नियमों का निर्माण करना आवश्यक होगा जिनमें प्रत्येक छात्र का खेलकूदों, विद्यालयी क्रियाकलापों और उनकी रुचियों से जुड़े कार्यक्रमों में सहभागिता सुनिश्चित की जा सकेगी।
प्रश्न e (iv) मूल्यों के पाठ्यक्रम में किन क्रियाओं को समावेशित किया जा सकता है?
उत्तर-मूल्यों के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित क्रियाएँ समावेशित की जा सकती हैं-
(i) विद्यालयी सभा और समूह गायन और मौन एवं ध्यान साधना का अभ्यास ।
(ii) पैगम्बरों, संतों और पंक्ति धर्मग्रन्थों से जुड़ी रुचिकर कथाओं और जीवनियों का वर्णन ।
(iii) खेल के मैदानों की गतिविधियाँ अर्थात् खेलकूद, ऐसे सामाजिक कार्य जो मनुष्य जाति के साथ-साथ अन्य प्राणियों यहाँ तक कि पद्धति की सेवा का दृष्टिकोण भी पैदा करें और ‘कार्य ही पूजा है’ की भावना उत्पन्न करें।
(iv) उपयुक्त विषयों, कथानकों पर आधारित कार्यक्रम और नाटकों का आयोजन ।
(v) माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ।
(vi) शिक्षक या अतिथि वक्ता द्वारा प्रातःकालीन सभा में ज्ञानयुक्त पुस्तकों एवं महान साहित्य के अंशों का वाचन एवं उपयुक्त सम्बोधन ।
(vii) विश्व के मुख्य धर्मों की आवश्यक शिक्षाएँ और धर्म दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन। (viii) अवकाश एवं विद्यालय से छूटने के बाद के समय में समाज सेवा ।
(ix) सामुदायिक गायन, कार्यक्रम, राष्ट्रीय एकता शिविर, राष्ट्रीय समाज सेवा एन.सी.सी. शिविर, स्काउट एवं गाइडिंग कार्यक्रम ।
प्रश्न e (v) राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कार्य-योजना का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
(1) पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने पर बल दिया जायेगा।
(2) पाठ्यक्रम में संशोधन करने तथा स्कूल प्रणाली में चरणाबद्ध ढंग से पाठ्य-पुस्तक विकसित करने के लिए कदम उठाये जायेंगे।
(3) न्यूनतम शिक्षण स्तर स्थापित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जायेंगे-
(i) न्यूनतम शिक्षण स्तर कार्य नीति में मुख्य ध्यान समग्र आधारित अध्यापन और शिक्षण के विकास पर दिया जायेगा।
(ii) मौजूदा स्तरों को जानने के लिए शिक्षण उपलब्धियों का प्रारम्भिक मूल्यांकन किया जायेगा। (iii) यदि अनिवार्य हुआ, तो स्थानीय उपलब्धियों के अनुकूल बनाने के लिए न्यूनतम शिक्षण स्तरों में संशोधन किया जायेगा।
(iv) क्षमता आधारित शिक्षण के लिए शिक्षकों का प्रारम्भिक तथा पुनर्विवेक अनुस्थापन किया जायेगा।
(v) न्यूनतम शिक्षण स्तरों पर आधारित शिक्षण के लिए शिक्षक प्रशिक्षण पुस्तिकाएँ तैयार की जायेंगी।
I
प्रश्न e (vi) पाठ्यक्रम तथा पाठ्य विवरण में अन्तर स्पष्ट कीजिए ।
अथवा
पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या में क्या अन्तर है?
उत्तर-
पाठ्यचर्या
पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अन्तर
1. पाठ्यचर्या में अनेक विषयों, क्रियाओं तथा
अनुभवों को रखा जाता है जो शिक्षा के. उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं।
2. पाठ्यचर्या व्यापक और विस्तृत होती है। इसमें
औपचारिक तथा अनौपचारिक सभी प्रकार की क्रियाओं को शामिल किया जाता है।
3. पाठ्यचर्या का उद्देश्य छात्र व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। I
4. पाठ्यचर्या सम्पूर्ण जीवन की तैयारी करवाता है। छात्रों को जीवन के सामान्य अनुभव प्रदान करता है।
5. पाठ्यचर्या जीवन-केन्द्रित होती है।
पाठ्यक्रम
1. पाठ्यक्रम के अन्तर्गत केवल विभिन्न विषयों तथा कौशलों का समावेश होता है।
2. पाठ्यक्रम में केवल औपचारिक विषयों तथा क्रियाओं का समावेश होता है।
3. पाठ्यक्रम से व्यक्तित्व के एक विशिष्ट अंग (ज्ञान व कौशल) का विकास कतिपय विशिष्ट विषयों के अध्ययन से होता है।
4. पाठ्यक्रम छात्र को विशिष्ट अनुभव प्रदान करके जीवन के एक सीमित पक्ष के लिए तैयार करता है।
5. पाठ्यक्रम केवल परीक्षा केन्द्रित होता है \
प्रश्न e (vii) वर्तमान पाठ्यक्रम के दोष बताइए ।
उत्तर- माध्यमिक शिक्षा आयोग ने प्रचलित पाठ्यक्रम के अधोलिखित दोषों की ओर संकेत किया है-
1. वर्तमान पाठ्यक्रम संकुचित दृष्टिकोण रखता है। इसको मुख्यतः शिक्षा-संस्थाओं में प्रवेश पाने की आवश्यकता की पूर्ति के रूप में ही अनुभूत किया गया है। यही स्थिति अभी तक लागू है, जबकि इसके दोषों को दूर करने के लिए समय-समय पर विभिन्न प्रयास किये गये हैं।
2. यह पुस्तकीय ज्ञान पर बल देता है, क्योंकि शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्य-विषय बहुत-कुछ शास्त्रीय एवं सैद्धान्तिक हैं और मुख्यतः सूक्ष्म विचारों एवं सामान्यीकरण से ही सम्बन्धित हैं।
3. प्रत्येक विषय की पाठ्य-वस्तु को बहुत अधिक तथ्यों एवं सूक्ष्म विचारों से लादने की प्रवृत्ति प्रचलित है। प्रायः ये तथ्य बहुत ही कम महत्त्व के हैं जो स्मरण-शक्ति पर अवांछनीय भार डालते हैं।
4. हमारे पाठ्यक्रम बनाने वालों ने ‘विशेषज्ञ’ के दृष्टिकोण को ग्रहण करके सामान्यतः क्षति उठायी है। इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप उन्होंने पाठ्यक्रम एवं पाठ्य-पुस्तकों में अपनी विषय- वस्तु को अधिकाधिक रखने का प्रयास किया और सीखने वालों की आवश्यकताओं, मनोविज्ञान एवं रुचियों की अपेक्षा विषयों के तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक तथ्यों पर अधिक ध्यान दिया है।
5. यह वैयक्तिक विभिन्नताओं से मेल नहीं खाता है। किशोरावस्था में छात्रों में विभिन्न वैयक्तिक अभिरुचियाँ, अभिवृत्तियाँ तथा विशेष दृष्टिकोण विकसित होते हैं, परन्तु वर्तमान पाठ्यक्रम शायद ही इन वैयक्तिक विभिन्नताओं की ओर ध्यान देता है।
प्रश्न e (viii) संरचनावादी उपागम क्या है? –
उत्तर-
अच्छी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए केवल पाठ्यक्रम में कुछ नवाचारों का समावेश करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आज के सूचना प्रधान युग में ज्ञान को भली प्रकार किस प्रकार प्रदान किया जाये यह सोचना भी है, जिसका प्रत्युत्तर हमें ज्ञान के संरचनावादी उपागम में मिलता है। इसका तात्पर्य है कि पाठ्यचर्या के सभी सन्दर्भों को बच्चों की सक्रियता व रचनात्मक सामर्थ्य को पोषित व सम्वर्द्धित करने वाली होना चाहिए। उसका दुनिया में वास्तविक तरीकों से सम्बन्ध बैठाने, दूसरों से जुड़ने की उनकी मूल अभिरुचि को प्रेषित करना चाहिए। संरचनावादी उपागम के अनुसार, सीखना अपने आप में एक सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है, अतः इसे संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में पूर्ण करना चाहिए।
संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। विद्यार्थी सक्रिय रूप से पूर्व प्रचलित विचारों में उपलब्ध सामग्री, गतिविधियों के आधार पर अपने लिए ज्ञान की रचना करते हैं (अनुभव)। उदाहरण के लिए, यातायात व्यवस्था को पाठ या चित्र सा दृश्य सामग्री का उपयोग करते पढ़ाने तथा उस पर विद्यार्थियों में चर्चा कराने से उनमें यातायात व्यवस्था सम्बन्धी ज्ञान के निर्माण में मदद की जा सकती है। बच्चों के संज्ञान में अध्यापकों की भूमिका को भी रचनावादी परिप्रेक्ष्य में बढ़ाया जा सकता है। यदि वे ज्ञान निर्माण की उस प्रक्रिया में ज्यादा सक्रिय रूप से शामिल हो जाएँ जिसमें बच्चे व्यस्त हैं।
प्रश्न f (i) मूल्यांकन उपागम के अन्तर्गत कोर पाठ्यक्रम बताइए।
अथवा
कोर पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
कोर- केन्द्रित पाठ्यक्रम-कोर पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं तथा अधिक विषय ऐच्छिक । अनिवार्य विषयों का अध्ययन करना प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य होता है तथा ऐच्छिक विषयों को व्यक्तिगत रुचियों तथा क्षमताओं के अनुसार चुना जा सकता है। यह पाठ्यक्रम अमरीका की देन है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बालक को व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों प्रकार की समस्याओं के सम्बन्ध में ऐसे अनुभव प्रदान किए जाते हैं जिनके द्वारा वह अपने भावी जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या को सरलतापूर्वक सुलझाते हुए कुशल तथा समाजोपयोगी एवं उत्तम नागरिक बन जाये। संक्षेप में, कोर पाठ्यक्रम का लक्ष्य व्यक्ति तथा समाज दोनों का अधिक से अधिक विकास करना है। इस पाठ्यक्रम की कई विशेषताएँ भी हैं, जैसे- इसके ‘ अन्तर्गत कई विषयों को एक साथ पढ़ाया जाता है, विभिन्न विषयों को पढ़ाने का समय भी निश्चित होता है तथा साथ ही यह बालक की आवश्यकताओं व अभिरुचियों के मूल्यांकन पर भी केन्द्रित है। जेम्स ली कोर पाठ्यक्रम को परिभाषित करते हुए लिखते हैं- “कोर पाठ्यक्रम वह है जो व्यक्तिगत- तथा शाश्वत दोनों ही प्रकार के हितों से सम्बन्धित अन्तःक्षेत्रीय समस्याओं में केन्द्रित होता है। इसमें विषयवस्तु को विचाराधीन समस्या के समाधान के लिए आवश्यक होने के नाते सीखने के लिए स्थान प्रदान किया जाता है।”
अलबर्टी ने कोर पाठ्यक्रम को परिभाषित करते हुए लिखा है, “कोर पाठ्यक्रम उस समग्र पाठ्यक्रम का एक अंग माना जा सकता है जो सभी छात्रों के लिए आधारभूत है तथा जिसमें सीखने की उन क्रियाओं का समावेश रहता है, जिनका संगठन परम्परागत विषयों से पृथक् रखकर किया जाता है।”
प्रश्न f (ii) पाठ्यक्रम अभिकल्प क्या है? इसके घटक बताइए ।
उत्तर- पाठ्यक्रम योजना के विभिन्न अंशों की व्यवस्था पाठ्यचर्या अभिकल्प कहलाती है। इसे पाठ्यचर्या संगठन एवं पाठ्यक्रम संरचना भी कहते हैं। इन अंशों को निर्माणक घटक अथवा तत्त्व कहते हैं। ये तत्त्व हैं – (1) अभिप्राय, लक्ष्य, उद्देश्य; (2) विषय सामग्री; (3) अधिगम अनुभव और (4) मूल्यांकन उपागम ।
–
अभिकल्प के घटक
पाठ्यक्रम अभिकल्प का सम्बन्ध पाठ्यचर्या के चार बुनियादी अंशों, यथा- उद्देश्य, विधि एवं संगठन, विषय सामग्री, मूल्यांकन की प्रकृति एवं व्यवस्था से होता है। गाइल्स (1942) ने घटक शब्द का उपयोग इनके सम्बन्ध को बताने के लिए किया है। उसने अधिगम अनुभवों की विधि एवं संगठन के अन्तर्गत सम्मिलित किया है।
प्रस्तुत अभिकल्प के चार घटक अनेक प्रश्नों के उत्तर देते हैं जैसे—क्या किया जाना है? क्या विषय-वस्तु शामिल करना है? अनुदेशन की कौन-सी व्यूह रचना, स्रोत एवं गतिविधियाँ उपयोग में लायी जाएँगी? पाठ्यचर्या के परिणामों के मूल्यांकन के लिए कौन-सी विधि एवं उपकरण उपयोग में लाए जाएँगे? गाइल्स के अनुसार ये चारों घटकों के बारे में लिए गए निर्णयों पर आश्रित होते हैं।
प्रश्न f (iii) पाठ्यक्रम विकास से आप क्या समझते हैं?
अथवा
पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
उत्तर- इस प्रत्यय में ‘पाठ्यक्रम विकास’ का प्रयोग साधारण रूप में तथा अधिक किया जाता है। पाठ्यक्रम विकास का अर्थ निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया जो कभी समाप्त नहीं होती है और यह कहाँ से आरम्भ हुई इसका भी बोध नहीं होता है। शिक्षण की आवश्यकता की जानकारी छात्रों की उपलब्धियों से हो जाती है जिनको शिक्षक प्राप्त करने का प्रयास करता है। परीक्षण के द्वारा यह भी जानकारी हो जाती है कि किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त हुए हैं।
इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि, “अधिगम-अवसरों के नियोजन द्वारा छात्रों के व्यवहारों में विशिष्ट परिवर्तन लाना तथा परीक्षण द्वारा यह जानना कि किस सीमा तक अपेक्षित परिवर्तन हुआ है। इस प्रत्यय को पाठ्यक्रम-विकास की संज्ञा दी जाती है।
पाठ्यक्रम का मुख्य लक्ष्य छात्रों का विकास करना है इसलिए पाठ्यक्रम का प्रारूप ऐसा हो, जिससे छात्रों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके। यह प्रक्रिया चक्रीय तथा निरन्तर चलने वाली मानी जाती है-
इसके प्रमुख चार तत्त्व माने जाते हैं-
1. शिक्षण उद्देश्य – सभी साधनों का प्रयोग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, पाठ्यवस्तु का साधन है उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि ।
2. शिक्षण विधि तथा पाठ्यवस्तु- छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिए अधिगम- परिस्थितियाँ तथा अवसर शिक्षण विधियों एवं पाठ्यवस्तु की सहायता से उत्पन्न किए जाते हैं। जिससे उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें।
3. परीक्षण प्रक्रिया – इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि शिक्षण विधियों तथा पाठ्यवस्तु से किसी सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है
4. पृष्ठपोषण – परीक्षण का अर्थापन शिक्षकों तथा छात्रों को पृष्ठपोषण प्रदान करता है तथा पाठ्यक्रम के प्रारूप को सुधार के लिए दिशा मिलती है। पृष्ठपोषण मूल्यांकन का प्रभाव पाठ्यक्रम में होता है।
प्रश्न f(iv) टोली शिक्षण क्या है?
उत्तर-टोली शिक्षण का अर्थ-
टोली शिक्षण का विकास सर्वप्रथम 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ। इसके बाद यह प्रत्यय 1960 में ब्रिटेन में पहुँचा। ब्रिटेन में इसका विकास जे. फ्रीमैन ने किया। धीरे-धीरे इसका प्रयोग स्कूलों व कॉलेजों में किया जाने लगा। शिकागो विश्वविद्यालय के फ्रांसिस चेज ने टोली शिक्षण (Team-Teaching) का प्रयोग प्रभावशाली शिक्षण के लिये किया। कॉलेजों में सफल प्रयोग के बाद इस उपागम का प्रयोग द्वितीय विश्वयुद्ध के समय सेना के प्रशिक्षण के लिये किया जाने लगा और भारत में भी इस उपागम का प्रयोग किया आरम्भ हो गया है, लेकिन अभी इसकी सफलता पर सन्देह बना हुआ है।
1
समूह (टोली) शिक्षण भारतीय परिस्थितियों में शिक्षा का एक नया दृष्टिकोण है। समूह शिक्षण या टोली शिक्षण, शिक्षण की एक सुव्यवस्थित प्रणाली है जिसमें कई शिक्षक मिलकर विद्यार्थियों के एक समूह को अनुदेशन (Instruction) प्रदान करते हैं और एक साथ मिलकर किसी विशिष्ट प्रकरण के लिये शिक्षण का संयुक्त उत्तरदायित्व लेते हैं। इसमें सामान्यतः दो या दो से अधिक शिक्षक भाग लेते हैं। ये शिक्षक, शिक्षण की योजना और उसका कार्यान्वयन छात्रों के समूह के लिये मिलकर करते हैं। इस प्रकार की शिक्षण विधियों की योजना, समय तथा प्रक्रिया लचीली रखी जाती है ताकि शिक्षण- उद्देश्यों के अनुसार तथा शिक्षकों की योग्यता के अनुसार समूह शिक्षक के कार्यक्रम में आवश्यक व इच्छित परिवर्तन लाये जा सकें। इस उपागम के अन्तर्गत शिक्षकों का समूह पारस्परिक सहयोग के आधार पर शिक्षण एवं मूल्यांकन सम्बन्धी उत्तरदायित्वों को मिल-जुलकर निभाते हैं। यह उपागम इस दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण तथा अद्भुत है क्योंकि इसके माध्यम से प्रत्येक शिक्षक अपने प्रभावशाली गुणों व क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर सकता है। कुछ अध्यापक कक्षा-शिक्षण अधिक प्रभावशाली ढंग से कर लेते हैं, तो कुछ प्रयोगशाला कार्य में अधिक दक्ष होते हैं, और अन्य सहायक सामग्री के निर्माण में। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक शिक्षक का अपना अनूठा योगदान रहता है। समूह शिक्षण की सफलता शिक्षकों के उचित चयन पर निर्भर करती है। कार्य विभाजन से शिक्षकों का कार्यभार हल्का हो जाता है और उन्हें अपने हिस्से के कार्य को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। छात्रों को इस उपागम में परिश्रम तो अधिक करना पड़ता है लेकिन अधिगम की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है।
प्रश्न f (v) पाठ्यचर्या विकास क्या है?
उत्तर- किसी भी प्रभावशाली शिक्षण हेतु पाठ्यचर्या की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और उससे भी महत्त्वपूर्ण है कि पाठ्यचर्या का विकास कैसे किया जाये क्योंकि यह एक विशेष क्षेत्र होता है। इसमें शिक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि उन्हें पाठ्यचर्या की अवधारणा व अधिगम अनुभवों के विषय में उचित जानकारी हो जिससे इस पाठ्यचर्या द्वारा समाज के अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। ‘पाठ्यचर्या विकास’ का अर्थ निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया से है जो कभी समाप्त नहीं होती है। शिक्षक, शिक्षण की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या द्वारा अधिगम समूह या लक्ष्य समूह की आवश्यकताओं को संज्ञान में रखते हुए विभिन्न आधारिक तत्त्वों को ध्यान में लेकर पाठ्यचर्या का विकास करता है। इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि, शिक्षक यह जानने का प्रयास करता है कि अधिगम अवसरों के नियोजन द्वारा छात्रों के व्यवहारों में विशिष्ट परिवर्तन किस प्रकार लाया जा सकता है व यह किस सीमा तक जाना जा सकता है कि उनमें कितना अपेक्षित परिवर्तन हुआ है। इसी प्रत्यय को पाठ्यक्रम विकास की संज्ञा दी जाती है।
प्रश्न f (vi) पाठ्यचर्या के विकास के प्रमुख तत्त्वों का वर्णन कीजिए।
उत्तर- पाठ्यचर्या विकास के प्रमुख तत्त्व निम्नलिखित हैं- (i) आवश्यकताओं का विश्लेषण। (ii) उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, (iii) आगत तत्त्वों का विश्लेषण, (iv) प्रक्रिया अभिकल्प तैयार करना, (v) प्रारम्भिक जाँच ।
प्रश्न f(vii) विषय-केन्द्रित पाठ्यक्रम की व्याख्या कीजिए।
अथवा
विषय-केन्द्रित पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए।
उत्तर-परम्परागत उपागम के अन्तर्गत विषय-केन्द्रित पाठ्यक्रम आता है जिससे पाठ्यक्रम के स्वरूप में विषय-वस्तु को अधिक महत्त्व दिया जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में बालक तथा इसकी रुचियों एवं योग्यताओं को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता है। इसमें शिक्षक ही सर्वेसर्वा होता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में विषय को ही आधार मानकर पाठ्यक्रम को नियोजित एवं संगठित किया जाता है
है जिसका उद्देश्य विषयों के ज्ञान को पृथक्-पृथक् रूप से प्रदान करना होता है। इस पाठ्यक्रम का सूत्रपात प्राचीन ग्रीक तथा रोम के विद्यालयों में हुआ। इसमें सभी विषयों के ज्ञान को अलग-अलग निश्चित कर लिया जाता है तथा उसी के अनुसार पुस्तकें तैयार कर ली जाती हैं। इन्हीं पुस्तकों से बालक विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस पाठ्यक्रम में पुस्तकों पर अधिक बल दिये जाने के कारण इसे ‘पुस्तक केन्द्रित’ पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। इसमें बालकों की अपेक्षा विषय-ज्ञान को महत्त्व दिया जाता है। परन्तु इस प्रकार के पाठ्यक्रम में पाठ्य-वस्तु पहले से निश्चित होने के कारण शिक्षक को यह मालूम होता है कि उसे क्या-क्या पढ़ाना है तथा विद्यार्थी भी यह जानते हैं या जान सकते हैं कि उन्हें क्या-क्या पढ़ना है। इसमें निश्चित पाठ्य-वस्तु से ही छात्रों की परीक्षा ली जाती है तथा इस मूल्यांकन से यह ज्ञात किया जाता है कि बालक ने कितना सीखा है अर्थात् उसकी उपलब्धि क्या रही है।
विषय-केन्द्रित पाठ्यक्रम में अध्यापक का शिक्षण पाठ्यक्रम तक ही सीमित रहता है। वह पाठ्यक्रम के अलावा छात्रों को कोई और ज्ञान देना उचित नहीं समझता है। वह छात्र के केवल ज्ञान भण्डार को बढ़ाने पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करता है, भले ही उस ज्ञान की छात्र के जीवन में कोई उपयोगिता हो या न हो ।
प्रश्न g (i) पर्यावरण पर आधारित उपागम की व्याख्या कीजिए।
अथवा
पाठ्यक्रम निर्धारकों के लिए पर्यावरणीय सरोकारों का आलोचनात्मक परिणामों के रूप में वर्णन कीजिए।
उत्तर—प्रत्येक व्यक्ति भौतिक, प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण में रहता है। वह भौतिक जगत् का एक भाग है। प्रकृति से वह वनस्पति, पानी, हवा इत्यादि के मध्य रहता है। वह एक सामाजिक प्राणी है और उसे विरासत में मिली एक संस्कृति होती है। अतः ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें उसके वातावरण से सम्बन्धित उपागम के पाठ्य-वस्तु निर्माण वातावरण से सम्बन्धित विभिन्न इकाइयों का चयन करते हैं। वातावरण आधारित उपागम में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शैक्षिक महत्ता तो है ही साथ ही इसमें क्रिया आधारित उपागम भी शामिल है। इस उपागम के क्रियान्वयन में जो * कठिनाइयाँ हैं, वे निम्न हैं-
विषय-वस्तु को वातावरण पर आधारित संगठित करने से पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है। कुछ विषय-वस्तु तो ऐसी होती है कि उसमें ज्ञानात्मक पक्ष होता है जिसको पर्यावरण से सम्बन्धित नहीं किया जा सकता है।
प्रश्न g (ii) व्यवहारिक उपागम का वर्णन कीजिए।
उत्तर- छात्रों के अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के रूप में उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। व्यवहार परिवर्तन का ज्ञान मूल्यांकन से होता है इसीलिए इसे मूल्यांकन प्रतिमान भी कहा जाता है।
बी. एस. ब्लूम ने शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षण एवं परीक्षण की क्रियाओं को उद्देश्य केन्द्रित बनाने पर बल दिया तथा कहा कि शिक्षण में जिन उद्देश्यों को महत्त्व दिया जाए उन्हीं उद्देश्यों के लिए परीक्षण भी किया जाना चाहिए। इस प्रतिमान के अन्तर्गत निम्नलिखित सोपानों का अनुसरण किया जाता है-
(a) शिक्षण उद्देश्यों का प्रतिपादन ।
(b) उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीखने के अनुभवों का सृजन ।
(c) बालकों में होने वाले व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन।
इस उपागम पर विकसित दो प्रतिमान निम्नलिखित हैं–
(i) हिल्दा टाबा का व्यापक मूल्यांकन पाठ्यक्रम प्रतिमान ।
(ii) मुखोपाध्याय निर्मित पाठ्य मूल्यांकन का प्रतिमान ।
प्रश्न g (iii) विषय आधारित उपागम की व्याख्या कीजिए।
अथवा
पाठ्यक्रम विकास में विषय केन्द्रित उपागम की विवेचना कीजिए।
उत्तर- मानव के ज्ञान का भण्डार तथ्यों, प्रत्ययों, तथा सामान्यीकरणों, सिद्धान्तों से भरा हुआ है। ये ज्ञान के तत्त्व एक समान लगते हैं। ये एक-दूसरे से सह-सम्बन्धित हैं। यह सहसम्बन्धिता इनको संगठित होने का अवसर प्रदान करती है जिससे कि इनको पूर्णता मिल सके। इसलिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने आरम्भ में ज्ञान के विभिन्न तत्त्वों को पहचाना और एक तर्कयुक्त तरीके में संगठित किया। ज्ञान के तत्त्वों में जो सम्पन्न पाया गया उसको बी. एम. ब्लूम के अन्तर अनुशासन सूत्र से परिभाषित किया, जबकि गुडलैण्ड महोदय ने इनको संगठन केन्द्र बताया। संगठित ज्ञान को ही विषय का अनुशासन कहते हैं।
व्यापक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माता किसी भी विषय का व्यापक क्षेत्र लेकर निर्माण करते हैं। जैसे-गणित, प्राकृतिक विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान आदि ।
मध्यम स्तर पर पाठ्यक्रम संगठनकर्त्ता, पाठ्यक्रम को विषय की इकाई में संगठित कर लेते हैं। जैसे—प्रकाशिकी, अम्ल, क्षार व लवण, मस्तिष्क आदि।
संकीर्ण स्तर पर इकाई की उप-इकाई बनाकर पाठ का संगठन करते हैं
इस उपागम से निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता है-
* विशेषज्ञों के विचार ।
• अनुभवी विषय अध्यापक के निष्कर्ष ।
* कक्षा में उपयोग में लाई गई निर्देशन सामग्री।
* विद्यार्थी की रुचि, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अनुभव आदि।
किसी भी विषय के पाठ्यक्रम में कई इकाइयाँ होती हैं। प्रत्येक इकाई की उप इकाइयाँ होती हैं। विषय आधारित उपागम विषय का संगठन तर्क पर आधारित होता है। यह दो प्रकार का होता है-
(1) विषय-वस्तु केन्द्रित, (2) संरचना केन्द्रित ।
प्रश्न g (iv) परम्परागत पाठ्यक्रम।
उत्तर—यह पाठ्यक्रम शिक्षा के प्रति परम्परागत दृष्टिकोण रखता है। इसमें आध्यात्मिक एवं नैतिक जीवन के विकास पर बल दिया जाता है। प्राचीन यूनान के स्कूलों तथा भारतीय गुरुकुलों ने* शास्त्रीय पाठ्यक्रम का सूत्रपात किया है। इसके अन्तर्गत शास्त्रीय भाषाओं, दर्शन, ज्योतिष, गणित, व्याकरण, अध्यात्मशास्त्र, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र आदि विषयों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यह पाठ्यक्रम विषय-केन्द्रित पाठ्यक्रम का ही एक रूप है। वर्तमान समय में सामान्य विद्यालयों में इस पाठ्यक्रम की कोई उपयोगिता नहीं मानी जा रही है।
प्रश्न g (v) दक्षता आधारित उपागम को बताइए।
उत्तर- दक्षता आधारित उपागम अधिगम की न्यूनतम दक्षता में तथा नैपुण्य अधिगम पर आधारित है। छात्रों में शैक्षिक उपलब्धि का स्तर सुधारने के लिए अधिगम के न्यूनतम स्तरों के निर्धारण की आवश्यकता अनुभूत की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि सभी बच्चों को बिना किसी जाति, धर्म, वंश, सम्प्रदाय, स्थान व लिंग भेद के अच्छी शिक्षा मिले। दूसरे शब्दों में छात्रों में शैक्षिक उपलब्धि के स्तर को सुधारने के लिए अधिगम के न्यूनतम स्तरों को निर्धारित करने की आवश्यकता, महसूस की गई। न्यूनतम अधिगम स्तर कार्यक्रम के मूल में शिक्षा की मौजूद विषमताओं को दूर करने व गुणवत्ता
को समता से जोड़ने की भावना निहित है।
अतः अधिगम के न्यूनतम स्तरों के क्षेत्र में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने यूनिसेफ की सहायता से 1978 में दो परियोजनाओं – ( 1 ) Primary Education Renewal तथा (2) Developmental Activities in Community Education and Particupation पर कार्य किया और ‘न्यूनतम अधिगम सातत्यक’ रेखांकित किये। इसमें उन अधिगम परिणामों का उल्लेख किया गया जिनकी प्राप्ति कक्षा 2, 3, 4 तथा 5 का अध्ययन पूरा करने वाले छात्रों से अपेक्षा की जा सकती थी। इस सातत्यक में वर्णित दक्षताओं के आधार पर प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम तकनीकीकरण परियोजना में निष्पत्ति परीक्षणों का विकास किया गया। 1986 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने प्राथमिक स्तर पर अधिगम के न्यूनतम स्तर विषयक दस्तावेज तैयार किया।
शिक्षा के विकास के लिए दबे समिति ने अपना विचार दिया-
दबे समिति ने प्राथमिक कक्षाओं के लिए भाषा में निम्न दक्षताओं के रूप में न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारित किये हैं— 1. सुनना, 2. बोलना, 3. पढ़ना, 4. लिखना, 5. समझना व अवबोध, 6. कार्यात्मक व्याकरण, 7. स्व-अधिगम, 8. भाषा-प्रयोग, तथा 9. शब्दावली नियन्त्रण।
दबे समिति के अनुसार ही अधिगम दक्षता मानव शक्ति के विकास में क्रमिक होती है। बच्चा पहले बैठना सीखता है फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है। बालक में शिक्षा द्वारा तीन शक्तियों का विकास किया जाता है—बौद्धिक शक्ति, कौशल शक्ति व नैतिक शक्ति ।
प्रश्न g (vi) बाल-केन्द्रित पाठ्यक्रम की व्याख्या कीजिए।
उत्तर- बाल-केन्द्रित पाठ्यक्रम-इस प्रकार के पाठ्यक्रम का विकास शिक्षा में बढ़ती हुई मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप हुआ जिसके अन्तर्गत विषयों की अपेक्षा बालकों को मुख्य स्थान दिया जाता है। अतः इस प्रकार के पाठ्यक्रम का आयोजन भी प्रयोगवादी विचारधारा के अनुरूप बालक को केन्द्र मानकर किया जाता है। ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण बालक की विभिन्न अवस्थाओं की रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं तथा योग्यताओं के अनुसार किया जाता है जिससे उसके व्यक्तित्व का समुचित विकास हो सके। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का सूत्रपात जॉन डीवी के लेबोरेटरी स्कूल से हुआ है। जेम्स एम. ली. ने बालकेन्द्रित पाठ्यक्रम को इस प्रकार परिभाषित किया है—“छात्र केन्द्रित पाठ्यक्रम वह है जो पूर्णतः और समग्र रूप में सीखने वाले में निहित है।”
प्रश्न g (vii) बाल-केन्द्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएँ बताइए।
उत्तर- बाल-केन्द्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
(i) इस पाठ्क्रम में बालकों की परिवर्तित आवश्यकताओं, रुचियों, अभिप्रायों, संवेगों आदि को आधार बनाया जाता है।
(ii) यह पाठ्यक्रम क्रियात्मक होने के कारण शिक्षार्थियों को उद्देश्यपूर्ण अनुभव भी प्रदान करता है।
(iii) यह बालकों पर सीखने का उत्तरदायित्व डालता है।
(iv) यह पाठ्यक्रम मनोविज्ञान की इस विचारधारा का भी समर्थन करता है कि यदि बालक की रुचियों एवं आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जायेगा तो उसका समुचित विकास नहीं हो सकेगा।
(v) आधुनिक शिक्षण पद्धतियाँ जैसे-मॉण्टेसरी पद्धति, किण्डरगार्टन पद्धति आदि बाल- केन्द्रित पाठ्यक्रम की ही देन है।
(vi) यह पाठ्यक्रम प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है।
(नवीन) बी.एड. द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) : तृतीय प्रश्न-पत्र : ज्ञान व पाठ्यक्रम (303)
प्रश्न g (viii) क्रिया-केंद्रित पाठ्यक्रम।
उत्तर- क्रियाकेन्द्रित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों को विशेष स्थान दिया जाता तथा आज के मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षाविद् भी इसकी प्रशंसा करते हैं। उनके अनुसार इस प्रकार का पाठ्यक्रम बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुरूप होता है क्योंकि क्रिया करना बालक का स्वाभाविक गुण है। बालक कोई न कोई क्रिया करता ही रहता है। वह शान्त तथा निष्क्रिय रूप में कठिनाई से ही बैठता है। बालक की इसी विशेषता के कारण जॉन डीवी किलपैट्रिक, मारिया मान्टेसरी तथा फ्रोबेल जैसे व्यावहारिक शिक्षाशास्त्रियों ने क्रिया-केन्द्रित पाठ्यक्रम को अपनी-अपनी शिक्षण प्रणालियों में अपनाया।
क्रिया केन्द्रित पाठ्यक्रम की परिभाषा देते हुए जॉन डीवी लिखते हैं, “क्रिया – केन्द्रित पाठ्यक्रम 1. बालक की क्रियाओं की सतत् प्रवाहित होने वाली धारा है जिससे व्यवस्थित विषयों में कोई व्यवधान
नहीं आता तथा जो बालकों की रुचियों तथा अनुभूत व्यक्तित्व आवश्यकताओं से उदित होती हैं।”
प्रश्न h (i) क्रिया-केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएँ बताइए ।
उत्तर- क्रिया-केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
(i) इसमें सभी विषयों का समस्त ज्ञान केवल क्रियाओं के आधार पर अथवा अधिगम क्रियाओं के आधार पर प्राप्त किया जाता है।
(ii) यह बालकों की मानसिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। अतः यह मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित होता है।
(iii) इसमें बालक स्वयं क्रिया करके सीखता है जिससे उसकी कल्पनाशक्ति एवं सृजनात्मकता में वृद्धि होती है।
(iv) यह छात्रों को आत्मानुभूति के अवसर देता है क्योंकि छात्र स्वयं करके वस्तु का निर्माण करते हैं। उनमें यह आत्म-गौरव भी विकसित होता है कि यह मैंने किया है।
(v) छात्रों से मिलकर क्रिया करने की प्रवृत्ति विकसित होती है जो अन्ततः सामाजिक विकास में सहायक होती है।
(vi) छात्रों में शारीरिक श्रम के प्रति सकारात्मकता की भावना विकसित होती है।
(vii) छात्रों में इस पाठ्यक्रम के द्वारा आत्मविश्वास की भावना आती है तथा अनुशासनहीनता की समस्या समाप्त हो जाती है।
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ बी.एड नोट्स
प्रश्न h (ii) पाठ्यक्रम नियोजकों के लिए उपयोगी अधिगम सम्बन्धी सामान्य तथ्य।
उत्तर—विभिन्न मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर अधिगम सम्बन्धी जिन तथ्यों की पुष्टि हो चुकी है, उनमें से प्रमुख निम्न प्रकार हैं-
1. अधिगम निरन्तर रूप से जीवनपर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है।
2. अधिगम शिक्षार्थी की परिपक्वता से सम्बन्धित होता है।
3.अधिगम बालक के शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास की दशाओं से प्रभावित होता है।
4. अधिगम समूह गुण वाली प्रक्रिया है। बालक एक साथ बहुत-सी बातें सीखता है। हम भले ही एक समय में किसी विशेष लक्ष्य पर ध्यान केन्द्रित रखें, किन्तु उसी समय वातावरण से हम अनेक दूसरी बातों को भी सीखते चलते हैं।
5. अधिगम में शिक्षकों की सक्रिय सहभागिता आवश्यक होती है
6. अधिगम अधिक प्रभावी तब होता है, जब बालकों को उसके लक्ष्य स्पष्ट हो ।
7. प्रभावशाली अधिगम के लिए अभिप्रेरणा का होना आवश्यक है।
8. अधिगम के परिणामों से शिक्षार्थी की किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है तथा उसे सन्तोष मिलता है तब अधिगम की गति तेज हो जाती है।
9. अधिगम के लिए मुक्त वातावरण सहायक होता है।
10. अधिगम तत्परता शिक्षार्थी के पूर्व अनुभव, अभिरुचियों एवं अभिवृत्तियों पर निर्भर करता है, परन्तु यह पूर्ण रूप से शिक्षार्थी पर ही नहीं, बल्कि कुछ सीमा तक उस स्थिति पर भी निर्भर करती है जिसके प्रति उसे प्रतिक्रिया व्यक्त करनी होती है अर्थात् पाठ्यक्रम का अपना महत्त्व होता है।
प्रश्न h (iii) मस्तिष्क की विप्लव नीति तथा उसकी विशेषताएँ ।
अथवा
मानसिक उद्वेलन के लाभ बताइए।
उत्तर-मस्तिष्क की विप्लव नीति एक ऐसी नीति है जिसमें ऐसे साधन प्रयोग किए जाते हैं जो छात्रों के मस्तिष्क में ज्ञान प्राप्ति तथा चिन्तन के प्रति हलचल मचा देते हैं। इसमें छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है जिस पर सभी छात्र स्वतन्त्रतापूर्वक विचार करते हैं, वार्तालाप तथा वाद- विवाद करते हैं। शिक्षक सभी विचारों को श्यामपट पर लिखता चला जाता है। वाद-विवाद और चिन्तन तथा वार्तालाप करते-करते एक ऐसा बिन्दु या अवस्था आ जाती है जब छात्र एकदम समस्या को हल कर देते हैं। मस्तिष्क विप्लव नीति छात्रों में चिन्तन विकसित करती है और उन्हें समस्या के विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन में प्रशिक्षण प्रदान करती है |
विशेषताएँ
1. यह शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित है।
2. यह भावात्मक तथा ज्ञानात्मक पक्षों के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है। 3. छात्रों को चिन्तन तथा समस्या समाधान करने के क्षेत्र में उत्साहित करती है।
4. छात्रों की सृजनात्मक क्षमताओं का प्रयोग करती है।
5. सामूहिक चिन्तन तथा वार्तालाप इस विधि में अधिक मूल्यवान विचार प्रदान करते हैं।
6 यह छात्रों को स्वतंत्रतापूर्वक सोचने के लिए प्रेरित करती है।
7 यह शिक्षण की सृजनात्मक शिक्षण नीति है तथा मौलिक विचारों को बढ़ावा देने वाली है।
प्रश्न h (iv) वार्तालाप नीति को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर-ली के अनुसार वार्तालाप “शैक्षिक समूह क्रिया है। इसमें छात्र सहयोगपूर्वक एक-दूसरे से किसी समस्या पर विचार करते हैं।” इस नीति में कोई एक विषय ले लिया जाता है और शिक्षक उस विषय पर छात्रों को वार्तालाप या वाद-विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। यह नीति शिक्षण एवं छात्र में अन्तःप्रक्रिया के अवसर बढ़ाती है। इस विधि की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को अपने विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये। वार्तालाप नीति में सभी छात्रों को बोलने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिये किन्तु शिक्षक एक निरीक्षक तथा निर्देशक के रूप में काम करता रहता है। वार्तालाप नीतियाँ तीन प्रकार की होती हैं-
औपचारिक वार्तालाप
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तथा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु औपचारिक वार्तालाप का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के वार्तालाप के अपने निर्धारित नियम तथा सिद्धान्त होते हैं। यह शिक्षक और छात्रों के मध्य होता है।
अनौपचारिक वार्तालाप
इसमें निर्धारित नियम तथा सिद्धान्तों का प्रयोग नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, अनौपचारिक
वार्तालाप में भाग लेने वाले किसी भी नियम से नहीं बँधे होते हैं। यह शिक्षक तथा छात्रों एवं छात्र-छात्र के मध्य हो सकता है।
शिक्षण बिन्दुओं पर वार्तालाप
वार्तालाप नीति के माध्यम से छात्रों के व्यवहार (उनके सम्प्रेषण, अभिवृत्तियों, मूल्यों, सामाजिक विकास आदि) में वांछित परिवर्तन लाया जाता है।
प्रश्न h (v) वार्तालाप विधि की विशेषताएँ व सीमाएँ।
उत्तर-
वार्तालाप विधि की विशेषताएँ
(1) इसमें गलत उपागमों को अनुत्साहित किया जाता है
(2) छात्रों में आत्मविश्वास जाग्रत होता है।
(3) छात्रों की अभिवृत्ति के विकास में सहायक है।
(4) छात्रों को ध्यानपूर्वक सुनने और उचित उत्तर देने के लिए प्रेरित करती है।
(5) शिक्षक तथा छात्र परस्पर निकट आते हैं और एक-दूसरे को भली-भाँति समझते हैं।
(6) ये छात्रों को सक्रिय बनाती है।
(7) छात्रों की सृजनात्मक विशेषताओं को बढ़ाती है।
(8) यह जनतान्त्रिक नीति है।
(9) इसमें सामाजिक-अधिगम के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं।
(10) इससे ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्षों के उच्च उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है।
वार्तालाप विधि की सीमाएँ
(1) सभी छात्र समान रूप से बोल नहीं पाते।
(2) छात्रों में कभी-कभी ईर्ष्या तथा स्पर्द्धा जगा देती है
(3) छात्र कभी-कभी विषय से काफी दूर चले जाते हैं।
(4) अनावश्यक आलोचना या बाल की खाल निकालने वाले लोग इसके उद्देश्य को नष्ट कर सकते हैं।
प्रश्न h (vi) वाद-विवाद विधि से आप क्या समझते हैं? इसकी परिभाषा लिखिए।
उत्तर-आधुनिक शैक्षिक विचारधारा के अनुसार, बालक को निष्क्रिय श्रोता नहीं माना जाता है वरन् उसको सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय बनाये रखने पर बल दिया जाता है। बालक जिस ज्ञान को क्रिया करके प्राप्त करता है वह स्थायी रहता है। बालक को सक्रिय बनाये रखने के लिए विभिन्न क्रियात्मक शिक्षण-विधियों का प्रयोग किया जाता है। उनमें से एक विचार-विमर्श या वाद-विवाद विधि हैं। यह शिक्षण की वह पद्धति है जिसमें बालक तथा शिक्षक मिल-जुलकर किसी प्रकरण, प्रश्न या समस्या के सम्बन्ध में स्वतन्त्रतापूर्वक सामूहिक वातावरण में विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। इस पद्धति के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए नीचे कुछ परिभाषाएँ दी जा रही हैं-
1. रिस्क के अनुसार, “विचार-विमर्श का अर्थ है-अध्ययन की जाने वाली समस्या का प्रकरण में निहित सम्बन्धों का विचारशील विवेचन।”
2. जेम्स एम. ली के अनुसार, “विचार-विमर्श एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र सहयोगी ढंग से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं।””
3. सिम्पसन व योकम के अनुसार, “विचार-विमर्श बातचीत का एक विशिष्ट स्वरूप है। इसमें सामान्य बातचीत की अपेक्षा अधिक विस्तृत एवं विवेकयुक्त विचारों का आदान-प्रदान होता है। सामान्यतः विचार-विमर्श में महत्त्वपूर्ण विचारों तथा समस्याओं को सम्मिलित किया जाता है।”
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ बी.एड नोट्स
प्रश्न h (vii) वाद-विवाद विधि के प्रकार बताइए।
उत्तर- वाद-विवाद विधि के प्रकार निम्नलिखित हैं-
1. सार्वजनिक वाद-
विवाद- इसमें जन-साधारण को प्रभावित करने वाली समस्याओं पर विचार-विमर्श किया जाता है। इनका आयोजन निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है-
(i) जन-साधारण के मनोरंजन हेतु ।
(ii) सूचनाओं तथा तथ्यों को प्रदान करने के लिए।
(iii) सामाजिक मूल्यों के निर्धारण के लिए।
इस प्रकार के वाद-विवाद दूरदर्शन पर प्रायः आते रहते हैं। इनके प्रमुख विषय होते हैं- बेरोजगारी की समस्या, महँगाई की समस्या आदि।
2. शैक्षिक वाद-विवाद-
इस प्रकार के वाद-विवादों द्वारा छात्रों की सूचनाओं तथा तथ्यों को बोधगम्य कराया जाता है। ये वाद-विवाद निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आयोजित किये जाते हैं-
(i) समस्या का समाधान खोजने के लिए।
(ii) सिद्धान्तों तथा अवधारणाओं को बोधगम्य बनाने हेतु ।
(iii) सूचनाओं तथा तथ्यों को प्रदान करने के लिए।
सामूहिक वाद-विवाद में निम्नलिखित चार प्रकार की भूमिकाएँ निभानी पड़ती हैं-
1. अनुदेशक-
अनुदेशक वाद-विवाद की सम्पूर्ण व्यवस्था करता है। वह इसका पूर्वाभ्यास भी कराता है।
2. अध्यक्ष –
अध्यक्ष की भूमिका वाद-विवाद के समय होती है। वह वाद-विवाद का संचालन करता है। उसको प्रकरण के सम्बन्ध में विशेषज्ञ होना चाहिए।
3. समूह के सदस्य –
इनकी संख्या 4 से 10 तक होती है। ये सदस्य अर्द्ध-गोलाकार स्थिति में अपना स्थान ग्रहण करते हैं। इनके मध्य में अध्यक्ष का स्थान होता है। ये सदस्य प्रकरण के विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिक्रिया करते हैं।
–
4. श्रोतागण — श्रोतागण वाद-विवाद की समाप्ति पर प्रश्न पूछते हैं और अपना दृष्टिकोण भी प्रस्तुत
करते हैं। सदस्यगण उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अन्त में, अध्यक्ष वाद-विवाद के निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है।
प्रश्न h (viii) उदाहरण विधि से आप क्या समझते हैं?
उत्तर-उदाहरण बालक की विचार-शक्ति एवं कल्पना को जाग्रत कर उसके मानसिक विकास के प्रति सहायक होते हैं। उदाहरणों द्वारा अमूर्त विषय को मूर्त बनाया जाता है। इसके द्वारा बालकों के मस्तिष्क पर ज्ञान की अमिट छाप पड़ जाती है। वह विषय के विविध पक्षों का पारस्परिक सम्बन्ध समझने में असमर्थ होता है। पिनसेण्ट के मतानुसार, “अच्छे उदाहरण दुरूह कथन को सजीव एवं सरल बना देते हैं।” तात्पर्य यह है कि उदाहरण विषय की क्लिष्टता को कम करते हैं। इनमें बालक के प्रत्यक्ष अनुभवों से सम्बन्ध होने के कारण विषय सरल तथा बोधगम्य बन जाता है। आमतौर से जब हम कोई गूढ़ बात कहते हैं तो उसे स्पष्ट बनाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। शिक्षा में उदाहरणों का प्रयोग करना एक कला है। विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले विषयों के शिक्षण में इनका प्रयोग आवश्यक होता है। संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि पाठ्य-वस्तु की स्पष्टता, रोचकता, बोधगम्यता एवं मूर्तता की दृष्टि से उदाहरणों का प्रयोग बड़ा महत्त्वपूर्ण है।
नवीन बी. एंड. द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) : तृतीय प्रश्न-पत्र : ज्ञान व पाठ्यक्रम (303)
प्रश्न h (ix) समस्या-आधारित पाठ्यक्रम क्या है? इसके गुण-दोष बताइए।
उत्तर- आवश्यकता -आधारित पाठ्यक्रम की बहुत अधिक कमियों के कारण उसे अपनाने में बहुत कम रुचि दिखलाई गई। इन कमियों को दूर करने के उद्देश्य से बालकों की समस्याओं को नियन्त्रित करने की योजना बनाई गई। इस योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित छात्रों द्वारा अनुभूत समस्याओं को नियन्त्रित करके, उसके आधार पर पाठ्यक्रम को नियोजित करने के प्रयास किये जाते. हैं। इसीलिए इंसे नियन्त्रित समस्या आधारित पाठ्यक्रम भी कहा जाता है।
विशेषताएँ- इस प्रकार के पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं-
(1) इसमें कोई निर्धारित अन्तर्वस्तु न होने के कारण शिक्षक स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य कर सकता है
(2) इस पाठ्यक्रम के द्वारा व्यापक तथा मूलभूत लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है
(3) इस पाठ्यक्रम में वास्तविक निर्देशन प्रदान करना सम्भव होता है
(4) इस पाठ्यक्रम में अनावश्यक विषय-वस्तु को हटाया जा सकता है।
(5) इस पाठ्यक्रम में अधिगम स्वाभाविक ढंग से होता है।
(6) इस पाठ्यक्रम में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं
(7) इस पाठ्यक्रम में आधुनिकतम कार्य विधियाँ अपनाई जा सकती हैं।
सीमाएँ—इस पाठ्यक्रम की प्रमुख सीमाएँ निम्न प्रकार हैं-
(1) इस पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है।
(2) अधिकांश विद्वान अपरिपक्व बालकों द्वारा अनुभूत समस्याओं को ठोस आधार मानना उपयुक्त नहीं समझते उनके अनुसार यह योजना गाड़ी को घोड़े के सामने रखने जैसी लगती है।
(3) इस योजना के क्रियान्वयन में प्रायः यह देखने में आता है कि क्रियाएँ तो अवश्य अधिक हो जाती हैं, किन्तु वही परम्परागत व विषयगत शिक्षण चलता रहता है।
प्रश्न i (i) उदाहरण विधि के प्रकार बताइए।
उत्तर- उदाहरण मुख्यतः निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं-
(i) शाब्दिक उदाहरण जैसे-दृष्टान्त, कहानी, लोकोक्ति, नीति-श्लोक आदि।
(ii) प्रदर्शनात्मक उदाहरण जैसे—मानचित्र, रेखाचित्र, ग्लोब, मॉडल, चार्ट तथा ग्राफ आदि। शाब्दिक उदाहरण में भाषा का प्रयोग आवश्यक है; अतः वे ही अध्यापक इसका प्रयोग कुशलतापूर्वक कर सकते हैं जिनका भाषा पर अधिकार हो। प्रदर्शनात्मक उदाहरणों के प्रयोग में चित्रकला तथा स्केचिंग आदि की दक्षता अपेक्षित है। दोनों ही प्रकार के उदाहरण बालकों की महत्त्वपूर्ण ज्ञानेन्द्रियों से सम्बन्धित हैं। शाब्दिक उदाहरण में सुनने तथा समझने की क्रिया तथा प्रदर्शनात्मक उदाहरण में देखने तथा समझने की क्रिया अधिक आवश्यक है। इन उदाहरणों के प्रयोग से सुनने तथा देखने की क्रियाओं के बारे में उचित प्रशिक्षण प्राप्त होता है।
उदाहरणों को प्रभावोत्पादक ढंग से प्रयोग करने के निमित्त कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, जो निम्नवत् हैं-
(i) पाठ में उदाहरणों का प्रयोग उचित स्थल पर एवं उचित भाषा में करना चाहिए।
(ii) शाब्दिक उदाहरणों में सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर के शिक्षण सूत्रों का प्रयोग आवश्यक है।
(iii) हमेशा एक ही प्रकार के उदाहरण न दिये जाएँ। उदाहरणों में विविधता लाने का प्रयास करना चाहिए।
(iv) उदाहरणों की सजीवता एवं स्पष्टता पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।
(v) ऐसे उदाहरण जिनके द्वारा व्यक्तिगत आक्षेप की सम्भावना हो, कभी नहीं प्रयुक्त करने चाहिए।
(vi) उदाहरण की भाषा सरल, शुद्ध तथा स्पष्ट होनी चाहिए।
(vii) विषय की व्याख्या करने की दृष्टि से उदाहरणों का उपयुक्त होना परमावश्यक है।
(viii) उदाहरणों को बालक के पूर्ण ज्ञान से सम्बन्धित होना आवश्यक है
(ix) अमूर्त या क्लिष्ट विचारों को रखने के तुरन्त बाद उदाहरण दिये जाने चाहिए जिससे बोधगम्यता बनी रहे।
(x) शाब्दिक तथा प्रदर्शनात्मक उदाहरणों का प्रयोग हेर-फेर के साथ होना आवश्यक है।
प्रश्न i (ii) पाठ्यचर्या विकास को प्रभावित करने वाले तत्व / कारक बताइए।
उत्तर- पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाले घटक निम्नलिखित हैं-
(1) सामाजिक घटक (2) शैक्षिक घटक ।
पाठ्यक्रम का सम्पादन शैक्षिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में किया जाता है। इसलिए शैक्षिक तथा सामाजिक घटक पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटकों का विवेचन निम्न रूप में किया गया है-
(i) शिक्षा व्यवस्था-शिक्षा के इतिहास से यह विदित होता है कि अतीत काल से ही शिक्षा व्यवस्था और पाठ्यक्रम का गहन सम्बन्ध रहा है और एक-दूसरे को प्रभावित करते रहे हैं। पाठ्यक्रम तो प्रायः लचीला तथा परिवर्तनशील रहा है। छोटे बालकों का पाठ्यक्रम अनुभव केन्द्रित रहा है। माध्यमिक स्तर विषय केन्द्रित रहा है। शिक्षा व्यवस्था के बदलने के साथ पाठ्यक्रम का प्रारूप भी बदल जाता है।
(i i) परीक्षा पद्धति-परीक्षा प्रणाली पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है। निबन्धात्मक परीक्षा के पाठ्यक्रम का स्वरूप वस्तुनिष्ठ परीक्षा से बिल्कुल भिन्न होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में पाठ्यवस्तु के सूक्ष्म पाठ्यवस्तु पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं।
छात्रों को अध्ययन हम उनके स्मरण के विकास के लिए करवाते हैं तथा उच्च स्तर के छात्रों को सौंदर्यानुभूति के विकास के लिए करवाते हैं। अतः अधिगम परिस्थितियों को विशिष्ट उद्देश्यों के रूप में समझना आवश्यक होता है।
ब्लूम ने भी अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्णन निम्न तीन प्रकार से किया है— (i) ज्ञानात्मक पक्ष, (ii) भावात्मक पक्ष तथा (iii) क्रियात्मक पक्ष ।
विद्यालयों के शिक्षण विषयों की पाठ्यवस्तु में शब्दावली, तथ्य, नियम, उपाय, साधन, विधियाँ प्रत्यय, सिद्धांत तथा सामान्यीकरण ही होते हैं। विज्ञान की पाठ्यवस्तु में नियम, विधियाँ तथा सिद्धान्त होते हैं। भाषा की पाठ्यवस्तु में शब्दावी, साधन, प्रत्यय, नियम होते हैं। इस प्रकार शिक्षण विषयों की सहायता से ज्ञान, उद्देश्य से मूल्यांकन उद्देश्यों तक की प्राप्ति की जाती है और इस प्रकार ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है। ज्ञानात्मक पक्ष का ज्ञान होने के बाद भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष का ज्ञान भी होता है।
प्रश्न : (iii) ‘पाठ्यक्रम एक उत्पाद है’ इस कथन की व्याख्या कीजिए।
उत्तर- पाठ्यक्रम को एक उत्पाद के रूप में लेने का तात्पर्य इसे उद्देश्य या मूल्यांकन पर आधारित प्रतिमान के रूप में विकसित करने से है। यह प्रतिमान इस बात का ज्ञान कराता है कि सम्पूर्ण अधिगम को इस तथ्य पर परिभाषित किया जाना चाहिए कि उस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद छात्र क्या जानने योग्य बन सकेंगे और इसका आकलन अधिगम उद्देश्यों के रूप में किया जा सकता है। पाठ्यक्रम के इस प्रतिमान का आधार व्यावहारिक मनोविज्ञान है जिसमें शैक्षिक उद्देश्यों पर अधिक बल देते हुए पाठ्यक्रम के प्रारूप को विकसित किया जाता है। उद्देश्यों की प्राप्ति छात्रों के अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के रूप में की जाती है, व्यवहार परिवर्तन का ज्ञान मूल्यांकन से होता है | अतः इसे मूल्यांकन प्रतिमान भी कह सकते हैं।
पाठ्यक्रम को प्रायः ज्ञान को हस्तान्तरित करने के एक ढाँचे के रूप में स्वीकार किया जाता है। सबसे पहले अरस्तू के प्रभाव में पाठ्यक्रम के सिद्धान्त को व्यवहार में लाया गया। उन्होंने ज्ञान को तीन अनुशासनों में बाँटा था-
सैद्धान्तिक – व्यावहारिक – उत्पादक
पाठ्यवस्तु – प्रक्रिया – उत्पाद
बी0 एस0 ब्लूम (1962) ने पाठ्यक्रम को एक उत्पाद की दृष्टि से देखते हुए व शिक्षा में सुधार हेत शिक्षण व परीक्षण की क्रियाओं को उद्देश्य केन्द्रित बनाने पर बल दिया तथा कहा कि शिक्षण में जिन उद्देश्यों को महत्त्व दिया जाये, उन्हीं उद्देश्यों के लिए परीक्षण भी किया जाए। इस दृष्टि में पाठ्यक्रम निर्माण हेतु निम्नांकित सोपानों का अनुसरण किया जाता है-
(i) शिक्षण उद्देश्यों का प्रतिपादन, (ii) इन उद्देश्यों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण, (iii) उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सीखने के अनुभवों का सृजन, (iv) बालकों में होने वाले व्यवहार परिवर्तनों का मूल्यांकन ।
प्रश्न i (iv) पाठ्यक्रम एक प्रक्रिया है।
उत्तर- पाठ्यक्रम का प्रक्रिया प्रतिमान-
पाठ्यक्रम के प्रक्रिया प्रतिमान में प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें उद्देश्यों को परिभाषित नहीं किया जाता है बल्कि पाठ्यक्रम के प्रारूप को विकसित करने में पाठ्यवस्तु की सहायता से मानवीय गुणों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए इस प्रकार के पाठ्यक्रम को मानववादी पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। चूँकि इसमें प्रक्रिया को महत्त्व दिया जाता है तथा शिक्षा-प्रक्रिया शिक्षक द्वारा ही सम्पादित की जाती है। अतः इस प्रतिमान में शिक्षक की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है।
पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रतिमान व्यवहार मनोविज्ञान पर आधारित होता है जबकि ‘प्रक्रिया प्रतिमान’ का प्रारूप ‘मानव व्यवस्था सिद्धान्त’ पर आधारित होता है। ‘मानव व्यवस्था’ में परिवर्तन के साथ-साथ शिक्षा का पाठ्यक्रम भी बदलता रहता है। मानव व्यवस्था का परम्परागत सिद्धान्त कार्य केन्द्रित है तथा सम्बन्ध सिद्धान्त सम्बन्ध केन्द्रित है। मानव व्यवस्था का आधुनिक सिद्धान्त कार्य एवं सम्बन्ध केन्द्रित है।
पाठ्यक्रम का प्रक्रिया प्रतिमान यह प्रकल्पित करता है कि विषय-वस्तु व अधिगम क्रियाओं का एक आन्तरिक मूल्य है और वे केवल अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन नहीं है और कि व्यावहारिक उद्देश्यों को त्रिआयामी संदर्भों में व्यक्त करना चाहिए। स्टेनहाउस के अनुसार शिक्षा की चार आधारभूत प्रक्रियाएँ हैं— (i) प्रशिक्षण (कौशल अर्जन), (ii) अनुदेशन (सूचना अर्जन), (iii) प्रारंभीकरण समाजीकरण व सामाजिक मानकों व मूल्यों के परिचित होने तक, (iv) आगमन (चिन्तन व समस्या समाधान) ।
पाठ्यक्रम के प्रक्रिया आधारित प्रतिमान को निम्न दो प्रतिमानों जिन्हें सेलर व एलैक्जेण्डर ने प्रतिपादित किया है, के अनुसार समझा जा सकता है। इसे निम्नांकित चित्र द्वारा समझाया जा सकता है-
प्रक्रिया प्रतिमान
पाठ्यक्रम विचार
मूल्यांकन —- विषय विधि
परिणाम
प्रश्न i (v) पाठ्यक्रम निर्माण हेतु शैक्षिक उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर – वर्तमान समय में पाठ्यक्रम की प्रभावोत्पादकता की दृष्टि से इसके उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इसके पश्चात् ही उपयुक्त शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्धारण हो पाता है व इसे क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करके इसकी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है। अतः पाठ्यक्रम का निर्माण करने से पूर्व सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को उन लक्ष्यों या उद्देश्यों के बारे में निश्चित जानकारी होनी चाहिए जिसकी प्राप्ति वे पाठ्यक्रम के द्वारा करना चाहते हैं।
कुछ विद्वानों का यह मानना है कि लक्ष्यों/उद्देश्यों के निर्धारण का कार्य समाज के शिक्षा नीति- निर्धारकों का है न कि पाठ्यक्रम निर्माताओं का। परन्तु उनके द्वारा बनाये गये लक्ष्यों से शिक्षण कार्य में प्रायः स्पष्टता का अभव होता है। अतः सामान्य लक्ष्यों को कक्षा में व्यावहारिक उद्देश्यों के रूप में परिवर्तित करना पाठ्यक्रम की संरचना का सबसे कठिन पक्ष होता है। अतः शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण का दायित्व भी पाठ्यक्रम निर्माताओं का ही होता है। अतः शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण से पूर्व इनकी कुछ विशेषताओं पर दृष्टि डालनी आवश्यक है-
(a) शैक्षिक उद्देश्य किसी अन्तिम लक्ष्य हेतु की जाने वाली क्रिया को गति प्रदान करते हैं।
(b) इसके अन्तर्गत किसी क्रिया द्वारा नियोजित परिवर्तन लाया जाता है।
(c) इनकी सहायता से क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है
अतः शैक्षिक उद्देश्यों से तात्पर्य छात्रों में होने वाले इस परिवर्तन से है जो शैक्षिक क्रियाओं द्वारा नियोजित रूप में लाया जाता है। बी0एस0ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य को निम्न रूप में परिभाषित करते हुए इसके अर्थ को अधिक स्पष्ट किया है—
“शैक्षिक उद्देश्यों की सहायता से केवल पाठ्यक्रम की ही रचना तथा अनुदेशन के लिए निर्देशन ही नहीं दिया जाता बल्कि ये मूल्यांकन की प्रविधियों के विशिष्टीकरण में भी सहायक होते हैं।”
प्रश्न i (vi) शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के मापदण्ड का वर्णन कीजिए।
उत्तर-किसी समाज के शिक्षा के उद्देश्य, मुख्य रूप से उसके व्यक्तियों के जीवन दर्शन पर आधारित होते हैं। समाज की विशेष संरचना, उसकी सभ्यता एवं संस्कृति तथा धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति का भी शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव पड़ता है। मानव की स्वयं की प्रकृति भी शिक्षा के स्वरूप को प्रभावित करती है। शिक्षा युग के प्रभाव से भी अछूत नहीं रह सकती है। वर्तमान युग विज्ञान का युग है। अतः इसका भी शिक्षा के उद्देश्यों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। निष्कर्ष यह है कि शिक्षा के उद्देश्यों का मनुष्य के जीवन और समाज के आदर्शों से गहरा सम्बन्ध होता है। इसीलिए शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में इनका सर्वाधिक महत्त्व होना चाहिए।
डी.के. ह्वीलर ने अपनी पुस्तक ‘करीक्युलम प्रोसेस’ में आधुनिकतम स्थिति और दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के कुछ महत्त्वपूर्ण मानदण्ड प्रस्तावित किये हैं। व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मानदण्ड के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को पाँच दृष्टियों से सार्थक होना चाहिए-
(i) मानवीय अधिकारों से तादात्म्य, (ii) लोकतान्त्रिक दृष्टि से अनुकूलित, (iii) सामाजिक दृष्टि से सार्थक, (iv) वैयक्तिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रवृत्त, (v) सन्तुलन ।
प्रश्न ; (vii) शैक्षिक उद्देश्य में सामाजिक सार्थकता का वर्णन कीजिए।
उत्तर- शैक्षिक उद्देश्य, लोकतान्त्रिक दृष्टि से अनुकूलित होने चाहिए किन्तु इससे ही उनकी सामाजिक सार्थकता सिद्ध नहीं होती है। परम्परागत एवं स्थिर समाज में शिक्षा के उद्देश्य वर्तमान मूल्यों को परिलक्षित करने के साथ-साथ भविष्य के लिए भी वैध हो सकते हैं, किन्तु परिवर्तनशील समाज में पूर्व-निर्धारित शैक्षिक लक्ष्यों का वर्तमान समय में सार्थक होना आवश्यक नहीं होता है। हो सकता है। कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास कर रही हो जो वास्तव में वर्तमान में विद्यमान ही नहीं है और कुछ अन्य नवीन आवश्यकताएँ उत्पन्न हो गई हों जिनकी पूर्ति शिक्षा के द्वारा नहीं हो पा रही हो। अतः यह आवश्यक है कि शैक्षिक उद्देश्यों की वर्तमान सार्थकता के साथ- साथ उनमें भावी आवश्यकताओं के पूर्वाभास का भी समावेश किया जाता रहना चाहिए।
पाठ्यक्रम के सतत् संशोधन एवं संवर्द्धन के द्वारा बालकों द्वारा प्राप्त किये जा रहे ज्ञान की के बारे में आश्वस्त तो हुआ जा सकता है किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। वर्तमान समयानुकूलता समाज में परिवर्तन की गति इतनी अधिक तीव्र है कि दो पीढ़ियों में तो बहुत अधिक अन्तर आ ही जाता है, एक ही पीढ़ी के विभिन्न चरणों में कई नवीन परिवर्तनों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वह शिक्षा जो वर्तमान शिक्षक को तैयार करने का साधन थी, अब सम्भवतः उसके द्वारा पढ़ाये जाने वाले बालकों के लिए प्रभावी नहीं हो पा रही है।
प्रश्न i (viii) शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में संतुलन की व्याख्या कीजिए।
उत्तर-सन्तुलन से तात्पर्य शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण करते समय पूर्ण-वर्णित चारों बिन्दुओं पर समुचित बल प्रदान करना है अर्थात् किसी एक बिन्दु पर आवश्यकता से अधिक बल नहीं दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, विगत कुछ वर्षों से यह देखने में आ रहा है कि शिक्षा में सूचनात्मक ज्ञान पर बहुत अधिक तथा एकांगी भाव से बल दिया जा रहा है जो कि त्रुटिपूर्ण है। शैक्षिक उद्देश्यों की किसी भी सूची को तभी सन्तोषप्रद कहा जा सकता है जब वह सभी पक्षों की दृष्टि से सन्तुलित हो । अतः पाठ्यक्रम निर्माताओं को शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में सभी आवश्यक पक्षों को ध्यान में रखते हुए उनमें सन्तुलन बनाये रखने का प्रयास करना चाहिए।
प्रश्न i (ix) शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्धारण में ब्लूम के वर्गीकरण के महत्त्व को बताइए।
उत्तर-यद्यपि पाठ्यक्रम के क्षेत्र में सम्बन्धित सभी व्यक्ति ब्लूम एवं उसके सहयोगियों द्वारा प्रस्तावित शैक्षिक उद्देश्यों के सूक्ष्म वर्गीकरण से पूर्णतः सहमत नहीं हैं, किन्तु वे सभी लोग निश्चित एवं स्पष्ट उद्देश्यों की अनिवार्यता को स्वीकार करते हैं। इसी दृष्टि से इस वर्गीकरण की उपयोगिता असंदिग्ध है। पाठ्यक्रम नियोजन की दृष्टि से इस वर्गीकरण के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं-
(i) यह वर्गीकरण ‘सरल से जटिल की ओर’ के सिद्धान्त पर आधारित है। इसलिए यह प्रणाली उस स्तर का समुचित ज्ञान प्राप्त करने में बहुत सहायक है जिस पर कोई सीखने वाला कार्य कर रहा होता है।
(ii) सीखने वाले के स्तर का सही ज्ञान होने पर मूल्यांकन की प्रविधियाँ, उपकरणों आदि को निश्चित करने तथा उन्हें तैयार करने में भी सुविधा होती है। इसके साथ ही उनका वर्गीकरण भी सरलता एवं स्पष्टता से किया जा सकता है। इस प्रकार इससे मूल्यांकन को उद्देश्य-केन्द्रित बनाने में सहायता होती है।
(iii) इस वर्गीकरण की सहायता से मूल्यांकन विधियों की वैधता की जाँच भी सरलता से की जा सकती है।
(iv) तर्क-आधारित होने के कारण, इस वर्गीकरण से अध्ययन सामग्री तथा शिक्षण-अधिगम स्थितियों के क्रमिक नियोजन में बहुत सहायता मिलती है।
(v) इस वर्गीकरण से उचित परीक्षा-स्थितियों के चयन में भी सुविधा होती है।
(vi) इस वर्गीकरण में शिक्षण एवं मूल्यांकन दोनों के समस्त पक्षों पर समुचित ध्यान देने के कारण विद्यार्थियों के सर्वांगीण एवं सन्तुलित विकास के सम्बन्ध में निश्चित हुआ जा सकता है।
(vii) इस वर्गीकरण से पाठ्य-पुस्तकों तथा अन्य पाठ्य-सामग्री के निर्माण, विश्लेषण, मूल्यांकन, संशोधन एवं संवर्द्धन आदि में बहुत अधिक सुविधा रहती है।
प्रश्न i (x) पाठ्यचर्या के मूल्यांकन के स्तर बताइए।
उत्तर- पाठ्यचर्या के मूल्यांकन के तीन प्रमुख स्तर निम्नलिखित हैं-
(i) उद्देश्य, (ii) गतिविधियाँ, (iii) मूल्यांकन ।
अर्थात् सबसे पहले उद्देश्य बनायें, फिर उससे सम्बन्धित गतिविधियाँ करवाई जाती हैं तत्पश्चात पाठ्यचर्या का मूल्यांकन किया जायेगा। किसी भी पाठ्यचर्या के मूल्यांकन की कुछ विशेषतायें होती हैं, जो कि निम्नलिखित हैं-
(i) पाठ्यचर्या के उद्देश्य के साथ उचित संगति स्थापित करना, (ii) पर्याप्त निदानात्मक मूल्यांकन, (iii) व्यापकता, (iv) वैधता, (v) निरन्तरता।
पाठ्यचर्या विकास करने व उन्हें लागू करने हेतु विभिन्न स्तरों पर वांछित सभी प्रमाण एकत्र करने हेतु अनेक तकनीकों व साधनों की आवश्यकता होती है। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि मूल्यांकन दो प्रकार का होता है- (a) छात्र मूल्यांकन, (b) पाठ्यचर्या मूल्यांकन ।
प्रश्न i (xi) अधिगम केन्द्रित पाठ्यक्रम क्या है? उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए।
उत्तर- पाठ्यक्रम नियोजकों के लिए अधिगम प्रक्रिया के सैद्धान्तिक पक्ष की अपेक्षा इसका व्यावहारिक एवं शैक्षिक पक्ष अधिक महत्त्वपूर्ण है, किन्तु मनोविज्ञान के विकास के साथ ही अधिगम मनोविज्ञान भी बहुत अधिक विकसित हो चुका है। अधिगम के क्षेत्र में निरन्तर अनुसन्धान एवं नये प्रयोग किये जा रहे हैं। अतः अधिगम के विभिन्न नये सिद्धान्त प्रकाश में आये हैं। सैद्धान्तिक पक्ष के गहरे ज्ञान की विवशता न होने के कारण यहाँ उनका विस्तृत विवेचन करना अभीष्ट नहीं लगता, परन्तु एक शैक्षिक कार्यक्रम के नियोजनकर्त्ता को उनके सामान्य ज्ञान का अभाव कठिनाई भी पैदा करता है। अतः यहाँ पर उनकी संक्षिप्त चर्चा करना समीचीन प्रतीत होता है।
अधिगम —अधिगम अथवा सीखने का अर्थ है कुछ क्रियाओं को एक साथ सम्पन्न करके “सम्पूर्ण रूप से किसी अनुभव को प्राप्त करना। यह सम्पूर्ण अनुभव अनेक क्रियाओं एवं उपक्रियाओं से प्राप्त अनुभवों से बनता है। अधिगम के सम्पूर्ण रूप का विश्लेषण निम्नलिखित बिन्दुओं के रूप में किया जा सकता है-
(i) उद्देश्य – प्रत्येक अधिगम के पीछे कोई-न-कोई उद्देश्य होता है।
(ii) अभिप्रेरणा- मनुष्य जो भी कार्य करता है, वह किसी-न-किसी अभिप्रेरणा से संचालित होता है। अभिप्रेरणा ही उद्देश्य की ओर ले जाने का कार्य करती है।
(iii) उत्तेजना या उद्दीपन-उत्तेजना क्रिया के सम्पादन में सहायक होती है। बाह्य वातावरण, साधनं तथ्य आदि कार्य करने के प्रति उत्तेजना उत्पन्न करते हैं।
(iv) प्रत्यक्षीकरण- प्रत्यक्षीकरण पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना की व्याख्या करता है। क्रिया की सम्पन्नता के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक होता है।
(v) पुनर्बलन- पुनर्बलन के अन्तर्गत वे सभी क्रियाएँ एवं तथ्य आ जाते हैं जिनके वशीभूत होकर छात्र को क्रियाएँ करनी पड़ती हैं। अध्यापक का आदेश, स्वयं की इच्छा तथा सामाजिक मर्यादा आदि के प्रभाव पुनर्बलन के अन्तर्गत आते हैं।
(vi) संगठन – पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में सम्बन्ध स्थापित करने के लिए अधिगम क्रिया के विभिन्न अंगों को संगठित करना होता है।
नहीन) बी.एड. द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर): तृतीय प्रश्न-पत्र : ज्ञान व पाठ्यक्रम (303)
प्रश्न i (xii) एक अच्छे पाठ्यक्रम की क्या विशेषताएँ होनी चाहिए?
उत्तर- एक आदर्श पाठ्यक्रम में निम्न गुण पाये जाते हैं-
1. प्रेरणा-
नागरिकशास्त्र के अच्छे पाठ्यक्रम छात्रों को प्रेरणा करने वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे छात्र स्वयं पाठ्यक्रम की क्रियाओं को सीखने हेतु प्रेरित हों।
2. लचीलापन –
एक अच्छे पाठ्यक्रम में लचीलेपन का गुण होना जरूरी है। इसके अभाव में छात्रों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं के अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना सम्भव नहीं होता है। अतः पाठ्यक्रम को इतना लचीला होना चाहिए कि उसमें आवश्यकतानुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सके।
3. रुचि के अनुकूल –
एक अच्छे पाठ्यक्रम को छात्रों की रुचि के अनुकूल होना चाहिए। उसमें छात्रों की रुचियों को ध्यान में रखना चाहिए और ऐसी क्रियाओं को सम्मिलित करना चाहिए जिनमें छात्रों की रुचि हो क्योंकि छात्रों की रुचि के अनुकूल पाठ्यक्रम न होने पर उसके अध्ययन में छात्रों को कोई रुचि न होगी और वह पाठ्यक्रम उनके लिए निरर्थक साबित होगा ।
4. व्यापकता –
एक अच्छे पाठ्यक्रम को व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उसमें संकुचित दृष्टिकोण-दलगत राजनीति, विशेष वर्ग हेतु अपमानजनक बातें आदि नहीं होनी चाहिए। पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों में वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना का विकास करते हुए व्यापक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए।
5. क्रियाशीलता –
एक अच्छे पाठ्यक्रम में क्रियाशीलता का गुण होना चाहिए। पाठ्यक्रम छात्रों को केवल निष्क्रिय श्रोता न बनाए वरन् उन्हें क्रियाशील बनाए। छात्र पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण क्रियाओं को स्वयं करके सीखें। इससे छात्रों की क्रियाशीलता बनी रहेगी।
6. जनतान्त्रिक आदर्श –
भारत एक जनतान्त्रिक राष्ट्र है। अतः भारत में नागरिकशास्त्र के एक अच्छे पाठ्यक्रम में जनतान्त्रिक आदर्शों को आधार बनाना चाहिए क्योंकि राष्ट्र की सफलता जनतन्त्र की सफलता पर निर्भर है और जनतन्त्र की सफलता उसके नागरिकों में जनतान्त्रिक आदर्शों के गुणों के विकसित होने पर निर्भर है।
7. उपयोगिता-
एक अच्छा पाठ्यक्रम हम उसी पाठ्यक्रम को कह सकते हैं जो छात्रों हेतु उपयोगी हो। छात्रों को जीवन में काम आने वाली बातें, संदर्भित तत्त्वों का ज्ञान करके वाला पाठ्यक्रम ही अच्छा पाठ्यक्रम माना जाता है। जिस पाठ्यक्रम में जीवनोपयोगी बातों का समावेश नहीं होता, ऐसे पाठ्यक्रम को सीखने में छात्र रुचि नहीं लेते हैं।
प्रश्न j (i) पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में उद्देश्यों का निरूपण क्यों आवश्यक है? पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया करते समय किन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को सूचीबद्ध करना चाहिए?
उत्तर—पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में उद्देश्यों का निरूपण इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे पढ़ने के पश्चात् छात्रों को निम्नलिखित तथ्यों का ज्ञान होगा-
* पाठ्यचर्या विकास के विविध उपागमों के विषय में जानकारी प्राप्त होगी।
* पाठ्यचर्या नियोजन के मॉडल की चर्चा कर सकेंगे।
* पाठ्यचर्या विकास की सीमाओं के विषय में जान सकेंगे
* विभिन्न शिक्षण अनुभवों व उद्देश्यों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
* पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया में मूल्यांकन के महत्त्व की चर्चा कर सकेंगे।
* पाठ्यचर्या से सम्बन्धित प्रमुख मुद्दों तथा प्रवृत्तियों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
प्रश्न j (ii) शैक्षिक कार्यक्रमों में अधिकाधिक सहभागिता हेतु शिक्षक के गुणों का वर्णन कीजिए।
उत्तर-कार्यरत शिक्षकों को पाठ्यक्रम नियोजन एवं अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों में समुचित भागीदारी प्रदान करने हेतु उन्हें भी उसके लिए सक्षम बनने का प्रयास करना चाहिए जिससे उनकी पात्रता में कोई सन्देह न रहे। सेलर एवं अलेक्जेन्डर ने शिक्षक में निम्नांकित गुणों की अपेक्षा की है-
(i) पहल, आत्मप्रेरणा एवं साहसिक कार्य करने की भावना ।
(ii) अवसरों के प्रति प्रत्युत्तरात्मक भावना, अध्ययन, तुलना तथा स्व-मूल्यांकन के लिए उद्यतता।
(iii) शैक्षिक विषयों में नवीन प्रवृत्तियों के प्रति सजगता ।
(iv) स्वतन्त्र रूप से तथा साथ मिलकर कार्य करने की क्षमता, धैर्य एवं सहकर्मियों के सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार।
(v) पर्याप्त आत्म-नियन्त्रण, दूसरों के साथ मिलकर गम्भीर कार्य कर सकने का कौशल।
(vi) अपने विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों (विशेष रूप से बाल मनोविज्ञान एवं अधिगम मनोविज्ञान) का भी पर्याप्त ज्ञान ।
(vii) स्वस्थ प्रकृति एवं आत्मनिर्देशन के साथ-साथ दूसरों के निर्देशन एवं नियन्त्रण में कार्य कर सकने की क्षमता।
(viii) अच्छा मानसिक स्वास्थ्य एवं भावात्मक स्थिरता ।
प्रश्न j (iii) शिक्षक एवं पाठ्यक्रम।
उत्तर- पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अभिकरण शिक्षक है। अतः पाठ्यक्रम नियोजन कार्य में इससे सम्बन्धित अन्य घटकों की भागीदारी एवं उनकी सीमाओं के बारे में विवाद हो सकता है किन्तु पाठ्यक्रम विकास के सभी चरणों एवं सभी स्तरों पर शिक्षक की भागीदारी असंदिग्ध एवं सर्वमान्य है। शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण, अन्तर्वस्तु के चयन एवं संगठन, शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों के चयन, सहायक सामग्री के चयन, मूल्यांकन विधियों के निर्धारण आदि सभी सोपानों में शिक्षक की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्तिगत रूप से छात्रों एवं उनकी समस्याओं को समझने, उन पर ध्यान देने तथा तदनुकूल निर्णय लेने का कार्य प्रभावी रूप से शिक्षक ही कर सकता है। अतः पाठ्यक्रम विकास में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भागीदारी शिक्षक की ही होनी चाहिए। शिक्षक की महत्त्वपूर्ण भागीदारी के प्रमुख आधार निम्न प्रकार हैं-
• शिक्षक उस नाविक के समान होता हैं जो यह भली-भाँति जानता है कि उसे कहाँ जाना है तथा वहाँ पहुँचने के लिए वह अपने मानसिक निर्णय के अनुसार पानी, नाव, पतवार आदि के विषय में बात करने के लिए सदैव तैयार रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षकों में ज्ञान, अनुभव एवं व्यावसायिक उत्तरदायित्व की प्रबल भावना होती है जो पाठ्यक्रम नियोजन में शक्ति का स्रोत सिद्ध होती है।
• शिक्षक का छात्र, विद्यालय तथा उनसे सम्बन्धित सभी पक्षों से भावनात्मक सम्बन्ध होता है। अतः वह विभिन्न शैक्षिक परिस्थितियों के प्रति मात्र बौद्धिक रूप से ही नहीं, बल्कि भावात्मक रूप से भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। पाठ्यक्रम निर्माण की भागीदारी में अपनत्व की वह भावना बहुत महत्त्वपूर्ण होती है क्योंकि यही भावना विद्यालय के पर्यावरण को आवश्यक स्थायित्व एवं व्यवस्था प्रदान करने में सहायक होती है।
पाठ्यक्रम को वास्तविक कार्यात्मक रूप कक्षा में ही प्रदान किया जाता है। अतः निस्सन्देह रूप से इस कार्य में शिक्षक को ही प्रमुख भूमिका निभानी होती है। एक विद्वान के मतानुसार, “पाठ्यक्रम तो उसी समय निर्मित होता है जब शिक्षक और छात्र यह निश्चित करते हैं कि अब हम पढ़ेंगे।” इसी तथ्य को दृष्टिगत करते हुए सेलर एवं अलेक्जेन्डर ने दो प्रकार के पाठ्यक्रम बताये हैं-
(i) नियोजित पाठ्यक्रम, (ii) क्रियान्वित पाठ्यक्रम ।
प्रश्न j (iv) त्रिभाषा सूत्र ।
उत्तर- त्रिभाषा सूत्र में संशोधन-त्रिभाषा सूत्र के सम्बन्ध में आयोग ने लिखा है – यह फार्मूला सन् 1956 ई0 में ‘केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड’ के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और सन् 1961 ई0 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकार किया गया था किन्तु व्यावहारिक रूप में इस फार्मूले को सफलता प्राप्त नहीं हुई है और इसका यह कहकर और विरोध किया जा रहा है कि इसने पाठ्यक्रम को भाषाओं की दृष्टि से बहुत बोझिल बना दिया है। अतः इस सूत्र में संशोधन किया जाना अनिवार्य है। यह संशोधन निम्नलिखित सिद्धान्तों के आधार पर किया जाना चाहिए-
–
1. संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी मातृभाषा के बाद महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करे।
2. छात्रों के लिए अंग्रेजी का ज्ञान उपयोगी है।
3. तीन भाषाओं की शिक्षा प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्तर निम्न स्तर माध्यमिक है।
4. हिन्दी या अंग्रेजी की शिक्षा उस समय आरम्भ की जाय जब इसके लिए प्रेरणा या आवश्यकता का अनुभव किया जाये।
5. किसी भी स्तर पर चार भाषाओं के अध्ययन को अनिवार्य न बनाया जाय।
‘आयोग’ ने उपर्युक्त सिद्धान्तों के आधार पर त्रिभाषा सूत्र का संशोधित रूप इस प्रकार प्रस्तावित किया है-
(i) मातृभाषा या क्षेत्रीय अथवा प्रादेशिक भाषा ।
(ii) संघ की राजभाषा या सह-राजभाषा। (जिस समय तक वह है)
प्रश्न j (v) राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन एवं विद्यालय शिक्षामण्डल परिषद के कार्य बताइए।
उत्तर-
(i) विद्यालयीय शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए पाठ्यचर्या क्षेत्र में अपेक्षित उपलब्धि स्तर तय करना ।
(ii) बालकेन्द्रित, गतिविधि उन्मुखी और दक्षता आधारित अध्ययन-अध्यापन सामग्री के लिए
अवधारणात्मक सामग्री और उसके नमूने तैयार करवाना।
(iii) संज्ञानात्मक और सह-संज्ञानात्मक अधिगम प्रतिफलों के पब्लिक आकलन के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का निर्माण करवाना और उन्हें राज्यस्तरीय एजेन्सियों को उपलब्ध करवाना।
(iv) मुख्य संसाधन व्यक्तियों के लिए प्रबोधन कार्यक्रमों का संचालन करना ।
(v) विभिन्न बोर्डों के लिए प्रश्न-पत्र निर्माताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना । (vi) अभिलेख रखने और परिणामों की रिपोर्ट देने के लिए किसी संचार तन्त्र की कल्पना करना तथा उसके विषय में परामर्श देना ।
(vii) अधिगम प्रतिफलों के मूल्यांकन के लिए बेहतर तरीकों और साधनों की खोज हेतु शोध करवाना। (viii) सेन्सस जैसे आँकड़े प्राप्त करने के लिए उपलब्धि सर्वेक्षण करना ।
(ix) सूचना प्रसार करना।
प्रश्न j (vi) अन्तर्वस्तु के मापदण्ड बताइए ।
उत्तर-किसी पाठ्यक्रम के लिए अन्तर्वस्तु के चयन का आधार क्या हो, इसके निर्देशक सिद्धांत क्या हों तथा उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाये, इस सम्बन्ध में सर्वमान्य दृष्टिकोण यद्यपि अभी तक नहीं बन सका है, किन्तु इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण प्रयास अवश्य किये गये हैं। यहाँ पर दो प्रमुख प्रयासों की चर्चा की जा रही है-
1. स्टेनली निस्बत द्वारा प्रस्तावित मानदण्ड – शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निस्बत द्वारा किया गया है। इसने दो वर्गों में 12 उद्देश्य निर्धारित किये हैं जिनमें वह सभी पक्षों को समाहित किया हुआ मानता है। निस्बत का सुझाव है कि किसी विषयवस्तु या पाठ्य-सहभागी क्रिया को किसी स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने या न करने का निर्णय लेने के लिए उसका इन 12 उद्देश्यों की दृष्टि से परीक्षण कर लेना चाहिए। सुविधा की दृष्टि से निस्बत ने एक तालिका भी तैयार की है। इस तालिका की सहायता से एक दृष्टि में देखा जा सकता है कि कोई विषयवस्तु किसी स्तर विशेष के पाठ्यक्रम में समाविष्ट करने की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं। निस्बत द्वारा निर्धारित उद्देश्य तथा तालिका में उनके लिए संक्षिप्त संकेत इस प्रकार हैं
तालिका
(अ) पर्यावरण समायोजन सम्बन्धी
1. कौशल (कौ.)
2. संस्कृति (सं.)
3. गृह सदस्यता (गृ.स.)
4. व्यवसाय (व्य.)
5. अवकाश (अव.)
6 . सक्रिय नागरिकता (स. ना.)
(ब) व्यक्तिगत विकास
7. शारीरिक विकास (शा.)
8. सौन्दर्य बोधात्मक विकास (सौ.)
9. सामाजिक विकास (सा.)
10. आध्यात्मिक विकास (आध्या.)
11. बौद्धिक विकास (बौ.)
12. नैतिक विकास (नै.)
प्रश्नj (vii) सी. आई.पी.पी. मॉडल की अवधारणा बताइए।
उत्तर- सी.आई.पी.पी. मॉडल 1960 के दशक में डैनियल स्टफलबीम द्वारा बनाया गया था और इसे एक निर्णय-उन्मुख मॉडल माना जाता है जो कार्यक्रम की प्रभावशीलता में सुधार करने या किसी कार्यक्रम के भविष्य की योजना बनाने के लिए सामग्री या वितरण में शक्तियों और सीमाओं की पहचान करने के लिए किसी कार्यक्रम के बारे में व्यवस्थित रूप से जानकारी एकत्र करता है। इस मॉडल के उपयोगकर्ता अक्सर प्रबंधन-उन्मुख मूल्यांकन पर ध्यान केन्द्रित करते हैं, क्योंकि यह ढाँचा मूल्यांकन के चार चरणों को जोड़ता है। किसी कार्यक्रम के चार क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके निरंतर सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। समग्र लक्ष्य या मिशन संदर्भ मूल्यांकन; योजनाएँ और संसाधन (इनपुट मूल्यांकन); गतिविधियाँ या घटक ( प्रक्रिया मूल्यांकन); और परिणाम या उद्देश्य (उत्पाद मूल्यांकन) ।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
(Long Answer Type Questions)
निर्देश: प्रश्न संख्या 2 से 9 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। परीक्षार्थियों को प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल चार प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 71⁄2 अंक निर्धारित हैं। -(4 x 71⁄2 = 30 अंक)
इकाई-1
प्रश्न 2 (i) ज्ञान का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएँ बताइए।
अथवा
(ii) ज्ञान की अन्तर्विषयी अवधारणा में भारतीय एवं पश्चिमी विचारधारा में अन्तर स्पष्ट करें।
अथवा
(iii) ज्ञान से आप क्या समझते हैं? ज्ञान प्राप्ति के विविध स्त्रोतों का वर्णन कीजिए।
अथवा
(iv) ज्ञान के विविध स्वरूप क्या हैं? ज्ञान प्राप्ति के विविध स्त्रोतों का वर्णन कीजिए।
ज्ञानेन्द्रियों से बौद्धिक अनुभव को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के निमित्त बुद्धि का होना परम आवश्यक है। अतः स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष अनुभव, प्रायोगिक कौशल और जानकारी के द्वारा किसी तथ्य, तत्त्व अथवा वस्तु से परिचित होना की ज्ञान है। पृथ्वी पर मनुष्य ही एक मात्र ऐसा चेतन प्राणी है, जो विचार, चिन्तन, मनन, मंथन और अनुभव प्राप्त करने में समर्थ है जिसके आधार पर वह नये तथ्यों व तत्त्वों से अवगत होता है और ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान उत्पत्ति में दो प्रमुख पक्ष होते हैं-ज्ञाता और ज्ञेय। जब मनुष्य वस्तु एवं विचारों अर्थात ज्ञातव्यों से परिचित हो जाता है तो ज्ञान की उत्पत्ति होती है ज्ञान ज्ञाता के ही इर्द-गिर्द घूमती है, अतः ज्ञाता के अभाव में ज्ञान का अस्तित्व सम्भव नहीं है। जब मनुष्य किसी वस्तु अथवा विचार को अनुभूति बोध विश्वास, तर्क और अनुभव के आधार पर स्वीकार कर लेता है तभी ज्ञान का सृजन होता है, इस क्रम के निरन्तर चलते रहने से ज्ञान की वृद्धि होती है और नित्यप्रति ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में नवीन उपलब्धियाँ होती रहती हैं और उसी के साथ-साथ ज्ञान का विस्तार होता है। ज्ञान का विकास निरन्तर होता रहता है। नवीन विचारों, तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर व्यावहारिक शोध का चक्र चलता रहता है, नवीन विषय क्षेत्रों का उदय होता है जो ज्ञान की उत्पत्ति में काफी सहायक होते हैं।
ज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र और प्रकृति काफी विस्तृत है। अतः इसे किसी परिभाषा के अन्तर्गत सीमित नहीं किया जा सकता। ज्ञान जगत असीम और इसका विकास बहुघातीय है, अतः इसके परिमाप को बताना असम्भव तो नहीं परन्तु जटिल अवश्य है। कुछ विद्वानों द्वारा दी गयी ज्ञान की परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं-
एस.आर. रंगनाथन के शब्दों में- “ज्ञान सभ्यता संरक्षित सूचना का समग्र योग होता है।” वेबस्टर्स न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार-“ज्ञान वास्तविक अनुभव व्यावहारिक अनुभव, कार्यकुशलता आदि के द्वारा प्राप्त जानकारी है।”
जे. एस. शेरा के शब्दों में-“ज्ञान बौद्धिक पद्धति द्वारा निस्पादित प्रक्रिया का परिणाम है।”
प्लेटो के शब्दों में- “ज्ञान चिर सत्य है। सत्य की ओर उन्मुख सम्बन्धी उसकी इस अनिवार्य विशेषता से यह सम्भव हो पाता है कि उसके लिये सक्रिय बुद्धि, इन्द्रियानुभव मूल अनुभूति और उसकी चेतना के संदर्भ में ज्ञान और अज्ञान, सत्य और अनुमान के मध्य भेद कर सकते हैं।”
रसेल के शब्दों में- “मस्तिष्क सच्ची अथवा झूठी धारणा निर्मित नहीं करता। मस्तिष्क विश्वास निर्मित करता है। जब विश्वास से सम्बन्धित तथ्य प्राप्त हो जाते हैं तब विश्वास सत्य में परिणित हो जाता है और यदि सम्बन्धित तथ्य प्राप्त नहीं होते जो विश्वास गलत सिद्ध हो जाता है। अतः यह कह सकते हैं कि ज्ञान सत्यता पर आधारित विश्वास है।”
ज्ञान की उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि “वह निश्चित जानकारी अथवा विचार समूह जिसे मनुष्य अर्जित कर सुरक्षित करता है जिससे कि इसे निरंतर दूसरे अन्य जिज्ञासुओं को प्रदान किया जा सके, ज्ञान कहलाता है।’
ज्ञान की विशेषताएँ
ज्ञान की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं-
1. ज्ञान बहुआयामी है जिसमें चिन्तन, अध्ययन और अनुसंधान के द्वारा नवीन ज्ञान और नए विषय क्षेत्रों की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है
2. ज्ञान जगत निरन्तर गतिशील है। निरंतर नए सकल विचारों और विषयों की उत्पत्ति होती रहती है।
3. ज्ञान जगत सतत रूप से विकसित होता रहता है जिसके फलस्वरूप विषयों की निरन्तरता बनी रहती है।
4. ज्ञान जगत अनन्त है। इसमें ज्ञान और अज्ञात सभी ज्ञान समाहित रहता है।
5. ज्ञान जगत अपरिमित होता है। इसमें सत्वों की संख्या को ज्ञात करना सम्भव नहीं है। विचार की उत्पत्ति एक सतत् प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप ज्ञान का परिसीमन सम्भव नहीं है।
उपर्युक्त वर्णित ज्ञान की समस्त विशेषताओं से स्पष्ट है कि वैश्विक स्तर पर ज्ञान एक समान नहीं पाया जाता है। साथ ही इसके आकार, प्रकार और प्रकृति में निरंतर परिवर्तन घटित होता रहता है।
ज्ञान के स्रोत अथवा ज्ञान-प्राप्ति के तरीके
ज्ञान-प्राप्ति के मूल रूप से पाँच स्रोत हैं-
(1) इन्द्रिय अनुभव –
ज्ञान का एक प्रमुख साधन इन्द्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव का प्रत्यक्षीकरण है। मनुष्य की पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा उसे क्रमशः देखकर सुनकर, सूंघकर, स्वाद लेकर तथा स्पर्श करके सांसारिक वस्तुओं के बारे में तरह-तरह का ज्ञान प्रदान करती हैं। ऐसे ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार से मनुष्य ज्ञानेन्द्रियों द्वारा ही संसार की वस्तुओं के सम्पर्क में आता है तो एक प्रकार की संवेदना उत्पन्न होती है, यह सब देना ज्ञानेन्द्रियों को प्राप्त उत्तेजना में ही होती है तथा वस्तु का ज्ञान प्रदान करती है। इसे प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। यह प्रत्यक्षीकरण ही हमें उस वस्तु की जानकारी देता है।
प्रत्यक्षीकरण द्वारा चेतन मन में अवधारणायें उत्पन्न होती हैं जिन पर हमारा ज्ञान निर्भर होता है। इन्द्रिय अनुभव दक्ष ज्ञान-प्राप्ति की इस क्रिया को सभी दार्शनिकों द्वारा ज्ञान-प्राप्ति का मुख्य स्रोत माना गया है। इन्द्रियों द्वारा प्राप्त इस ज्ञान की विश्वसनीयता का आकलन तो किया जा सकता है परन्तु उस ज्ञान की वैधता ज्ञात करना कठिन होता है अर्थात् सत्यता की दृष्टि में कठिनाई आती है।
(2) साक्ष्य –
जब हम दूसरों के अनुभव तथा निरीक्षण पर आधारित ज्ञान को मान्यता देते हैं तो इसे साक्ष्य कहा जाता है, साक्ष्य में व्यक्ति स्वयं निरीक्षण नहीं करता। वह दूसरों के निरीक्षण पर ही तथ्य का ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार साक्ष्य दूसरों के अनुभव पर आधारित ज्ञान है। हम प्रायः अपने जीवन में साक्ष्य का बहुत उपयोग करते हैं। हमने स्वयं बहुत से स्थानों को नहीं देखा है किन्तु जब दूसरे उनका वर्णन करते हैं तो हम उन स्थानों के अस्तित्व में विश्वास करने लगते हैं।
(3) तार्किक चिन्तन-
तार्किक चिन्तन ऐसी मानसिक प्रक्रिया/योग्यता है जिसके बिना कोई भी ज्ञान सम्भव नहीं है। हमारा अधिकांश ज्ञान तर्क पर ही आधारित होता है। हमें अनुभव द्वारा जो संवेदनायें प्राप्त होती हैं उनको तर्क द्वारा संगठित करके ज्ञान का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार यह अनुभव पर काम करता है और हमें ज्ञान में परिवर्तित करता जाता है।
इन्द्रियों से प्राप्त अनुभव के द्वारा हम- रंग, स्वाद तथा गन्ध आदि से सम्बन्धित कुछ संवेदनाएँ प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु जब वस्तुओं में भेद करने का प्रश्न आता है, वहाँ हमें तार्किकता की आवश्यकता होती है जिसमें अमूर्त चिन्तन निहित होता है। अतः ज्ञान का आधार तर्कबुद्धि ही है।
(4) अन्तः प्रज्ञा तथा अन्तः प्रज्ञावाद –
यह भी ज्ञान प्राप्ति का एक मुख्य स्रोत है। यह एक प्रकार का आन्तरिक बोध है जिसमें ज्ञान की स्पष्टता निहित होती है। अन्तः से हमारा तात्पर्य है किसी तथ्य को अपने मन में जानना। इसके लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि इसके अन्तः अचानक ज्ञान के प्रकाश की किरण उत्पन्न होती है जिसे हम ज्ञान की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार के ज्ञान का एकमात्र प्रमाण यह है कि उसकी निश्चितता तथा वैधता में सन्देह नहीं होता तथा हम उस ज्ञान पर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अन्तःप्रज्ञा हमारे अन्दर निहित वह सद्धत क्षमता है जो कभी अचानक ही क्रियाशील होकर हमें आलोकित करती है।
परन्तु इस अन्तःप्रज्ञा के साथ कभी-कभी आत्मनिष्ठता का ऐसा गुढ़ा आबद्ध हो जाता है कि यदि हम इस यथार्थ ज्ञान का साथ मान भी लें तो फिर इस ज्ञान में वस्तुनिष्ठता तथा सार्वजनिकता जैसी चीज नहीं रह जायेगी और हम यह दावा नहीं कर सकेंगे कि कौन-सी प्रतिज्ञप्ति सत्य है और कौन-सी असत्य है।
(5) सत्ता अधिकारिक ज्ञान–
उच्च शिक्षित व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त ज्ञान को सत्ता अधिकारिक ज्ञान की संज्ञा दी जा सकती है। मनोविज्ञान ने अब यह सिद्ध कर दिया है कि मानव समाज में व्यक्तिगत भिन्नताएँ हैं। कुछ मनुष्य अत्यन्त प्रतिभाशाली हैं, जिनकी संख्या कम होती है, वे ही ज्ञान क्षेत्र में नई बातें जोड़ते हैं। इनके द्वारा दिया गया ज्ञान आर्ष या प्रति ज्ञान कहलाता है। शिक्षा का समस्त पाठ्यक्रम इन महान व्यक्तियों द्वारा जीवन के अनुभवों का भार है। अतः इन महान व्यक्तियों को सत्ता माना जाना
चाहिए। परन्तु इस तथ्य में एक यहीं कमी है कि इनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान के प्रति हमें इतना भी अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए कि हमारा ज्ञान संकीर्ण हो जाये व उस ज्ञान से हमारे विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाये।
प्रश्न 2 (ii) ज्ञान वर्गीकरण की प्रचलित प्राचीन पद्धतियों को स्पष्ट कीजिए।
प्राचीन युग से ही ज्ञान का उद्भव एवं विकास क्रमिक रूप से हुआ है। मनुष्य ने ज्ञान के विकास के साथ-साथ इसके व्यवस्थापन की आवश्यकता भी अनुभव की। फलतः भिन्न-भिन्न विद्वानों और दार्शनिकों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से ज्ञान को परखने और जाँचने के साथ-साथ इसके व्यवस्थापन हेतु वर्गीकरण का विचार किया। वर्गीकरण के अंतर्गत वस्तुओं अथवा विचारों को उनके सादृश्य के आधार पर वर्गों या समूहों में व्यवस्थित किया जाता है। वर्गीकरण की प्रक्रिया में कम सामान्य की तरफ से अधिक सामान्य अथवा कम विस्तार से अधिक विस्तार की ओर अग्रसर होते हैं। वस्तुओं और विचारों के गुणों, विशेषताओं अथवा समानताओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न प्रचार धाराओं का वर्गीकरण और श्रेणीबद्धता ही ज्ञान वर्गीकरण है, जिन्हें सुव्यस्थित एवं उपयुक्त शाखाओं में विभक्त करने का प्रयास कुछ प्रमुख पश्चिमी तथा भारतीय दार्शनिकों ने इकाई हजार वर्ष पूर्व किया था। दार्शनिकों ने ज्ञान के वर्गीकरण को अपने विषय क्षेत्र में शामिल किया। ज्ञान से सम्बन्धित समस्याओं को स्पष्ट एवं उनका निदान करने का प्रयास भी दार्शनिकों ने समय-समय पर किया है। प्रत्येक दार्शनिक विचारधारा के दार्शनिकों ने अपने-अपने ढंग से अपने-अपने दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है। ज्ञान वर्गीकरण का यह विभाजन उस समय की संस्कृति और काल के अनुसार था जो तत्कालीन ज्ञान की स्थिति का व्यवस्थापन करता था ।
उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ज्ञान का वर्गीकरण एक जटिल कार्य है, फिर विश्व के कुछ महान् दार्शनिकों ने ज्ञान को वर्गीकृत करने का यथासंभव प्रयत्न किया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-
(1) वैदिककालीन वर्गीकरण-वैदिक, वर्गीकरण पद्धति का वर्णन उपनिषदों में मिलता है। वैदिक काल में सम्पूर्ण ज्ञान का प्रमुख चार वर्गों में वर्गीकरण है जो इस प्रकार हैं-
(अ) धर्म-जिसमें मानव व समाज को एकत्रिकृत करने की क्षमता हो उसे धर्म कहते हैं। मानव समाज में नैतिकता और आध्यात्मिकता के लिये उस ज्ञान को प्रमुख भागों, जैसे-विधि, धर्मशास्त्र, नैतिकशास्त्र / आचारशास्त्र और समाजशास्त्र में विभक्त किया गया।
(ब) अर्थ-समाज के कल्याण तथा भरण-पोषण का ज्ञान अर्थ का क्षेत्र है जिसमें अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास तथा व्यावहारिक विज्ञान आदि सम्मिलित किये गये हैं।
(स) काम-काम के अन्तर्गत मानवीय आवश्यकओं, इच्छाओं, वेद-विहित शारीरिक भोगेच्छाओं, आन्तरिक अभिलाषाएँ आदि की पूर्ति से सम्बन्धित विषय आते हैं
(द) मोक्षं-मोक्ष या निर्वाण के अन्तर्गत मानव की सर्वोत्तम अवस्था अर्थात् मोक्ष (सांसारिक आवागमन-जन्म-मरण) के विषय आते हैं, जिसमें दर्शनशास्त्र, आध्यात्मिक विद्या अथवा पराविद्या, अलौकिक अनुभूतियाँ आदि से सम्बन्धित विषय सम्मिलित हैं।
वस्तुतः समस्त वैदिक साहित्य को इन्हीं आधार पर विषयानुसार बाँटा गया है।
(2) ग्रीक वर्गीकरण पद्धति-
ग्रीक दर्शन शास्त्रियों ने ज्ञान का वर्गीकरण को एक नया आयाम दिया है। यद्यपि प्लेटो के ही समय से ज्ञान वर्गीकरण की पद्धति प्रचलित रही है, जिसमें तर्कशास्त्र, भौतिक तथा आचारशास्त्र सम्मिलित थे, किन्तु आरिस्टोटल ने जिस ज्ञान वर्गीकरण की योजना को संस्थापित किया था, उसे ग्रीक वर्गीकरण पद्धति कहा जाता है। आरिस्टोटल ने ज्ञान को निम्नलिखित तीन वर्गों में वर्गीकृत किया है-
(अ) सैद्धान्तिक दर्शनशास्त्र- इसमें तर्कशास्त्र, ज्ञान मीमांसा, गणित तथा भौतिकी प्रमुख विषय रहे हैं।
(ब) व्यावहारिक दर्शनशास्त्र-इसमें आचार संहिता तथा नैतिक व्यवहार से सम्बन्धित विषय थे।
(स) उत्पादनशील कलाएँ-इसके तहत उपयोगी तथा व्यावहारिक विज्ञान समाहित था।
(3) फ्रांसिस बेकन-फ्रांस बेकन का नाम प्रमुख विचारकों में शामिल है। इन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हासिल की। बेकन ने ज्ञान जगत को निम्नलिखित तीन वर्गों में वर्गीकृत किया है।
(अ ) इतिहास-इतिहास में स्मृति के आधार पर उत्पन्न प्राकृतिक और सामाजिक इतिहास को सम्मिलित किया है।
(ब) काव्यशास्त्र/कविता-ये कल्पनाओं पर आधारित था।
(स) दर्शनशास्त्र- इसमें तर्क के आधार पर उत्पन्न विषय सम्मिलित थे।
बेकन के पश्चात् ज्ञान वर्गीकरण की परम्पराएँ नवीन तर्कपूर्ण पद्धति और प्रचलित परम्पराओं के अनुसार निर्मित की गई।
(4) काण्ट का ज्ञान वर्गीकरण-13वीं सदी का जर्मन दार्शनिक इमैन्युल काण्ट का अर्वाचीन दार्शनिकों में विशिष्ट स्थान है। इन्होंने ज्ञान को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया है- (i) दार्शनिक अवधारणाएँ और (ii) गणितीय अवधारणाएँ।
(5) हीगल की ज्ञान वर्गीकरण पद्धति-
जर्मनी के निवासी हीगल दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। साथ ही इनको एक अच्छा विचारक भी माना जाता है। इन्होंने ज्ञान वर्गीकरण को निम्न तीन समूहों में विभक्त किया था-(i) तर्कशास्त्र, (ii) प्राकृतिक विज्ञान, इसके अंतर्गत मैकेनिक्स, भौतिकी और जीव विज्ञान तथा (iii) मानसिक विज्ञान।
(6) स्पेन्सर की ज्ञान वर्गीकरण योजना-
काम्टे की भाँति हरबर्ट स्पेन्सर भी आधुनिक समाजशास्त्र के विकास में विशेष योगदान दिया । स्पेन्सर ने सामाजिक विज्ञानों का विकास की * वैज्ञानिक परम्परा के अनुसार ही सिद्ध किया है। इस क्रमानुसार तर्कशास्त्र, गणित, रसायनशास्त्र, खगोलशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, जीवविज्ञान मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र के क्रम में विषयों को व्यवस्थित किया गया है। यद्यपि स्पेन्सर की क्रम परम्परा को अधिक उपयुक्त नहीं माना गया है, किन्तु उसने ज्ञान वर्गीकरण के सिद्धान्तों को स्पष्ट किया है जिससे वर्गीकरण योजना को बनाने में एक दिशा मिलती है।
(7) आगस्ट काटे की वर्गीकरण पद्धति-
विश्व प्रसिद्ध समाजशास्त्रीय विचारक एवं आधुनिक समाजशास्त्र के जन्मदाता आगस्ट काम्टे का सामाजिक विज्ञानों को प्राकृतिक विज्ञानों के ‘अनुसार अध्ययन करने के योग्य बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान है। 1830 में काम्टे ने गणित, खगोलशास्त्र, भौतिकी, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान और सामाजिक भौतिकी के अनुसार विषयों का क्रमबद्ध रूप से विकसित किया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि पूर्व विषय वर्ग अगले विषय के अनुप्रयोग से विकसित होता है, अतः पूर्व विषय बाद के विषय पर आधारित होता है।
(8) एम्परे की ज्ञान वर्गीकरण पद्धति-
एण्ड्रे मारले एम्परे ने भी वर्गीकरण की पद्धति विकसित की। इन्होंने ज्ञान वर्गीकरण के अन्तर्गत भौतिकी, अभियांत्रिकी, भूगर्भशास्त्र, खदान, वनस्पतिशास्त्र, कृषि, जीव विज्ञान, पशुपालन आयुर्विज्ञान विषयों को क्रमबद्ध किया है। 19वीं सदी के दार्शनिकों द्वारा निर्मित वर्गीकरण व्यवस्था में इसे उत्तम पद्धति कहा जा सकता है
प्रश्न 2 (iii) उपलब्धता एवं प्रकृति के आधार पर ज्ञान के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए।
उपलब्धता एवं प्रकृति के आधार पर ज्ञान को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है-
1. उपलब्धता के आधार पर-ज्ञान को उपलब्धता के आधार पर निम्नलिखित तीन भागों में बाँटा जा सकता है, जो इस प्रकार है-
(a) वैयक्तिक ज्ञान-
किसी व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में उपलब्ध ज्ञान को वैयक्तिक ज्ञान कहा जाता है। यह ज्ञान किसी व्यक्ति विशेष का अपनी स्वानुभूति से प्राप्त निजी ज्ञान होता है, अतः इसे उस व्यक्ति विशेष के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति विशेष के साथ विचार-विमर्श कर अथवा पत्र-व्यवहार कर व्यक्तिगत अथवा वैयक्तिक ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है।
(b)सामाजिक ज्ञान-
मानव जीवन में सामाजिक ज्ञान का विशेष महत्त्व होता है। यह ज्ञान स्वतंत्र एवं समान रूप से समाज के सभी सदस्यों के लिये उपलब्ध रहता है। विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र इस प्रकार के ज्ञान को उपलब्ध कराने में सहयोग करते हैं। इसे
सार्वजनिक ज्ञान भी कहते हैं।
(c) अर्द्ध-सामाजिक ज्ञान-
यह वह ज्ञान है जो कुछ विशेष व्यक्तियों तक की सीमित रहता है। इसका क्षेत्र भी संकुचित होता है। इस प्रकार के ज्ञान के अन्तर्गत अर्द्ध-प्रकाशित प्रलेख, शासकीय प्रकाशन, आलेख, विभिन्न अभिलेख आदि आते हैं।
उपरोक्त वर्णित तीनों प्रकार के ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। तर्क, प्रयोग और विश्लेषण के आधार पर वैयक्तिक ज्ञान सामाजिक ज्ञान में विकसित हो जाता है। वैयक्तिक ज्ञान की वृद्धि में सामाजिक ज्ञान एक महत्त्वपूर्ण और आवश्यक स्रोत के रूप में कार्य करता है और वैयक्तिक ज्ञान के आधार पर सामाजिक ज्ञान का निर्माण होता है। इस प्रकार दोनों प्रकार के ज्ञान के मध्य कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं है। दोनों ही एक दूसरे की वृद्धि और विकास में सहायक हैं। ऐसे में यह कहना उचित प्रतीत होता है कि ज्ञान तथ्यपूर्ण विचारों का समूह है। जब यह किसी व्यक्ति के मस्तिष्क तक सीमित होता है तब यह व्यक्तिगत अथवा निजी ज्ञान होता है और जब किसी अभिव्यक्ति तर्क, प्रयोग और विश्लेषण के आधार पर सार्वजनिक रूप से कर दी जाती है, तब यह सामाजिक ज्ञान बन जाता है। अतः स्पष्ट रूप से हम यह कह सकते हैं कि समाज ज्ञान के उद्भव व विकास का एक प्रभावशाली साधन व स्रोत है।
प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री जिमान ने सामाजिक ज्ञान के संगठन के महत्त्व की विवेचना करते हुए इसकी वृद्धि और विकास के तीन कारक या साधन माने हैं-रचनात्मक ज्ञान संगठन, स्वयं संगठित और ग्रन्थात्मक संगठन जिसमें पुस्तकालयों का संगठन शामिल है। रचनात्मक ज्ञान संगठन उन प्रयासों का परिणाम है जिनमें अनुभव प्रयोग और निरीक्षण के आधार पर तथा अनुसंधान की विभिन्न विधियों के द्वारा ज्ञान की रचना या सृष्टि की जाती है और उसे सम्प्रेषित किया जाता है। स्वयं संगठित ज्ञान का निर्माण एक प्रलेख में अन्य प्रलेखों के संदर्भ उद्धरण प्रस्तुत किये जाते हैं। इससे विचारों के द्वारा दोनों प्रलेखों के मध्य स्थापित किया जाता है। इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। यह ज्ञान का रुचिकर बौद्धिक संगठन है। इसे पुस्तकालयाध्यक्षों ने ज्ञान के पारस्परिक वर्गीकृत तत्वों में से एक माना है। ग्रन्थात्मक संगठन एवं सूचियों, सारकरण और अनुक्रमणीकरण पत्रिकाओं एवं अन्य सूचना उत्पादों तथा सेवाओं के अंतर्गत मूल या प्राथमिक प्रलेखों के संगठन को बताता है। इन सभी प्रकार के ज्ञान का संग्रह व संकलन पुस्तकालय व सूचनाकेन्द्र करते हैं।
2. प्रकृति के आधार पर-ज्ञान को उसकी प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में बाँटा गया है-
(अ) वैज्ञानिक ज्ञान-
वैज्ञानिक ज्ञान भी विशेष महत्त्व रखता है। सहज अथवा अंतर्बोध ज्ञान जब सुस्पष्ट सिद्धांतों, सूत्रों, परिकल्पनाओं, निरीक्षण, परीक्षण और विश्लेषण द्वारा संगठित, परिष्कृत और परिभाषित हो जाता है, तब वह वैज्ञानिक ज्ञान बन जाता है। यह ज्ञान सत्यापित और व्यवस्थित होता है। वैज्ञानिक ज्ञान में कई विशेषतायें पायी जाती हैं जिनमें निम्नांकित प्रमुख हैं-
(i) यह सुस्पष्ट सिद्धान्तों, नियमों, सूत्रों और प्रयोगों पर आधारित होता है।
(ii) यह अविभाजित होता है। इसका विभाजन तभी सम्भव है जब विभाजन कुछ निश्चित तथ्यों पर आधारित हो ।
(iii) यह सत्यापित और सुव्यवस्थित होता है।
(ब) तर्क अथवा बुद्धि संगत ज्ञान-
यह एक प्राकृतिक ज्ञान है जो सभी लोगों में विद्यमान होता है। हम सामान्यतः प्रत्येक वस्तु/पदार्थ के बारे में जानने का प्रयास करते हैं किन्तु उसके सम्बन्ध में सीखने का प्रयास नहीं करते। तर्क संगत ज्ञान को अनुभूति मूलक, प्रयोगाश्रित अथवा सकारात्मक ज्ञान भी कहते हैं। यह प्रामाणिक तर्क संगत विचारों पर आधारित होता है। यह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र के सैद्धान्तिक ज्ञान के रूप में तथा अन्य सामाजिक विषयों के क्षेत्र में दर्शन-शास्त्र के रूप में विकसित होता है।
(स) सहज अथवा अन्तर्बोध ज्ञान-
यह ज्ञान तर्क अथवा बुद्धि संगत ज्ञान का विकसित रूप है। यह ज्ञान की सर्वोच्च श्रेणी है जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती। इसमें मस्तिष्क, अन्तः प्रेरज्ञता, समझ और बौद्धिकता प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध रहते हैं। कभी-कभी यह ज्ञान मस्तिष्क की अवचेतन अवस्था में प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति में यह ज्ञान एक समान नहीं होता।
आजकल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जगत में संगठित व सतत अनुसंधानों के फलस्वरूप निरंतर वैज्ञानिक ज्ञान के जगत में विकास हो रहा है। नए-नए विषयों का सृजन एक ऐसी श्रृंखला है जिसका कोई अंत नहीं है। वर्तमान दौर में वैज्ञानिक ज्ञान एक शक्ति का रूप ले चुका है जिसे नियन्त्रित करना सम्भव नहीं है
प्रश्न 2 (iv) ज्ञान से आप क्या समझते हैं? इसके प्राप्ति के तरीके का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
ज्ञान पद का अनुवाद ‘नालेज’ पद से किया जाता है। भारतीय दर्शन के अनुसार ‘ज्ञान’ का अर्थ समझने से पूर्व सत्य की वस्तुनिष्ठता, ज्ञान की सार्थकता, ज्ञान की सत्यता तथा तार्किक प्रतिज्ञप्ति सत्यता से लगाया जाता है। इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं-
(i) ज्ञान की सत्यता हेतु उसकी वस्तुनिष्ठता का आकलन किया जाना आवश्यक है।
(ii) ज्ञान के अस्तित्व में कोई संशय नहीं होना चाहिए।
(iii) ज्ञान की सत्यता की पुष्टि भी सन्देहरहित होनी चाहिए।
(iv) तार्किक प्रतिज्ञप्ति भी सत्य होनी चाहिए।
ज्ञान की अवधारणा स्पष्ट करते हुए यह प्रश्न उठाया जाता है कि क्या ज्ञान का स्वरूप परिवर्तनीय है या अपरिवर्तनीय है? यह प्रश्न भी जटिल है ज्ञान के सम्मिलित तथ्य, विचार प्रत्यय, नियम और निष्कर्ष आदि ज्ञान के श्रव्य हैं अर्थात् जब अध्यापक छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है तो इन सभी तत्त्वों को बताता और समझाता है। अब जहाँ तक ज्ञान के तत्त्वों के बदलने या न बदलने का प्रश्न है तो इसमें सन्देह नहीं है कि ज्ञान के कुछ तत्त्व नहीं बदलते या इनके परिवर्तन की दर इतनी धीमी होती है कि उनका बदलाव महसूस नहीं होता। वहीं अनेक तथ्य, प्रत्यय व नियम ऐसे भी हैं जो लगभग नहीं बदलते। ज्ञान के यही तत्त्व शिक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। बहुत से जीवन मूल्य ऐसे होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता। शिक्षा छात्रों के मन में उनके प्रति आस्था उत्पन्न करती है और यह शिक्षा का दायित्व भी है। इसके विपरीत ज्ञान के कुछ तत्त्व परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। वैज्ञानिक खोजों से भी ज्ञान में अभिवृद्धि होती है, उसमें परिवर्तन आता है। उदाहरणार्थ, पहले शिक्षक द्वारा छात्रों को यह ज्ञान दिया जाता था कि सूर्य प्रातःकाल पूर्व दिशा से चलना आरम्भ करता है और शाम को पश्चिम दिशा में अपनी यात्रा समाप्त करता है। परन्तु अब छात्रों को यह बताया जाता है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। इस रूप में यदि देखा जाये तो पुरातन ज्ञान अज्ञान था। एक और उदाहरण द्वारा भी इसे समझा जा सकता है कि चलती हुई रेलगाड़ी में बैठने पर हमें पेड़ चलते हुए प्रतीत होते हैं परन्तु वास्तव में चलती स्थिति में तो रेलगाड़ी ही है। पृथ्वी की गति का ज्ञान हो जाने से भूगोल की शिक्षा में परिवर्तन आया। अतः शिक्षा को ज्ञान के तत्त्वों में आने वाले परिवर्तनों पर दृष्टि रखनी होगी। प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक ड्यूवी ने ज्ञान को अनुभव की सतत पुनर्रचना कहा है। विद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी समय-समय पर कुछ बदलाव किए जाने चाहिए। सत्य के अन्वेषण से जो नये नियम और सिद्धान्त प्रकाश में आते हैं, वे ज्ञान के स्थूल रूप में परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं।
ज्ञान की अवधारणा / संकल्पना
ज्ञान की अवधारणा के सन्दर्भ में एक तथ्य और है कि ज्ञान केवल अनुभूति मात्र नहीं है। अनुभूति मात्र बाह्य स्वरूप की होती है परन्तु जब वस्तु के बाह्य रूप को देखने के बाद हम उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो यह स्थिति संभवतः ज्ञान की कही जा सकती है। ऐसा ज्ञान प्राप्त होने की स्थिति को ही ज्ञान चक्षु का खुल जाना कहा जा सकता है। शिक्षा यदि हमारे ज्ञान चक्षु खोल दे तो वह अर्थात् हमारी शिक्षा का इस प्रकार भारतीय दर्शन के अनुसार चेतना को ही ज्ञान की संज्ञा दी जाती है। ज्ञान इन्द्रियों के अनुभव तक ही सीमित नहीं है, अपितु इन्द्रियों से प्राप्त अनुभूतियों द्वारा भी ज्ञान की प्राप्ति होती है जिसके लिए कर्म, ज्ञान व भक्ति में समन्वय आवश्यक है।
ज्ञान के स्रोत या तरीके
ज्ञान प्राप्ति के मूल रूप से निम्नलिखित पाँच प्रकार हैं-
(a) इन्द्रिय अनुभव –
ज्ञान का एक प्रमुख साधन इन्द्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव का प्रत्यक्षीकरण है। मनुष्य की पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा उसे क्रमशः देखकर सुनकर, सँघकर, स्वाद लेकर तथा स्पर्श करके सांसारिक वस्तुओं के बारे में तरह-तरह का ज्ञान प्रदान करती हैं। ऐसे ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार से मनुष्य ज्ञानेन्द्रियों द्वारा ही संसार की वस्तुओं के सम्पर्क में आता है तो एक प्रकार की संवेदना उत्पन्न होती है, यह सब देना ज्ञानेन्द्रियों को प्राप्त उत्तेजना में ही होती हैं तथा वस्तु का ज्ञान प्रदान करती है। इसे प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। यह प्रत्यक्षीकरण ही हमें उस वस्तु की जानकारी देता है।
(b) साक्ष्य –
जब हम दूसरों के अनुभव तथा निरीक्षण पर आधारित ज्ञान को मान्यता देते हैं तो इसे साक्ष्य कहा जाता है, साक्ष्य में व्यक्ति स्वयं निरीक्षण नहीं करता। वह दूसरों के निरीक्षण पर ही तथ्य का ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार साक्ष्य दूसरों के अनुभव पर आधारित ज्ञान है। हम प्रायः अपने जीवन में साक्ष्य का बहुत उपयोग करते हैं। हमने स्वयं बहुत से स्थानों को नहीं देखा है किन्तु जब दूसरे उनका वर्णन करते हैं तो हम उन स्थानों के अस्तित्व में विश्वास करने लगते हैं।
(c) तार्किक चिन्तन-
तार्किक चिन्तन ऐसी मानसिक प्रक्रिया/योग्यता है जिसके बिना कोई भी ज्ञान सम्भव नहीं है। हमारा अधिकांश ज्ञान तर्क पर ही आधारित होता है। हमें अनुभव द्वारा जो संवेदनायें प्राप्त होती हैं उनको तर्क द्वारा संगठित करके ज्ञान का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार यह अनुभव पर काम करता है और हमें ज्ञान में परिवर्तन करता जाता है।
इन्द्रियों से प्राप्त अनुभवों के द्वारा हम-रंग, स्वाद तथा गन्ध आदि से सम्बन्धित कुछ संवेदनाएँ प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु जब वस्तुओं में भेद करने का प्रश्न आता है, वहाँ हमें तार्किकता की आवश्यकता होती है जिसमें अमूर्त चिन्तन निहित होता है। अतः ज्ञान का आधार तर्क बुद्धि ही है।
(d) अन्तःप्रज्ञा तथा अन्तःप्रज्ञावाद-
यह भी ज्ञान प्राप्ति का एक मुख्य स्रोत है। यह एक प्रकार का आन्तरिक बोध है जिसमें ज्ञान की स्पष्टता निहित होती है। अन्तः से हमारा तात्पर्य है किसी तथ्य को अपने मन में जानना। इसके लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि इसके अन्तः अचानक ज्ञान के प्रकाश की किरण उत्पन्न होती है जिसे हम ज्ञान की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार के ज्ञान का एकमात्र प्रमाण यह है कि उसकी निश्चितता तथा वैधता में सन्देह नहीं होता तथा हम उस ज्ञान पर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अन्तः प्रज्ञा हमारे अन्दर निहित वह सद्धत क्षमता है जो कभी अचानक ही क्रियाशील होकर हमें आलोकित करती है।
परन्तु इस अन्तःप्रज्ञा के साथ कभी-कभी आत्मनिष्ठता का ऐसा गुढ़ा आबद्ध हो जाता है कि यदि हम इस यथार्थ ज्ञान का साथ मान भी लें तो फिर इस ज्ञान में वस्तुनिष्ठता तथा सार्वजनिकता जैसी चीज नहीं रह जायेगी और हम यह दावा नहीं कर सकेंगे कि कौन-सी प्रतिज्ञप्ति सत्य है और कौन-सी असत्य है।
प्रश्न 3 (i) कोर-प्रधान पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? इसके गुण एवं दोष बताइए।
कोर प्रधान पाठ्यक्रम से तात्पर्य है-ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य हों और कई विषय ऐसे हों जिनमें से विद्यार्थी कुछ को अपनी रुचियों के अनुसार चुन सकें। इस प्रकार का पाठ्यक्रम अमेरिका के स्कूलों में बहुत प्रचलित हो गया है। हर विद्यार्थी जो माध्यमिक स्तर पर होता है, अपनी वैयक्तिक रुचियों और योग्यताओं में एक-दूसरे से बहुत भिन्न होता है इसलिए सब विद्यार्थियों के लिए एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारित करना ठीक नहीं होता। फिर भी कुछ विषय ऐसे अवश्य होते हैं जिनका पढ़ना प्रत्येक विद्यार्थी को (जो एक विशेष स्तर पर है) आवश्यक होता है। कोर-प्रधान पाठ्यक्रम द्वारा यह चेष्टा की जाती है कि वे विषय जो प्रत्येक बालक के जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं, सब बालकों को अनिवार्य रूप से पढ़ाये जायें। इसके साथ ही साथ बालकों को से विषयों में से कुछ ऐसे विषयों को चुनकर पढ़ने की सुविधाएँ प्रदान की जायें जो उनकी रुचि तथा बहुत- योग्यता के अनुसार हों।
कोर-प्रधान पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य “समस्त युवकों को व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं से सम्बन्धित अनुभव प्रदान करना है। बालकों को वास्तविक समस्याओं के सुलझाने का अनुभव देना है और इस प्रकार उन्हें भावी समस्याओं का सामना करने के योग्य बनाना है। इसके द्वारा बालकों को वह अनुभव प्रदान करना है, जो उन्हें समाज का अच्छा नागरिक बनने में सहायता दे।” इस प्रकार कोर-प्रधान पाठ्यक्रम का लक्ष्य – व्यक्ति तथा समाज, दोनों का विकास करना है। इसके द्वारा बालक को ऐसा ज्ञान प्रदान करना है जो उनको वर्तमान तथा भावी समस्याओं को सुलझाने में सहायक हो तथा बालक को एक अच्छा नागरिक बनाये।
जिन विषयों का कोर-प्रधान, पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान होना चाहिए, वे हैं – (1) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, (2) कला-कौशल, (3) बागवानी, (4) गणित, (5) इतिहास तथा (6) भूगोल इत्यादि ।
स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा – इस प्रकार की शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रधान स्थान रखती है, क्योंकि प्रत्येक बालक के शारीरिक विकास के लिए बिना शिक्षा के किसी भी प्रकार के उद्देश्य की
प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार की शिक्षा व्यायाम, तैरना, नाचना और टीम के खेलों की क्रियाओं का विद्यालय में आयोजन करके दी जा सकती है।
कला-कौशल-बालकों को कला-कौशल तथा प्रयोगात्मक क्रियाएँ रुचिकर लगती हैं, विशेष तौर पर वे जब किशोरावस्था में होते हैं। अतएव उनके पाठ्यक्रम में कला तथा प्रयोगात्मक कार्यों की प्रधानता दिया जाना भी आवश्यक है। उनको इस प्रकार की क्रियाएँ सिखायी जाती हैं (जैसे-बुनाई, जिल्द बाँधना, लकड़ी का काम, धातु का काम, कुम्हारगीरी इत्यादि) ।
इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र इत्यादि-ये विषय बालक की सामाजिक भावना के विकास में अत्यन्त आवश्यक हैं। इन सब विषयों का सम्बन्ध मानव-जीवन से है, इसके द्वारा समय और स्थान के अनुसार मानव जीवन की व्यवस्था की जाती है। अतएव मानवता सम्बन्धी उचित दृष्टिकोण का विकास करने में इनका स्थान महत्त्वपूर्ण है।
विज्ञान — यह भी एक प्रधान विषय है। वर्तमान युग में किस प्रकार प्राकृतिक शक्तियों पर मानव ने विजय प्राप्त की है, यह हर बालक को सीखना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उसमें परीक्षण तथा अन्वेषण करने की भावना का विकास करना भी आवश्यक है। बालक में निरीक्षण, समता और तुलना तथा शुद्ध सामान्य सिद्धान्तों के बनाने की आदतों का निर्माण करना भी समाज तथा मानव- कल्याण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। विज्ञान का अध्ययन इन्हीं कारणों से आवश्यक है।
गणित – पाठ्यक्रम में इस विषय को भी प्रधान विषय की भाँति रखा जाना आवश्यक है, क्योंकि यह विषय तर्क तथा अमूर्त विचारों के विकास में अत्यन्त सहायक होता है। इसके अतिरिक्त
इसकी उपयोगिता दैनिक जीवन में भी बहुत है। बिना गणित के ज्ञान के हम दैनिक जीवन की साधारण से साधारण समस्याओं को हल करने में असफल रहेंगे। वर्तमान युग में गणित का महत्त्व इस कारण
भी अधिक है कि समस्त विज्ञान का विकास इसी विषय पर निर्भर है।
भाषा-भाषा को में प्रधानता दिये बिना किसी भी प्रकार के विषय की शिक्षा सम्भव नहीं है। बिना भाषा – ज्ञान के न तो बालक व्यक्तिगत और न सामाजिक समस्याओं का समाधान करने में सफल होगा। भाषा को भली-भाँति पढ़े बिना बालक अपने विचार व्यक्त नहीं कर पायेगा और इस प्रकार उसका विकास रुक जायेगा।
कोर पाठ्यक्रम की विशेषताएँ /गुण
कोर पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ/गुण निम्न प्रकार हैं-
1. यह पाठ्यक्रम सभी छात्रों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है।
2. इसमें विषय-वस्तु के परम्परागत शिक्षण को समाप्त कर दिये जाते हैं तथा कई विषयों को एक साथ मिलाकर पढ़ाया जाता है।
3. इसमें समय-विभाग चक्र लचीला होता है तथा कालांश बड़े होते हैं।
4. इसमें छात्रों एवं शिक्षकों के सम्बन्ध अधिक घनिष्ठ होते हैं तथा अध्ययन-अध्यापन के साथ- साथ परामर्श भी चलता है।
5. इसमें शिक्षण समस्या-केन्द्रित होता है तथा छात्रों को कार्यों एवं समस्याओं को हल करने का अनुभव प्राप्त होता है।
6. यह पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं बाल-केन्द्रित होता है।
7. इसमें विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव प्रयुक्त किये जाते हैं।
8. इसमें अधिकतर शैक्षिक कार्यक्रम छात्र और शिक्षक मिलकर आयोजित करते हैं।
9. इसके अन्तर्गत व्यापक निर्देशन कार्यक्रम की व्यवस्था रहती है।
10. यह पाठ्यक्रम सबसे अधिक प्रचलित है।
कोर पाठ्यक्रम की सीमाएँ
1. इस पाठ्यक्रम में छात्रों के सभी महत्वपूर्ण अनुभवों को स्थान प्राप्त नहीं होता है।
2. इस पाठ्यक्रम द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान में कोई क्रमबद्धता नहीं पायी जाती तथा ज्ञान असंगठित रहता है।
3. इस पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षण में अधिक समय लगता है।
4. हमारे आज के शिक्षक कोर पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा देने में कुशल नहीं होते।
5. इस पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़े छात्र कॉलेजों में प्रवेश पाने के नियमों को पूरा नहीं कर पाते। अतः उनका प्रवेश कठिन हो जाता है।
प्रश्न 3 (ii) ज्ञान की प्रकृति का वर्णन कीजिए।
ज्ञान की प्रकृति पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो इसे दो रूपों में व्यक्त किया जा सकता है-
1. ज्ञान एक साध्य के रूप में
एक साध्य के रूप में ज्ञान को तब माना जाता है जब उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। ज्ञान स्वतंत्र रूप में उपस्थित होता है परन्तु जब तक उसका अर्जन न किया जाए तब तक उसका उपयोग न व्यक्ति के लिए और न ही समाज के लिए किया जा सकता है। परम्परागत रूप में ज्ञान को एक साध्य के रूप में ही देखा जाता है जिसकी प्राप्ति प्राचीन काल में घर के सदस्यों द्वारा की जाती थी। प्राचीन काल में शिक्षा गुरुकुलों में प्रदान की जाती थी और शिक्षण विधि के रूप में मौखिक प्रणाली का प्रयोग किया जाता था परन्तु बाद में ज्ञानार्जन के लिए लिखित प्रणाली का प्रयोग किया जाने लगा।
वर्तमान काल में प्राचीन काल की तुलना में मशीनों का अधिक प्रयोग होने लगा है। ज्ञानार्जन के लिए पाठ्यक्रम में निरन्तर वृद्धि तथा परिवर्तन होता जा रहा है।
वर्तमान समय में स्कूलों में प्रदान किया जाने वाले ज्ञान का क्षेत्र पहले की तुलना में अधिक विस्तृत हो गया है अर्थात् ज्ञान एक साध्य के रूप में अधिक विस्तृत हो गया है। वर्तमान समय में ज्ञान की मात्रा में ही नहीं अपितु उसके स्वरूप में भी परिवर्तन आ गया है। आजकल नये-नये आधुनिक ज्ञान भी दिये जाने लगे हैं। जैसे विदेशी भाषाओं का ज्ञान, कम्प्यूटर का ज्ञान, आदि। स्कूली पाठ्यक्रम में प्राथमिक कक्षाओं से ही कम्प्यूटर पढ़ाया जाने लगा है। इण्टर स्तर तक के छात्रों के लिए आई.टी. औद्योगिक व्यवसायों के रूप में तकनीकी ज्ञान रखने वालों के लिए उपलब्ध है। ज्ञान साध्य के रूप में तब भी बन जाता है जब कोई छात्र ज्ञानार्जन इसलिए करता है ताकि उच्चतर स्तर का ज्ञान प्राप्त कर सके। प्रत्येक स्तर पर दिया जाने वाला ज्ञान अपने से पहले स्तर पर दिये गये ज्ञान से अधिक व्यापक तथा एक-दूसरे से किसी-न-किसी रूप में सम्बन्धित होता है । साध्य के रूप में ज्ञान व्यवस्थित, क्रमिक पाठ्यक्रम का एक भाग बनाकर दिया जाता है।
2. ज्ञान एक साधन के रूप में
ज्ञान एक साधन के रूप में तब बन जाता है जब ज्ञान प्राप्त करके किसी प्रत्यय की समझ विकसित करनी हो, जैसे-अधिगम का सिद्धान्त ज्ञान के रूप में तब साधन बन जाता है जब इसका प्रयोग सीखने की प्रक्रिया को समझने हेतु किया जाए। जब हम कुछ सीखते या समझते हैं तब ज्ञान का प्रयोग एक साधन के रूप में करते हैं। समझने के लिए सैद्धान्तिक ज्ञान का प्रयोग करना पड़ता है। मानव में बोध उत्पन्न करने हेतु वैध ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि वैध ज्ञान की मदद से ही किसी अवधारणा के नियमों को समझा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु या प्रकरण का ज्ञान अर्जित करके इसका अनुप्रयोग करने हेतु उसका व्यावहारिक जीवन में प्रयोग किया जाए। इस प्रकार ज्ञान की किसी वास्तविक परिस्थिति में प्रयोग किया जाए।
ज्ञान का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तथा उत्कृष्ट पहलू यही है कि ज्ञान की मदद से समझ विकसित करने के पश्चात् यह जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में उत्पन्न स्थिति में इस ज्ञान का प्रयोग किया जा सकता है। जब हम ज्ञान का वास्तविक जीवन में प्रयोग करके अपने कार्य को आसान एवं उपयोगी बनाते हैं तब ज्ञान एक साधन के रूप में हमारी मदद करता है। विज्ञान के नियमों को जब हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तब इस ज्ञान को एक साधन के रूप में ही समझा जाता है। भाषा के ज्ञान का अनुप्रयोग हम व्यावहारिक संचार के रूप में करते हैं। इंजीनियरिंग से सम्बन्धित ज्ञान को व्यावहारिक रूप में मशीनों एवं घरों के निर्माण में प्रयोग करना, आदि सिद्ध करता है कि ज्ञान एक साधन है। ज्ञान है का प्रयोग विश्लेषण हेतु भी किया जाता है। विश्लेषण की योग्यता यदि उद्देश्य की प्राप्ति हो तो ज्ञान एक साधन के रूप में इसमें सहायक सिद्ध होता है। ज्ञान का प्रयोग कई बार हम परिस्थितियों के विश्लेषण हेतु भी करते हैं। ऐसा ज्ञान जो विश्लेषण करने के काम आता है, साधन के रूप में ही होता है। ज्ञान का प्रयोग संश्लेषण के लिए भी किया जाता है। संश्लेषण की प्रक्रिया कुछ नवीन सृजन करने से सम्बन्धित होती है। इस प्रक्रिया में ज्ञान एक साधन के रूप में सहायता प्रदान करता है। ज्ञान का प्रयोग मूल्यांकन कार्यों के लिए भी किया जाता है और इसके द्वारा निष्कर्ष भी निकाले जाते हैं।
यह वर्तमान से लेकर भविष्य तक चलता है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए सदैव परिमार्जित एवं संशोधित रूप में हस्तांतरित होता है। ज्ञान की यदि प्रकृति पर ध्यान दिया जाए तो इसके विषय में निम्नलिखित बातें कही जा सकती हैं-
1 ज्ञान किसी परिस्थिति और प्रक्रिया से सम्बन्धित तथ्य और सत्य है। इसे सत्य से अलग नहीं किया जा सकता है।
2.यह अनुभवों की समझ पर आधारित सूचनाएँ हैं।
3 ज्ञान आत्मगत होता है इसका हस्तांतरण नहीं होता है।
4. ज्ञान वह सूचना है जो मस्तिष्क में प्रेषित हो जाती है।
5. ज्ञान सम्पूर्ण समाज के लिए उपयोगी साबित होता है। यह केवल व्यक्ति को ही लाभ नहीं.
• पहुँचाता है बल्कि सम्पूर्ण समाज को लाभ पहुँचाता है इसलिए यह सबके लिए उपयोगी माना जाता है।
प्रश्न 3 (iii) ज्ञान के विविध स्वरूप क्या हैं? उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए।
उत्तर – ज्ञान किसी वस्तु के सम्बन्ध में जानकारी है। वह वस्तु कुछ भी हो सकती है बन्दर बैंक द्वारा दिया हुआ कर्ज या गणित की समस्या इत्यादि। ज्ञान का उद्देश्य किसी वस्तु के सम्बन्ध में जैसी वह है वैसी ही उसकी जानकारी होना है। हमारी इस बात की चिन्ता कि हम ठीक से जान जायें कि यह वस्तु यथार्थ में वैसी ही है जैसा उसका ज्ञान यह जाहिर कर देता है कि इस बात की सम्भावना है कि हम धोखा खा रहे हों और हमारे कुछ निर्णय उस वस्तु के सम्बन्ध में गलत भी हो सकते हैं। एक गलत निर्णय हमें इस बात से अवगत न कराकर कि वस्तु यथार्थ में कैसी है इस बात का ज्ञान हमें करायेगी कि वस्तु हमें ऐसी प्रतीत होती है। अतएव यदि हम उन दशाओं के सम्बन्ध में जानकारी रख सकते हैं जिनमें हमारे निर्णय सत्य हैं तब हम उसके साथ-साथ ऐसे स्तर निर्धारित कर सकते हैं जिनके द्वारा हम कृत्रिम का यथार्थता से विभेद कर सकते हैं।
किसी वस्तु के सम्बन्ध में जब हम यह कहते हैं कि हमें उसकी जानकारी है तो हम यह मानकर चलते हैं कि यह जानकारी सत्य है। अतएव ज्ञान की धारणा में पहली बात तो यह निहित है कि ज्ञान अवश्य सत्य होना चाहिए। जैसे जब हम कहते हैं कि सोहन को हम जानते हैं तो सोहन से हमारा परिचय सत्य होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ज्ञाता को उस बात की सत्यता में विश्वास होना चाहिए। हमें विश्वास होना चाहिए कि हम सोहन को जानते हैं तथा तीसरी बात यह कि ज्ञाता के पास इस बात के पर्याप्त प्रमाण होने चाहिए कि यह बात सत्य है। हमारे पास इस बात के प्रमाण होने चाहिए कि हम सोहन को जानते हैं जैसे हम सोहन से कई बार मिल चुके हैं या हम और सोहन साथ-साथ पढ़े हैं इत्यादि। इस प्रकार ज्ञान के अर्थ में तीन बातें आती हैं—सत्यता, सत्यता में विश्वास तथा सत्यता के लिए पर्याप्त प्रमाण
ज्ञान के प्रकार
हम तीन प्रकार के ज्ञान का वर्णन कर सकते हैं-
(i) आगमनात्मक ज्ञान-इस प्रकार का ज्ञान हमारे अनुभव तथा निरीक्षण पर आधारित है। जॉन लॉक इस प्रकार के ज्ञान के प्रवर्तक हैं। उनके अनुसार बालक का मन जन्म के समय कोरी पटिया के समान होता है। जैसे-जैसे अनुभव मिलते जाते हैं इस पटिया पर लेखन होने लगता है। इससे तात्पर्य है कि ज्ञान अनुभवों द्वारा वृद्धि करता रहता है। शिक्षा में इस प्रकार के ज्ञान के प्रवर्तक कहते हैं कि सीखने के लिए समग्र अनुभव प्रदान करने चाहिए। इस प्रकार के ज्ञान में अलौकिक का कोई स्थान नहीं है।
(ii) प्रयोगमूलक ज्ञान-ज्ञान प्रयोग द्वारा प्राप्त होता है, ऐसा प्रयोजनवादियों की धारणा है ड्यूवी का कहना है कि ज्ञान की प्रक्रिया ‘एक प्रयास एवं सहन’ की प्रक्रिया है—एक विचार का अभ्यास में प्रयास करना एवं ऐसे प्रयास के परिणाम से जो फल प्राप्त होते हैं उनसे सीखना। इस धारणा के अनुसार ज्ञान कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे हम समझें कि वह अनुभव या निरीक्षण से अन्तिम रूप से समझी जा सकती है, जबकि हम ऐसी विधियों का प्रयोग करते हैं जैसे आगमन। यह तो कुछ ऐसी वस्तु है जो अनुभव में सक्रिय होती है। एक कृत्य की भाँति जो अनुभव को सन्तोषपूर्ण ढंग से आगे की ओर ले जाती है।
(iii) प्रागनुभव ज्ञान – ज्ञान स्वयं-प्रत्यक्ष की भाँति समझा जाता है। सिद्धान्त जब समझ लिए जाते हैं, सत्य पहचान लिए जाते हैं फिर उन्हें निरीक्षण, अनुभव या प्रयोग द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। इस विचारधारा के प्रवर्तक काण्ट हैं जो कहते हैं कि सामान्य सत्य अनुभव से स्वतन्त्र होने चाहिए—उन्हें स्वयं में स्पष्ट तथा निश्चित होना चाहिए। गणित का ज्ञान प्रागनुभव ज्ञान समझा जाता है।
उपर्युक्त वर्णन के अनुसार एक प्रकार का ज्ञान वह है जो अनुभव के पश्चात् प्राप्त होता है। दूसरे प्रकार का वह है जो प्रयोग, निरीक्षण तथा अनुभव पर केन्द्रित है तथा तीसरे प्रकार का ज्ञान अनुभव
से परे है। इस प्रकार के ज्ञान के सम्बन्ध में धारणा होती है कि अनुभव केवल तथ्य ही देता है तथ्य किसी बात को सिद्ध नहीं करते। उनसे सत्य का ज्ञान उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि उनको संगठित न किया जाए। तर्क द्वारा वह संगठित किये जाते हैं। इस प्रकार तर्क या बुद्धि अनुभव को ज्ञान में परिवर्तित करता जाता है, किन्तु कुछ सत्य को अनुभव से प्राप्त तथ्यों की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह स्वयं स्पष्ट तथा स्वयंसिद्ध है। प्रागनुभविक ज्ञान ऐसा ज्ञान कहलाता है जिसे बुद्धि अनुभव की सहायता के बिना प्राप्त करती है।
.
शिक्षण प्रदान करने में हमें इन तीनों प्रकार के ज्ञान को ध्यान में रखना चाहिए। विभिन्न विषयों का ज्ञान हमें अनुभव द्वारा प्राप्त होता है। गणित या तर्कशास्त्र का ज्ञान प्रागनुभविक प्रकार का ज्ञान है। गणित के शिक्षण के समय हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।
(नवीन) बी. एड. द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) : तृतीय प्रश्न-पत्र : ज्ञान व पाठ्यक्रम (303) .
प्रश्न 3 (iv) ज्ञान के प्राप्ति की विधियों की विवेचना कीजिए।
ज्ञान के स्रोत यदि ज्ञान की उत्पत्ति अथवा उद्गम की चर्चा करते हैं तो ‘ज्ञान प्राप्ति की विधियों’ के अन्तर्गत इस विषय पर विचार किया जा सकता है कि उस ज्ञान को प्राप्त कैसे किया जाए। मानव का स्वभाव प्रकृति से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है अर्थात् वह अपने आसपास घटने वाली प्रत्येक घटना का ज्ञान प्राप्त करने के प्रयास में सदैव लगा रहता है। ज्ञान कभी भी समाप्त न होने वाली भूख है। इसलिए मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने ज्ञान को समय के साथ निरन्तर समायोजित युग करता रहे। ज्ञान प्राप्त करने की यह जिज्ञासा प्रत्येक आयु के व्यक्ति में पायी जाती है। आज के में बदलती परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति यदि अपने ज्ञान को नहीं बदलेगा तो वह समय व अपने साथियों से पिछड़ जाएगा। विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएँ ज्ञान के स्वरूप, प्रकार तथा स्रोतों के विषय में विचार करने के साथ-साथ उसको प्राप्त करने की विधियों के विषय में भी अपने विचार व्यक्त करती *हैं। ये विधियाँ वास्तव में ज्ञान के स्वरूप तथा स्रोतों पर ही आधारित होती हैं। इन्द्रियों, तर्क और विश्वासों के आधार पर शिक्षाविदों और दार्शनिकों ने ज्ञान प्राप्त करने की कुछ विधियों का निर्माण किया है। ये विधियाँ निम्नलिखित हैं-
1. अंतर्बोध-इस विधि में न तो तर्क का इस्तेमाल होता है और न ही ज्ञानेंद्रिय अनुभव का। सम्पूर्ण ज्ञान में अंतर्ज्ञान का तत्त्व मौजूद होता है। यह केवल भूतकाल के अनुभवों और सोच पर आधारित होता है। इस विधि में हमें वस्तुओं की वास्तविकता का ज्ञान होता है। इस विधि से उच्चतम एवं दार्शनिक ज्ञान की प्राप्ति होती है।
2. एकाग्रता एवं ध्यान विधि-परम सत्ता तथा ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह विधि प्रभावशाली है। इस विधि का सम्बन्ध भी ज्ञान के आध्यात्मिक स्तर के साथ है। सभी भारतीय दर्शनों ने इस विधि के महत्त्व को स्वीकार किया है। इस विधि के अन्तर्गत व्यक्ति अपने ध्यान को अन्य विषयों से हटाकर केवल उसी वस्तु या विचार विधि के माध्यम से शांत स्थान पर ध्यान केन्द्रित करके अपना सम्बन्ध अलौकिक शक्ति के साथ जोड़ने का प्रयास करते थे। महात्मा बुद्ध ने इसी विधि द्वारा परम बोध को प्राप्त किया।
3. शब्द – विधि- ज्ञान प्राप्ति की यह काफी महत्त्वपूर्ण विधि है। आज हमारी शिक्षा प्रणाली में इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। इस विधि के अन्तर्गत व्यक्ति लिखित विषय सामग्री को पढ़कर अथवा विश्वसनीय व्यक्तियों के विचारों को सुनकर ज्ञान अर्जित करता है। साधारण भाषा में हम इसे मौखिक अथवा लिखित शब्दों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कराने वाली विधि कह सकते हैं। मानव जाति ने युगों से जिन ज्ञान को संचित किया है, उसे न प्रत्यक्ष विधि से प्राप्त किया जा सकता है और न ही केवल अन्तःप्रज्ञा, एकाग्रता अथवा प्रयोग द्वारा। इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि है— शब्द-विधि।
4. अथॉरिटी को अपील करना-अथॉरिटी ज्ञान का स्रोत न तो बुद्धि है न ही इन्द्रियानुभव। इस विधि की मुख्य विचारधारा किसी प्रकार की अथॉरिटी से अपील करना है। जैसे चर्च, विशेषज्ञों की राय आदि। प्रायः देखा गया है कि बहुत-सा ज्ञान जो हमारे पास है, उसे न तो ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा प्राप्त किया गया है और न ही इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धि का प्रयोग किया गया है। हमें ऐसे ज्ञान के लिए विशेषज्ञों पर निर्भर रहना पड़ता है। ज्ञान के अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग विशेषज्ञ होते हैं। विशेषज्ञ वह व्यक्ति होता है जो अपने अनुभव के आधार पर किसी क्षेत्र का इतना ज्ञान रखता है कि उसके ज्ञान को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए उसके ज्ञान को सच माना जाता है। कभी यह विश्वास किया जाता था कि धरती गोल नहीं चपटी है। बाद में तर्क को आधार बनाकर खोज की गई। ऐसी संस्था जो काफी समय से अस्तित्व में हो उसे अथॉरिटी समझा जा सकता है। प्रत्येक आदमी इस विधि का प्रयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए करता है। उदाहरण के लिए, हमारे माता-पिता द्वारा बताए गए जीवन-मूल्यों, परम्पराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को हम बिना चुनौती दिए स्वीकार करते हैं।
5. हेतुवाद- हेतुवादियों का मानना है कि ज्ञान विचारों की तुलना के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तर्क के आधार पर ज्ञान प्राप्त करने की दो विधियाँ हैं-
(क) आगमन विधि-इस विधि में हम विशेष से सामान्य की ओर चलते हैं तथा मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं। इससे सिद्धान्त का निर्माण होता है। हम उदाहरणों से शुरू करते हैं और सिद्धान्तों पर पहुँचते हैं।
(ख) निगमन विधि-यह विधि आगमन विधि से विपरीत है। हम इस विधि में सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हैं। हम एक सिद्धान्त से शुरू करते हैं और इसकी व्याख्या उदाहरणों के द्वारा करते हैं।
6. प्रयोगात्मक विधि-इस विधि में ज्ञान लेबोरेट्री में प्रयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यह विधि भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल आदि विषयों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाई जाती है।
7. समस्या समाधान विधि-प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में समस्याओं का सामना करता है। इन समस्याओं का हल ज्ञान बन जाता है। यह विधि मानसिक और बौद्धिक विकास करने के लिए उत्तम है। यह विधि गणित में सबसे अधिक कारगर है।
8. प्रत्यक्ष विधि- प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो के अनुसार, “ज्ञानेन्द्रियाँ ज्ञान के द्वार हैं।” जब हमारी इन्द्रियाँ बाहरी विषयों के सम्पर्क में आती हैं तो हमें उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त करने की इस विधि को प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। इस विधि में ज्ञान प्राप्ति के लिए अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की सबसे आरम्भिक विधि है— ज्ञानेन्द्रियों का प्रयोग। हमारी पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं—आँख, कान, नाक, मुख व त्वचा। इनके द्वारा देखकर, सुनकर, सूंघकर, स्वाद लेकर व स्पर्श कर व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। न्याय दर्शन के अनुसार, “इस विधि से यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानेन्द्रियों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है।”
9. ज्ञानेन्द्रिय अनुभव – ज्ञानेंद्रिय अनुभव ज्ञान प्राप्त करने की एक मुख्य विधि हैं। आधुनिक विज्ञान की प्रकृति अनुभव पर आधारित है। अवधारणाओं का विकास ज्ञानेंद्रिय अनुभवों के परिणामस्वरूप होता है। न्याय दर्शन के अनुसार, “इस विधि से यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है।”
(अ) करके सीखना-
हम ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हुए कुछ कार्य करते हैं और ज्ञान प्राप्त, करते हैं। जब एक बच्चा बर्फ को छूता है तो उसे पता लगता है कि बर्फ ठंडी है। इस प्रकार प्राप्त किया गया ज्ञान स्थायी होता है।
(ब) निरीक्षण-
समाज में रहते हुए बालक अपने आसपास के वातावरण का प्रेक्षण करता है। इस निरीक्षण के आधार पर वह अनुभवों को वास्तविक जीवन से जोड़कर देखता है। इस प्रक्रिया में तथ्यों का तर्क के आधार पर देखा जाता है। प्राकृतिवाद इस विधि में विश्वास करता है, क्योंकि इसका मानना है कि प्रकृति ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत होता है।
उपर्युक्त समस्त विवेचन से स्पष्ट है कि विभिन्न दर्शनों के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने की सम विधियाँ ज्ञान प्राप्ति में अपने ढंग से सहयोग देती है। ज्ञान प्राप्ति की प्रत्येक विधि का ज्ञान प्राप्त करने में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खेल विधि, समस्या समाधान विधि, विवाद, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि आदि विधियाँ बालकों को ज्ञान प्राप्त करने में सहायता हेतु प्रयुक्त की जाती है
.
इकाई-II
प्रश्न 4 (i) पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रकृति एवं महत्व पर प्रकाश डालिए।
पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी के करीकुलम (Curriculum) शब्द का हिन्दी रूपान्तर है। ‘करीकुलम’ शब्द लैटिन भाषा से अंग्रेजी में लिया गया है। यह शब्द लैटिन शब्द ‘कुर्रेर’ से बना है। कुर्रेर का अर्थ है दौड़ का मैदान । अतः दूसरे शब्दों में, करीकुलम वह क्रम है जिसे किसी व्यक्ति को अपने गन्तव्य स्थान तक पहुँचने के लिए पार करना होता है। अतः पाठ्यक्रम वह साधन है, जिसके द्वारा शिक्षा तथा जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। यह अध्ययन का निश्चित तथा तर्कपूर्ण क्रम है, जिसके माध्यम से छात्र के व्यक्तित्व का विकास होता है तथा वह नवीन ज्ञान एवं अनुभव अर्जित करता है। शिक्षा के अर्थ के सन्दर्भ में दो धाराएँ प्रचलित हैं- प्रथम प्रचलित अथवा संकुचित अर्थ और द्वितीय वास्तविक एवं व्यापक अर्थ । संकुचित अर्थ में शिक्षा केवल स्कूली शिक्षा या पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित होती है. परन्तु विस्तृत अर्थ पाठ्यक्रम के अन्तर्गत वे सभी अनुभव आ जाते हैं जिसे एक नयी पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ियों से प्राप्त करती है। साथ ही विद्यालय में रहते हुए एक शिक्षक के संरक्षण में छात्र जो भी क्रियाएँ करता है, वे सभी पाठ्यक्रम के अन्तर्गत आती हैं तथा इसके अतिरिक्त विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएँ भी पाठ्यक्रम का अंग होती हैं। अतः वर्तमान समय में पाठ्यक्रम से तात्पर्य उसके विस्तृत स्वरूप से ही है।
पाठ्यक्रम की प्रकृति
पाठ्यक्रम के स्वरूप को अच्छी तरह समझने के लिए हमें शिक्षा के विकास पर दृष्टिपात करना होगा। प्राचीनकाल में शिक्षा का स्वरूप पूर्णतया अनौपचारिक होता था। अर्थात् शिक्षा किसी विधि एवं क्रम में बँधी हुई नहीं थी। उस समय बालकों की शिक्षा उनके परिवार एवं समाज की जीवनचर्या के मध्य चलती रहती थी तथा बालक उसमें सहभागी बनकर प्रत्यक्ष अनुभव निरीक्षण के माध्यम से तथा अपने बड़ों एवं पूर्वजों के अनुभव सुनकर शिक्षा प्राप्त करता था । पाठ्यक्रम का अर्थ पाठ्यवस्तु लगाया जाता था। वस्तुतः पाठ्यवस्तु को विद्यालय विषयों तक सीमित कर दिया जाता था। कक्षा-कक्ष के बाहर ग्रहण किये गये अनुभवों को पाठ्यक्रम का अंग नहीं माना जाता था, किन्तु सभ्यता के विकास के साथ-साथ मानव के ज्ञानराशि के संचित कोष में निरंतर वृद्धि होती गई तथा मनुष्य के जीवन में जटिलताएँ एवं विविधताएँ आती गईं। इसके फलस्वरूप व्यक्ति के पास समय एवं साधन का अभाव होने लगा तथा उसकी शिक्षा अपूर्ण रहने लगी। अतः प्रत्येक विकासशील समाज ने अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इसे विधिवत् एवं क्रमबद्ध बनाने के प्रयास प्रारम्भ किए। विद्यालयों का उद्भव तथा उनकी स्थापना इन्हीं प्रयासों के परिणाम हैं। इस प्रकार समाज जो उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण ज्ञान अपने बालकों को समुचित ढंग से नहीं दे पा रहा था उसने उसकी जिम्मेदारी अनुभवी विद्वानों को सौंप दी। इन विद्यालयों द्वारा बालकों को जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा उन्हें समुचित ढंग से शिक्षा प्रदान करने हेतु जो धनराशि निश्चित एवं निर्धारित की गई तथा की जाती है उसे पाठ्यक्रम कहते हैं। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम अध्ययन का ही एक क्रम जिसके अनुसार चलकर छात्र अपना विकास करता है। अतः यदि शिक्षा की तुलना दौड़ से की जाए तो पाठ्यक्रम उस दौड़ के मैदान के समान है जिसे पार करके दौड़ने वाले अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं।
आधुनिक समय में पाठ्यक्रम के स्वरूप में काफी परिवर्तन हो गये हैं। जहाँ प्राचीन अवधारणा के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ पाठ्यवस्तु की एक सूची के रूप में लगाया जाता था और पाठ्यवस्तु को अध्ययन विषय के नाम से पुकारा और पाठ्यवस्तु को विद्यालयीय विषयों तक सीमित कर दिया जाता था पर आज पाठ्यक्रम की परिभाषाएँ काफी व्यापक हो गयी हैं। इसमें केवल विद्यालयीय विषयों को ही समाहित नहीं किया जाता बल्कि बालक की अन्य सभी क्रियाओं तथा उनके अनुभवों को भी सम्मिलित किया जाता है जिनके लिए विद्यालय मार्गदर्शन करता है। आधुनिक समय में पाठ्यक्रम को बहुत व्यापक रूप में देखा जाने लगा है और इसके अन्तर्गत वे सभी क्रियाएँ आ जाती हैं जो अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं के नाम से प्रचलित थीं। विद्यालयों का प्रमुख कार्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना होता है और इसको पूर्ण करने के लिए वहाँ पर जो कुछ भी किया जाता है उसे पाठ्यक्रम का नाम दिया जाता है। इसीलिए पाठ्यक्रम को परिभाषित करते हुए विद्वानों ने इसे ‘व्हाट ऑफ एजूकेशन’ कहा है। प्रथम दृष्टि में यह परिभाषा बहुत अधिक सरल एवं स्पष्ट प्रतीत होती है, परन्तु इस ‘व्हाट’ की व्याख्या करना तथा कोई निश्चित उत्तर प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है। इस सन्दर्भ में अमेरिका के नेशनल एजूकेशन एसोसिएशन ने अपनी टिप्पणी निम्न प्रकार की है—
“विद्यालयों का कार्य क्या है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर कई बार अनेक ढंग से दिया जा चुका है फिर भी बार-बार उठाया जाता है। कारण स्पष्ट है यह एक ऐसा शाश्वत प्रश्न है जिसका उत्तर अंतिम रूप से कभी दिया भी नहीं जा सकता है तथा प्रत्येक समाज एवं प्रत्येक पीढ़ी की बदलती हुई प्रकृति एवं आवश्यकताओं के अनुसार बदलता रहता है।”
इसी प्रकार शिक्षा के इतिहास से भी इस बात की पुष्टि होती है कि समय के साथ-साथ पाठ्यक्रम परन्तु में भी परिवर्तन होते रहे हैं तथा इसमें कभी व्यापकता तथा कभी संकीर्णता. आती रही है, शिक्षाविदों को जब इस बात का आभास मिला कि विद्यालयों में शिक्षित युवक सदैव अपने भावी जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं तब यह निष्कर्ष निकाला गया कि जीवन की तैयारी के लिये पढ़ना- लिखना ही सब कुछ नहीं है। मनोविज्ञान के विकास ने भी इस धारणा को बल प्रदान किया कि केवल अध्ययन-अध्यापन पर ही पूरा ध्यान रखना बालकों के विकास की दृष्टि से न केवल एकाकी है, बल्कि अन्य प्रवृत्तियों के समुचित विकास के अभाव में हानिप्रद भी हो सकता है। इस दृष्टिकोण का प्रभाव विद्यालयों के कार्यक्रमों पर पड़ा और उनमें व्यापकता आनी प्रारम्भ हुई। अतः विद्यालयों में पाठ्य-विषयों के साथ-साथ ऐसी प्रवृत्तियों का भी समावेश किया जाने लगा, जिनमें बालकों में बौद्धिक ज्ञान के साथ-साथ स्वास्थ्य, सौन्दर्यबोध, सृजनात्मकता तथा अन्य मानवीय एवं सामाजिक गुणों का समुचित विकास हो सके। इस प्रकार उतार-चढ़ाव के पश्चात् वर्तमान शताब्दी में पाठ्यक्रम की व्यापकता की दृष्टि से अनेक विद्वानों ने इसे अपने-अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया। बविट के अनुसार, “उच्चतर जीवन के लिए प्रतिदिन और चौबीस घण्टे की जा रही समस्त क्रियाएँ पाठ्यक्रम के अन्तर्गत आ जाती हैं।”
ले के अनुसार, “पाठ्यक्रम का विस्तार वहाँ तक है जहाँ तक जीवन का।”
परन्तु विद्वानों के उपर्युक्त विचारों को पाठ्यक्रम की समुचित परिभाषा मानना तर्कसंगत नहीं लगता है, क्योंकि पाठ्यक्रम का सम्बन्ध शिक्षा के औपचारिक अभिकरण विद्यालय से है तथा विद्यालय ही पाठ्यक्रम की सीमा भी है। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम को विद्यालय के घेरे में ही परिभाषित करना उचित लगता है।
बाल्टर एस. मुनरो के शब्दकोश के अनुसार, “पाठ्यक्रम को किसी विद्यार्थी द्वारा लिये जाने वाले विषयों के रूप में परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम की कार्यात्मक संकल्पना के अनुसार इसके अंतर्गत वह सब अनुभव आ जाते हैं जो विद्यालय में शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं।” इस संकल्पना के अनुसार पाठ्यक्रम विकास के अन्तर्गत प्रयुक्त किये जाने वाले अनुभवों के आयोजन में पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करने, उसे क्रियान्वित करने तथा उसका मूल्यांकन करने सम्बन्धी पक्ष सम्मिलित होते हैं।
माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार, “पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धान्तिक विषयों से नहीं है जो विद्यालयों में परम्परागत रूप से पढ़ाये जाते हैं, बल्कि इसमें अनुभवों की वह सम्पूर्णता भी सम्मिलित होती है, जिनको विद्यार्थी विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, खेल के मैदान तथा शिक्षक एवं छात्रों को अनेक अनौपचारिक सम्पर्कों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का सम्पूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है और उनके सन्तुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता करता है।”
महत्त्व
किसी भी विषय सम्बन्धी शिक्षण लक्ष्य को पाने के लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम का होना नितान्त आवश्यक है। शिक्षा सम्बन्धी सभी अनुभव का समावेश इसी पाठ्यक्रम में किया जाता है। पाठ्यक्रम से विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। विषय शिक्षण के सन्दर्भ में ही पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता निरन्तर बनी रहती है। पाठ्यक्रम के महत्त्व निम्नलिखित हैं-
1. पाठ्यक्रम शिक्षण को नियमित बनाता है-
विद्यालय में शिक्षण कार्य को नियमित बनाने व उसे सुनियोजित करने में पाठ्यक्रम की विशेष आवश्यकता पड़ती है कि विद्यालय में अमुक कक्षा के छात्रों को अमुक विषय का कितना ज्ञान प्रदान किया जाएगा।
2. शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में सहायक-
पाठ्यक्रम का निर्धारण हो जाने के बाद ही शिक्षक कक्षा में अपनी शिक्षण प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है कि कौन से विषय में से कौन-सा उपविषय किस विधि से कितने समय में पढ़ाया जाए।
3. छात्रों के मानसिक स्तर व विकास का मूल्यांकन करने में सहायक –
पाठ्यक्रम के निर्धारित हो जाने पर शैक्षिक सत्र के समाप्ति के बाद यह मूल्यांकन किया जा सकता है कि छात्रों के मानसिक स्तर में कितना सुधार हुआ, उसका कितना विकास हुआ। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित अवधि के उपरान्त छात्र के ज्ञान की परीक्षा ली जाती है तथा इस परीक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रम में से ही प्रश्न-पत्र बनाए जाते हैं। चूँकि सभी विद्यार्थियों ने एक ही पाठ्यक्रम को समान अवधि में पढ़ा है, अतः उनके मानसिक स्तर की परीक्षा लेने के कार्य को न्याय-संगत कहा जा सकता है ।
प्रश्न 4 (ii) पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन हेतु शिक्षक का योगदान बताइए
अथवा
पाठ्यक्रम को व्यावहारिक स्वरूप देने, विकसित करने में शिक्षक की क्या भूमिका है? व्याख्या कीजिए।
अथवा
पाठ्यक्रम विकास में अध्यापकों की भूमिका का वर्णन कीजिए।
उत्तर
किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम की सफलता या असफलता उस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाले शिक्षकों पर निर्भर करती है। शिक्षकों के आचार-विचार आस्थाएँ, मान्यताएँ, सामाजिक पृष्ठभूमि एवं शैक्षिक योग्यता आदि पाठ्यक्रम को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। शिक्षक, शिक्षा प्रक्रिया की महत्त्व पूर्ण धुरी होता है। अतः शिक्षक से जुड़ा प्रत्येक पक्ष इस प्रक्रिया को प्रभावित करता है। उदाहरणार्थ- अधिकांश शिक्षक समाज के मध्यम एवं उच्च वर्ग से आते हैं, अतः वे केवल ऐसे ही अधिगम अनुभव ही कक्षा में प्रस्तुत करते हैं जो केवल उसी वर्ग के बालकों के लिए उपयुक्त होते हैं। साथ ही शिक्षकों का आयुवर्ग भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। युवा एवं प्रौढ़ शिक्षकों की सोच एवं अनुभव में पर्याप्त अन्तर होता है। पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव दो प्रमुख रूपों में कार्य करता है-
(i) वैयक्तिक रूप में, (ii) संगठित शक्ति के रूप में।
प्रत्येक शिक्षक कुछ नैतिक मूल्यों में आस्था रखता है तथा जाने-अनजाने वह उनका शिक्षण भी करता रहता है। इसलिए कहावत भी प्रचलित है कि प्रत्येक शिक्षक अनिवार्य रूप से धर्म का शिक्षक होता है। यहाँ पर धर्म का तात्पर्य सामान्य नैतिक आचरण से है। पाठ्यक्रम शिक्षक के लिए अपने विचारों को बालकों तक पहुँचाने का माध्यम होता है। वह प्रायः पाठ्यक्रम की अन्तर्वस्तु का उपयोग अपने विश्वास, दृष्टिकोण एवं मान्यताओं को विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए करता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष ढंग से शिक्षक व्यक्तिगत रूप में पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है।
वर्तमान समय में शिक्षक संगठन शक्ति के रूप में भी उभर रहा है। अन्य व्यावसायिक वर्गों के समान ही शिक्षक वर्ग में संगठन भी कार्य करने लगे हैं जो उनकी आर्थिक एवं सेवा सम्बन्धी माँगों को करवाने के साथ-साथ कुछ सीमा तक पाठ्यक्रम को भी प्रभावित करते हैं। ऐसा भी देखने में आया पूरा है कि शिक्षक संगठनों के अलग-अलग गुटों का सम्बन्ध अलग-अलग विचारधाराओं वाले राजनीतिक दलों के साथ होता है। अतः वे अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार पाठ्यक्रम पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरणार्थ, ब्रिटेन की सरकार पाठ्यक्रम के बारे में कोई भी निर्णय लेने से पहले वहाँ के शक्तिशाली शिक्षक संघ एन.यू.टी. (नेशनल यूनियन ऑफ टीचर्स) से अवश्य परामर्श करती है। अपने देश भारत में भी शिक्षक संगठनों का प्रभाव-क्षेत्र उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। अखिल भारतीय स्तर पर ‘ऑल इण्डिया सैकण्डरी टीचर्स एसोसिएशन’, ‘ऑल इण्डिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स ऑर्गनाइजेशन’ आदि तथा राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय शिक्षक संगठन पाठ्यक्रम विकास कार्य को प्रभावित करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में तो पाठ्यक्रम विकास का अधिकांश कार्य वहाँ का प्रभावशाली एवं सम्पन्न शैक्षिक संगठन ‘नेशनल एजूकेशन एसोसिएशन’ अपने पाठ्यक्रम विभाग के माध्यम से कर रहा है। इस प्रकार संगठित शक्ति के रूप में शिक्षक वर्ग पाठ्यक्रम विकास में एक दबाव समूह के रूप में कार्य करता है।
पाठ्यक्रम एवं शिक्षक
पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अभिकरण शिक्षक है। पाठ्यक्रम नियोजन कार्य में इससे सम्बन्धित अन्य घटकों की भागीदारी एवं उनकी सीमाओं के बारे में विवाद हो सकता है किन्तु पाठ्यक्रम विकास के सभी चरणों एवं सभी स्तरों पर शिक्षक की भागीदारी असंदिग्ध एवं सर्वमान्य है। शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण, अन्तर्वस्तु के चयन एवं संगठन, शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों के चयन, सहायक सामग्री के चयन, मूल्यांकन विधियों के निर्धारण आदि सभी सोपानों में शिक्षक की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्तिगत रूप से छात्रों एवं उनकी समस्याओं को समझने, उन पर ध्यान देने तथा तद्नुकूल निर्णय लेने का कार्य प्रभावी रूप से शिक्षक ही कर सकता है।
पाठ्यक्रम विकास में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भागीदारी शिक्षक की ही होती है। इस प्रकार शिक्षक के महत्त्वपूर्ण भागीदारी के प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं-
(i) शिक्षक का छात्र, विद्यालय तथा उनसे सम्बन्धित सभी पक्षों से भावनात्मक सम्बन्ध होता है। अतः वह विभिन्न शैक्षिक परिस्थितियों के प्रति मात्र बौद्धिक रूप से ही नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। पाठ्यक्रम निर्माण की भागीदारी में अपनत्व की यह भावना बहुत महत्त्वपूर्ण होती है क्योंकि यही भावना विद्यालय के पर्यावरण को आवश्यक स्थायित्व एवं व्यवस्था प्रदान करने में सहायक होती है।
(ii) शिक्षक उस नाविक के समान होता है जो यह भली-भाँति जानता है कि उसे कहाँ जाना है तथा वहाँ पहुँचने के लिए वह अपने मानसिक निर्णय के अनुसार पानी, नाव, पतवार आदि के विषय में बात करने के लिए सदैव तैयार रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षकों में ज्ञान, अनुभव एवं व्यावसायिक उत्तरदायित्व की प्रबल भावना होती है जो पाठ्यक्रम नियोजन में शक्ति का स्रोत सिद्ध होती है।
(iii) पाठ्यक्रम को वास्तविक कार्यात्मक रूप कक्षा में ही प्रदान किया जाता है। अतः निस्सन्देह रूप से इस कार्य में शिक्षक को ही प्रमुख भूमिका निभानी होती है। एक विद्वान के मतानुसार ‘पाठ्यक्रम तो उसी समय निर्मित होता है जब शिक्षक और छात्र यह निश्चित करते हैं कि अब हम पढ़ेंगे।” इसी तथ्य को दृष्टिगत करते हुए सेलर एवं अलेक्जेन्डर ने दो प्रकार के पाठ्यक्रम बताये हैं.
(a) नियोजित पाठ्यक्रम, (b) क्रियान्वित पाठ्यक्रम ।
इस वर्गीकरण का तर्क यह है कि कदाचित ही किसी कक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरी तरह अपनाया जाता होगा। उसमें शिक्षकों द्वारा परिस्थितियों के अनुसार प्रायः संशोधन कर लिये जाते हैं। अतः अनेक बार ‘क्रियान्वित पाठ्यक्रम को ही वास्तविक पाठ्यक्रम मान लिया जाता है। व्यावहारिक दृष्टि से यह तर्कसंगत भी लगता है। इसीलिए ‘क्रियान्वित पाठ्यक्रम’ को ही वास्तविक पाठ्यक्रम मानने वाला वर्ग पाठ्यक्रम निर्माण कार्य में शिक्षक को प्रमुख घटक मानता है। लीज, फ्रेजर एवं जॉनसन अपनी पुस्तक ‘दि टीचर इन करीक्युलम मेकिंग’ में लिखते हैं कि, “छात्रों एवं शिक्षक को कक्षा में प्रविष्ट हो जाने पर जब द्वार बन्द हो जाता है तो छात्र ज्ञान, अन्तर्दृष्टि, प्रेरणा आदि सभी के लिए शिक्षक पर ही निर्भर करते हैं। अतः पाठ्यक्रम उन्नयन का अर्थ वास्तव में कक्षा-कार्य उन्नयन ही है।”
उपर्युक्त कथन के विषय में जॉन डी. वी. लिखते हैं कि “मेरे एवं मेरे सहकर्मियों के समक्ष नवयुवकों की शिक्षा के सम्बन्ध में कोई पूर्व निर्धारित सिद्धान्त नहीं थे। सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। विद्यालय मात्र कुछ विचारों को लेकर प्रारम्भ किया गया था।”
एडवर्ड ए. क्रग शिक्षकों के सम्भागित्व को पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग मानते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि पाठ्यक्रम आयोजन में शिक्षकों को भागीदार बनाना उन पर कोई एहसान करना नहीं है। क्रग महोदय के अनुसार, “शिक्षकों के पास वह ज्ञान और अनुभव होता है जो पाठ्यक्रम विकास कार्य में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होता है।” इसके साथ ही क्रग महोदय एक प्रकार की चेतावनी भी देते हैं तथा कहते हैं कि “कक्षा शिक्षकों को मात्र सम्भागित्व प्रदान करना तब तक व्यर्थ रहेगा जब तक उनकी सहमति, उनकी अपनत्व की भावना, उनकी उद्यतता प्राप्त नहीं होती। यह कैसे प्राप्त हों ? इस प्रश्न का सीधा और स्पष्ट उत्तर यह है कि शिक्षकों का विश्वास प्राप्त किया जाए।” इस सम्बन्ध में विश्व शिक्षक संघ में एक विद्वान द्वारा व्यक्त किये गये विचार निश्चित रूप से उल्लेखनीय हैं—“शिक्षकों के सम्भागित्व में यह अर्थ निहित है कि जिन शिक्षकों से परामर्श किया जाता है वे सक्रिय भूमिका निभा सकें, अन्य घटकों विशेषकर अधिकारी वर्ग द्वारा व्यक्त विचारों एवं प्रतिपादित सिद्धान्तों का विरोध कर सकें, अपनी सहमति एवं असहमति दोनों व्यक्त कर सकें, किसी योजना का विरोध अथवा अनुमोदन दोनों कर सकें।”
पाठ्यक्रम आयोजन का कार्य तो लगभग सभी जगह विशेषज्ञों के हाथ में ही केन्द्रित है। यद्यपि उन विशेषज्ञों में बहुत-से सफल एवं अनुभवी शिक्षक होते किन्तु वे प्रायः वर्तमान में कार्यरत शिक्षक नहीं होते तथा कार्य-क्षेत्र की स्थितियों, समस्याओं एवं कठिनाइयों को कार्यरत शिक्षक की दृष्टि से नहीं देख पाये। इसलिए उनके द्वारा निर्मित योजनाएँ प्रायः आदर्श एवं महत्त्वाकांक्षा की ओर झुक जाती हैं। अनेक अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों से यह भी पता चलता है कि शिक्षक की अपेक्षा केवल शैक्षिक सामग्री एवं शिक्षण की विधियों पर केन्द्रित योजनाएँ प्रायः सफल नहीं हो सकी हैं। जहाँ कहीं शिक्षकों की भागीदारी के प्रयास भी हुए वे भी प्रायः अपर्याप्त ही रहे हैं तथा वे मात्र वांछनीय दिशा में कदम बढ़ाने के सूचक ही हैं। भारत में भी शिक्षकों की भागीदारी को अपर्याप्त मानते हुए कोठारी आयोग एवं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ‘शैक्षिक आयोजन, प्रशासन एवं मूल्यांकन’ के लिए गणित कार्यकारी दल ने भी इसके लिए सशक्त शब्दों में अनुशंसा की है तथा शिक्षकों के सम्भागित्व को अपरिहार्य माना है।
उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि प्रायः सभी सरकारें शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन में शिक्षकों की समुचित भागीदारी के प्रति उदासीन रही हैं, किन्तु इस चित्र का दूसरा पक्ष भी उतना ही धूमिल है। ऐसा देखने में आया है कि भागीदारी के प्रति शिक्षक भी प्रायः उदासीन भाव ही रखते रहे हैं। इस बारे में पूर्व सन्दर्भित कार्यकारी दल ने अपने प्रतिवेदन में निराशा व्यक्त करते हुए लिखा है कि “देश की पंचवर्षीय योजनाओं के प्रति देश के शिक्षकों एवं उनके संगठनों ने कोई विशेष प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है जबकि उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे मामलों में सुधार के सुझाव तथा आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक योजनाएँ भी प्रस्तुत करें।”
शिक्षकों की इस उदासीनता के कुछ प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं-
(i) शिक्षण व्यवसाय को अन्य जीविकोपार्जन साधनों की तरह एक साधन मानना ।
(ii) शिक्षकों द्वारा केवल दैनन्दिन कार्यों तक ही अपने को सीमित रखना ।
(iii) ज्वलन्त शैक्षिक प्रश्नों को महत्त्व न देना तथा उन पर चर्चा को समय एवं शक्ति का अपव्यय समझना ।
(iv) शिक्षकों में विषयों के आवश्यक ज्ञान का अभाव।
(v) अधिकांश शिक्षकों में कठोर एवं पुरातनपंथी प्रवृत्ति का होना। (vi) पाठ्यक्रम निर्माण के लिए आवश्यक योग्यता का अभाव। (vii) आत्म-विश्वास एवं उद्यमशीलता का अभाव।
(viii) अच्छे शिक्षकों की उपेक्षा ।
(ix) समाज में शिक्षकों के प्रति अनुचित दृष्टिकोण । (x) आर्थिक तंगी।
प्रश्न 4 (iii) शैक्षिक एजेंसी के रूप में विद्यालय का पाठ्यचर्या क्रियान्वय हेतु योगदानों का वर्णन कीजिए।
राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु व पाठ्यचर्या क्रियान्वयन हेतु विद्यालय की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
विद्यालय
राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय (गाँव/नगर) स्तरों पर विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु जिम्मेदार संस्थाओं और संगठनों के अन्दर और उन सबके बीच आपस में मानव संसाधन विकास के लिए अच्छा सामंजस्य होना चाहिए। इस नेटवर्क के माध्यम से विद्यालयी शिक्षा प्रणाली की पाठ्यचर्या को सरल व प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सकता है। इसके लिए सभी स्तरों पर जिम्मेदारी बाँटने की आवश्यकता है, जिसके लिए राज्य, जिला व स्थानीय स्तर पर टास्क फोर्स भी गठित किये जा सकते हैं जिसमें सरकार के प्रतिनिधि और अपने कार्यों के सम्बन्ध में स्वायत्तता प्राप्त विद्यालय और समुदाय शामिल होंगे। ये टास्क फोर्स अग्रलिखित कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे-
(i) अपने क्षेत्रों के विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की पहचान और समय-समय पर उनके आकलन के लिए।
(ii) समानता और गुणवत्ता दोनों के लिए भौतिक व मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने और ऐसे आवश्यक संसाधनों में वृद्धि करने की दृष्टि से योजना और कार्य-नीतियाँ बनाने के लिए उदाहरणार्थ, समुदाय में उपलब्ध संसाधनों में साझेदारी जैसे स्थानीय पुस्तकालय का उपयोग, उपयोग में लाई गई पाठ्य-पुस्तकों और वाचन सामग्री का संग्रह उन बच्चों को वितरित करके जो स्वयं इन्हें खरीद नहीं सकते।
(iii) क्रियान्वयन प्रणाली का पर्यवेक्षण आदि की मॉनीटरिंग करने के लिए।
(iv) समुदाय और सरकार के बीच सहसम्बन्ध बरकरार रखने के लिए।
पाठ्यचर्या क्रियान्वयन हेतु विद्यालय ही ऐसी एजेन्सियाँ हैं जो पाठ्यचर्या को संचालित करती हैं और छात्रों के विकास से भी सीधे-सीधे जुड़ी होती हैं। इसलिए पहली से बारहवीं कक्षा तक के विद्यालयों को ही मूल्यांकन की योजना व युक्ति विकसित करनी होगी। इससे देशकार्य (असाइनमेंट), परीक्षण और परीक्षाओं की बारम्बारता भी शामिल होगी। विशिष्ट संज्ञानात्मक और सह-संज्ञानात्मक क्षेत्रों की मात्रा या संख्या भी तय करनी होगी।
इसके साथ ही जिस प्रकार के परीक्षण दोनों ही क्षेत्रों के लिए लागू किए जाएंगे उनके अधिगम प्रतिफलों का आकलन किया जायेगा, उनका अभिलेख रखा जायेगा और परिणामों की रिपोर्ट की जायेगी। कक्षा में अध्ययन-अध्यापन का स्तर ऊंचा उठाने और शिक्षकों को मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार करने हेतु क्रियात्मक शोध करने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विद्यालय उपचारात्मक सामग्री का विकास भी करेंगे। स्कूलों व कक्षाओं के स्थान का अधिकतम उपयोग शिक्षा के संसाधनों के रूप में किया जा सकेगा तथा बच्चों को उन गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकता है जो स्कूलों और कक्षा की पढ़ाई को आकर्षक बनायें। विद्यालय सामाजिक स्थान होते हैं अतः यहाँ समानता का मूल्य व सभी कामों के प्रति सम्मान कभी बेहद महत्त्वपूर्ण है।
स्कूल की पाठ्यचर्या में कुछ ऐसे अनुभव भी होते हैं जिनसे बच्चे अपनी एकल व सामाजिक जिम्मेदारियों से भी वाकिफ होते हैं। अतः सार्वजनिक स्थल के रूप में स्कूल में समानता, सामाजिक विविधता व बहुलता के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए, साथ ही बच्चों के अधिकारों और उनकी गरिमा के प्रति सजगता का भाव होना चाहिए। इन मूल्यों को सजगतापूर्वक स्कूल के दृष्टिकोण का हिस्सा बनाया जाना चाहिए और उन्हें स्कूली व्यवहार की नींव बनना चाहिए। इस सन्दर्भ में ‘एक समान स्कूल’ या ‘कॉमन स्कूल प्रणाली’ काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है।
राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा मूल्यांकन सुधारों को लागू करने के पीछे उद्देश्य यह होगा कि ये बोर्ड न केवल स्वयं द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता, वैधता और प्रबन्धन में सुधार करें बल्कि विद्यालयी मूल्यांकन की गुणवत्ता में भी सामान्य सुधार करें। इसके अतिरिक्त बोर्डों की यह जिम्मेदारी भी होगी कि वे शैक्षिक उद्देश्यों की पुष्टि और शिक्षण के जटिल स्थलों की पहचान का काम परीक्षा परिणामों के विश्लेषण के माध्यम से करें।
विभिन्न बोर्डों के पास जो विशेषता है वह अलग-अलग विद्यालयों को गुणवत्तापूर्वक परीक्षण सामग्री बनाने के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती, इसलिए वे ऐसी सामग्री के नमूने बनाकर विद्यालयों को उपलब्ध करायें। बोर्डों को विद्यालयों में शिक्षकों के क्षमता-संवर्द्धन की दृष्टि से शैक्षिक मूल्यांकन में शिक्षक प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित करने होंगे। बोर्डों को शैक्षिक मूल्यांकन के क्षेत्र में शोध और उपलब्धि-सर्वेक्षण कराना चाहिए ताकि सेंसस जैसे आँकड़े प्राप्त हो सकें और उनके निष्कर्ष विद्यालयों को उपलब्ध करा दिये जायें ताकि विद्यालय उनके गुण-दोषों को सही ढंग से जान सकें।
प्रश्न 4 (iv) शैक्षिक दृष्टि से राज्यस्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तरीय एजेंसियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
पाठ्यक्रम विकास हेतु विभिन्न राज्यस्तरीय एजेन्सियों जैसे—शिक्षा निदेशालय, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषदें, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान और स्वैच्छिक संगठनों को भी विद्यालयों को उपयुक्त शिक्षण सामग्री का चयन और निर्माण करने और शैक्षिक उद्देश्यों की सम्प्राप्ति एवं उपयुक्त शिक्षण युक्तियाँ अपनाने के लिए सहयोग एवं मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी लेनी होगी। शिक्षा मुख्य रूप से राज्य का विषय है तथा सभी राज्यों की अपनी कुछ स्थानीय आवश्यकताएँ एवं आकांक्षाएँ होती हैं इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा के समान कोर पाठ्यक्रम में भी स्थानीय (राज्य) मुद्दों को समाविष्ट करने का प्रावधान रखा गया है। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया में राज्य शिक्षा विभाग की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है तथा राज्य शिक्षा विभाग के सहयोग के बिना पाठ्यक्रम विकास सम्भव ही नहीं हो पाता है।
भारत में विद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) नई दिल्ली द्वारा तैयार की जाती है जिसे विभिन्न राज्यों के शैक्षिक अभिकरणों द्वारा जैसे विद्यालयी शिक्षा के राजकीय बोर्ड और राज्यों के शिक्षा विभाग (प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए) उन्हें यथावत् या थोड़े बदलाव के साथ स्वीकार कर लेते हैं। फिर भी पाठ्यचर्या निर्माण के कार्य में जुड़ी इन संस्थाओं/अभिकरणों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे इस प्रकार की स्थितियाँ और आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करें जिनसे सभी की अनुभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाठ्यचर्याओं का विकास किया जा सके व वर्तमान पाठ्यचर्याओं की विसंगतियों को दूर किया जा सके। NCERT में इसी उद्देश्य से अलग से ‘पाठ्यक्रम विकास विभाग’ की स्थापना की गई है। यह विभाग अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए प्रयासरत भी है तथा इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं।
राज्य शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषदों को शैक्षिक क्षेत्रों के अलावा मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों में भी योगदान देने की आवश्यकता है। उनमें मौजूद मार्गदर्शन ब्यूरो/ इकाइयों को सन्दर्भ केन्द्र के रूप में बदलकर मजबूत बनाया जा सकता है ताकि ये इकाइयाँ राज्य में शिक्षक-प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक उपकरण परीक्षण, कैरियर साहित्य इत्यादि के क्षेत्र में योगदान दे सकें तथा जिला/ब्लॉक व विद्यालयी स्तरों पर व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की सहायता से परामर्श सेवाओं को उपलब्ध करा सकें।
इसके साथ ही समस्त विद्यालयों व वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पाठ्यचर्या के प्रभावी संचालन की जरूरत को देखते हुए केन्द्र और राज्य दोनों ही सरकारों को न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान करना होगा जिसकी पहल हो चुकी है व इसके अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी विद्यालयों के पास अध्ययन-अध्यापन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों। जैसे- कक्षाओं के लिए कमरों सहित शाला भवन, पेयजल, प्रसाधन सुविधाएँ, शिक्षण सामग्री और सहायक शिक्षण सामग्री। इसके लिए समुदाय के सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के सहयोग से कार्य सम्बद्ध व समयबद्ध कार्य-नीतियाँ तय की जाती हैं ताकि स्वीकृत पद संख्या की अपर्याप्तता, स्वीकृत पदों को भरने में विलम्ब, शिक्षकों को अन्य सरकारी कामों में लगाकर शिक्षण अवधि के समय की हानि, न्यूनतम स्कूल दिवसों का गम्भीर और शाश्वत समस्याओं का निराकरण किया जा सकें।
अध्यापक शिक्षा संस्थाएँ – जो संस्थाएँ देश में सेवा पूर्व शिक्षकों से शिक्षा के लिए जिम्मेदार हैं वे मूल्यांकन सुधारों के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। इसके लिए वे अपनी पाठ्यचर्याओं में मूल्यांकन को एककेन्द्रिक घटक बना सकती हैं और प्रचलित प्रणाली की अच्छी तरह समीक्षा कर सकती हैं। ये संस्थाएँ शोधकार्य हाथ में लेने के अतिरिक्त उन शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रबोधन कार्यक्रम संचालित कर सकती हैं जो इन संस्थाओं के आसपास के विद्यालयों में कार्यरत हैं |
पाठ्यचर्या ढाँचे के विस्तृत लक्ष्यों के प्रति विश्वविद्यालयों की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। विद्यार्थियों के विविध सामाजिक, सांस्कृतिक सन्दर्भों और भारत में कक्षा सम्बन्धी जटिलताओं को देखते हुए शिक्षा में ज्ञान के आधार को विस्तृत किया जाना चाहिए। बहु-अनुशासनात्मक व साझे उद्देश्य को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा करना पाठ्यचर्या की संरचना को व्यावहारिक रूप देने के लिए शोध आधार तैयार करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होगा। अतः विश्वविद्यालयों, SCERT और DIET जैसी संस्थाओं को आपस में जोड़ने की भी आवश्यकता है। इससे शिक्षक शिक्षा के अकादमिक कार्यक्रम सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा अपने अन्दर ही शोध की क्षमता विकसित करने का अवसर मिलेगा
राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न एजेंसियों का दायित्व निम्नलिखित है-
(i) विद्यालयी शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए प्रत्येक पाठ्यचर्या क्षेत्र में अपेक्षित उपलब्धि स्तर तय करना।
(ii) बालकेन्द्रित, गतिविधि उन्मुखी और दक्षता आधारित अध्ययन-अध्यापन सामग्री के लिए अवधारणात्मक सामग्री और उसके नमूने तैयार करवाना।
(iii) संज्ञानात्मक और सह-संज्ञानात्मक अधिगम प्रतिफलों के पब्लिक आकलन के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का निर्माण करवाना और उन्हें राज्यस्तरीय एजेन्सियों को उपलब्ध करवाना।
(iv) मुख्य संसाधन व्यक्तियों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम का संचालन करना
(v) विभिन्न बोर्डों के लिए प्रश्न-पत्र निर्माताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
(vi) अभिलेख रखने और परिणामों की रिपोर्ट देने के लिए किसी संचार तन्त्र की कल्पना करना तथा उसके विषय में परामर्श देना।
(vii) अधिगम प्रतिफलों के मूल्यांकन के लिए बेहतर तरीकों और साधनों की खोज हेतु शोध करवाना।
(viii) सेन्सस जैसे आँकड़े प्राप्त करने के लिए उपलब्धि सर्वेक्षण करना ।
(ix) सूचना का प्रसार करना।
(x) उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों को लाभ देने के लिए मार्गदर्शन व परामर्श की ऐसी व्यवस्था करना जो इन छात्रों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, दृष्टिकोण योग्यता व प्रकृति के अनुरूप हो।
अध्यापक शिक्षा संस्थाएँ – जो संस्थाएँ देश में सेवापूर्ण शिक्षकों की शिक्षा के लिए जिम्मेदार हैं वे मूल्यांकन सुधारों के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। इसके लिए वे अपनी पाठ्यचर्याओं में मूल्यांकन को एक केन्द्रिक घटक बना सकती हैं और प्रचलित प्रणाली की अच्छी तरह से समीक्षा कर सकती हैं। वे संस्थाएँ शोधकार्य हाथ में लेने के अतिरिक्त उन शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रबोधन कार्यक्रम संचालित कर सकती हैं जो इन संस्थाओं के आसपास के विद्यालयों में कार्यरत हैं।
महिला और बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खेल एवं युवा मामलों का विभाग, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, आदिवासी मामलों का विभाग, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण विभाग, संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, पंचायती राज्य संस्थाएँ आदि ऐसे विभाग हैं जो बच्चों के विकास एवं कल्याण में रुचि रखते हैं। ये सभी विभाग बच्चों और शिक्षकों की शिक्षा को समृद्ध बनाने में सक्षम हैं। पाठ्यचर्या के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित कर सके।
प्रश्न 5 (i) पाठ्यक्रम को स्वरूप प्रदान करने में अनुभवी शिक्षकों को महत्त्व दिया जाना चाहिए, क्यों? अपना मत दीजिए।
अध्यापक का पाठ्यक्रम के दोनों पक्षों अर्थात् निर्माण में तथा क्रियान्वयन में विशेष महत्त्व है। पाठ्यक्रम शिक्षा प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण अंग है। शिक्षा के उद्देश्य तभी सार्थक होते हैं, जबकि पाठ्यक्रम का निर्माण तथा क्रियान्वयन प्रभावपूर्ण ढंग से हो और यह निर्माण तथा क्रियान्वयन प्रभावपूर्ण ढंग से तभी हो सकता है, जबकि अध्यापक सजग तथा जागरूक हो और उत्साह एवं लगन के साथ इस कार्य में भाग ले ।
आदर्श पाठ्यक्रम तो वही है जो प्रत्येक छात्र का सर्वांगीण विकास कर सके, परन्तु ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण तो कोरी कल्पना है। यह कार्य तभी सम्भव है जबकि प्रत्येक अध्यापक, प्रत्येक छात्र के लिए अलग-अलग पाठ्यक्रम का निर्माण करें। वैसे विकसित देशों में इस प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं जिनमें शिक्षा तथा पाठ्यक्रम बाल-केन्द्रित हों। भावार्थ यह है कि बालक की रुचियों, अभिरुचियों तथा शक्तियों के विकास के लिए अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हों।
प्रायः अध्यापकों के मन में यह धारणा प्रचलित है कि पाठ्यक्रम निर्माण में उनका कोई योगदान नहीं लिया जाता। शिक्षाविद् पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं और उसके पश्चात् स्कूलों, अध्यापकों तथा छात्रों पर पाठ्यक्रम थोप दिया जाता है। सरसरी तौर पर सोचने से तो इस धारणा में बल दिखायी देता है, परन्तु गम्भीरतापूर्वक सोचने और चिन्तन करने पर यह तथ्य ठीक प्रतीत नहीं होता है। पाठ्यक्रम निर्माण के लिए भिन्न-भिन्न विषयों तथा क्रियाओं के लिए कई समितियों का गठन किया जाता है। इन समितियों में शिक्षाविदों के साथ-साथ विषय अध्यापक भी होते हैं। प्रत्येक शिक्षाविद् तथा प्रत्येक अध्यापक को पाठ्यक्रम प्रक्रिया में सम्मिलित करना असम्भव है। प्रत्येक वर्ग के कुछ प्रतिनिधि ही लिए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया का दूसरा चरण होता है अध्यापकों के लिए गोष्ठियाँ, कर्मशाला आदि का आयोजन करना। विषय समितियों द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम में इस प्रकार से अध्यापकों की राय भी राय भी ली जाती है। कई बार पाठ्यक्रम को नमने के तौर पर कुछ स्कूलों में लागू किया जाता है तथा अनुभवों के आधार पर पाठ्यक्रम में संशोधन किये जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम के निर्माण में अध्यापकों का भी हाथ होता है।
पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में तो प्रत्येक अध्यापक का हाथ होता है। अध्यापक पाठ्यक्रम से दिशा-निर्देश प्राप्त करता है, परन्तु यह उस पर निर्भर है कि वह पाठ्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में कितना उत्साह दिखाता है, पाठ्यक्रम में दिये गये कार्य को करने की कई विधियाँ हो सकती हैं। अध्यापक को अपनी सूझबूझ से यह निर्णय लेना होता है कि किस विधि से पाठ्यक्रम में दी गई विषय-वस्तु क्रियाओं का प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वयन किया जा सकता है। उसे यह सोच-विचार करना होता है कि किस प्रकार के प्रश्न छात्रों जागें पूछे जो जिनसे वे नयी पाठ्य-वस्तु का दैनिक जीवन या पहले पढ़ी गई पाठ्य-वस्तु के साथ तारतम्य स्थापित कर सकें। किस प्रकार के उदाहरण सहायक हो सकते हैं। किस प्रकार की दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है? इस प्रकार अध्यापक को पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में पर्याप्त स्वतन्त्रता होती है
राज्य सरकारें विभिन्न स्कूल-विषयों के लिए विषय अध्यापक संस्थाएँ बनाने के कार्य को प्रोत्साहन दें। इससे पहल-शक्ति को और प्रयोग करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा और अधिक अच्छी शिक्षण सामग्रियों और शिक्षण तथा मूल्यांकन की सुधरी तकनीकों के प्रयोग के द्वारा पाठ्यचर्या को संशोधित और उन्नत बनाने में सहायता मिलेगी। राज्य स्कूल शिक्षा बोर्डों के माध्यम से काम करने वाले राज्य शिक्षा विभाग की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे विषय-अध्यापक संस्था की सहायता करें ताकि विषय अध्यापक संस्थाएँ नियतकालिक सेमिनार और सभाएँ चलाया करें और अपनी ही पत्रिकाएँ निकालें, जिनमें से अधिकतर स्वभावतः प्रान्तीय भाषाओं में होंगी। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् को चाहिए कि राज्य स्तर की प्रत्येक संस्था के बीच समन्वय स्थापित करे, अखिल भारतीय विषय अध्यापक संस्थाएँ बनाने में और भारत में सब जगह अध्यापकों के उपयोग के लिए हिन्दी और अंग्रेजी में राष्ट्रीय स्तर पर पत्रिकाएँ निकालने में सहायता दे।
इसके अतिरिक्त शिक्षक को नये पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ समझाना भी आवश्यक है ताकि . शिक्षक की क्षमता विकसित की जा सके, शिक्षण कौशल में उन्नति लायी जा सके और आज की परिवर्तित परिस्थिति से सम्बन्धित पढ़ाने और सिखाने की प्रक्रिया को अधिक सूक्ष्मता से समझा जा सके। इसलिए शिक्षकों को संशोधित पाठ्यचर्या में अनुस्थापित (ओरियन्टेड) करने के लिए अन्तः सेवा शिक्षा का एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया जाए, जिनमें सेमिनार और पुनश्चर्या – पाठ्यक्रम का भी आयोजन हो।
पाठ्यचर्या शिक्षा का एक गतिशील साधन है। शीघ्रता से परिवर्तित संसार में यह आवश्यक हो जाता है कि शैक्षिक संस्थाएँ भी पाठ्य-वस्तु को नवीन आवश्यकताओं तथा तकनीकों के सन्दर्भ में बदलें। इस दिशा में निम्नलिखित सुझाव दिये जा रहे हैं-
1. उच्च पाठ्यक्रम चालू करने की शर्तें –
राज्य स्कूल शिक्षा बोर्डों को शिक्षकों की योग्यता और क्षमता तथा आवश्यक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किसी विषय में उच्च पाठ्यक्रम लागू करने की शर्तें निर्धारित कर देनी चाहिए। जो स्कूल इन शर्तों को पूरा करें, उन्हें उच्च पाठ्यक्रम चालू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। दूसरे स्कूल तो केवल साधारण ही पाठ्यक्रम चलाएँ। उच्च पाठ्यक्रम लागू करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने पड़ेंगे-
(i) यह जरूरी नहीं है कि स्कूल सभी विषयों में उच्च पाठ्यक्रम अपनाएँ। शुरू-शुरू में एक या दो विषय लिए जा सकते हैं और फिर धीरे-धीरे सुविधा के अनुसार सुनियोजित कार्यक्रम के रूप में और अधिक विषय या सारा पाठ्यक्रम समेटा जा सकता है।
(ii) जिस स्कूल में उच्च पाठ्यक्रम नहीं अपनाया गया हो, वहाँ अगर छात्र चाहें तो उन्हें निजी रूप से उच्च पाठ्यक्रम के लिए तैयार करने की छूट होनी चाहिए।
(iii) स्कूल शिक्षा बोर्ड की बाहरी परीक्षाओं में उच्च और साधारण दोनों ही पाठ्यक्रमों में छात्रों की परीक्षा लेने की व्यवस्था करनी चाहिए।
(iv) प्रारम्भ में जो स्कूल उच्च पाठ्यक्रम अपनाने को तैयार हों (या सहायता देने पर थोड़े ही समय में तैयार हों) उनमें विज्ञान, गणित, भाषा जैसे कम से कम, कुछ विषयों में उच्च पाठ्यक्रम लागू किये जा सकते हैं।
(v) कालान्तर में योग्य शिक्षक उपलब्ध कराकर और आवश्यक सुविधाएँ देकर अधिकाधिक स्कूलों को उच्च पाठ्यक्रम अपनाने में सहायता दी जानी चाहिए। प्रतिवर्ष इस प्रकार के ‘आकांक्षी’ स्कूल खोज निकालने चाहिए और उन्हें ‘उच्च’ पाठ्यचर्या के निर्माण के लिए आवश्यक सहायता दी जानी चाहिए। इस सहायता का एक आवश्यक अंग नये पाठ्यक्रमों के अनुसार शिक्षण देने में समर्थ शिक्षक तैयार करना है।
2. उच्च पाठ्यचर्याओं को क्रमिक रूप से लागू करना-इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड, उच्च पाठ्यक्रम बनाकर क्रमिक कार्यक्रम के रूप में अनेक वर्षों से उन्हें सभी स्कूल और विषयों में लागू करें। इस प्रयोजन के लिए बोर्ड को उच्च और साधारण दो पाठ्यक्रम बनाने चाहिए। सामान्य पाठ्यक्रम सभी स्कूलों के लिए समान होना चाहिए। उच्च पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, जिसे इस समय केवल अच्छे स्कूल ही अपना सकें, लेकिन वह कुछ समय बाद सम्भवतः साधारण पाठ्यक्रम बन जाये।
3. उपलब्ध सुविधाओं से पाठ्यक्रम का सम्बन्ध बैठाना तथा प्रायोगिक पाठ्यक्रम अपनाने के बारे में स्कूलों को स्वतन्त्रता- पाठ्यक्रम का शिक्षकों की कोटि, स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं और छात्रों की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के अनुकूल उनकी आवश्यकताओं से सम्बन्ध बैठाना चाहिए। इन विषयों की दृष्टि से हर संस्था में बड़ा अन्तर होता है। परिणामतः औसत स्कूल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाया गया राज्य सरकार का एकमात्र पाठ्यक्रम राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं के लिए बेकार सिद्ध हो जाता है। एक ओर वह कमजोर संस्थाओं की पहुँच के बाहर सिद्ध होता है, तो दूसरी ओर अच्छी संस्थाओं के लिए उसका स्तर बहुत नीचा सिद्ध होता है। समस्या का समाधान इसमें है कि स्कूलों को अपनी ही आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम बनाकर प्रयोग में लाने और उन्हें उन्नत बनाने के लिए एक-दूसरे से होड़ करने दिया जाये।
4. पाठ्य-पुस्तकें और शिक्षण साधन तैयार करना – पाठ्यचर्या में सुधार के किसी भी प्रयत्न की सफलता का आधार उचित पाठ्य-पुस्तकें, शिक्षक-गाइडें और पढ़ने और सीखने की अन्य सामग्रियाँ हैं। ये चीजें स्कूल के हित को ध्यान में रखकर नये कार्यक्रमों की विषय-वस्तु और उनके उद्देश्य निर्धारित करती हैं और छात्र के वास्तविक साधन होने के कारण प्रस्तावित परिवर्तनों को सारवान बनाती हैं।
5. पाठ्यचर्या में अनुसंधान-व्यवस्थित रूप से पाठ्यचर्या के सम्बन्ध में अनुसंधान किया जाए, विशेषज्ञों की खोजों के आधार पर समन्वित सुधार कार्यक्रम के रूप में संशोधन किया जाए। ऐसे अनुसंधान की सुविधाएँ विश्वविद्यालयों, माध्यमिक शिक्षण कॉलेजों, राज्य की शिक्षा-संस्थाओं और राज्य के स्कूल शिक्षा बोर्डों में उपलब्ध होनी चाहिए। यदि राज्य शिक्षा-संस्थाओं के निकट सहयोग में काम कर सकें, तो और भी अच्छा हो ।
प्रश्न 5 (ii) पाठ्यक्रम निर्माण में ज्ञान के चयन एवं प्रस्तुतीकरण का मापदण्ड बताइए।
वर्तमान में मानवीय ज्ञान के वृद्धि की दर बहुत अधिक तीव्र हो गई है। ज्ञान का प्रत्येक क्षेत्र संसार को देखने का एक अलग दृष्टिकोण देता है जिससे संसार से जुड़ने और उसमें कर्म करने का नजरिया भी मिलता है। ज्ञान के ये क्षेत्र अतीत में दिए गए लोगों के योगदान से विकसित हुए हैं और आज भी बढ़ रहे हैं। ये क्षेत्र अपनी संरचना और मुद्दों की प्राथमिकता में भी बदले हैं। इनको सीखने में कई प्रकार की बौद्धिक क्षमताएँ और ज्ञान-अर्जन के तरीके भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे—सुस्पष्ट तर्क व अभिव्यक्ति प्रमाण की खोज एवं उसका मूल्यांकन अनुभव पर आधारित उपलक्षित ज्ञान, समन्वय, अवलोकन एवं व्यावहारिक सम्बद्धता एवं मुद्दों को सम्बोधित किया जा सके व काम करने की दिशा तय हो सके।
लगभग तीन सौ वर्ष पूर्व प्रसिद्ध शिक्षाविद् कमेनियस ने एक ऐसा विषय कोष तैयार करने का विचार किया था जिसमें सम्पूर्ण ज्ञान समा जाये। यद्यपि उनकी आकांक्षा पूर्ण नहीं हो सकी, किन्तु उस समय यह कार्य कठिन होते हुए भी असम्भव नहीं माना गया था। इन तीन शताब्दियों में ज्ञान के भण्डार में इतनी अधिक वृद्धि हो गई है कि उसे हजारों पुस्तकों में प्रस्तुत कर सकने का विचार भी तर्कसंगत नहीं हो सकता है। एक सामान्य अनुमान के अनुसार सन् 1901 में जितना ज्ञान था वह सन् 1950 तक तीन गुना हो गया तथा 1950 के बाद प्रत्येक दस वर्ष में पुनः दुगुना होता जा रहा है। वर्तमान में ज्ञान का विस्तार इतना अधिक हो गया है कि कोई व्यक्ति यदि किसी, एक ही विषय को सौ वर्ष तक पढ़ता रहे तो वह उस विषय का सामान्य-ज्ञान रखने वाला व्यक्ति कहलाने का अधिकारी हो सकता है। वर्तमान ज्ञान को ही ग्रहण कर सकने की क्षमता के सन्दर्भ में प्रखर बौद्धिक क्षमता के धनी व्यक्ति लाला हरदयाल जी ने कहा कि “ज्ञान का भण्डार यदि एक विशाल सागर है तो मानव मस्तिष्क एक छोटी बाल्टी के समान हैं जो उसमें से एक सीमित अंश ही भरकर निकाल सकता है।”
भारत में हमने परम्परागत रूप से पाठ्यचर्या निर्धारण में विषय आधारित दृष्टिकोण अपनाया है जो केवल विषयों पर आधारित होता है। यह तरीका ज्ञान को पाठ्य-पुस्तकों में एक ‘पुलिंदे’ की तरह प्रस्तुत करता है जिसके साथ विषय क्षेत्रों से जुड़ी योग्यता को परीक्षण के लिए दी जाने वाली परीक्षाओं की विधि भी दी जाती है तथा उस विषय क्षेत्र में दक्षता को जाँचने हेतु अंक भी दिये जाते हैं। इसी कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी कई समस्याएँ आ गई हैं।
प्रथम, ज्ञान के जो स्वरूप पाठ्य- पुस्तकों के अन्तर्गत नहीं आते या जिनका मूल्यांकन अंकों के आधार पर नहीं हो सकता, उनको एक तरफ करके ‘अतिरिक्त’ या ‘पाठ्य-विषयेत्तर’ करार कर दिया जाता है जबकि उन्हें पाठ्यचर्या का समेकित अंग होना चाहिए। ज्ञान के अन्य रूप जैसे शिल्प व खेलकूद, जो कौशल सौन्दर्यबोध, चतुराई, रचनात्मकता, समूह में काम करने की क्षमता आदि की दृष्टि से बेहद समृद्ध होते हैं, पूरे छूट जाते हैं।
दूसरे, विषयों का आपस में कोई तालमेल नहीं होता है बिल्कुल अपरिवर्तनीय उपखण्ड बन जाते हैं इसलिए ज्ञान भी समेकित और जुड़ा हुआ लगने की बजाय खण्डित लगता है। बच्चे की दुनिया को देखने के दृष्टिकोण की बजाय ये विषय ही ज्ञान के आरम्भ बिन्दु बन जाते हैं और स्कूली ज्ञान व बाहरी ज्ञान के बीच एक सीमा रेखा खिंच जाती है।
तीसरा, पहले से मौजूद ज्ञान को ज्यादा तरजीह दी जाती है जिसमें बच्चे की खुद ज्ञान सृजित करने और इस प्रक्रिया के नए तरीके खोजने की क्षमता नष्ट हो जाती है। सूचना, ज्ञान से ज्यादा महत्त्वपूर्ण हो जाती है, सूचना को प्राथमिकता मिल जाती है, जिससे भारी-भरकम पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण होता है। यान्त्रिक विधि से दोहराने की पद्धति और प्रश्नों के उत्तर देने पर जोर दिया जाता है न कि समझ बढ़ाने या समस्या सुलझाने पर। ज्ञान को सूचना समझने की इस पद्धति के कारण पाठ्यचर्या में याद करने के लिए कितने ही तथ्यों का बोझा बढ़ा दिया जाता है
।
चौथी समस्या का सम्बन्ध नए विषयों को शामिल करने से है। यह एक महत्त्वपूर्ण जरूरत है कि विषय समाज के समकालीन मुद्दों को सम्बोधित करें लेकिन इससे एक अनुचित पद्धति यह बन गई है कि स्कूली पाठ्यचर्या में इन मुद्दों को सम्बोधित करने के लिए नए विषय बना दिए जाते हैं और साथ ही उसकी पाठ्य-पुस्तकों और मूल्यांकन के तरीके भी बना दिये जाते हैं। अगर पहले से मौजूद विषयों और चल रही गतिविधियों के द्वारा इनको पाठ्यचर्या में शामिल किया जाए तो इन मुद्दों को कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से सम्बोधित किया जा सकता है जिसमें ज्ञान के अवांछनीय विखण्डन को बढ़ावा न मिल सके।
पाँचवीं समस्या पाठ्यचर्या में शामिल करने के लिए ज्ञान के चयन के सिद्धान्तों के बारे में है। ये सिद्धान्त ठीक से बने ही नहीं हैं। विकासात्मक पहलुओं के दृष्टिकोण से उपयुक्तता पर, विभिन्न कक्षाओं में जुड़ाव और तार्किक क्रमिकता एवं गति पर सोच-विचार नहीं किया गया है। ऐसी अवधारणाएँ विषयों की सीमाओं को लाँघती हैं। उदाहरणार्थ- माध्यमिक स्कूल में गणित एवं भौतिकी की अवधारणाएँ, उन्हें एक-दूसरे से जोड़ा नहीं जाता है
अतः ज्ञान के चयन के सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि आज ज्ञान की सीमाओं का काफी विस्तार हुआ है इसलिए यह आवश्यक है कि पाठ्यचर्या में क्या शामिल किया जाए, इसका चुनाव किया जाए। प्रासंगिकता इस सन्दर्भ में काफी व्यावहारिक तथ्य माना जा सकता है। यदि चुनाव व्यावहारिक न हो तो बच्चों के वर्तमान के ज्ञान-निर्माण में यह बिल्कुल सहायक नहीं होता है इसलिए किसी भी तरह यह ज्ञान उसके भविष्य निर्माण के काम नहीं आता। अभिरुचि भी एक उपयोगी तरीका हो सकता है लेकिन यह इस सरलीकरण पर आधारित नहीं होना चाहिए कि बच्चे को किस चीज में आनन्द आता है, मसलन कार्टून और खेलकूद । कोशिश यह होनी चाहिए कि बच्चे की रुचि जाग्रत हो और वह उत्साह से काम कर सके। इसके साथ ही ज्ञान के चयन के सन्दर्भ में सार्थकता भी सबसे महत्त्वपूर्ण उपाय है। अगर बच्चा उस गतिविधि या ज्ञान को उपयोगी समझता है तो पाठ्यचर्या में उसे शामिल करने को प्रासंगिक ठहराया जा सकता है।
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि ज्ञान के विशाल भण्डार की अन्तर्वस्तु के स्रोत के रूप में उपलब्धता होने पर जब हम इसके चयन की आवश्यकता का अनुभव करते हैं तो कई तरह की समस्याएँ भी हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाती हैं। जब इस बात पर विचार किया जाता है कि पाठ्यक्रम में क्या-क्या सम्मिलित किया जाए तथा उनका आधार क्या हो, तो इस समय जो प्रमुख प्रश्न उभर कर आते हैं, वे प्रश्न इस प्रकार के होते हैं-
(i) क्या किसी ज्ञान के चयन का आधार प्रमुख रूप से उसकी सांस्कृतिक उपयोगिता होनी चाहिए?
(ii) क्या किन्हीं तत्त्वों का कालजयी होना ही उन्हें पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए पर्याप्त है?
(iii) क्या किसी सामग्री को केवल इसलिए प्रदान की जाए, क्योंकि वह विद्यार्थियों की रुचियों के अनुकूल है ?
(iv) क्या वर्तमान समाज की समस्याओं से सम्बन्धित अन्तर्वस्तु को ही चुना जाये ?
परम्परागत समाजों में तो इन प्रश्नों के सर्वसम्मत अथवा अधिकतम सहमत वाले उत्तर मिल सकते हैं, किन्तु परिवर्तनशील तथा तीव्र गतिमान वर्तमान समाजों में इन प्रश्नों के भिन्न- भिन्न उत्तर होंगे। क्योंकि वर्तमान समाजों में शिक्षा-दर्शन से लेकर अधिगम सिद्धान्तों तक में भिन्नताएँ तो होती ही हैं साथ ही अन्तर्विरोध भी पाये जाते हैं। विभिन्न समाजों में तथा कहीं-कहीं एक ही समाज में ही अन्तर्वस्तु के चयन एवं उनके संगठन को लेकर अलग-अलग उपागम अपनाये जाते हैं। अतः इन प्रश्नों पर विचार करते समय हमें चयन की कुछ सामान्य समस्याओं का भी ध्यान रखना होगा।
प्रश्न 5 (iii) अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर – क्षेत्र का सामान्य अभिप्राय उस परिवेश से है जिसमें सभी घटनाएँ घटित होती हैं। क्षेत्र सिद्धान्तों के अन्तर्गत आने वाले प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं-
1. पूर्णाकारवाद का सिद्धान्त, 2. तलरूप सिद्धान्त, 3. प्रतीक पूर्णाकार सिद्धान्त ।
गेस्टाल्ट का अर्थ समग्र रूप है। पूर्णाकारवाद के अनुसार व्यक्ति किसी क्रिया को आंशिक रूप से नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है। पूर्णाकारवाद के जन्मदाता जर्मनी के मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्दीमर हैं। इस सिद्धान्त का मूल यह है कि जब मानवीय आँख एक के बाद दूसरे दृश्य उद्दीपन को देखती है तो उसकी प्रतिक्रिया ऐसी होती है कि उन उद्दीपनों का रूप युगपत् बनता है। इसी के आधार पर बाद में कोहलर ने सूझ या अन्तर्दृष्टि के सिद्धान्त का विकास किया है। इसके अनुसार व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ लेता है और सहसा उसे ठीक से करना सीख जाता है। वह ऐसा अपनी सूझ के कारण करता है |
तलरूप सिद्धान्त के जन्मजाता कुर्टलेविन ने जीवन के वातावरण को अधिगम का आधार माना है। उसने इन आधारों में आकांक्षा स्तर, उद्देश्य आकर्षण, स्मृति की गति तथा पुरस्कार एवं दण्ड को अधिक महत्त्व दिया है।
प्रतीक पूर्णाकार सिद्धान्त के प्रतिपादक टालमैन की मान्यता है कि मानव का व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है। अतः यह अधिगम के चिन्हों एवं आशाओं को अधिक महत्त्व देता है। इसके अनुसार उद्दीपन में अर्थ उसी समय उत्पन्न होता है, जबकि वह व्यक्ति की आवश्यकता और उद्देश्य पूर्ति में सहायक होते हैं।
अधिगम के उपर्युक्त संज्ञानात्मक सिद्धान्तों के संक्षिप्त विवेचन से यह प्रतीत होता है कि क्षेत्र सिद्धान्त, साहचर्य सिद्धान्त का ही विस्तार है, क्योंकि ये सिद्धान्त भी अधिगम को उद्दीपक अनुक्रिया के सम्बन्धों का ही परिणाम मानते हैं, परन्तु साहचर्य एवं क्षेत्र सिद्धान्तों में प्रक्रिया सम्बन्धी अन्तर है। साहचर्य सिद्धान्त के अन्तर्गत सम्बन्ध स्थापित होने की प्रक्रिया को प्रायः यान्त्रिक माना जाता है, जबकि क्षेत्र सिद्धान्त में इसे जीवन्त तथा क्रियाशील माना जाता है। क्षेत्र सिद्धान्त के मनोवैज्ञानिकों के अनुसार उत्तेजक या उद्दीपन को अनुक्रिया तक पहुँचने से पूर्व मध्यवर्ती क्षेत्र की क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं में से होकर गुजरना पड़ता है तथा जो सम्बन्ध स्थापित स्थापित होता है वह मुख्य रूप से इन्हीं मध्यवर्ती क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं के प्रभाव का ही परिणाम होता है। जिस प्रकार पूर्व में हमने उद्दीपन-अनुक्रिया सिद्धान्त को टेलीफोन व्यवस्था के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया था जिसमें मध्यवर्ती मशीन का कार्य मात्र यान्त्रिक सम्बन्ध स्थापित करने का होता है, उसी प्रकार क्षेत्र सिद्धान्त को ट्रान्जिस्टर रेडियो व्यवस्था के उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत ध्वनि की तरंगें यन्त्र के एक विशिष्ट भाग से टकराती हैं और ध्वनि हमारे कानों तक लाउडस्पीकर के माध्यम से पहुँचती हैं। ऐसे रेडियो में यद्यपि विद्युतीय सम्बन्ध व्यवस्था होती है, किन्तु इसके महत्त्वपूर्ण अंग ट्रान्जिस्टर ही होते हैं जिनसे गुजरकर ऊर्जा पुनर्गठित होकर भिन्न रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार के यन्त्र ध्वनि के संचरण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
इस प्रकार अधिगम का क्षेत्र सिद्धान्त उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच में होने वाली प्रक्रियाओं की संकल्पना पर आधारित है। इसके अनुसार विद्यार्थी को ऐसी सक्रिय ऊर्जा व्यवस्था माना जाता है जो किसी पर्यावरण में स्थित होती है तथा यह पर्यावरण भी अनेक दूसरी सक्रिय ऊर्जा व्यवस्थाओं का संगम होता है। अतः पाठ्यक्रम नियोजकों एवं शिक्षकों को S-R सम्बन्ध स्थापित करते समय उनकी मध्यवर्ती क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं के प्रति भी सजग रहने की आवश्यकता होती है।
प्रश्न 5 (iv) प्रभावशाली पाठ्यक्रम सम्प्रेषण के कारकों की विवेचना कीजिए।
अथवा
प्रभावशाली पाठ्यक्रम सम्प्रेषण में शिक्षक, शिक्षार्थी, विद्यालय एवं समुदाय की भूमिका की विवेचना कीजिए।
उत्तर – पाठ्यक्रम के प्रभावशाली निर्धारक
बाल केन्द्रित पाठ्यक्रम
बालक के स्वाभाविक विकास का अध्ययन करने के पश्चात् उसकी आवश्यकताओं, योग्यताओं, अभिरुचियों तथा रुचियों के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना बाल केन्द्रित पाठ्यक्रम है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम से बालक की बुद्धि, संवेग, शरीर और सामाजिकता के इष्टतम विकास की सम्भावना रहती है। दर्शन के रूप में इस प्रकार के पाठ्यक्रम की संस्तुति रूसो ने की। बाद में इस पर पेस्तालॉजी, फ्रोबेल, ड्यूवी एवं मॉण्टेसरी ने भी बल दिया। भारत में गाँधीजी तथा टैगोर ने बाल- केन्द्रित पाठ्यक्रम को क्रियात्मक रूप देने का प्रयत्न किया।
बाल-केन्द्रित पाठ्यक्रम बनाने के आधार
गाँधीजी ने बाल-केन्द्रित पाठ्यक्रम निर्माण के लिए बालक के तीन प्रकार के वातावरण पर बल दिया और आग्रह किया कि बालक की सारी शिक्षा निम्नलिखित वातावरण पर आधारित हो-
(1) बालक के भौतिक वातावरण पर आधारित पाठ्यक्रम ।
(2) बालक के सामाजिक वातावरण पर आधारित पाठ्यक्रम ।
(3) क्राफ्ट पर आधारित पाठ्यक्रम ।
विदेशों में मुख्यतः तीन प्रकार के बाल-केन्द्रित पाठ्यक्रम अनेक स्कूलों में चलाये जा रहे हैं।
डाल्टन प्रणाली-
इस प्रणाली के अनुसार स्कूल को घर जैसा रूप दे दिया जाता है और कक्षाएँ प्रयोगशालाओं का रूप धारण कर लेती हैं। सीखने वालों को कुछ कार्य दे दिये जाते हैं जो उन्हें एक निश्चित समय में पूरे करने होते हैं। उन्हें इस समय में पूरी छूट होती है कि वे किसी भी विषय के अध्ययन में जितना समय चाहें, लगायें। इस प्रकार प्रत्येक बालक को अवसर मिलता है— अपनी स्वयं की गति से सीखने का और अपनी योग्यतानुसार सीखने का ।
विटेनका प्रणाली-
कारलेटनं वाशबर्न ने इस प्रणाली का आविष्कार किया। इस प्रणाली में जो प्रमुख शिक्षा-सिद्धान्त है, वह यह है कि सीखने वाले को स्वयं अपनी सीखने की गति के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। हर एक उस विषय को जो उसके पाठ्यक्रम में है, सूझ द्वारा सीखने से उत्साहित करना चाहिए। यह प्रणाली डाल्टन प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि इसमें हर सीखने वाले को विभिन्न विषयों में विभिन्न गति से सीखने की स्वतन्त्रता है, जबकि डाल्टन प्रणाली में बालकों को सब विषयों में एक ही स्तर पर रहना पड़ता है। पाठ्य सामग्री इकाई कार्य या उद्देश्य के रूप में संगठित की जाती है और बालक स्वयं अपने सीखने का परीक्षण कर सकता है। इसके पश्चात् ही वह अपने आपको शिक्षक द्वारा दिये जाने वाली परीक्षण के लिए प्रस्तुत करता है। इस प्रकार इस प्रणाली में असफल होने का प्रश्न नहीं उठता।
प्रोजेक्ट प्रणाली- इस प्रणाली में बालकों को प्रोजेक्ट दिये जाते हैं जो बहुधा चार प्रकार के होते हैं-(1) उत्पादक प्रोजेक्ट, (2) उपभोक्ता प्रोजेक्ट, (3) समस्यात्मक प्रोजेक्ट और (4) अभ्यास प्रोजेक्ट ।
कई बालक मिलकर एक प्रोजेक्ट पर कार्य करती हैं और इस प्रकार सीखना व्यक्तिगत योग्यता तथा रुचि पर निर्भर करता है।
प्रोजेक्ट पद्धति में पाठ्यक्रम एक प्रकार से जीवन्त क्रिया बन जाता है। छात्र समस्याओं का प्रयोगात्मक हल ढूँढ़ना सीखते हैं। सामूहिक परियोजनाओं को पूरी कक्षा करती है। पाठ्यक्रम कई परियोजनाओं का समूह बन जाता है। ये परियोजनाएँ छात्र स्वयं चुनते हैं। अध्यापक एक मार्गदर्शक तथा परामर्शदाता का रूप लेता है। परियोजनाओं में पाठ्य विषयों का सार्थक स्वाभाविक सह-सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम से प्रेरणा, प्रयत्नशीलता, रचनात्मक सक्रियता, उत्तरदायित्व, सहकारिता तथा सहिष्णुता आदि गुणों का विकास होता है।
पाठ्यक्रम तथा अध्यापक
अध्यापक का पाठ्यक्रम के दोनों पक्षों अर्थात् निर्माण में तथा क्रियान्वयन में विशेष महत्त्व है। पाठ्यक्रम शिक्षा प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण अंग है। शिक्षा के उद्देश्य तभी सार्थक होते हैं, जबकि
पाठ्यक्रम का निर्माण तथा क्रियान्वयन प्रभावपूर्ण ढंग से हो और यह निर्माण तथा क्रियान्वयन प्रभावपूर्ण ढंग से तभी हो सकता है, जबकि अध्यापक सजग तथा जागरूक हो और उत्साह एवं लगन के साथ इस कार्य में भाग ले ।
आदर्श पाठ्यक्रम तो वही है जो प्रत्येक छात्र का सर्वांगीण विकास कर सके, परन्तु ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण तो कोरी कल्पना है। वह कार्य तभी सम्भव है जबकि प्रत्येक अध्यापक, प्रत्येक छात्र के लिए अलग-अलग पाठ्यक्रम का निर्माण करे। वैसे विकसित देशों में इस प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं जिनमें शिक्षा तथा पाठ्यक्रम बाल-केन्द्रित हों। मतलब यह है कि बालक की रुचियों, अभिरुचियों तथा शक्तियों के विकास के लिए अधिक से अधिक अवसर प्राप्त
पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया तथा अध्यापक
प्रायः अध्यापकों के मन में यह धारणा प्रचलित है कि पाठ्यक्रम निर्माण में उनका कोई योगदान नहीं लिया जाता। शिक्षाविद् पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं और उसके पश्चात् स्कूलों, अध्यापकों तथा छात्रों पर पाठ्यक्रम थोप दिया जाता है। सरसरी तौर पर सोचने से तो इस धारणा में बल दिखायी देता है, परन्तु गम्भीरतापूर्वक सोचने और चिन्तन करने पर यह तथ्य ठीक प्रतीत नहीं होता है। पाठ्यक्रम निर्माण के लिए भिन्न-भिन्न विषयों तथा क्रियाओं के लिए कई समितियों का गठन किया जाता है। इस समितियों में शिक्षाविदों के साथ-साथ विषय अध्यापक भी होते हैं। प्रत्येक शिक्षाविद् तथा प्रत्येक अध्यापक को पाठ्यक्रम प्रक्रिया में सम्मिलित करना असम्भव है। प्रत्येक वर्ग के कुछ प्रतिनिधि ही लिए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया का दूसरा चरण होता है अध्यापकों के लिए गोष्ठियाँ, कर्मशाला आदि का आयोजन करना। विषय समितियों द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम में इस प्रकार से अध्यापकों की राय भी ली जाती है। कई बार पाठ्यक्रम को नमूने के तौर पर कुछ स्कूलों में लागू किया जाता है तथा अनुभवों के आधार पर पाठ्यक्रम में संशोधन किये जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम के निर्माण में अध्यापकों का भी हाथ होता है।
विद्यालय तथा पाठ्यक्रम
पाठ्यचर्या शिक्षा का एक गतिशील साधन है। शीघ्रता से परिवर्तित संसार में यह आवश्यक हो जाता है कि शैक्षिक संस्थाएँ भी पाठ्य-वस्तु को नवीन आवश्यकताओं तथा तकनीकों के सन्दर्भ में बदलें। इस दिशा में निम्नलिखित सुझाव दिये जा रहे हैं-
1. पाठ्यचर्या में अनुसंधान-
व्यवस्थित रूप से पाठ्यचर्या के सम्बन्ध में अनुसंधान किया जाए, विशेषज्ञों की खोजों के आधार पर समन्वित सुधार कार्यक्रम के रूप में संशोधन किया जाए। ऐसे अनुसंधान की सुविधाएँ विश्वविद्यालयों, माध्यमिक शिक्षण कॉलेजों, राज्य की शिक्षा-संस्थाओं और राज्य के स्कूल शिक्षा बोर्डों में उपलब्ध होनी चाहिए। यदि राज्य शिक्षा संस्थाओं के निकट सहयोग में काम कर सकें, तो और भी अच्छा हो।
2. पाठ्य-पुस्तकें और शिक्षण साधन तैयार करना –
पाठ्यचर्या में सुधार के किसी भी प्रयत्न की सफलता का आधार उचित पाठ्य-पुस्तकें, शिक्षक-गाइडें और पढ़ने और सीखने की अन्य सामग्रियाँ हैं। ये चीजें स्कूल के हित को ध्यान में रखकर नये कार्यक्रमों की विषय-वस्तु और उसके उद्देश्य निर्धारित करती हैं और छात्र के वास्तविक साधन होने के कारण प्रस्तावित परिवर्तनों को सारवान बनाती हैं। 1
3. शिक्षकों की अन्तः सेवा शिक्षा-
इसके अतिरिक्त शिक्षक को नये पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ समझाना भी आवश्यक है ताकि शिक्षक की क्षमता विकसित की जा सके, शिक्षण कौशल में उन्नति लायी जा सके और आज की परिवर्तित परिस्थिति से सम्बन्धित पढ़ाने और सिखाने की प्रक्रिया को अधिक सूक्ष्मता से समझा जा सके। इसलिए शिक्षकों को संशोधित पाठ्यचर्या में अनुस्थापित (ओरियन्टेड) करने के लिए अन्तःसेवा शिक्षा का एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया जाए, जिसमें सेमिनार और पुनश्चर्या-पाठ्यक्रम का भी आयोजन हो।
4. उपलब्ध सुविधाओं से पाठ्यक्रम का सम्बन्ध बैठाना तथा प्रायोगिक पाठ्यक्रम अपनाने के बारे में स्कूलों को स्वतन्त्रता-
पाठ्यक्रम का शिक्षकों की कोटि, स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं और छात्रों की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के अनुकूल उनकी आवश्यकताओं से सम्बन्ध बैठाना चाहिए। इन विषयों की दृष्टि से हर संस्था में बड़ा अन्तर होता है। परिणामतः औसत स्कूल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाया गया राज्य सरकार का एकमात्र पाठ्यक्रम राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं के लिए बेकार सिद्ध हो जाता है। एक ओर वह कमजोर संस्थाओं की पहुँच के बाहर सिद्ध होता है, तो दूसरी ओर अच्छी संस्थाओं के लिए उसका स्तर बहुत नीचा सिद्ध होता है। समस्या का समाधान इसमें है कि स्कूलों को अपनी ही आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम बनाकर प्रयोग में लाने और उन्हें उन्नत बनाने के लिए एक-दूसरे से होड़ करने दिया जाये।
5. उच्च पाठ्यचर्याओं को क्रमिक रूप से लागू करना-
इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड, उच्च पाठ्यक्रम बनाकर क्रमिक कार्यक्रम के रूप में अनेक वर्षों में उन्हें सभी
स्कूल और विषयों में लागू करें। इस प्रयोजन के लिए बोर्ड को उच्च और साधारण दो पाठ्यक्रम बनाने चाहिए। सामान्य पाठ्यक्रम सभी स्कूलों के लिए समान होना चाहिए। उच्च पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, जिसे इस समय केवल अच्छे स्कूल ही अपना सकें, लेकिन वह कुछ समय बाद सम्भवतः साधारण पाठ्यक्रम बन जाये ।
समुदाय तथा पाठ्यक्रम
(1) टैक्नोलोजी तथा सांस्कृतिक खाई को पाटना-
औपचारिक शिक्षा पद्धति और देश की समृद्धि तथा विविधतापूर्ण सांस्कृतिक परम्पराओं के बीच विद्यमान खाई को पाटना होगा। आधुनिक टैक्नोलोजी के नशे में नई पीढ़ी की जड़ें भारत के इतिहास और संस्कृति से कट नहीं जानी चाहिए। हर कीमत पर संस्कृति-विहीनता, मानव गुण-विहीनता और अलगाव से बचना होगा। शिक्षा को परिवर्तन उन्मुख प्रौद्योगिकियों और देश की सांस्कृतिक परम्पराओं के सातत्य के बीच संश्लेषण का कार्य करना होगा और शिक्षा इसे बखूबी कर सकती है।
शिक्षा की पाठ्यचर्या तथा प्रक्रियाओं को विविध प्रकार से सांस्कृतिक विषय-वस्तु के जरिए समृद्ध बनाया जायेगा। बच्चों में सौन्दर्य, समन्वय और परिमार्जन की भावना विकसित की जायेगी। समाज के साधन सम्पन्न व्यक्तियों को, उनकी औपचारिक शैक्षिक योग्यता पर ध्यान दिये बिना, शिक्षा की सांस्कृतिक समृद्धि में योगदान देने के लिए आमंत्रित किया जायेगा जिसमें अभिव्यक्ति की साहित्यिक और मौखिक परम्पराएँ शामिल होंगी। सांस्कृतिक परम्पराओं को कायम रखने तथा उन्हें आगे ले जाने के लिए परम्परागत तरीकों से पढ़ाने वाले शिक्षकों की भूमिका को सुदृढ़ किया जायेगा तथा इस कार्य को मान्यता दी जायेगी।
(2) मूल्य शिक्षा का विकास –
सारभूत मूल्यों के गिरते हुए स्तर के प्रति बढ़ती हुई चिन्ता और समाज में बढ़ती हुई कटुता से यह जरूरी हो गया है कि पाठ्यचर्या में पुनर्समायोजन लाया जाए ताकि शिक्षा को सामाजिक, नीतिपरक और नैतिक मूल्य पैदा करने के लिए एक सशक्त साधन बनाया जा सके।
(3) सार्वभौमिक भावना का निर्माण-
हमारे सांस्कृतिक और विराट समाज में शिक्षा के जरिए विकसित किये जाने वाले मूल्यों में सार्वभौमिक भावना होनी चाहिए और इनसे हमारे लोगों में एकता और एकीकरण की भावना विकसित होनी चाहिए। इस प्रकार की मूल्य शिक्षा रूढ़िवाद, धार्मिक कट्टरता, हिंसा, अन्धविश्वास और भाग्यवाद को समाप्त करेगी।
इस निर्णायक भूमिका के अतिरिक्त, मूल्य शिक्षा की एक गहन और ठोस विषय-वस्तु हमारी विरासत, राष्ट्रीय और सार्वभौमिक उद्देश्य और विचारों पर आधारित हो। इसमें इस पहलू पर मुख्य रूप से जोर दिया जाना चाहिए।
(4) भाषाएँ –
1968 की शिक्षा नीति में भाषाओं के विकास पर विस्तृत रूप से विचार किया गया था। इसके अनिवार्य उपबन्धों पर अब विचार करने की जरूरत नहीं है और ये आज भी पहले की तरह आवश्यक हैं, तथापि 1968 की नीति के इस भाग का कार्यान्वयन अनियमित रहा है। इस नीति को और अधिक तेजी और सार्थकता से कार्यान्वित किया जायेगा।
(5) मीडिया तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग-
शैक्षिक प्रौद्योगिकी को औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही क्षेत्रों में लाभदायक सूचना और शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा पुनः प्रशिक्षण के प्रसार के लिए लाया जायेगा ताकि गुणवत्ता को सुधारा जा सके, कला और संस्कृति की जागरूकता को प्रखर किया जा सके और अपनाये जाने योग्य मूल्य पैदा किये जा सकें। उपलब्ध व्यवस्थापन का अधिक से अधिक लाभ उठाया जायेगा। जिन गाँवों में विद्युत नहीं पहुँची है वहाँ बैटरी अथवा सौर- ऊर्जा व्यवस्था से कार्यक्रम चलाये जायेंगे।
प्रश्न 6 (i) ‘संरचनावादी उपागम’ की व्याख्या कीजिए।
उत्तर –
वर्तमान में ‘शिक्षा’ संरचनावादी क्रिया है। संरचनात्मक शिक्षा में क्षमताओं का विकास करना भी जोड़ा जाता है, किन्तु क्षमताओं में कई प्रश्न शामिल हैं। अच्छी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए केवल पाठ्यक्रम में कुछ नवाचारों का समावेश करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आज के सूचना प्रधान युग में ज्ञान को भली प्रकार किस प्रकार प्रदान किया जाये यह सोचना भी है, जिसका प्रत्युत्तर हमें ज्ञान के संरचनावादी उपागम में मिलता है। इसका तात्पर्य है कि पाठ्यचर्या के सभी सन्दर्भों को बच्चों की सक्रियता व रचनात्मक सामर्थ्य को पोषित व सम्वर्द्धित करनेवाली होना चाहिए। उसका दुनिया में वास्तविक तरीकों से सम्बन्ध बैठाने, दूसरों से जुड़ने की उनकी मूल अभिरुचि को प्रेषित करना चाहिए। संरचनावादी उपागम के अनुसार, सीखना अपने आप में एक सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है, अतः इसे संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में पूर्ण करना चाहिए।
संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। विद्यार्थी सक्रिय रूप से पूर्व प्रचलित विचारों में उपलब्ध सामग्री, गतिविधियों के आधार पर अपने लिए ज्ञान की रचना करते हैं (अनुभव)। उदाहरण के लिए, यातायात व्यवस्था को पाठ या चित्र या दृश्य सामग्री का उपयोग करते. हुए पढ़ाने तथा उस पर विद्यार्थियों में चर्चा कराने से उनमें यातायात व्यवस्था सम्बन्धी ज्ञान के निर्माण मैं मदद की जा सकती है। बच्चों के संज्ञान में अध्यापकों की भूमिका को भी रचनावादी परिप्रेक्ष्य में बढ़ाया जा सकता है। यदि वे ज्ञान निर्माण की उस प्रक्रिया में ज्यादा सक्रिय रूप से शामिल हो जाएँ जिसमें बच्चे व्यस्त हैं।
इसी आधार पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को ‘रचनावादी’ या ‘निर्माणवादी’ परिप्रेक्ष्य में समझा जाता है जैसे कि एन.सी.एफ. 2005 में इसकी रचनावादी शिक्षा की वकालत की गई है। इस दृष्टिकोण से यह अर्थ सामान्य तौर पर निकलता है कि हर बच्चा अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करता है। हर बच्चा विलक्षण है और इसलिए उसे न सिर्फ व्यक्तिगत ध्यान की जरूरत है वरन् उसे अपने तरीके से सीखने का मौका मिलना चाहिए इसे प्रदान करना स्कूल व कक्षा की जिम्मेदारी है। रचनावाद की सतही समझ यह अर्थ देती है कि कोई भी बच्चा गलत नहीं समझा जा सकता है। मतलब जो भी बच्चे ने उत्तर दिया, वह उसके दृष्टिकोण से सही है। वैसे रचनावादी पाठ्यक्रम की वकालत कई प्रकार से की जाती है। कुछ लोगों के अनुसार इसके अन्तर्गत स्कूल में पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्य-पुस्तक व किसी भी निर्धारित प्रक्रिया अथवा ढाँचे को नकारा जाता है। इसके अनुसार बच्चों की ज्ञान निर्माण की इच्छा, गति और अनुभव के आधार पर बढ़ना ही ठीक माना जाता है, जबकि कुछ दूसरे शिक्षाविदों के अनुसार इस उपागम हेतु निश्चित पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शिक्षा की प्रक्रिया की रचना अधिगमकर्त्ता के पूर्व अनुभवों को केन्द्र में रखकर की जानी चाहिए।
समावेशी शिक्षा नोट्स
| विषय | समावेशी शिक्षा नोट्स
Inclusive Education |
| पेपर | 304 |
| विश्वविद्यालय | महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बी.एड तृतीय सेमेस्टर के नोट्स |
| सेमेस्टर | तृतीय सेमेस्टर |
| lnfo | यहा महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बी.एड तृतीय सेमेस्टर के नोट्स के पेपर -304 विषय शिक्षण प्रथम नोट्स दिया गया है | यह विषय सभी स्टूडेंट्स का समान होता है | |