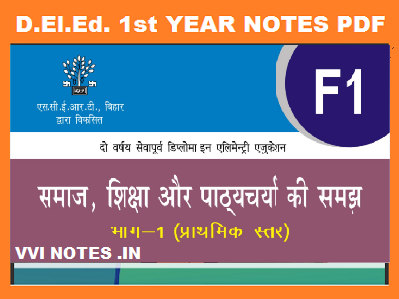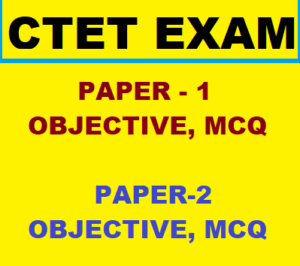समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ
Samaj shiksha aur pathyacharya ki samajh
| विषय | समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ सिलेबस नोट्स क्वेश्चन पेपर प्रश्न उत्तर |
| SUBJECT | Samaj shiksha aur pathyacharya ki samajh |
| SUBJECT | Understanding Of Society,Education And Curriculum |
| COURSE | Bihar D.El.Ed. 1st Year |
| PAPER | First (F 1 ) |
VVI NOTES के इस पेज में बिहार डी.एल.एड 1st ईयर पेपर F 1 समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ सिलेबस , समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ नोट्स , समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ क्वेश्चन पेपर , समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ बुक, समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ गाइड साथ ही टेलीग्राम एवं व्हाट एप्प का लिंक दिया गया है जिससे आप अपने अन्य सहपाठियों से जुड़ सके | और वहा बहुत सारे डी एल एड – CTET सम्बन्धित बूक गाइड pdf प्रप्त कर सके |
समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ सिलेबस
| विषय | समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ |
| TYPE | सिलेबस |
| पेपर कोड | F 1 |
इकाई 1 : बच्चे, बचपन और समाज
* बच्चे तथा बचपन : सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ।
* समाजीकरण की समझ : अवधारणा, कारक तथा विविध सन्दर्भ।।
* बच्चों का समाजीकरण : माता-पिता, परिवार, पड़ोस, जेण्डर एवं समुदाय की भूमिका।
* बाल अधिकारों का सन्दर्भ : उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा के साथ।
इकाई 2 : विद्यालय और समाजीकरण
* शिक्षा, विद्यालय और समाज : अन्तर्सम्बन्धों की समझ।
* विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया : विभिन्न कारकों की भूमिका व प्रभावों की समझ।
* शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय : सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक आधार।
इकाई 3 : शिक्षा और ज्ञान : विविध परिप्रेक्ष्य की समझ
* शिक्षा : सामान्य अवधारणा, उद्देश्य एवं विद्यालयी शिक्षा की प्रकृति ।
* शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार/दृष्टिकोण : दर्शनशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, समाज शास्त्रीय शिक्ष का साहित्य, शिक्षा का इतिहास आदि।
* ज्ञान की अवधारणा : दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। – ज्ञान के विविध स्वरूप एवं अर्जन के तरीके।
इकाई 4 : प्रमुख चिनकों के मौलिक लेखन की शिक्षाशास्त्रीय समझ
* महात्मा गाँधी-हिन्द स्वराज : सामाजिक दर्शन और शिक्षा के सम्बन्ध को रेखांकित करते हुए। –
* गिजुभाई बधेका-दिवास्वप्न : शिक्षा में प्रयोग के विचार को रेखांकित करते हुए।
* रवीन्द्रनाथ टैगोर-शिक्षा : सीखने में स्वतन्त्रता एवं स्वायत्तता की भूमिका को रेखांकित करते हुए।
* मारिया माण्टेसरी-ग्रहणशील मन पुस्तक से ‘विकास के क्रम’ शीर्षक अध्याय : बच्चों के सीखने के सम्बन्ध में विशेष पद्धति को रेखांकित करते हुए।
* ज्योतिबा फुले-हण्टर आयोग (1882) को दिया गया बयान : शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक असमानता को रेखांकित करते हुए।
* डॉ. जाकिर हुसैन–शैक्षिक लेख : बालकेन्द्रित शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए।
* जे. कृष्णमूर्ति- ‘शिक्षा क्या है’ : सीखने-सिखाने में संवाद की भूमिका को रेखांकित करतेहुए।
* जॉन डीवी–शिक्षा और लोकतन्त्र से ‘जीवन की आवश्यकता के रूप में शिक्षा’ शीर्षक लेख : शिक्षा और समाज की अन्तक्रिया को रेखांकित करते हुए।
इकाई -5 पाठय चर्या की समझ : बच्चो तथा समाज के सन्दर्भ में
* पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम : अवधारणा तथा विविध आधार।।
* बच्चों की पाठ्य-पुस्तकें : शिक्षा, ज्ञान एवं समाजीकरण के माध्यम के तौर पर। .
* स्थानीय पाठ्यचर्या की समझ।
समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ नोट्स
| विषय | समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ प्रश्न – उत्तर |
| TYPE | नोट्स |
| पेपर कोड | F 1 |
लघु उत्तरीय प्रश्न
(Short Answer Type Questions)
प्रश्न 1. समाज का अर्थ बताइये।
उत्तर – शिक्षा व समाजशास्त्र के सम्बन्ध को समझने के लिए समजा का अर्थ समझना अति आवश्यक होता है। इस विषय में हम कह सकते हैं कि जब दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति परस्पर प्रेम, सहानुभूति, मित्रता, सहयोग अथवा इसके विपरीत भावनाओं का अनुभव करने लगते हैं, तो उनके बीच एक समाजिक वातावरण उत्पन्न हो जाता है। इसी सामाजिक वातावरण को ही समाज कहा जाता है।
समाज का निर्माण व्यक्तियों से मिलकर होता है, फिर भी समाजवादियों के अनुसार व्यक्ति की अपेक्षा समाज की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं तथा आदर्शों को अधिक महत्व दिया जाता है। विद्वानों का मानना है कि समाज सामाजिक बन्धनों का एक ऐसा जाल है, जो स्थिर न रहकर सदैव बदलता रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि समाज गतिशील (Dynamic) है। समाज व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण करता है तथा उसे इस बात का ज्ञान कराता है कि वह उसका एक उत्तरदायी नागरिक है। मैकाइवर तथा पेज ने यहाँ पर कहा है कि “मनुष्य समाज पर अपनी सुरक्षा, आराम, पालन-पोषण, शिक्षा तथा अन्य महत्वपूर्ण अवसरों एवं सेवाओं हेतु निर्भर है। यह समाज पर अपने विचारों, स्वप्नों तथा आकांक्षाओं एवं अपने मन और शरीर की बहुत-सी व्याधियों हेतु निर्भर है। उसका समाज में जन्म लेना ही समाज की आवश्यकताओं को अपने साथ लाता है।”
प्रश्न 2. समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्त कीजिए ।
उत्तर- समाजीकरण की प्रक्रिया (Process of Socialization) – समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा बालक को सामाजिक बनाया जाता है। इस प्रक्रिया के अनेक कारक होते हैं जिसमें वे महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित हैं-
(1) बालकों के पालन-पोषण का गहरा प्रभाव सामाजिक प्रक्रिया पर पड़ता है। जिस प्रकार का वातावरण बालक को प्रारम्भिक जीवन में मिलता है तथा जिस प्रकार से माता-पिता बालक का पालन-पोषण करते हैं उसी के अनुसार बालक में भावनायें तथा अनुभूतियाँ विकसित हो जाती हैं। इसका अर्थ यह है कि जिस बालक की देखरेख उचित नहीं होती, वह समाज विरोधी आचरण वाले हो जाते हैं। अतः उचित समाजीकरण हेतु बालक का पालन-पोषण ठीक प्रकार से किया जाना चाहिए।
(2) बालकों को शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक उचित सहानुभूति की आवश्यकता होती है। शैशवावस्था में वह परिवार से सहानुभूति चाहता है, परन्तु किशोरावस्था तक आते-आते बालकों की सहानुभूति से सम्बन्धित समस्यायें तथा क्रियाओं की पूर्ति उनके मित्र करते हैं। इस प्रकार सहानुभूति के द्वारा बालकों में अपनत्व की भावना का विकास होता है।
(3) माता-पिता, परिवार तथा पड़ोस की सहानुभूति द्वारा बालकों में आत्मीकरण की भावना विकसित होती है। जो लोग बालकों को अपना समझकर उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं बालक उन्हीं को अपना समझने लगता है तथा उन्हीं के आदर्शों के अनुसार ही बालक व्यवहार करते हैं।
(4) अनुकरण के अतिरिक्त सामाजिक शिक्षण का भी बालकों के व्यक्तित्व पर तथा समाजीकरण पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सामाजिक शिक्षण का प्रारम्भ परिवार से ही होता है। यहीं पर रहकर बालक माता-पिता, भाई-बहन तथा अन्य सदस्यों के साथ रहकर अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं तथा समाजीकरण की प्रवृत्ति उनमें जन्म लेती हैं।
(5) व्यक्ति को समाज ही सामाजिक बनाता है तथा कहा जाता है कि समाज की सहकारिता ही बालक को सामाजिक बनाने में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसे-जैसे बालक अपने सहयोगियों का साथ पाता जाता है वैसे-वैसे ही वह दूसरे लोगों को अपना सहयोग देता जाता है। इससे बालक की सामाजिक प्रवृत्तियाँ संगठित हो जाती हैं।
प्रश्न 3. समाजीकरण में बाधक तत्व बताइये।
उत्तर – बालकों के समाजीकरण में बाधक तत्व (Factors Resisting Social- ization of the Child) – बालकों के समाजीकरण में अनेक बाधक तत्व होते हैं। मैस्लो (Maslow) ने बालकों के समाजीकरण में निम्नलिखित बाधक तत्वों का समावेश किया है-
(1) बालकों के जीवन में प्यार तथा सहानुभूति का अभाव होने के कारण पक्षपात, अनुचित दण्ड, माता-पिता में झगड़ा या तालक आदि कारणों से बालकों का समाजीकरण बाधित होता है।
(2) सांस्कृतिक परिस्थितियाँ भी समाजीकरण में बाधक तत्व होती हैं। यह सांस्कृतिक परिस्थितियाँ हैं-जाति या धर्म आदि से सम्बन्ध रखने वाली धारणायें आदि ।
(3) बालकों के समाजीकरण में जीवन को तत्कालीन परिस्थितियाँ भी बाधा उत्पन्न करती हैं। जैसे उनके साथ कठोरता दिखाना, ठीक से पेश न आना आदि ।
(4) अन्य कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी होती हैं, जैसे-निर्धनता, असफलता, की कमी होना, आत्मविश्वास की कमी आदि तत्व भी बालकों के समाजीकरण को बाधित करते हैं।
प्रश्न 4. समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक के कार्य बताइये।
उत्तर- समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का कार्य (Role of the Teacher in the Process of Socialization) – बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षकों का स्थान महत्वपूर्ण होता है। अतः समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी चाहिए-
(1) शिक्षक माता-पिता के साथ सम्पर्क स्थापित करके बालकों की रुचियों तथा मनोवृत्तियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करे तथा उन्हीं के अनुसार उसे विकसित करने के अवसर प्रदान करे।
(2) शिक्षक का कर्त्तव्य है कि वह बालकों को उचित सांस्कृतिक शिक्षा प्रदान करे जिससे बालकों का समाजीकरण हो सके।
(3) शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा तथा खेल के मैदानों व अन्य सांस्कृतिक व साहित्यिक क्रियाओं में बालकों के समक्ष सामाजिक आदर्श को प्रस्तुत करे। इन आदर्शों के अनुसरण से ही बालकों का समाजीकरण हो सकता है।
(4) शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यालय में विभिन्न सामाजिक योजनाओं के द्वारा बालकों को सामूहिक क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के अवसर प्रदान करे। इन क्रियाओं में भाग लेने से उसका समाजीकरण स्वयं ही हो जायेगा।
(5) विद्यालय की परम्पराओं का भी बालकों के समाजीकरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह बालक में विद्यालय की परम्पराओं के प्रति विश्वास उत्पन्न करे तथा उसे उन्हीं के अनुसार कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करे।
(6) बालकों के समाजीकरण में प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण स्थान होता है पर ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि बालक के समाजीकरण के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता का होना ही अच्छा है। अतः शिक्षक को बालक के स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना विकसित करनी चाहिए।
इस प्रकार कहा जाता है क बालक का समाजीकरण करने में परिवार का, शिक्षकों का, पड़ोस का तथा समुदाय आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
प्रश्न 5. घर या परिवार की शिक्षा के सिद्धान्त बताइये।
उत्तर-घर या परिवार शिक्षा के सिद्धान्त (Principles of Home or Family Education) –
1. शारीरिक विकास का सिद्धान्त- बालक को समुचित आहार, व्यवहार सन्तुलित भोजन, स्वच्छ-शुद्ध-परिष्कृत वातावरण, शारीरिक विकास में सहयोग देते हैं।
2. मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त-बालक के विकास के लिए उसका मनोवैज्ञानिक महत्व है। बालक की रुचि, आदत, प्रवृत्ति, बुद्धि एवं मानसिकता का ज्ञान अनिवार्य है। 3. क्रियाशीलता का सिद्धान्त-बालक स्वतः ही कुछ करना चाहता है, अत: उसे रचनात्मक क्रियाओं के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
4. स्वतन्त्रता का सिद्धान्त-बालक के विकास के लिए स्वतन्त्र वातावरण आवश्यक है। बालक को रुचि के अनुसार अध्ययनोन्मुख करना चाहिए।
5. बालकेन्द्रित शिक्षा का सिद्धान्त-शिक्षा बाल केन्द्रित बालक की योग्यता, शक्ति एवं रुचि के अनुसार होनी चाहिए।
6. क्रीड़ा द्वारा शिक्षा का सिद्धान्त-क्रीड़ा बालक की सामान्य प्रवृत्ति है। घर में या परिवार में क्रीड़ा के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। इससे, शारीरिक, मानसिक विकास के साथ ज्ञानेन्द्रियों एवं कर्मेन्द्रियों का भी विकास होता है।
7. सहानुभूति तथा निष्पक्ष व्यवहार का सिद्धान्त-डॉ. डी. पी. जोशी के अनुसार बालक के माता-पिता या परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्वक निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। किसी भी प्रकार का पक्षपात बालक में दोष पैदा कर सकता है।
8. अच्छी आदतों का निर्माण-डॉ. के. एल. जोशी के अनुसार बालक के कार्यों में अच्छी आदतों का समावेश हो, व्यावहारिक जीवन में महत्व देना पड़ता है।
प्रश्न 6. अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों हेतु चलायी जा रही शैक्षिक योजनायें बताइये।
उत्तर-
अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए चलाई जा रही शैक्षिक योजनायें (Educational Schemes Being Undertaken for SCs and STs)—अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अग्र योजनायें चलायी जा रही हैं-
1. छात्रवृत्तियाँ- मैट्रिक से पहले शिक्षा के लिए उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है जिनके माता-पिता शौचालय साफ करने, चमड़ा सफाई आदि करने का कार्य करते हैं। मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं।
2. छात्रवास की सुविधा – मिडिल, हाईस्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति तथा जनजाति की लड़कियों के रहने के लिए छात्रावास स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत धन केन्द्र सरकार और 50 प्रतिशत राज्य सरकार देती है।
3. पुस्तक भण्डार योजना- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो विद्यार्थी चिकित्सा या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ तीन विद्यार्थियों के लिए 5,000 रुपये तक की पुस्तकों का एक सेट दिया जाता है।
4. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र- इन जातियों के विद्यार्थियों को विभिन्न सेवाओं की भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रशिक्षण देने के लिए निःशुल्क केन्द्र स्थापित किये गये हैं।
5. अनुसन्धान और प्रशिक्षण – ऐसी संस्थायें जो अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के विकास व कल्याण के लिए अनुसन्धान या प्रशिक्षण कार्य में लगी हुयी हैं उन्हें शत-प्रतिशत धन दिया जाता है।
6. विकास की योजनायें – केन्द्र सरकार के सभी विभाग ऐसी योजनायें बनाते हैं जिससे इन जातियों का कल्याण हो तथा वे समाज के अन्य वर्गों के समान स्तर प्राप्त कर सकें।
7. अनुसूचित जाति विकास निगम-सभी राज्यों में इस प्रकार के निगम बनाये गये हैं। ये निगम अनुसूचित जाति के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं जिससे परिवार का विकास हो और इसके साथ ही उन्हें सामाजिक न्याय भी प्राप्त हो सके।
प्रश्न 7. शैक्षिक असमानता को दूर करने के कुछ सुझाव बताइये।
उत्तर-शैक्षिक असमानता को दूर करने के सुझाव-
1. समान स्कूल पद्धति-शिक्षा आयोग 1964-66 ने स्पष्ट कहा कि यदि इन बुराइयों को दूर करना है और शिक्षा प्रणाली को सामान्य राष्ट्रीय विकास तथा सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण का विशेष रूप से एक शक्तिशाली साधन बनाना है, तो हमें लोक शिक्षा की ऐसी स्कूल पद्धति की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, जिसकी निम्नलिखित विशेषतायें हों-
(1) जो जाति, सम्प्रदाय, समाज, धर्म, आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक प्रतिष्ठा का विचार किये बिना सभी बच्चों को सुलभ हो
(2) जिसमें अच्छी शिक्षा का अवसर प्राप्त करना, धन या वर्ग पर निर्भर न होकर प्रतिभा पर निर्भर होगा।
(3) जो सभी स्कूलों में एक समुचित स्तर बनाये रखे तथा कम-से-कम एक युक्तिसंगत संख्या में अच्छे स्तर की संस्थायें सुलभ कराये।
(4) जिसमें पढ़ाई की कोई फीस नहीं ली जाये ।
(5) जो औसत माता-पिता की आवश्यकताओं की पूर्ति करे ताकि उसे इस प्रणाली से बाहर के खर्चीले स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने की आवश्यकता साधारणतः अनुभव न हो ।
2. योग्यता के आधार पर शिक्षा-आयोग ने इस बात पर बल दिया है कि अच्छी शिक्षा आर्थिक व्यवस्था अथवा वर्गभेद के स्थान पर नहीं, अपितु योग्यता पर निर्भर करे तथा जहाँ कोई शुल्क न लिया जाये।
3. पड़ोसी स्कूल–सामान्य स्कूल-प्रणाली अपनाने की दिशा में आयोग ने ‘पड़ोस के स्कूल’ (Neighbourhood school) का सुझाव दिया है, जिसमें प्रत्येक बच्चे को अपने निकटतम स्थित स्कूल में जाना चाहिए ।
4. छात्रवृत्तियाँ-छात्रों की असमानता दूर करने के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रतिभाशाली छात्रों को प्रतियोगिता द्वारा चुनकर पब्लिक या सैनिक स्कूलों में प्रविष्ट किया जाये और उन्हें इतनी पर्याप्त छात्रवृत्ति दी जाये कि वे सम्पन्न घरों के बच्चों के समान ही रहन-सहन का स्तर बनाये रख कर पढ़ें।
5. अध्ययन केन्द्र – कहीं-कहीं बच्चों को घर पर पढ़ने की सुविधायें नहीं होतीं जैसे दिन को आने-जाने वालों का ताँता अथवा घर के कामों में फँसाव और रात को एकान्त एवं रोशनी की व्यवस्था का अभाव । ऐसे छात्रों के लिए यदि घर के पास ही अध्ययन केन्द्र खोले जा सकें तो छात्रों की कठिनाइयाँ दूर हो सकती हैं।
6. ‘पढ़ो और कमाओ’ की सुविधा – जो गरीब परन्तु परिश्रमी छात्र स्वावलम्बी होकर पढ़ाना चाहते हों उन्हें ऐसे कार्य उपलब्ध कराने चाहिए जिनके द्वारा वे अपनी पढ़ाई का खर्च अंशतः या पूर्णतः चला सकें।
7. पिछड़े वर्गों की शिक्षा- अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अतिरिक्त कुछ और भी पिछड़ी जातियाँ हैं जिनके बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उनमें से कुछ तो अपनी गरीबी के कारण, कुछ अज्ञान के कारण तथा कुछ सुविधाओं के अभाव में विद्यालय नहीं जा पाते। सर्वेक्षण द्वारा उनकी कठिनाइयों का पता लगाना चाहिए और उन्हें विद्यालयों में भेजने का उपाय करना चाहिए। कुछ परिवारों में शिक्षा के प्रति उपेक्षा का भाव होता है। ये सब सुविधायें देने पर भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना पसन्द नहीं करते। ऐसे माता-पिता को शिक्षा के लाभों से परिचित कराना और कुछ प्रभोलन देना आवश्यक है-जैसे दिन का भोजन और जलपान, नये कपड़े, पढ़ने की सामग्री इत्यादि ।
8. निःशुल्क शिक्षा-गरीब छात्रों के लिए सभी प्रकार की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए।
उपसंहार- इसमें कोई सन्देह नहीं है कि शिक्षा में समान अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनायें जिनका विवरण ऊपर दिया गया है, चलाई जा रही हैं। उनके कुछ परिणाम भी अच्छे दृष्टिगोचर हुये हैं परन्तु अभी भी सतत् प्रयासों की आवश्यकता है।
प्रश्न 8. समाजीकरण के प्रमुख सिद्धान्तों का उल्लेख कीजिए ।
उत्तर- समाजीकरण के प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं –
(अ) व्यवहारवादी परस्पर क्रियावादी सिद्धान्त (Behaviouristic Interactionistic School of Socialization ) —
इस सिद्धान्त का प्रतिपादन जॉर्ज सी. होम्स (George C. Homes) ने किया था। होम्स का मत है कि हमारी इसमें रुचि नहीं है कि मानव कैसे सीखता है ? क्या सीखता है ? हमारी इसमें रुचि है कि कि सीखने के बाद वह क्या करता है। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यक्ति में होने वाले व्यवहार परिवर्तन को समाजीकरण कहा जाता है। यह समाजीकरण किस प्रकार होता है ? इसमें उसकी प्रक्रिया का अध्ययन नहीं किया जाता है। इस कारण यह सिद्धान्त अपूर्ण है।
(ब) प्रतीकात्मक व्यक्तिपरक सिद्धान्त (Symbolic Subjectivistic School of Socialization)—
इस सिद्धान्त का प्रतिपादन सोरोकिन (Sorokin), जॉर्ज मीड (George Mead), कूले (Cooley) आदि के द्वारा किया गया। इस सिद्धान्त के अनुसार समाजीकरण मूल्यों को आत्मसात् करने या सांस्कृतिक अर्थों, प्रतिमानों, आदतों आदि का संचरण करने की प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप मनुष्य को सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित किया जाता है।
(स) प्रतीकात्मक-परस्पर क्रियात्मक सिद्धान्त (Symbolic -Interactionistic School of Socialization)—
इस सिद्धान्त का प्रतिपादन मर्टन (Murton), टालकोट पारसन्स (Talcott Parsons) आदि ने किया था। इस सिद्धान्त के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति तथा सामाजिक परिस्थितियों के बीच पारस्परिक क्रिया चलती हैं जिसके फलस्वरूप मनुष्य समाज-सम्मत मूल्यों तथा दक्षताओं को अपने व्यक्तित्व का अंग बना लेता है। आजकल यही सिद्धान्त अधिक प्रचलित है।
प्रश्न 9. बालक के जीवन में परिवार के महत्व को बताइये।
उत्तर—आज परम्परागत परिवार का स्थान आधुनिक परिवार ने ले लिया है। इसका संगठन बदल गया है और इसके कुछ मौलिक कार्य दूसरी संस्थाओं द्वारा किये जाने लगे हैं। फिर भी, यह एक आधारभूत सामाजिक संस्था है और इसके कुछ विशेष कार्य और विशेष महत्व हैं। अभी तक छोटे बच्चों का पालन-पोषण केवल यही करता है। सामाजिक संस्था के रूप में यह अब भी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा देता है। परिवार का वातावरण उसके व्यवहार को सुधारने के लिए उत्तरदायी है।
रेमॉण्ट (Raymont) ने ठीक ही लिखा है-“दो बच्चे भले ही एक ही विद्यालय में पढ़ते हों, एक ही समान शिक्षकों से प्रभावित होते हों, एक-सा ही अध्ययन करते हों, फिर भी वे अपने सामान्य ज्ञान, रुचियों, भाषण, व्यवहार और नैतिकता में अपने घरों के कारण, जहाँ से वे आते हैं, पूर्णतया भिन्न हो सकते हैं।”
इस प्रकार, परिवार बालक पर अपना स्थायी प्रभाव अंकित कर देता है। वह वैसा ही बनता है, जैसा उसका घर उसको बनाता है। घर के प्रभाव के कारण ही गाँधीजी ने प्रेम और सत्य के सिद्धान्तों को अपनाया। शिवाजी ने अपनी माता से रामायण और महाभारत की शिक्षा प्राप्त करके ही मराठा राज्य की नींव डाली। इस बात की पुष्टि करने के लिए कि घर में ही अच्छे और बुरे गुणों की शिक्षा मिलती है, बहुत-से उदाहरण दिये जा सकते हैं। एच. सी. एण्डरसन (H. C. Anderson) का कथन है- हमारे अपराधियों में से 80 प्रतिशत असहानुभूतिपूर्ण घरों से आते हैं।
यहाँ यह कहना असंगत न होगा कि घर के वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के विकास के सभी स्तरों पर पड़ता है। इसलिए लॉरी ने लिखा है- “शैक्षिक इतिहास के सभी स्तरों पर परिवार, बालक की शिक्षा का प्रमुख साधन है।”
प्रश्न 10. घर के कार्य व महत्व पर विभिन्न विद्वानों के विचारों का उल्लेख कीजिए ।
उत्तर
–
शिक्षा के अनौपचारिक साधन के रूप में घर के कार्यों और महत्व पर समय-समय पर विभिन्न विचार व्यक्त किये गये हैं। यहाँ हम उनमें से कुछ का वर्णन कर रहे हैं; यथा-
1. प्राचीन भारतीय विचार (Ancient Indian View )—
प्रागैतिहासिक काल से ईसा की 10वीं शती पूर्व तक भारत में बालकों को कई वर्ष तक व्यवस्थित रूप से शिक्षा देने के लिए विद्यालय नहीं थे। उस समय तक यह कार्य केवल परिवार के द्वारा ही किया जाता था। परिवार का नेता अपने पुत्रों को वेदों, शास्त्रों, साहित्य, धर्म, कृषि, वाणिज्य, व्यवसाय आदि की शिक्षा देता था ।
2. रूसो का विचार (Rousseau’s View) —
रूसो प्रकृतिवादी दार्शनिक था। अतः उसे विश्वास नहीं था कि आधुनिक सभ्यता में परिवार बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर सकता है। उसने स्वयं पिता के रूप में ईमाइल (Emile) को समाज से दूर प्रकृति की गोद में शिक्षा दी।
3. पेस्टालॉजी का विचार (Pestalozzi’s View) –
पेस्टालॉजी बालक के प्रशिक्षण के लिए घर को अनिवार्य मानता था। उसने माता को सब शिक्षा का वास्तविक स्रोत बताया। उसका कहना था-“घर, शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है।”
4. फ्रोबेल का विचार (Frobel’s View) –
फ्रॉबेल, पेस्टालॉजी से सहमत था। उसका विचार था-“मातायें आदर्श अध्यापिकायें हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली और स्वाभाविक है।”
5. मॉण्टेसरी का विचार (Montessori’s View) मॉण्टेसरी ने छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए घर के वातावरण और परिस्थिति को अति आवश्यक तत्व माना। इसलिए, उसने अपने विद्यालय को ‘बचपन का घर’ (House of childhood) के नाम से पुकारा। इनमें ये दोनों तत्व अति महत्वपूर्ण कार्य करते थे।
जिस प्रश्न का उत्तर चाहिए उसे क्लिक करे
प्रश्न -(01) वैदिक काल में भारत में शिक्षा के अर्थ एवं उदेश्य >>
प्रश्न -(02) बच्चो के समाजीकरण में समुदाय की भूमिका
प्रश्न -(03) समाज का अर्थ बताइये
प्रश्न -(04) समाजीकरण में बाधक तत्व बताइये
प्रश्न -(05)
प्रश्न -(06)
प्रश्न -(07)
प्रश्न -(08)
प्रश्न -(09)
प्रश्न -(10)
जल्द ही बिहार डी.एल.एड फर्स्ट ईयर पेपर कोड F1 , विषय नाम – ” समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ ” के सभी प्रश्नों के उत्तर जोड़े जायेंगे | कृपया स्क्रीन के ऊपर व्हाट एप्प का सिम्बल दिया गया है .उसपे क्लिक कर व्हाट एप ग्रुप एवं टेलीग्राम से जुड़े |
समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ BOOK -1 pdf
समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ BOOK 2 PDF
समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ क्वेश्चन पेपर
| विषय | समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ प्रश्न |
| TYPE | क्वेश्चन पेपर |
| पेपर कोड | F 1 |
समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ २०२३ का प्रश्न
PREVIOUS YEAR QUESTIONS PAPER २०२३
खण्ड ‘क’ लघु उत्तरीय प्रश्न : सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है।
1. बच्चे तथा बचपन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण के माध्यम से इसे स्पष्ट कीजिए।
अथवा, समाजीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करें।
2. ‘शिक्षा’ का क्या तात्पर्य है? परिभाषा के माध्यम से स्पष्ट कीजिए।
अथवा, शिक्षा की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट कीजिए।
3. ज्ञान क्या है? ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है?
अथवा, ज्ञान तथा सूचना में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
4. शिक्षा नए समाज बनाने की एक प्रक्रिया है। स्पष्ट करें।
अथवा, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। वर्णन करें।
5. विद्यालय के अंदर और बाहर के ज्ञान के बीच गहरा जुड़ाव है। क्या आप सहमत हैं? उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें।
अथवा, स्थानीय तथा सार्वभौम ज्ञान में अन्तर स्पष्ट कीजिए ।
6. पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
अथवा, विद्यालय में पाठ्यचर्या की आवश्यकता क्यों पड़ती है? स्पष्ट कीजिए।
खण्ड ख दीर्घ उत्तरीय प्रश्न :-: प्रत्येक का उत्तर 200 से 250 शब्दों में दें। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें।
7. “सर्वोच्च शिक्षा वही है जो सम्पूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करें।” व्याख्या करें।
8. बच्चों के समाजीकरण में माता-पिता तथा समुदाय की भूमिका को उपयुक्त उदाहरणों के साथ वर्णन करें।
9. जे० कृष्णमूर्ति के शैक्षिक विचारों की चर्चा करें। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रासंगिकता पर विचार करें।
10. बच्चों की पाठ्य-पुस्तकें शिक्षा, ज्ञान एवं समाजीकरण के माध्यम के रूप में किस प्रकार है? उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए।
11. निम्नांकित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें :
(क) अच्छे शिक्षण की विशेषताएँ।
(ख) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005
(ग) डॉ० जाकिर हुसैन।
\\\\ \\\\\\ \\\\\\
”””””’ ”””””””’ ”””””””
समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ PREVIOUS YEAR QUESTION PAPER
****** ********* ****************
समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ Previous Year Question Paper
समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ Previous Year Question Paper pdf Download
samaj shiksha aur pathyacharya ki samajh Previous Year Question Paper
samaj shiksha aur pathyacharya ki samajh pdf
F-1 Previous Year Question Paper
BIHAR D.El.Ed Whatsapp Teligram Link
| डी.एल.एड. सम्बन्धी न्यूज नोट्स pdf के लिए ग्रुप एवं चैनल को ज्वाइन करे | |
| डी.एल.एड (व्हाट एप ग्रुप) |  |
| बी.एड (व्हाट एप ग्रुप) |  |
| टेलीग्राम (व्हाट एप ग्रुप) |  |
| CTET (व्हाट एप ग्रुप) |  |
| ALL IN ONE- व्हाट एप चैनल |  |
| Instagram Join |  |