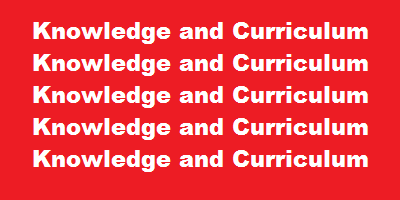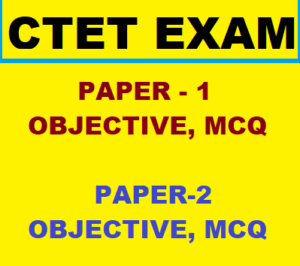Knowledge and Curriculum
| विषय | ज्ञान और पाठ्यक्रम |
| SUBJECT | Knowledge and Curriculum |
| COURSE | B.Ed. 2nd Year |
VVINOTES.IN के इस पेज में B.Ed. 2nd Year Paper -1 Knowledge and Curriculum से सम्बन्धित निम्नलिखित सामग्री को सामिल किया गया है | जैसे Knowledge and Curriculum B.Ed. Notes ,Knowledge and Curriculum B.Ed. 2nd Year Notes ,Knowledge and Curriculum b-ed Notes pdf free download , Knowledge and Curriculum handwritten Notes , Knowledge and Curriculum B.Ed. 2nd Year pdf, Knowledge and Curriculum ignou pdf , Knowledge and Curriculum Notes in hindi , Knowledge and Curriculum assignment इत्यादी
Knowledge and Curriculum Question Answer
| B.Ed 2nd Year Knowledge and Curriculum (ज्ञान और पाठ्यक्रम ) के यहा पर नोट्स दिया गया है | |
01. प्रश्न – पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकार | अथवा पाठ्यक्रम के संगठक कारक का वर्णन करे ?
उत्तर –
पाठ्यक्रम के संगठन के विषय में अलग-अलग दृष्टिकोण होते हैं ! इसी आधार पर पाठ्यक्रम भी अनेक प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं –
(01) बाल केंद्रित पाठ्यक्रम (Child Centred Curriculum)
(02) विषय केंद्रित पाठ्यक्रम (Subject Centred Curriculum)
(03) कार्य / क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम (work/activity centred curriculum)
(04) अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम (Experience centred curriculum)
(05) शिल्पकला -केंद्रित पाठ्यक्रम (Craft Centred curriculum)
(06) कोर पाठ्यक्रम (core curriculum)
01. बाल केंद्रित पाठ्यक्रम (Child Centred Curriculum)
बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का अभिप्राय उस पाठ्यक्रम से है, जिसका संगठन बालक की प्रवृत्ति, रुचि, रुझान, आवश्यकता आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है अर्थात इस पाठ्यक्रम में विषयों की अपेक्षा बालकों को मुख्य स्थान दिया जाता है ! इस पाठ्यक्रम को हम मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम भी कह सकते हैं, क्योंकि यह बालक की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं पर आधारित होता है ! इस पाठ्यक्रम में जो भी विषय रखे जाते हैं वे बालकों के विकास के स्तर, उनकी रूचियो, रुझानों एवं आवश्यकताओं के अनुकूल होते हैं ! वर्तमान समय की सभी शिक्षण विधियों में जैसे – मोंटेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन आदि बाल- केंद्रित पाठ्यक्रम पर ही जोर दिया जाता है ! इस प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है !
02. विषय केंद्रित पाठ्यक्रम (Subject Centred Curriculum) –
विषय केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें विषय को आधार मानकर पाठ्यक्रम को नियोजित किया जाता है ! अथार्त इसमें बालकों की अपेक्षा विषयों को अधिक महत्व दिया जाता है ! इस पाठ्यक्रम का सूत्रपात प्राचीन ग्रीक तथा रोम के विद्यालयों में हुआ ! इस पाठ्यक्रम में विषयों के ज्ञान को पृथक-पृथक रूप देने की व्यवस्था होती है ! इसमें सभी विषयों के अंतर्गत आने वाले ज्ञान को अलग-अलग निश्चित कर दिया जाता है और उसी के अनुसार विभिन्न विषयों पर पुस्तके लिखी जाती है जिनसे बालकों को ज्ञान प्राप्त होता है ! चुकी इस प्रकार के पाठ्यक्रम में पुस्तकों पर बल दिया जाता है ! अतः इसे ‘पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम ‘ भी कहा जाता है !यह पाठ्यक्रम बालको में रटने की आदत एवं केवल परीक्षा पर ही बल देता है ! परंतु इसमें कुछ लाभ भी है, उदाहरनार्थ, इस पाठ्यक्रम में शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है, पाठ्य-वस्तु पूर्व निश्चित होती है तथा एक से अधिक विषय की पाठ्य-वस्तु को एकीकृत रूप में प्रस्तुत भी किया जा सकता है ! यह एक निश्चित सामाजिक तथा शैक्षिक विचारधारा पर आधारित होता है !
3. कार्य / क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम
(work/activity centred curriculum)-
कार्य/ क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम अनेक प्रकार के कार्यों पर आधारित होता है अर्थात इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यों को विशेष स्थान दिया जाता है ! बालक को सामाजिक मूल्य के अनेक ऐसे कार्य करने होते हैं जो उनके सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं ! अतः कार्य -केंद्रित पाठ्यक्रम का अभिप्राय: उस पाठ्यक्रम से है जिसमें विभिन्न कार्यों द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की योग्यता होती है ! इन कार्यों व क्रियाओं का आयोजन छात्रों की रुचि, आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है ! कार्यों का चयन शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के सहयोग से किया जाता है !
जॉन डीवी का मत है कि कार्यकेंद्रित पाठ्यक्रम द्वारा बालक समाज उपयोगी कार्यों के करने में रूचि लेने लगेगा जिससे उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना निश्चित है
4. अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम (Experience centred curriculum) –
अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का अभिप्राय उस पाठ्यक्रम से है जिसमें मानव जाति के अनुभव सम्मिलित किए जाते हैं ! दूसरे शब्दों में अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम विषयों की अपेक्षा अनुभव पर आधारित होता है ! इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य बालकों को प्रेरणा प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवन को उपयोगी बना सके ! यह भौतिक तथा सामाजिक वातावरण का अधिक -से -अधिक प्रयोग करता है क्योंकि इसमें बालकों को स्वाभाविक ढंग से ‘अनुभव ‘ प्राप्त करने को मिलते हैं ! यही कारण है कि यह पुण्तया मनोविज्ञान पर आधारित होता है अथार्त इसका संबंध छात्रों की रुचियो, आवश्यकता तथा योग्यताओं से होता है !
5. शिल्पकला -केंद्रित पाठ्यक्रम (Craft Centred curriculum) –
शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम का अभिप्राय उस पाठ्यक्रम से है जिसमें ‘शिल्प’ व ‘क्राफ्ट’ को बिषय मानकर अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती है ; जैसे – कताई, बुनाई, चमड़े तथा लकड़ी के काम आदि को केंद्र मानकर दूसरे विषयों की शिक्षा दी जाती हैं ! इस प्रकार का पाठ्यक्रम संगठन महात्मा गांधी के विचार पर आधारित है कि छात्रों को कुछ ऐसे शिल्पो की शिक्षा दी जानी चाहिए जिनके द्वारा एक तो विद्यालय का खर्च निकल आए तथा दूसरे भविष्य में छात्र इसके सहारे अपनी जीविका भी चला सके ! इस प्रकार यह पाठ्यक्रम ‘करके सीखने’ पर आधारित है जिसके द्वारा छात्र कोई- न -कोई उपयोगी कार्य अवश्य लेते हैं जो उन्हें भविष्य में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना देता है ! इस पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने से छात्रों के मन में श्रम के प्रति आदर उत्पन्न होता है तथा उनके ह्रदय में श्रमजीवियो के प्रति सम्मान व सहानुभूति प्राप्त होती है !
6. कोर पाठ्यक्रम (core curriculum) –
कोर / केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें कुछ तो अनिवार्य होते हैं तथा अधिक विषय ऐच्छिक होते हैं ! अनिवार्य विषयों का अध्ययन करना प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य होता है तथा व्यक्तिगत ऐच्छिक विषयों को व्यक्तिगत रूचि तथा क्षमता के अनुसार चुना जा सकता है !यह पाठ्यक्रम अमेरिका का देन है जिसके अंतर्गत प्रत्येक बालक को व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों प्रकार की समस्याओं के संबंध में ऐसे अनुभव दिए जाते हैं जिनके द्वारा वह अपने भावी जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या को सरलतापूर्वक सुलझाने हेतु कुशल एवं समाजोपयोगी एवं उत्तम नागरिक बन सकता है ! कोर पाठ्यक्रम की आवश्यकता सभी विद्यार्थियों को होती है लेकिन प्रारंभिक स्तर पर विद्यालय में कोर पाठ्यक्रम की अति आवश्यकता है ! माध्यिक स्तर पर विद्यालय के आधे समय में कोर पाठ्यक्रम के कार्यक्रम होते हैं व उच्च शिक्षा स्तर पर इसकी मात्रा और घट जाती है !
02. प्रश्न – पाठ्यचर्या निर्माण के प्रमुख सिद्धांत
Major theory of curriculum construction
उत्तर –
पाठ्यचर्या विद्यालयी शिक्षा के केंद्र बिंदु है ! पाठ्यचर्या एक सुनिश्चित क्रिया है ! इसका निर्माण बिना सोचे-समझे नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके द्वारा कुछ निश्चित उद्देश्य प्राप्त करने होते है ! पाठ्यचर्या निर्माण के अनेक दृष्टिकोण है ! ये दृष्टिकोण विभिन्न दार्शनिको एवं प्रवृत्तियों की देन है ! पाठ्यचर्या निर्माण के निम्नलिखित सिद्धांत हैं –
1. शैक्षिक उद्देश्यों की अनुकूलता का सिद्धांत –
2.बच्चों को आवश्यकताओ योग्यताओ रुचिओ एवं भावनाओं की अनुकूलत्ता का सिद्धांत –
3. जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत –
4. पाठ्यचर्या में मानव जीवन के समस्त उपयोगी अनुभवो के समावेश का सिद्धांत –
5. उपयोगिता का सिद्धांत –
6. पाठ्यचर्या के विभिन्न विषयों एवं क्रियाओं में सह -सम्बन्ध तथा एकीकरण का सिद्धांत –
7. प्रदान किये जानेवाले ज्ञान के वर्गीकरण का सिद्धांत
8. पाठ्यचर्या में अगुवाई एवं सामान्यीकरण का सिद्धांत –
9. आगे की ओर देखने का सिद्धांत –
10 सीखने के अनुभव में निरंतरता का सिद्धांत –
11. क्रिया का सिद्धांत –
12. तत्परता का सिद्धांत –
13. अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत –
14. विविधता और लचीलेपन का सिद्धांत –
15. राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं लोकतंत्रात्मक गुणों के विकास का सिद्धांत –
पाठ्यचर्या निर्माण के निम्नलिखित सिद्धांत हैं –
1. शैक्षिक उद्देश्यों की अनुकूलता का सिद्धांत –
पाठयचर्या को शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का सदा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उद्देश्य ही निर्धारित करते हैं कि उन विषयों एवं क्रियाओं को जो उद्देश्यों को जो उदेश्यो को प्राप्त करने के लिए बालको को दी जानी है !
2.बच्चों को आवश्यकताओ योग्यताओ रुचिओ एवं भावनाओं की अनुकूलत्ता का सिद्धांत –
इस सिद्धांत को बाल-केंद्रित सिद्धांत भी कहा जाता है ! यह तो सभी जानते हैं और मानते हैं कि बच्चे योग्यता, रुचि एवं भावना की दृष्टि से संपन्न नहीं होते ! इसलिए पाठ्यचर्या सामान्य बालकों की आवश्यकताओं, योग्यताओं, रुचियों, भावनाओं एवं क्रियाओं के आधार पर बनाई जाती है ! बच्चों की आत्माभीव्यक्ति और उपक्रम को प्रभावित करने के लिए केवल वही विषय एवं क्रियाएं सम्मिलित नहीं की जाती है जो उनके अनुकूल हो ! छात्रों में असमानता होती है, इसलिए उसके रुझान, रुचि एवं आवश्यकता के आधार पर उन्हें अनेक वर्गो में बांटा जाता है ! इन विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग पाठ्यचर्या बनाई जानी चाहिए इससे उन्हें अपनी योग्यताओं, क्षमताओं को विकास करने का अवसर मिल सकेगा !
3. जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत –
पाठ्यचार्य का निर्माण करते समय ध्यान रखा जाए कि यह शैक्षिक विषयों से संबंधित पाठय -पुस्तकों तक ही सीमित न रहे, वरन यह ऐसी होनी चाहिए कि छात्रों को समस्त शैक्षिक वातावरण की अभिव्यक्ति कराने की क्षमता रखती हो ! साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि छात्रों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे ! यह व्यवस्था ही छात्रों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में सहायक सिद्ध होगी !
4. पाठ्यचर्या में मानव जीवन के समस्त उपयोगी अनुभवो के समावेश का सिद्धांत –
यह सर्वविदित है कि मानव अपने पूर्वजों के अनुभवो से सीखता है और उनमें अपने अनुभव जोड़कर उन्हें विकसित करता है ! यदि मानव जाति के समस्त अनुभवो का लाभ छात्रों को पहुंचाना है तो उन्हें पाठ्यचर्या में स्थान देना होगा ! साथ ही, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दूसरो के अनुभवो की कसौटी पर रखकर सत्य तथा असत्य का निर्णय लिया जा सकेगा !
5. उपयोगिता का सिद्धांत –
पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कौन-कौन से विषय एवं क्रियाएं छात्रों के लिए उपयोगी है ! इसलिए उपयोगिता के आधार पर विषय एवं क्रियाओं का क्रम निर्धारित करना चाहिए ! स्वतंत्र भारत ने स्वेच्छा से लोकतांत्रिक शासन एवं समाजिक पद्धति अपनाई है ! इसलिए प्रत्येक स्तर की पाठ्यचर्या में लोकतांत्रिक के आवश्यक गुणों राष्ट्रिय अखंडता एवं राष्ट्रिय भावना को उपयुक्त स्थान मिलना चाहिए !
6. पाठ्यचर्या के विभिन्न विषयों एवं क्रियाओं में सह -सम्बन्ध तथा एकीकरण का सिद्धांत –
ज्ञान को एक इकाई के रूप में माना व् समझा जाता है ! परंतु शिक्षाविदों ने शिक्षण के सुविधा के लिए विश्लेषणात्मक ढंग से ज्ञान को विभिन्न विषयों में विभाजित कर दिया है ! सीखने की सुविधा एवं उपयोगिता के आधार पर पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय उन्हीं विषयों और क्रियाओं को शामिल किया जाना चाहिए तो परस्पर संबंधित हो ! विभिन्न विषयों की सामग्री का चयन करते समय भी ऐसी सामग्री का चयन करना होगा जिसे एक -दूसरे के आधार पर पढ़ाया या विकसित किया जा सके ! ऐसी ही पाठ्यचर्या को एकीकृत पाठ्यचर्या कहा जाता है !
7. प्रदान किये जानेवाले ज्ञान के वर्गीकरण का सिद्धांत –
यह सर्वविदित है कि मानव जीवन सीमित है और इसके विपरीत ज्ञान असीमित है और साथ ही ज्ञान का विस्फोट भी हो रहा है ! ऐसी स्थिति में, मानव अपने सीमित जीवन काल में समस्त ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता ! प्रत्येक व्यक्ति को लिखने पढ़ने और सामान्य व्यवहार में दक्ष होना चाहिए ! इसी प्रकार भाषा, गणित और समाजशास्त्र या समाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान अनिवार्य विषय होने चाहिए ! कृषि, वाणिज्य आदि जैसे विषय एकचक्षिक वर्ग में रखे जाने चाहिए ! प्रत्येक व्यक्ति की अपनी रूचि के अनुसार विषय चुनने का अवसर मिल सके !
8. पाठ्यचर्या में अगुवाई एवं सामान्यीकरण का सिद्धांत –
इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यचर्या का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उसमें अगुआई की भावना जागृत हो सके ! इसके फलस्वरूप छात्र ज्ञान प्राप्त करने एवं क्रियाओं में दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण लेने की भावना तथा जिज्ञासा प्रकट करेंगे !
<> प्राप्त ज्ञान बेकार है यदि छात्र उसका प्रयोग ना कर सके ! इसलिए प्रयोग करने की क्षमता को ही ज्ञान का सामान्यीकरण कहा जायेगा ! इसलिए पाठ्यक्रम ऐसी बनाई जाए कि छात्र ज्ञान प्राप्त कर सके और क्रियाओं की ओर आकर्षित हो सकें ! यही योग्यता उनके भावी जीवन को सफल बनाने में सहायक सिद्ध होगी !
9. आगे की ओर देखने का सिद्धांत –
आज का बच्चा कल का नागरिक है ! उसे ही आगे चलकर विभिन्न उत्तर दायित्व संभालने होंगे ! इसलिए पाठ्यचर्या की रचना ऐसे ढंग से की जानी चाहिए कि वे समाज के की प्रगति एवं भलाई में प्रभावशाली योगदान दे सके और अपने वातावरण में आवश्यकतानुसार वांछित परिवर्तन ला सकें !इसलिए कहा जा सकता है कि बालक को दिया जाने वाले ज्ञान ऐसा हो कि उज्जवल भविष्य के लिए सहायक सिद्ध हो सके !
10. सीखने के अनुभव में निरंतरता का सिद्धांत –
छात्रों की अधिगम गति को तेज करने के लिए सीखने के अनुभवों में निरंतरता होनी चाहिए ! यहा स्थल से सूक्ष्म की ओर के सिद्धांतों का अनुकरण किया जाना हितकर सिद्ध होगा !
11. क्रिया का सिद्धांत –
आज के युग में क्रिया द्वारा सीखना श्रेष्ठ माना जाता है और प्राप्त ज्ञान स्थाई होता है ! इसलिए पाठ्यचर्या में छात्रों की सक्रियता को बनाए रखने के लिए विभिन्न उपयोगी क्रियाओं का समावेश किया जाना चाहिए !
12. तत्परता का सिद्धांत –
यह सभी मानते हैं कि वही ज्ञान प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण होता है जिसके सीखने के लिए छात्र प्रेरित होता है या उसमें सीखने के प्रति तत्परता होती है ! तत्परता के लिए आवश्यक है कि छात्र के पास उपयुक्त ज्ञान एवं कौशल हो और सीखने के प्रति उसका सकारात्मक दृष्टिकोण हो ! इसके साथ वातावरण भी अधिगम तत्परता को प्रभावित करता है ! इसलिए पाठ्यचर्या रचना ऐसे ढंग से की जानी चाहिए कि अध्यापक उपयुक्त समय पर ही विषय पढ़ा सके !
13. अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत –
शिक्षा के उद्देश्य व्यवसाय के लिए तैयार करना नहीं होता वरन छात्रों को अवकाश के समय सदुपयोग का भी प्रशिक्षण देना चाहिए ! इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पाठ्यचर्या में समाजिक सौंदर्य, बोधक, रुचि एवं क्रिडात्मक क्रियाओं का समावेश होना चाहिए !
14. विविधता और लचीलेपन का सिद्धांत –
पाठ्यचर्या की रचना में ज्ञान, कुशलता और भावनाओं के उन विस्तृत क्षेत्रों का समावेश किया जाना चाहिए जो बालक की व्यक्तिगत भिन्नता की दृष्टि से विकास की प्रक्रिया को विकसित कर सके ! ऐसी स्थिति में आवश्यकता हो जाता है कि पाठ्यचर्या में विविधता के साथ लचीलापन भी हो !
15. राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं लोकतंत्रात्मक गुणों के विकास का सिद्धांत –
स्वतंत्र भारत ने अपने राष्ट्र लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं ! देश की समस्त शिक्षा प्रणाली का आधार राष्ट्रीय लक्ष्य है ! पाठ्यचर्या की रचना करते समय राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान कौशल एवं भावनाओं का समावेश करना आवश्यक है ! इसके अंतर्गत हमें अपने छात्रों को जनसंख्या की समस्या, उत्पादन वृद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने होंगे !
हमें स्वेच्छा से अपने देश की शासन व्यवस्था के लिए लोकतंत्रात्मक प्रणाली अपनानी है ! इसे सफल बनाने के लिए हमें पाठ्यक्रम में समानता, स्वतंत्रता सहिष्णुता एवं सहयोग जैसे – लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास के लिये बिभिन्न क्रियाकलापों का आयोजन कर व्यावहारिक रूप देने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने होंगे !
***** ******* ******** ****** ****** ****** ******
प्रश्न – रास्ट्रीय पाठचर्या की रुपरेखा 2005 की मुख्य सिफारिस पर प्रकास डाले
उतर-
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 (NCF 2005) की मुख्य सिफारिशें
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 (NCF 2005) को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी, समावेशी और व्यावहारिक बनाना था। यह रूपरेखा आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, बाल-केंद्रित शिक्षा और समग्र विकास पर आधारित थी।
NCF 2005 की मुख्य सिफारिशें:
1. शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में सुधार
पाठ्यक्रम को बच्चों की समझ, रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए बनाया जाए।
रटने की प्रवृत्ति (rote learning) को समाप्त कर बच्चों में प्रयोगात्मक और अनुभवजन्य शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए।
पाठ्यक्रम को अधिक लचीला और व्यावहारिक बनाया जाए ताकि बच्चे आनंदपूर्वक सीख सकें।
विषय-वस्तु को बच्चों के अनुभवों और पर्यावरण से जोड़ा जाए।
2. मूल्यांकन प्रणाली में सुधार
परीक्षा प्रणाली को सुधारकर समग्र और सतत मूल्यांकन (CCE – Continuous and Comprehensive Evaluation) लागू किया जाए।
परीक्षा का उद्देश्य केवल अंक प्राप्त करना न हो, बल्कि बच्चों के संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को सुनिश्चित करना हो।
केवल स्मरण शक्ति आधारित मूल्यांकन के बजाय समस्या-समाधान कौशल, विश्लेषण और तर्क शक्ति को परखा जाए।
3. बाल-केंद्रित शिक्षा और समावेशी शिक्षा
बच्चों को सीखने की स्वतंत्रता और रुचियों के अनुसार अवसर दिए जाएं।
दिव्यांग (विकलांग) बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की नीति अपनाई जाए, जिससे वे सामान्य स्कूलों में पढ़ सकें।
लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए और लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाए।
समाज के सभी वर्गों (गरीब, ग्रामीण, आदिवासी, पिछड़े वर्ग) के बच्चों को समान शिक्षा के अवसर दिए जाएं।
4. मातृभाषा और बहुभाषिकता पर जोर
प्राथमिक स्तर पर शिक्षा बच्चों की मातृभाषा में दी जानी चाहिए ताकि वे आसानी से समझ सकें।
हिंदी, अंग्रेज़ी और अन्य भारतीय भाषाओं को संतुलित तरीके से शामिल किया जाए।
बच्चों को कई भाषाएँ सीखने के अवसर दिए जाएं ताकि वे संस्कृति और संचार कौशल विकसित कर सकें।
5. गणित और विज्ञान शिक्षा में सुधार
गणित और विज्ञान को रटने के बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण से पढ़ाया जाए।
विज्ञान और गणित को अनुभव आधारित गतिविधियों से जोड़ा जाए, ताकि छात्र इसे रुचिकर और उपयोगी समझें।
पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और इसे पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया जाए।
6. कला, स्वास्थ्य और खेल शिक्षा
शिक्षा में कला (ड्राइंग, संगीत, नाटक, नृत्य आदि) को अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए, ताकि बच्चों की रचनात्मकता विकसित हो।
खेल और योग को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बना रहे।
नैतिक शिक्षा, जीवन-कौशल और स्वास्थ्य शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए।
7. शिक्षक प्रशिक्षण और उनकी भूमिका
शिक्षकों को नई शिक्षण विधियों पर प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे बच्चों को अधिक प्रभावी तरीके से पढ़ा सकें।
शिक्षकों को लचीलापन और स्वतंत्रता दी जाए, ताकि वे बच्चों के स्तर के अनुसार पढ़ाने की विधियाँ अपना सकें।
शिक्षक और छात्र के बीच सकारात्मक और प्रेरणादायक संबंध बनाए जाएं।
8. तकनीकी और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा
सूचना और संचार तकनीक (ICT) का अधिकतम उपयोग किया जाए ताकि शिक्षा को रोचक और प्रभावी बनाया जा सके।
डिजिटल संसाधनों (ऑनलाइन पाठ्यक्रम, स्मार्ट क्लास, वर्चुअल लैब) को शिक्षा में शामिल किया जाए।
9. पर्यावरण और सामाजिक जागरूकता
बच्चों को पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता और सतत विकास के प्रति जागरूक किया जाए।
सामाजिक न्याय, समानता, लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।
निष्कर्ष
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश की, जिससे शिक्षा अधिक बच्चों-केंद्रित, समावेशी, व्यावहारिक और आनंदमय बन सके। इसका उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं, बल्कि समग्र विकास, रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच, नैतिक मूल्यों और जीवन-कौशल को विकसित करना था।
Knowledge and Curriculum guide
| Knowledge and Curriculum – B.Ed first Year Knowledge and Curriculum के यहा पर Guide का pdf दिया गया | आप इसे Download कर सकते है | |
Knowledge and Curriculum Ignou book pdf
| Knowledge and Curriculum – B.Ed first Year Knowledge and Curriculum के यहा पर Ignou book pdf दिया गया है | आप Knowledge and Curriculum Ignou book pdf download कर सकते है | |
Knowledge and Curriculum Assignment
| Knowledge and Curriculum – B.Ed first Year Knowledge and Curriculum के यहा पर Assignment दिया गया है | आप Knowledge and Curriculum Assignment pdf download कर सकते है | |
| डी.एल.एड. बी.एड सम्बन्धी न्यूज नोट्स pdf के लिए ग्रुप एवं चैनल को ज्वाइन करे | |
| डी.एल.एड (व्हाट एप ग्रुप) |  |
| बी.एड (व्हाट एप ग्रुप) |  |
| टेलीग्राम (व्हाट एप ग्रुप) |  |
| CTET (व्हाट एप ग्रुप) |  |
| ALL IN ONE- व्हाट एप चैनल |  |
| Instagram Join |  |
- Knowledge and Curriculum B.Ed 2nd Year Full Marks ,
- Knowledge and Curriculum B.Ed 2nd Year Pass Marks ,
- Knowledge and Curriculum B.Ed 2nd Year Pratical marks ,
- Knowledge and Curriculum B.Ed 2nd Year book pdf download ,
- Knowledge and Curriculum B.Ed 2nd Year guide pdf download ,
- Knowledge and Curriculum B.Ed 2nd Year notes ,
- Knowledge and Curriculum B.Ed 2nd Year notes Hindi Medium ,
- Knowledge and Curriculum B.Ed 2nd Year English Medium ,
- Knowledge and Curriculum assignment ,
- Knowledge and Curriculum assignment in Hindi ,
- Knowledge and Curriculum assignment in English ,
- Knowledge and Curriculum B.Ed 2nd Year notes in english ,
- Knowledge and Curriculum B.Ed 2nd Year notes in hindi ,
- Knowledge and Curriculum assignment in Hindi pdf ,
- Knowledge and Curriculum ignou notes ,
- Knowledge and Curriculum ignou pdf ,
- Knowledge and Curriculum book pdf free download ,
- Knowledge and Curriculum assignment ,
- Knowledge and Curriculum b.ed book pdf in english ,
- Knowledge and Curriculum b.ed 2nd Year notes ,
- Knowledge and Curriculum b.ed notes in hindi pdf ,