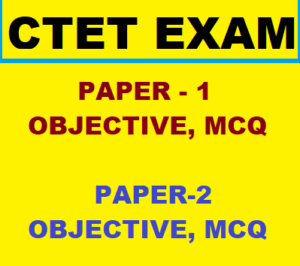अभिप्रेरणा के प्रत्यय अर्थ परिभाषा विशेषताए एवं प्रकार
| Abhiprerana ke prastaavana , Abhiprerana ke arth , abhiprerana ke pratyay , abhiprerana ke paribhaasha , abhiprerana ke visheshatae, abhiprerana ke evan, abhiprerana ke prakaar ,chhaatron ko abhiprerit karanevaalee kaarak . Introduction of Motivation , Meaning of motivation, suffix of motivation, definition of motivation, characteristics of motivation , types of motivation and Factors that motivate students. |
| VVI NOTES के इस पेज में अभिप्रेरणा के प्रस्तावना अभिप्रेरणा के अर्थ , अभिप्रेरणा के प्रत्यय , अभिप्रेरणा के परिभाषा , अभिप्रेरणा के विशेषताए ,अभिप्रेरणा के प्रकार एवं छात्रों को अभिप्रेरित करनेवाली कारक के बारे में वर्णन किया गया है| |
अभिप्रेरणा के प्रस्तावना (Introduction of Motivation)
व्यक्ति किन्ही विशेष व्यवहारों को क्यों करता है ? यह मनोवैज्ञानिकों के लिए सदैव ही एक विवादास्पद प्रश्न रहा है। मैकडुगल ने मूल प्रवृत्तियों (Instincts) के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार को स्पष्ट करने का प्रयास किया। परंतु आधुनिक मनोवैज्ञानिक मूल प्रवृत्तियों को व्यवहार का कारण स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ किसी जाति (Species) विशेष के व्यवहार प्रतिमानों (Behavioural Patterns) को व्यक्त करती है जो जाति विशेष के समस्त सदस्यों में विद्यमान होती है तथा उस जाति विशेष के सदस्य उन्हें अपने वंशजों से जन्म के साथ ही प्राप्त करते हैं । आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्राणी के विभिन्न व्यवहारों को संचालित (Activate), निर्देशित (Direct) तथा संगठित (Organize) करने वाली शक्ति अभिप्रेरणा है । प्राणियों के द्वारा किये जाने वाले विभिन्न व्यवहारों को समझने तथा उनसे संबंधित समस्याओं का समाधान करने में अभिप्रेरणा का ज्ञान महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर सकता है । वास्तव में प्राणी के व्यवहारों को समझने के लिए अभिप्रेरणा के प्रत्यय का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक हैं । प्रस्तुत अध्याय में अभिप्रेरणा की चर्चा की गई है ।
अभिप्रेरणा का प्रत्यय (Concept of Motivation)
| Concept of Motivation | abhiprerana ka pratyay |
अभिप्रेरणा वास्तव में एक परिकल्पित प्रक्रिया है जो प्राणी के व्यवहार के निर्धारण व संचालन से संबंधित होती है। व्यवहार को अनुप्रेरित, सक्रिय, प्रारम्भ अथवा बनाए रखने वाले कारकों को अभिप्रेरणात्मक कारक (Motivational Factors) कहा जाता है । अभिप्रेरणा शब्द प्राणी की सभी प्रकार की अभिप्रेरणात्मक प्रक्रियाओं को इंगित करता है। अभिप्रेरणा एक आन्तरिक शक्ति होती है जो प्राणी को किसी विशिष्ट प्रकार के कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है । अभिप्रेरणा को प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा देखा जाना सम्भव नहीं होता है। यह एक अदृश्य शक्ति होती है जिसके प्रभावों का निरीक्षण करना ही सम्भव होता है । प्राणी क व्यवहार का अवलोकन करके अभिप्रेरणा को समझा जा सकता है। अभिप्रेरणा वास्तव में क्यों के प्रश्न का उत्तर देती है । व्यक्ति खाना क्यों खाता है ? व्यक्ति दूसरों से क्यों लड़ता है ? व्यक्ति वस्तु का संग्रह क्यों करना चाहता है ? व्यक्ति अधिक धन अर्जित क्यों करना चाहता है ? जैसे प्रश्नों का उत्तर अभिप्रेरणा से संबंधित है ।
अभिप्रेरणा” के परिभाषा (Definition of motivation)
| Definition of motivation | Abhiprerana ke paribhaasha |
गुड के अनुसार –
अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारम्भ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है ।
” Motivation is the process of arousing, sustaining and regulating activity. Good
ब्लेयर, जोन्स तथा सिम्पसन के अनुसार –
“अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले व्यक्ति की आन्तरिक शक्तियाँ अथवा आवश्यकतायें उसके वातावरण के विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं ।
Motivation is a process in which the learner’s internal energies or needs are directed towards various goal objects in his environment. Blair, Jones and Simpson.
मैकडोनाल्ड के अनुसार –
“अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर शक्तिपरिवर्तन है जो भावात्मक जागृति तथा पूर्व अपेक्षित उद्देश्य सम्बंध से निर्धारित होता है ।
” Motivation is an energy change within the person characterized by affective arousal and anticipatory goal relation. -F.J.Mcdonald
एटकिन्सन के अनुसार –
“अभिप्रेरणा का सम्बन्ध किसी एक अथवा अधिक प्रभावों को उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति में कार्य करने की प्रवृत्ति को उद्वेलित करने से होता है ।
” The term motivation refers to the arousal of a tendency to act, to produce one or more effects. – Atkinson
ड्रेवर के अनुसार –
“अभिप्रेरणा एक भावात्मक-क्रियात्मक कारक है जो चेतन अथवा अचेतन ढंग से किसी लक्ष्य की ओर व्यक्ति के व्यहार को निर्धारित करने के लिए क्रियाशील होता है ।
” Motivation is an affective conative factor which operates in determining the direction of an individual’s behaviour towards an end or goal apprehended consciously or unconsciously.
-James Drever
उपरोक्त परिभाषाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिप्रेरणा प्राणी में वह आन्तरिक स्थिति अथवा तत्परता है जो उसे किसी विशिष्ट प्रकार के व्यवहार को प्रारम्भ करने तथा उसे कोई निश्चित दिशा देने के लिए प्रवृत्त करती है ।
अभिप्रेरणा की प्रमुख विशेषताए (Main characteristics of motivation)
| Main characteristics of motivation | Abhiprerana kee pramukh visheshataayen |
(i) अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य निदेशित (Goad Directed) होता है अर्थात् अभिप्रेरित व्यवहार का कोई न कोई लक्ष्य अथवा उद्देश्य अवश्य होता है तथा प्राणी इस उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए प्रयासरत रहता है ।
(ii) अभिप्रेरित व्यवहार अधिक प्रबल (Dominated) होता है अर्थात् अभिप्रेरित अवस्था में प्राणी अधिक उत्तेजित (Stimulated), क्रियाशील (Activate) तथा ऊर्जित (Energized ) होता है ।
(iii) अभिप्रेरित व्यवहार चयनात्मक (Selective) होता है अर्थात् अभिप्रेरित अवस्था में प्राणी लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ चयनित प्रतिक्रियायें ही करता है ।
(iv) अभिप्रेरित व्यवहार में निरन्तरता (continuity) होती है अर्थात् अभिप्रेरित व्यवहार एक बार उत्पन्न होने के बाद तब तक निरन्तर चलता रहता है जब तक प्राणी वांछित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर लेता है ।
अभिप्रेरकों के प्रकार (Kinds of Motives)
| abhiprerakon ke prakaar | types of motivators |
अभिप्रेरकों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। मॉसलों (Maslow) के अनुसार अभिप्रेरकों को जन्मजात अभिप्रेरक ( Innate Motives) तथा अर्जित अभिप्रेरक (Acuired Motives) में बाँटा जा सकता है । थाम्पसन (Thompson) महोदय के अनुसार अभिप्रेरकों को स्वाभाविक अभिप्रेरक (Natural Motives) तथा कृत्रिम अभिप्रेरक (Artificial Motives) में बाँटा जा सकता है। गैरेट (Garrett ) के अनुसार अभिप्रेरकों को जैविक अभिप्रेरक (Biogenic Motives), मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक (Psychogenic Motives) तथा सामाजिक अभिप्रेरक (Social Motives) में बांटा जा सकता है |
जन्मजात अभिप्रेरक (Innate Motives)
जन्मजात अभिप्रेरक वे अभिप्रेरक हैं जो व्यक्ति में जन्म से पाए जाते हैं। जैसे—भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा आदि । व्यक्ति में जन्म से पाए जाते हैं। जैसे—भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा आदि ।
अजित अभिप्रेरक (Acquired Motives)
वे प्रेरक जिन्हें प्राणी अपने प्रयासों से प्राप्त करता है अर्जित अभिप्रेरक कहते हैं । जैसे—सामाजिकता, रुचि, प्रतिष्ठा आदि ।
स्वाभाविक अभिप्रेरक (Natural Motives)
स्वाभाविक अभिप्रेरक व्यक्ति में स्वभाव से पाए जाते हैं। जैसे-खेलना, सुख प्राप्त करना आदि ।
कृत्रिम अभिप्रेरक (Artificial Motives)
ये प्रेरक प्राणी के कार्य अथवा व्यवहार को नियंत्रित करने, प्रोत्साहित करने अथवा वांछित दिशा देने के लिए स्वाभाविक अभिप्रेरकों के पूरक के रुप में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे—पुरस्कार, प्रशंसा, दंड आदि ।
जैविक अभिप्रेरक (Biogenic Motives)
जैविक अभिप्रेरक प्राणी की जैविकी आवश्यकताओं के फलस्वरुप उत्पन्न होते हैं । इसके अंतर्गत प्रायः संवेगों को रखा जाता है । जैसे-क्रोध, भय, प्रेम आदि ।
सामाजिक अभिप्रेरक (Sociogenic Motives)
सामाजिक अभिप्रेरक सामाजिक मान्यताओं, सम्बन्धों, परिस्थितियों, आदर्शों आदि के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे-प्रतिष्ठा, सुरक्षा, रचनात्मकता आदि ।
अभिप्रेरकों के उपरोक्त वर्णित वर्गीकरण एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न नही हैं। जन्मजात अभिप्रेरक तथा स्वाभाविक अभिप्रेरक काफी मिलते-जुलते हैं तथा इनका आधार शारीरिक होता है इसलिए इनको कभी-कभी शारीरिक अभिप्रेरक (Physiological Motives) भी कहा जाता है। सीखने में अभिप्रेरणा (Motivation in Learning) शिक्षा प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है । अभिप्रेरणा के प्रत्यय का उचित प्रयोग करके अध्यापक सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को अधिक अच्छे ढंग से सम्पादित कर सकता है। अभिप्रेरित बालक ज्ञानार्जन के लिए तत्पर होते हैं तथा वे शीघ्रता, सरलता व सुगमता से सीख सकते हैं । इसके विपरीत अअभिप्रेरित बालकों की रुचि सीखने में नहीं होती हैं तथा वे सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं । अध्यापक आवश्यकतानुसार अभिप्रेरकों का उपयोग करके बालकों को शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है । शिक्षा प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की उपयोगिता स्वस्पष्ट ही है । कक्षा शिक्षण के अतिरिक्त अन्य शैक्षिक परिस्थितियों में छात्रों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के कार्य में भी अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है । चरित्र-निर्माण में भी अभिप्रेरणा सहायक होती है। अध्यापक बालकों को उत्तम चारित्रिक गुणों तथा आदर्शों को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। बालकों को शिक्षा की महत्ता बता कर शिक्षा की आवश्यकता स्पष्ट की जा सकती है जिससे वे अपने लिए शिक्षा की आवश्यकता को महसूस कर सकें तथा शिक्षा प्राप्ति की ओर अभिप्रेरित हो सके। पढ़ते समय पाठ्य-वस्तु पर ध्यान केन्द्रित कराने में अभिप्रेरणा का उपयोग किया जा सकता है। अभिप्रेरण पाकर बालकों में अध्ययन करने की गति बढ़ जाती है इसलिए शिक्षा प्रदान करते समय अध्यापक को छात्रों को ज्ञान प्राप्ति की ओर अभिप्रेरित करना चाहिए। छात्रों में अभिप्रेरणा जितनी अधिक होगी, शिक्षा प्रक्रिया के सफल होने की सम्भावना भी उतनी ही अधिक होगी । शिक्षा प्रांगणों में अनुशासनहीनता की समस्या वर्तमान समय की एक ज्वलंत समस्या है। इस समस्या का काफी सीमा तक समाधान अभिप्रेरणा द्वारा किया जा सकता है। यदि वालकों को विभिन्न प्रकार के शैक्षिक, सामूहिक, सामाजिक तथा अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए अभिप्रेरित किया जाये, अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार व प्रशंसा तथा अवांछित कार्यों के लिए निंदा व दंड का प्रयोग उचित ढंग से किया जाये तो शिक्षा प्रांगणों में अनुशासन को बनाए रखना सम्भव हो सकेगा । पाठ्यक्रम रचना, शिक्षण विधियों के चयन आदि में भी अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है । पाठ्यक्रम रचना तथा शिक्षण विधियों के चयन में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पाठ्यचर्या ऐसी हो जो बालकों को अभिप्रेरित कर सके। अध्यापक को अपनी शिक्षण विधि का चयन भी अभिप्रेरणा को ध्यान में रखकर करना चाहिए जिससे छात्र अधिकाधिक अभिप्रेरित हो सके । अभिप्रेरणा के द्वारा बालकों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाए जा सकते हैं। पुरस्कार, प्रशंसा, निन्दा, भर्त्सना जैसे कृत्रिम अभिप्रेरकों का उचित ढंग से उपयोग करके अध्यापक वालकों के व्यवहार को वांछित दिशा में निर्देशित कर सकता है।
छात्रों को अभिप्रेरित करनेवाली कारक
| Chhaatron ko abhiprerit karanevaalee kaarak | Factors that motivate students |
1. सीखने की इच्छा (Will to Learn)
अभिप्रेरणा प्रदान करने का प्रथम कदम बालकों में सीखने की इच्छा जागृत करना है। सीखने की प्रक्रिया तब ही सरल, शीघ्र तथा स्थायी होती है जब व्यक्ति सीखने का इच्छुक होता है । यद्यपि कभी-कभी बालक बिना इच्छा के भी कुछ बातें सीख जाते हैं, परंतु सीखने की इच्छा सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है । इच्छा एक अत्यंत साधारण अभिप्रेरक हैं तथा अध्यापक इसका उपयोग सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को गति प्रदान करने में अत्यन्त सहजता से कर सकता है।
2. सीखने में आवेष्टन (Involvement in Learning)
किसी कार्य में आवेष्टित हो जाने पर व्यक्ति उस कार्य को सफलतापूर्वक करने का यथासम्भव प्रयास करता है । आवेष्टन से तात्पर्य किए जाने वाले कार्य में मानसिक रूप से समाविष्ट हो जाने से है । यदि बालकों का लगाव सीखने की प्रक्रिया में होता है तब वे सरलता व शीघ्रता से नवीन बातों को सीख लेते हैं ।
3. आकांक्षा स्तर (Level of Aspiration)
आकांक्षा स्तर सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण अभिप्रेरक का कार्य करता है । आकांक्षा स्तर व्यक्ति के जीवन लक्ष्यों को इंगित करता है । व्यक्ति अपने आकांक्षा स्तर के अनुरुप ही प्रयास करता है । सफलता प्राप्त हो जाने पर उसका भावी आकांक्षा स्तर प्रायः ऊँचा हो जाता है, जबकि असफलता प्राप्त करने पर व्यक्ति का आकांक्षा स्तर नीचा हो जाता है । अध्यापक छात्रों के आकांक्षा स्तर को ऊँचा करा कर उन्हें अधिकाधिक अध्ययन करने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं ।
4. प्रतियोगिता (Competition)
अभिप्रेरणा प्रदान करने की एक अन्य विधि बालकों में प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना है । अध्यापक को अपने छात्रों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। परंतु ईर्ष्या, क्रोध, घृणा आदि पर आधारित प्रतिद्वंदिता को सराहनीय नहीं माना जाता है । प्रतियोगिता के फलस्वरुप बालक कठिन कार्यों को भी करने के लिए अभिप्रेरित होता हैं तथा प्रायः सफलता प्राप्त करते हैं ।
5. सफलता का ज्ञान (Knowledge of Success)
सफलता का ज्ञान भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करता है। यदि बालकों को यह पता है कि उन्होंने क्या सफलतायें प्राप्त की हैं तो वे आगे बढ़ने के लिए अभिप्रेरित होते हैं । परीक्षा के उपरान्त बालकों को अपनी शैक्षिक उपलब्धि का ज्ञान परीक्षा फल —————— या जाता है। सफल छात्र अपनी शैक्षिक उपलिब्ध का ज्ञान परीक्षाफल के ७. अधिकाधिक सफलता प्राप्त करने के लिए तथा असफल छात्र -.के लिए अभिप्रेरित होते हैं। •पियों को दूर करने ——
6. पुरस्कार (Reward)
पुरस्कार प्रशंसा का अधिक स्पष्ट व प्रखर रु. किसी वस्तु, धन, छूट आदि के रुप में दिये जाने वाले पुरस्कार प्रायः बालकों के लिए अत्यंत शक्तिशाली अभिप्रेरक सिद्ध होते हैं । किन्तु पुरस्कारों का प्रयोग अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। ऐसा न हो कि वालक पुरस्कार प्राप्ति के लिए अनुचित तरीकों का प्रयोग करने लगे ।
7. दंड (Punishment)
दंड भी निंदा की तरह से एक निषेधात्मक अभिप्रेरक है जो निंदा से अधिक प्रखर होता है। दंड से तात्पर्य मानसिक अथवा शारीरिक पीड़ा देने से है, जिससे बालक भविष्य में उन कार्यों को न करे। दंड वास्तव में भय पर आधारित होता है इसलिए इसका प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए।
8. प्रतिष्ठा (Prestige)
प्रतिष्ठा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है वह चाहता है कि अपने समूह में अधिकाधिक प्रतिष्ठापूर्ण स्थान प्राप्त करें तथा इसके लिए वह सतत् चेष्टा करता है । बालक भी कक्षा तथा विद्यालय में प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं । प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न छात्रों की अपेक्षायें भिन्न-भिन्न होती हैं । वालक अपनी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के अनुरुप कक्षा में प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है ।
9. प्रशंसा (Praise)
प्रशंसा एक सकारात्मक अभिप्रेरणा है यदि किसी छात्र के अच्छे कार्यों की प्रशंसा की जाती है तो उसके द्वारा उस प्रकार के कार्य को करने की सम्भावना बढ़ जाती है । वास्तव में अपने से बड़े तथा मान्य व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली प्रशंसा बालक को वांछित कार्य करने के लिए उत्तेजित करती हैं । उचित समय तथा स्थान पर की जाने वाली प्रशंसा अभिप्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं ।
10. निंदा (Blame)
निंदा एक निषेधात्मक अभिप्रेरक हैं । निंदा को एक प्रकार का सामाजिक व मानसिक उत्पीड़न माना जा सकता है । निंदा के परिणामस्वरुप बालक अपने व्यवहार में सुधार लाते हैं । अभिप्रेरक के रुप में निन्दा का प्रयोग अत्यन्त सावधानीपूर्वक करना चाहिए।
@@@@ @@@@@ @@ @@ @@ @@@ @ @@ @@ @@ @@@ @@ @ @@@ @@ @@@ @@@ @@ @@ @@ @ @@@ @@@ @@ @ @@@ @@@ @@ @ @ @@@ @@@ @@@ @@ @ @@@ @ @@ @@@ @@@ @@ @@ @@ @@ @@@ @@@ @@@
| vvi notais ke is pej mein abhiprerana ke arth , abhiprerana ke pratyay , abhiprerana ke paribhaasha , abhiprerana ke visheshatae evan abhiprerana ke prakaar ke baare mein jaanakaaree diya gaya hai.Introduction of Motivation , Meaning of motivation, suffix of motivation, definition of motivation, characteristics of motivation , types of motivation and Factors that motivate students. |
| VVI NOTES के इस पेज में अभिप्रेरणा के प्रस्तावना अभिप्रेरणा के अर्थ , अभिप्रेरणा के प्रत्यय , अभिप्रेरणा के परिभाषा , अभिप्रेरणा के विशेषताए ,अभिप्रेरणा के प्रकार एवं छात्रों को अभिप्रेरित करनेवाली कारक के बारे में वर्णन किया गया है | आप इस टॉपिक से सम्बन्धित निचे कमेंट क्र प्रश्न पूछ सकते है | |