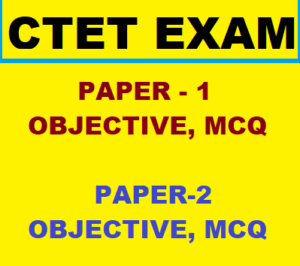Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith B.Ed 1st Semester Notes
| TOPIC | महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बी.एड प्रथम सेमेस्टर के नोट्स |
| विषय | 1O1 – शिक्षा का समाजशास्त्रीय एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य 102 – शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य 103 – लिंग विद्यालय एवं समाज नोट्स 104 – शिक्षा में क्रियात्मक अनुसन्धान नोट्स |
| कोड | 101 ,102 ,103 ,104 |
| सेमेस्टर | प्रथम सेमेस्टर |
| lnfo | इस पेज में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बी.एड के प्रथम सेमेस्टर के सभी (चार पेपर) के नोट्स दिया गया है | |
शिक्षा का समाजशास्त्रीय एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य नोट्स
(101) Perspectives in Sociological and Philosophical bases of Education
(101) shiksha ka samaajashaastreey evan daarshanik aadhaaragat pariprekshy
| विषय | शिक्षा का समाजशास्त्रीय एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य नोट्स , |
| कोड | 101 |
| विश्वविद्यालय | महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बी.एड प्रथम सेमेस्टर |
| सेमेस्टर | प्रथम सेमेस्टर |
| lnfo | यहा से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बी.एड प्रथम सेमेस्टर के पेपर 101 – शिक्षा का समाजशास्त्रीय एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य नोट्स दिया गया है | |
(Short Answer Type Questions – Answer)
प्रश्न a (i) सामाजिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं?
उत्तर-सामाजिक व्यवस्था वह स्थिति या अवस्था है जिसमें सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाले विभिन्न अंग या इकाइयाँ सांस्कृतिक व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित पारस्परिक प्रकार्यात्मक सम्बन्ध के आधार पर सम्बद्ध समग्रता की ऐसी सन्तुलित स्थिति उत्पन्न करते हैं जिससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होती है। सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा सावयवी सिद्धान्त पर आधारित है। इसके अंतर्गत् समाज की विभिन्न इकाइयाँ क्रमबद्ध रूप से परस्पर सम्बद्ध रहती हैं। इन इकाइयों के बीच प्रकार्यात्मक सम्बन्ध पाए जाते हैं। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था किसी न किसी सांस्कृतिक व्यवस्था के अंतर्गत ही क्रियाशील रहती है।
प्रश्न a (ii) प्रयोजनवादी शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य लिखिए।
उत्तर-प्रयोजनवादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं-
(i) सामाजिक कुशलता का विकास,
(ii) नवीन मूल्यों का निर्माण करने की योग्यता का विकास,
(iii) छात्र का विकास,
(iv) गतिशील निर्देशन,
(v) लोकतांत्रिक जीवन की शिक्षा,
(vi) सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलता की योग्यता ।
प्रश्न a (iii) आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है?
उत्तर- आर्थिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण कारक वस्तुओं की उत्पादकता तथा उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना है। यह कार्य शिक्षा, वस्तुओं में सीधे सुधार की अपेक्षा मनुष्य में सुधार करती है। इसलिए शिक्षा आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष के साथ-साथ परोक्ष रूप से भी योगदान देती है। शिक्षा समाज में आर्थिक तथा सामाजिक समाज का विकास करती है। शिक्षा लोगों की वर्तमान और वैज्ञानिक अवधारणाओं तक पहुँच बढ़ाती है। यह नई प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने के लिए लोगों की दक्षता और क्षमता में सुधार करता है। यह संभावित संभावनाओं और श्रम गतिशीलता का ज्ञान बढ़ाता है।
प्रश्न a (iv) प्रयोजनवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ ।
उत्तर- प्रयोजनवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
1. शिक्षा दर्शन की प्रयोगशाला के रूप में-डीवी का कथन है कि शिक्षा और दर्शन एक- दूसरे से सम्बन्धित हैं। दर्शन सिद्धान्तों का निर्माण करते हैं तथा शिक्षा उन्हें कसौटी पर कसते उनकी उपयोगिता की परीक्षा करती है।
2. शिक्षा का सामाजिक अर्थ-प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा की मुख्य विशेषता उसका सामाजिक कार्य है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसका सामाजिक विकास होना चाहिए। उसे सफल लोकतान्त्रिक जीवन बिताना चाहिए। इस सम्बन्ध में बूबेकर ने कहा है-“प्रयोजनवादी सामाजिक मूल्यों को बहुत अधिक महत्त्व देते हैं। समाज सम्मिलित रूप से प्राप्त अनुभव का ढंग है। सामाजिक कार्यों में भाग लेना महत्त्वपूर्ण ढंगों में एक है।”
3. बालक का वास्तविक जीवन का अनुभव-प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा द्वारा बालक को वास्तविक जीवन का अनुभव प्रदान करना चाहिए। इस तरह वे अपने जीवन में सफल हो सकेंगे। उनके अनुसार सच्चा वही नहीं है जो कुछ करके प्राप्त किया जाये। प्रयोजनवादियों का मत है कि बालक स्वयं किसी कार्य को सीखेगा तो वह ज्ञान स्थायी होगा और वह ज्ञान उसके जीवन का अंग बन जायेगा। इस प्रकार का ज्ञान बालक तभी अर्जित कर पायेगा जब उसको जीवन की ठोस परिस्थितियों में रखा जायेगा. साथ ही उसे ऐसा वातावरण प्रदान किया जाय कि वह आदर्श मूल्यों का निर्माण कर सके।
4. बालक का महत्त्व – प्रकृतिवादी विचारधारा की भाँति प्रयोजनवादी भी शिक्षा के क्षेत्र में बालक को अधिक महत्त्व देते हैं। उनके अनुसार बालक को शिक्षा के अनुसार नहीं बल्कि शिक्षा को बालक के अनुसार होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि बालक की शिक्षा उसकी शक्ति, रुचियों, संवेगों और क्षमताओं के अनुरूप होनी चाहिए।
प्रश्न a (v) शिक्षा दर्शन का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
उत्तर – जॉन डीवी ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि “सामाजिक जीवन के लिए शिक्षा को उसी प्रकार आवश्यक बताया है जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है।” दर्शन को परिभाषित करते हुए राधाकृष्णन ने कहा है, “दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कपूर्ण खोज है।” इस प्रकार दर्शन से ही शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण होता है। शिक्षा के प्रत्येक पक्ष के लिए दर्शन परमावश्यक है। जेण्टिल का कथन है कि “जो व्यक्ति इस बात में विश्वास करते हैं कि दर्शन हीन होने पर भी शिक्षा प्रक्रिया उत्तम रीति से चल सकती है वे शिक्षा के अर्थों को पूर्णरूपेण समझने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं।” इसी प्रकार हार्न का मत है कि “शैक्षिक समस्या के प्रत्येक दृष्टिकोण से दार्शनिक आधार की माँग उठती हैं।” फिक्टे का कहना है कि “दर्शन के अभाव में शिक्षा कलापूर्ण स्पष्टता को नहीं प्राप्त कर सकती है। ”
प्रश्न a (vi) शिक्षा में यथार्थवाद का क्या अभिप्राय है?
उत्तर- यथार्थवाद वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारों के प्रति एक दृष्टिकोण है, जिसके अनुसार, जगत की वस्तुएँ यथार्थ हैं अर्थात् जिस वस्तु को हम देख, सुन और छू सकते हैं, वही यथार्थ है। इस प्रकार यथार्थवादी इन्द्रिय ग्राह्य भौतिक पदार्थ और भौतिक संसार को ही सत्य मानते हैं और आध्यात्मिक तत्त्वों की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। जे. एस. रॉस के अनुसार “यथार्थवाद इस बात पर बल देता है कि जो कुछ हम प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं उनके पीछे तथा उनसे मिलता-जुलता वस्तुओं का एक यथार्थ जगत है।” यथार्थवाद को बटलर ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि “यथार्थवाद संसार को सामान्यतः उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है।” इस प्रकार यथार्थवाद इस भौतिक जगत की सत्ता और सत्यता में विश्वास करता है तथा केवल वास्तविक अस्तित्व को ही स्वीकार करता है
प्रश्न a (vii) मानवाधिकारों के शिक्षा की संकल्पना की व्याख्या कीजिए।
उत्तर- सन् 1948 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की प्रस्तावना को प्राप्त करने के लिये मानवाधिकारों का घोषणा-पत्र जारी किया गया। इस घोषणा-पत्र में प्रस्तावना के साथ 30 धाराएँ या अनुच्छेद हैं। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि “विश्व के सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं के अधिकारी हैं।” इस घोषणा-पत्र के अनुच्छेद 26 में कहा गया “प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी है।” इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित सिद्धान्तों को निर्धारित किया गया है-
(1) शिक्षा प्रारम्भिक तथा मूल स्तरों पर निःशुल्क होगी। प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य होगी।
(2) प्राविधिक तथा वृत्तिक शिक्षा को सामान्यतः उपलब्ध कराया जायेगा और उच्च शिक्षा को योग्यता के आधार पर सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिये प्रयास किये जायेंगे।
(3) शिक्षा को मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिये निर्देशित किया जायेगा।
(4) शिक्षा को मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं के सम्मान के लिए समृद्ध बनाया जायेगा।
(5) शिक्षा सभी राष्ट्रों, प्रजातीय तथा धार्मिक समूहों में समझदारी, सहिष्णुता तथा मित्रता को बढ़ाने के लिये कार्य करेगी।
(6) शिक्षा शान्ति स्थापना के लिये विभिन्न क्रिया-कलापों का संचालन करेगी।
(7) अभिभावकों को अपने बच्चों के लिये उपयुक्त शिक्षा का चयन करने का अधिकार होगा
प्रश्न a (viii) बेसिक शिक्षा का क्या तात्पर्य है?
अथवा
बेसिक शिक्षा क्या है?
उत्तर- बेसिक शिक्षा का अर्थ-‘बेसिक’ शब्द का हिन्दी-रूपांतर ‘आधारभूत’ है। इस प्रकार ‘बुनियादी’ शब्द का अभिप्राय भी ‘आधारभूत’ से ही है। इस नवीन शिक्षा को भारत की राष्ट्रीय सभ्यता एवं संस्कृति का आधार बनाया गया है और यह प्रयत्न किया गया कि शिक्षा ऐसी हो, जो बालक की आधारभूत आवश्यकताओं व उसकी रुचियों से घनिष्ठ सम्बन्ध रखे, उसके सर्वाङ्गीण विकास में सहायक हो तथा उसके जीवन की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो। इस शिक्षा-प्रणाली के विषय में कहा गया है कि “यह शिक्षा सभी भारतीयों को ऐसा आधारभूत ज्ञान प्रदान करने के लिए निर्मित की गयी जो उनको अपने वातावरण को बुद्धिमत्तापूर्वक समझने एवं प्रयोग करने में सहायक हो।” यह बेसिक शिक्षा हस्तकला के माध्यम से दी जाती है, ताकि बालक इस शिक्षा का अपने जीवन में उपयोग कर सके।
प्रश्न a (ix) समाजीकरण की परिभाषा दीजिए।
अथवा
समाजीकरण की अवधारणा की संक्षिप्त विवेचना कीजिए।
अथवा
समाजीकरण क्या है?
उत्तर-मनुष्य का जन्म समाज में होता है। समाज में जन्म लेने के पश्चात् वह धीरे-धीरे आसपास के वातावरण के सम्पर्क में आता है और उससे प्रभावित भी होता है। प्रारम्भ में मनुष्य एक प्रकार से जैविक प्राणी मात्र होता है, क्योंकि आहार एवं निद्रा आदि के अतिरिक्त उसे और किसी बात का ज्ञान नहीं होता, अतः उसकी अवस्था बहुत कुछ पशुओं के समान होती है। सामाजिक गुणों का विकास करके ही उसे सामाजिक प्राणी बनाया जाता है। सामाजिक सीख के कारण ही वह जैविक प्राणी से एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। समाजशास्त्र में बच्चे के सामाजिक बनने की इस प्रक्रिया को ही ‘समाजीकरण’ कहा जाता है। स्पष्ट है कि समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। इसी के परिणामस्वरूप व्यक्ति समाज में रहना सीखता है अर्थात् एक सामाजिक प्राणी बनता है। संस्कृति का हस्तान्तरण भी इसी प्रक्रिया के माध्यम से होता है। बोगार्डस के अनुसार, “समाजीकरण वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति एक-दूसरे पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है और इसके द्वारा सामाजिक आत्म-नियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सन्तुलित व्यक्तित्व का अनुभव प्राप्त करता है।”
आधुनिक समाज में अनेक सांस्कृतिक संस्थाएँ-जैसे संगीत अकादमी, नाटक-मण्डली, कवि- सम्मेलन एवं क्लब आदि व्यक्ति के विकास में योग देती हैं। ये संस्थाएँ व्यक्ति को अपनी संस्कृति से परिचित कराती हैं। इनके द्वारा व्यक्ति अपनी प्रथाओं, परम्पराओं, वेश-भूषा, साहित्य, संगीत, कला, भाषा आदि से परिचित होता है और ये संस्थाएँ उसके व्यक्तित्व के विकास में योग देती हैं।
प्रश्न a (x) संस्कृति को परिभाषित कीजिए।
उत्तर-संस्कृति की परिभाषा–संस्कृति के अन्तर्गत मनुष्य के समस्त अर्जित तथा संक्रमित व्यवहार का समावेश होता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार संस्कृति में पैदा होता है। संस्कृति के माध्यम से ही उसका सामाजिक विकास होता है। इसके अन्तर्गत व्यक्तियों की आदतों, विश्वासों, प्रथाओं तथा परम्पराओं के सभी रूप आते हैं जो कि समाज का सदस्य होने के नाते व्यक्ति को सुलभ है। संस्कृति की प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं-
(1) थापर और स्कॉलर के मतानुसार, “संस्कृति को अर्जित या सीखे हुए व्यवहार के प्रतिमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका विशिष्ट तत्त्व समुदाय की सम्पत्ति होती है और जिसका एक विशिष्ट सामाजिक समूह द्वारा विभाजन और हस्तान्तरण होता है।”
(2) बोगार्डस-बोगार्डस ने समूह में प्रचलित विश्वासों, रीति-रिवाजों तथा व्यवहार के प्रतिमानों के आधार पर संस्कृति को परिभाषित किया है। बोगार्डस के शब्दों में, “संस्कृति समूह से सम्बद्ध रीति-रिवाजों और प्रचलित व्यवहार व प्रतिमानों से बनती है। यह समूह की सम्पत्ति है। यह मूल्यों की एक ऐसी पूर्ववर्ती समष्टि है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का जन्म होता है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें व्यक्ति विकसित और परिपक्व होते हैं।”
(3) ए0डब्ल्यू ग्रीन- ग्रीन ने संस्कृति के अन्तर्गत मनुष्य की समस्त भौतिक तथा अभौतिक उपलब्धियों को शामिल किया है। ग्रीन के शब्दों में, “संस्कृति, ज्ञान, व्यवहार, विश्वास तथा उपकरण आदि की समाज द्वारा संक्रमित व्यवस्था है।”
( 4 ) फ्रैंक – फ्रैंक ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए यह उल्लेख किया है कि “संस्कृति एक ऐसा प्रभाव है जो व्यक्ति पर प्रभाव रखता है और उसके व्यक्तित्व की विचारों, धारणाओं तथा विश्वासों आदि के द्वारा जो उसे सामुदायिक जीवन से प्राप्त होते हैं, उनको साँचे में ढालने की चेष्टा करता है।”
उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि संस्कृति में मनुष्य समाज की वे सभी चीजें आती हैं जिन्हें मनुष्य ने समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त किया है। इसे व्यक्ति अन्य लोगों से सीखता है तथा परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से दूसरों को सिखाता भी है।
प्रश्न a (xi) सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा ।
उत्तर- सामाजिक परिवर्तन के लिए हम निम्नलिखित विद्वानों की परिभाषाएँ दे रहे हैं-
1. सर जोन्स – “सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक संगठन के किसी अंग में अन्तर अथवा रूपान्तर को वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है।”
2. गिलिन तथा गिलिन- “सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। चाहे ये परिवर्तन भौगोलिक दशाओं के परिवर्तन में हुए हों अथवा सांस्कृतिक साधनों में अथवा जनसंख्या की रचना या सिद्धान्तों के परिवर्तन में अथवा प्रयास से अथवा समूह अन्दर ही आविष्कारों के फलस्वरूप ही हुए हों।”
3. मेरिल तथा एल्ड्रेज- “सामाजिक परिवर्तन का यह अर्थ है कि बहुत बड़ी संख्या में व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कुछ दिनों पहले अथवा उनके पूर्वजों के कार्य से भिन्न है अर्थात् जब मानव- व्यवहार संशोधित हो रहा है तो वह सामाजिक परिवर्तन का संकेत है।’
प्रश्न a (xii) दर्शन और शिक्षा के सम्बन्ध की चर्चा कीजिए।
उत्तर- शिक्षा और दर्शन का सम्बन्ध
डॉ० राधाकृष्णन का कथन है, “दर्शन यथार्थता के स्वरूप का तार्किक ज्ञान है।” इसी कारण कहा जाता है कि शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ सम्बन्ध है। शिक्षा की प्रक्रिया व्यक्ति को अपने जीवन में पूर्ण बनाने का प्रयास करती है। व्यक्ति को पूर्ण बनाने तथा उसके विकास के लिए अनुभव आवश्यक होता है। दर्शन अनुभव प्राप्त करने में विशेष रूप से सहायता प्रदान करता है। स्पष्ट है कि शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ सम्बन्ध है। बिना दर्शन की सहायता शिक्षा को पूर्णतः नहीं मिल सकती।
.
‘शिक्षा दर्शन’ दर्शन की एक शाखा है। शिक्षा दर्शन ऐसे प्रश्नों से सम्बन्धित है-जैसे शिक्षक क्या है ? शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए? आदि। शिक्षा दर्शन से सम्बन्धित अनेक समस्याओं पर गम्भीरता से विचार करता है और उनका समाधान भी करता है। शिक्षा दर्शन के उद्देश्य के विषय में कनिंघम ने इस प्रकार लिखा है- “शिक्षा दर्शन अनेक दार्शनिक विचारधाराओं द्वारा निकाले गये सिद्धान्तों के प्रयोग के रूप में इन विचारधाराओं से भिन्न समस्याओं की खोज के लिए निर्देशन लेता है-” निम्नलिखित पंक्तियों में हम यह स्पष्ट करेंगे कि दर्शन किस प्रकार शिक्षा को प्रभावित करता है और शिक्षा किस प्रकार दर्शन को प्रभावित करती है-
1. दर्शन शिक्षा का पूरक है-दर्शन शिक्षा का पूरक है। इसका मुख्य कारण यह है कि शिक्षण कला दर्शन के अभाव में पूर्णता प्राप्त करने में असमर्थ रहती है। जर्मन दार्शनिक फिक्टे के अनुसार, “दर्शन के अभाव में शिक्षा की कलापूर्ण स्पष्टता प्राप्त नहीं कर सकती।”
2. दर्शन शिक्षा का आधार है-शिक्षा का आधार दर्शन है। जेण्टाइल के अनुसार, “बिना दर्शन की सहायता से शिक्षा प्रक्रिया सही मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती।”
3. दर्शन शिक्षा की अमूल्य सहायता करता है-दर्शन शिक्षा की अमूल्य सहायता करता है। बटलर के शब्दों में- “दर्शन शिक्षा के प्रयोगों के लिए एक पथ-प्रदर्शक है, शिक्षा अनुसन्धान के क्षेत्र के रूप में दार्शनिक निर्णय हेतु निश्चित सामग्री को आधार के रूप में प्रदान करती है
”
4. दर्शन शिक्षा का सिद्धान्त है-दर्शन शिक्षा का सिद्धान्त है। ड्यूवी के अनुसार, “अपने सामान्यतम रूप में दर्शन शिक्षा सिद्धान्त है। ”
प्रश्न a (xiii) सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं? उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए ।
उत्तर- सामाजिक परिवर्तन
संसार की समस्त वस्तुएँ, विचार, सभ्यता, संस्कृति आदि परिवर्तनशील हैं। समाज भी परिवर्तनशील है। जब सामाजिक व्यवस्था प्रक्रिया या सामाजिक संरचना में स्पष्ट रूप से कोई अन्तर दृष्टिगोचर होता है तब हम उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, “सामाजिक संरचना अथवा सामाजिक सम्बन्धों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं।
जेन्सन ने सामाजिक परिवर्तनों को लोगों के कार्य करने तथा विचार करने की पद्धतियों में रूपान्तरण कहकर परिभाषित किया है। डॉसन एवं गेटिस के अनुसार, “सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है क्योंकि समस्त संस्कृति अपनी उत्पत्ति, अर्थ एवं प्रयोग में सामाजिक हैं।
इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में कुछ प्रमुख बातें होती हैं, जो निम्नलिखित हैं-
(1) सामाजिक परिवर्तन का सम्बन्ध किसी व्यक्ति या समूह-विशेष के जीवन में होने वाले परिवर्तनों से नहीं है। सामाजिक परिवर्तन वास्तव में सामुदायिक परिवर्तन से सम्बन्धित है
(2) सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है।
(3) सामाजिक परिवर्तन की गति असमान होती है।
(4) सामाजिक परिवर्तन की गति समय से प्रभावित होती है।
(5) सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी कठिन है।
प्रश्न a (xiv) रूसो के अनुसार निषेधात्मक शिक्षा से क्या तात्पर्य है? सोदाहरण समझाइए।
उत्तर-निषेधात्मक शिक्षा-निषेधात्मक शिक्षा वह शिक्षा है जो बालक की प्रवृत्तियों और शक्तियों के अनुसार दी जाती है। “बालकों को शिक्षा में सबसे अनिवार्य भाग उन्हें अपनी क्षमता, कमजोरी और निर्भरता का अनुभव करना है और उस आवश्यकता के भारवाहन को धारण कराना है जो प्रकृति ने मानव जाति पर रखा है।” इस अनुभव एवं आवश्यकता के लिए आरम्भ से बालकों को निषेधात्मक शिक्षा देने के लिए कहा है। यह बालकों को प्रौढ़ों के गुण प्रदान नहीं करती किन्तु दुर्गुणों से उसकी रक्षा करती है। यह बालक को पहले ‘गुण’ और ‘सत्य’ के सिद्धान्त नहीं पढ़ाती वरन् हृदय की पाप से तथा मस्तिष्क की भ्रम से रक्षा करती है। रूसो का कथन है, “पुस्तकें, बालक और वस्तुओं के बीच में आ जाती हैं और उसे अपने अनुभव द्वारा सीखने देती हैं।” अतः बालकों को अनुभव प्राप्त करने के लिए उन्हें कुछ समय के लिए पुस्तकों से दूर रखना चाहिए क्योंकि वस्तुएँ ही अनुभव ग्रहण करने का साधन होनी चाहिए। रूसो ने उक्त दोनों प्रकार की शिक्षा में अन्तर स्पष्ट करते हुए लिखा है, “मैं निश्चयात्मक शिक्षा उसे कहता हूँ जो समय से पहले मस्तिष्क को बनाना चाहती है और बालक को ऐसे कामों को सिखाना चाहती है जो प्रौढ़ों से सम्बन्ध रखते हैं। मैं निषेधात्मक शिक्षा उसे कहता हूँ जो ज्ञान देने के पहले ग्रहण करनेवाले अंगों को दृढ़ बनाती है और जो इन्द्रियों के उचित उपयोग से विवेक शक्ति को बढ़ाती है। इसका तात्पर्य आलस्य में समय बिताना नहीं है, वह इससे बहुत दूर है। यह गुण प्रदान करती है, वरन् दुर्गुण से बचाती है। यह सच बोलना नहीं सिखाती, वरन् झूठ से बचाती है। यह बालकों को सत्य की ओर ले जाने, समझने और अपनाने के लिए तैयार कर देती है। यह बालक को सत्य की ओर नहीं ले जाती जब तक उसमें सत्य को पहचानने और उससे प्रेम करने की शक्ति उत्पन्न नहीं हो जाती है।
प्रश्न a (xv) यथार्थवाद की प्रमुख विशेषताएँ ।
उत्तर-
यथार्थवाद की प्रमुख विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं-
(1) यथार्थवादी कल्पना को कोई स्थान नहीं देते वरन् यह वास्तविक या भौतिक तथ्यों को ही स्वीकार करते हैं।
(2) यथार्थवाद इस प्रत्यक्ष भौतिक जगत को ही वास्तविक मानता है। उसके अनुसार, इस लोक से परे कोई अन्य लोक नहीं है। इस प्रकार यह विचारधारा वस्तुनिष्ठता दृष्टिकोण पर बल देती है। यह विचारधारा आत्मा-परमात्मा के अस्तित्व के विचार को नहीं मानती। यह आत्मा को न मानकर उसको भौतिक सत्ता के रूप में स्वीकार करती है।
(3) यथार्थवादी निरीक्षण और प्रयोग में विश्वास करते हैं। वह उस समय तक किसी अनुभव को सत्य स्वीकार नहीं करते जब तक कि उसका वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण नहीं कर लेते।
(4) यह दार्शनिक विचारधारा निरीक्षण, अवलोकन तथा प्रयोग पर बल देती है। इसके अनुसार किसी अनुभव को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि वह निरीक्षण व प्रयोग की कसौटी पर सिद्ध न हो गया हो।
(5) प्राकृतिक तत्त्वों व सामाजिक संस्थाओं का महत्त्व ।
प्रश्न a (xvi) आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य।
अथवा
आदर्शवादी शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
आदर्शवादी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य मानते हैं-
1. व्यक्तित्व का विकास अथवा आत्मानुभूति – आदर्शवाद मनुष्य को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानता है। इस दर्शन के समर्थक व्यक्ति के व्यक्तित्व को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान देते हुए उसके व्यक्तित्व का विकास करने पर बल देते हैं। व्यक्तित्व के विकास का अर्थ है आत्मानुभूति अथवा आत्म-साक्षात्कार। जेण्टिल के कथनानुसार, “आत्मानुभूति शिक्षा का अन्तिम लक्ष्य है।”
2. आध्यात्मिक विकास करना – आदर्शवाद के अनुसार भौतिक जगत् की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत् अधिक महत्त्वपूर्ण है। अतः शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानव का आध्यात्मिक विकास करना है। आध्यात्मिक विकास के लिए आदर्शवादियों ने उन मूल्यों तथा तथ्यों की प्राप्ति को आवश्यक समझा है, जो शाश्वत् है और सब देशों तथा कालों में उपयोगी और सर्वमान्य है
3. सत्यं, शिवम् तथा सुन्दरम् को विकसित करना-आदर्शवादियों का विश्वास है कि आध्यात्मिक जगत् को उन्नति के लिए सत्यं शिवं, सुन्दरम् जैसे चिरन्तन मूल्यों को विकसित करना आवश्यक है। जब तक इन मूल्यों को विकसित नहीं किया जायेगा तब तक आध्यात्मिक पूर्णता नहीं होगी। इन मूल्यों का विकास शिक्षा द्वारा सम्भव है।
4. सांस्कृतिक सम्पत्ति की रक्षा, विकास तथा हस्तान्तरण – आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का एक उद्देश्य सांस्कृतिक उन्नति करना है। शिक्षा के द्वारा संस्कृति का संरक्षण, विकास तथा हस्तान्तरण होता है। विलियम हाकिंग का विचार है कि “जाति द्वारा संचित की गयी संस्कृति को जाति के युवा लोगों तक पहुँचाने का उत्तरदायित्व शिक्षा का है। इस प्रकार युवा पीढ़ी को इन अनुभवों का लाभ मिल जाता है, जो जाति के संस्कृति के रूप में संचित किये जाते हैं।”
प्रश्न a (xvii) आदर्शवाद में विद्यार्थी का स्थान।
उत्तर-
आदर्शवाद और बालक- आदर्शवादी बालक को एक पौधे के रूप में मानते हैं, जिसे मनचाहा रूप दिया जा सकता है। आदर्शवाद के अनुसार बालक कँटीली झाड़ी है जिसे साज-सँवार कर उचित रूप दिया जा सकता है। एमरसन ने इसीलिए कहा है, “एक सन्तुलित, सम्बद्ध, समन्वित व्यक्तित्व वही है जिससे व्यक्ति ने अपने मन, वचन और कर्म में समन्वय कर लिया है और वह जो सोचता है, वही अनुभव करता है और वही कार्य करता है।” इस दृष्टि से आदर्शवादी बालक में सद्गुण एवं सन्तुलित व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं।
प्रश्न a (xviii) अनौपचारिक शिक्षा।
उत्तर-
जनसंख्या की निरन्तर वृद्धि से पढ़ने वालों की संख्या में अनवरत वृद्धि होने से और मध्यावधि में ही विद्यालय छोड़ देने वाले व औपचारिक शिक्षा पद्धति के नियमों के प्रतिबन्धों से शिक्षा- संस्थाओं में प्रवेश न पा सकने वाले बालक-बालिकाओं की संख्या बढ़ती जाने से ये संस्थागत सुविधाएँ पर्याप्त सिद्ध हुईं। परिणामस्वरूप शिक्षा में आमूल परिवर्तन के विचार व्यक्त किए गए तथा उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु एक सशक्त विकास की खोज का प्रयास अनौपचारिक शिक्षा के रूप में प्रस्फुटित हुआ। स्पष्टतः अनौपचारिक शिक्षा सर्वत्र औपचारिक शिक्षा के अनुसार कार्य के रूप में एक महत्त्वपूर्ण विकल्प तथा उपयोगी कदम है।
विद्यालय में इतर जीवन जीविका से सम्बन्धित औपचारिक शिक्षा की अवधारणा एवं उसके लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए कहा जा सकता है कि औपचारिकताओं से लचीली यह शिक्षा प्रमुख रूप से, सिखाने की नहीं, स्वतः सीखने की प्रक्रिया पर अधिक बल प्रदान करती है और ‘शिक्षार्थी जो सीखना चाहे, जब सीखना चाहे और जहाँ सीखना चाहे’ के सिद्धान्त पर अग्रसर होती है। इस हेतु शिक्षा उन सभी. सम्भव वस्तुओं से देना वांछनीय है, जिनका सम्बन्ध बालक और समाज के दैनिक परिसर से हो। अतः शिक्षा मनोविज्ञान और अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि औपचारिक शिक्षा में भी अनौपचारिक शिक्षा पद्धतियों का समावेश अभीष्ट है अतएव सामाजिक जीवन में निष्णात होने के लिए औपचारिक शिक्षान्तर्गत अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम, यथा-सामाजिक क्रियाएँ तथा उनके प्रतीकों-पत्र-पत्रिका, वाचनालय-पुस्तकालय, खेलकूद, रेडियो-टेलीविजन, मेले, हाट, नृत्यगृह- नाट्यशाला, पर्यटन-देशाटन, कला-संस्कृति, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्राकृतिक स्थलों के भ्रमण, गोष्ठी-परिचर्चा आदि को सम्मिलित करना अपेक्षित है, जिससे शैक्षिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो सके और शिक्षा देश के सृजन से सहज ही जोड़ी जा सके। नये-नये आविष्कारों और अनुभवों का विवरण तत्काल अनौपचारिक साधनों से ही हो पाता है।
प्रश्न a (xix) प्रजातान्त्रिक शिक्षा की विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर-
(i) इससे नेतृत्व का विकास होता है। ।
(ii) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय भावना का विकास होता है।
(iii) जनतन्त्री शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों को नागरिकता का प्रशिक्षण देना है।
(iv) जनतन्त्र के मूल्यों का विकास होता है
(v) प्रजातान्त्रिक शिक्षा से उत्तम अभिरुचियों का विकास होता है।
(vi) इससे व्यावसायिक कुशलता का विकास होता है।
(vii) इससे विचार-शक्ति का विकास होता है।
(viii) इससे सामाजिक दृष्टिकोण का विकास होता है।
(ix) इससे व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास होता है।
प्रश्न a (xx) शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य क्या हैं?
उत्तर-
जब शिक्षा मनुष्य को किसी व्यवसाय के लिए तैयार करे अथवा यह क्षमता और कुशलता प्रदान करे कि वह अपनी रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या हल करने में समर्थ एवं सफल हो जाय तो वहाँ शिक्षा का लक्ष्य व्यावसायिक कहा जाता है। इस उद्देश्य को शिक्षाशास्त्रियों ने कई नाम दिये हैं जैसे दाल-रोटी का उद्देश्य, जीविका का उद्देश्य इत्यादि। ये सब जीविकोपार्जन या धनोपार्जन की ओर संकेत करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को स्वावलम्बी बनाया जाय और कमाने के योग्य बनाया जाय तो वहाँ व्यावसायिक उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य का यह सबसे बड़ा गुण है। भोजन, वस्त्र, आवास की सुविधा और सुख इस उद्देश्य से प्राप्त होते हैं, व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। अतः जीवन और अस्तित्व, सुख और स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए यह उद्देश्य अत्यावश्यक है।
धनोपार्जन होने से लोग कला, साहित्य, संगीत, कौशल आदि के विकास की ओर ध्यान देते हैं। व्यक्ति की निष्क्रियता दूर होती है और वह काम में लगा रहता है-लोगों में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, उत्साह, स्वप्रयत्नशीलता लगन के साथ काम करने की भावना, संतोष आदि का विकास होता है।
इस उद्देश्य के कारण मनुष्य अपने आपको भौतिक सुख के लिए बना लेता है। धन कमाने के पीछे स्वास्थ्य, सामाजिकता, शीलता आदि को भूल जाता है। आदर्शों को भी वह नहीं मानता है। उसमें दूषित मनोवृत्ति भी आ जाती है। समाज में धनी और गरीब दो वर्ग बन जाते हैं और वर्ग-संघर्ष होता है। धनिकों के हाथ में सत्ता केन्द्रित हो जाती है और झूठ, भ्रष्टाचार, चोर-बाजारी आदि होने लगती है। जेजस क्राइस्ट ने कहा है कि “मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रह सकता।” अर्थात् उसमें अन्य मानवीय गुण होना जरूरी है। बी. डी. भाटिया ने भी संकेत किया है कि “एक विशुद्ध व्यावसायिक प्रशिक्षण जीवन के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण को संकुचित बना देती है। यह एक अच्छा यांत्रिक, अच्छा डॉक्टर, अच्छा वकील, मिस्त्री, अच्छा बिजलीवाला कारीगर बन सकता है, न कि एक अच्छा मनुष्य । ”
आधुनिक युग में जीविकोपार्जन को ही शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य समझा जा रहा है तथा अभिभावकों एवं छात्रों का यही उद्देश्य रहता है कि किस प्रकार पढ़-लिखकर अधिक-से-अधिक धन कमायें। विषयों के चुनाव में भी छात्र इसी प्रकार के विषयों को चुनते हैं जिनसे नौकरी जल्दी तथा पैसे वाली मिले। अतः आवश्यक है कि विचारक और शिक्षाशास्त्री लोगों को इस उद्देश्य की सीमायें बतायें तथा इसके साथ अन्य उद्देश्यों को भी प्रधानता दें।
प्रश्न b (i) गाँधीजी की बुनियादी शिक्षा ।
उत्तर-
बुनियादी शिक्षा योजना
बुनियादी शिक्षा योजना का सूत्रपात-गाँधीजी अपने समाचार-पत्र ‘हरिजन’ में 2 अक्टूबर, 1937 ई0 में एक लेख लिखा जिसमें शिक्षा के प्रति अपना दृष्टिकोण प्रकट किया और वर्धा नामक स्थान पर 22 व 23 अक्टूबर, 1937 ई0 को देश के शिक्षाविदों की एक सभा बुलाई। इस सम्मेलन में देश के कोने-कोने से लोग आये और शिक्षा के नव-निर्माण में भाग लिया। यहीं से योजना का सूत्रपात हुआ।
बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य-गाँधीजी ने बुनियादी शिक्षा के निम्न उद्देश्य कहे हैं-
(क) सभी बालक-बालिकाओं को भारत का उत्तम नागरिक बनाना।
(ख) सभी बालक-बालिकाओं में भारतीय संस्कृति का विकास करना ।
(ग) बालक-बालिकाओं के मन, मस्तिष्क, हाथ और आत्मा का विकास
(घ) सर्वोदय समाज की स्थापना करना।
(ङ) धनोपार्जन की क्षमता प्रदान करके उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना।
प्रश्न b (ii) शिक्षा में यथार्थवाद ।
उत्तर-
शिक्षा में यथार्थवाद कई रूपों में हमारे सामने आता है। इसके प्रमुख रूप निम्न प्रकार हैं-
1. मानवतावादी यथार्थवाद – मानवतावादी यथार्थवादियों का कहना है कि शिक्षा यथार्थवादी होनी चाहिए जिससे मानव जीवन सुखमय एवं समृद्ध बन सके। इस दृष्टिकोण से उन्होंने प्राचीन रोमन एवं यूनानी साहित्य के अध्ययन पर बल दिया क्योंकि जीवन को सफल एवं समृद्ध बनाने के लिए समस्त ज्ञान इस साहित्य में उपलब्ध है। मानवतावादी इस साहित्य के अध्ययन को व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक मानते हैं।
2. सामाजिक यथार्थवाद – यथार्थ के इस रूप का विकास प्राचीन परम्परावादी पुस्तकीय ज्ञान के विरोध स्वरूप हुआ। सामाजिक यथार्थवादियों का कहना है कि शिक्षा शब्द जाल मात्र नहीं है वरन् वह जीवन को विकास के मार्ग पर ले चलने का साधन है। यथार्थवाद के इस रूप के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य जीवन को सभ्य, सुन्दर तथा उपयोगी बनाना है। यह विद्यालय को ऐसा स्थान मानता है जहाँ कृत्रिम ज्ञान के स्थान पर व्यावहारिक सफल एवं सुखी जीवन का निर्माण होता है।
3. ज्ञानेन्द्रिय यथार्थवाद – शिक्षा के क्षेत्र में यथार्थवाद के इस रूप का विकास मानवतावादी तथा सामाजिक दोनों प्रकार के यथार्थवाद के मिश्रण तथा विज्ञान के परिणामस्वरूप हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञानेन्द्रिय यथार्थवाद का अन्य रूपों की अपेक्षा अधिक प्रभाव हुआ। इसके अनुसार समस्त ज्ञान का आधार ज्ञानेन्द्रियाँ हैं।
प्रश्न b (iii) प्रयोजनवाद एवं पाठ्यक्रम।
उत्तर-
प्रयोजनवाद एवं पाठ्यक्रम निश्चित उद्देश्यों के बिना निश्चित पाठ्यक्रम सम्भव नहीं है। प्रयोजनवाद के अनुसार मनुष्य के अनुभव और आवश्यकताएं बदलती रही हैं, अतः पाठ्यक्रम भी बदलते रहना चाहिए। पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में उनके विचार ही उनके सिद्धान्त बन गये।
1. उपयोगिता का सिद्धान्त-बच्चों को उन्हीं विषयों एवं क्रियाओं का ज्ञान देना चाहिए, जो उनके लिए उपयोगी हो ।
2. बालक की रुचि का सिद्धान्त-बच्चों की स्वाभाविक रुचियों का ध्यान रखना पाठ्यक्रम के निर्माण का दूसरा सिद्धान्त है। डीवी के अनुसार बालकों की प्रवृत्ति गतिशीलता होती है, अतः उन्हें स्वाभाविक प्रवृत्तियों और रुचियों के आधार पर ही शिक्षा देनी चाहिए।
3. क्रिया का सिद्धान्त-प्रयोजनवाद में क्रिया को अधिक महत्त्व देते हैं। उनके अनुसार पाठ्यक्रम का सम्बन्ध बच्चों की वास्तविक क्रियाओं, इन क्रियाओं से प्राप्त अनुभवों और भावी व्यवसायों इन तीनों से होना चाहिए। क्रिया पाठ्यक्रम का मुख्य आधार है।
4. बालक के अनुभव का सिद्धान्त-प्रयोजनवाद के पाठ्यक्रम में अनुभव को अधिक महत्त्व दिया गया है। सामाजिक अनुभवों को प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम का सिद्धान्त मानते हैं।
प्रश्न b (iv) प्रयोजनवाद का शिक्षा पर प्रभाव।
उत्तर-
प्रयोजनवाद का शिक्षा पर प्रभाव।
प्रयोजनवाद ने दर्शन के रूप में कम, परन्तु व्यवहार के रूप में शिक्षा को बहुत प्रभावित किया। य शिक्षा दर्शन के रूप में प्रयोजनवाद एक प्रगतिशील दर्शन है। वह शिक्षा को सामाजिक गतिशील और विकास की प्रक्रिया मानता है। इस वाद के इस विचार ने प्रगतिशील शिक्षा को जन्म दिया है। यथार्थवाद एवं आदर्शवाद ने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक आधार ही दिये थे, प्रयोजनवाद ने एक तीसरा आधार दिया- सामाजिक आधार ।
शिक्षा का रूप व्यापक और विस्तृत हो गया और अब शिक्षा का उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन हो गया। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया हो गयी है। शिक्षा के माध्यम से समाज का पोषण हो रहा है। शिक्षा बालक की स्वाभाविक रुचियों एवं योग्यताओं को ध्यान में रखकर दी जाने लगी है।
अतः शिक्षा जीवन के लिए नहीं है, बल्कि अब शिक्षा जीवन का लक्ष्य है। वर्तमान अधिक मूल्यवान है। प्रयोजनवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नयी क्रान्ति को जन्म दिया। कक्षा में छात्रों की सक्रियता बढ़ गयी। शिक्षक रोमांचित हो गये।
प्रश्न b (v) मानवतावाद एवं पाठ्यक्रम।
उत्तर-
मानवतावाद एवं पाठ्यक्रम-मानवतावाद का शिक्षा दर्शन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उद्देश्यों के अनुसार पाठ्यक्रम बनाने की बात करता है। बूबेकर के अनुसार, “मानवतावाद मानव स्वभाव एवं मानवीय दृष्टिकोण पर बल देता है।”
इस दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों का समावेश हो जो मनुष्य के जीवन को सफल एवं सुखमय बनाने के लिए आवश्यक है। टैगोर, गाँधी आदि की दृष्टि में शिक्षा का उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय एवं उसकी अच्छाइयों को शिक्षा के कार्यक्रमों में समाविष्ट करना है। अतः पाठ्यक्रम में मानवतावादी कला, शिल्प व अन्य विषयों का समावेश होना चाहिए। उनके अनुसार जीवन में जो कुछ भी उत्तम है उसका समावेश पाठ्यक्रम में होना चाहिए
मैसलो एवं अन्य मनोवैज्ञानिक के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को यह बताता है कि जीवन मूल्यवान है एवं जीने की इच्छा करना ज्यादा महत्त्वपूर्ण है बजाय मरने की इच्छा से परन्तु पाठ्यक्रम में विज्ञान का विशेष स्थान है। मानव को शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए केवल ज्ञान ही आवश्यक नहीं है वरन् उसके लिए कार्य-अभ्यास भी आवश्यक है।
प्रश्न b (vi) प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएँ ।
उत्तर-
प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं-
1. बालक की स्वतन्त्रता पर बल-प्रकृतिवाद की एक सैद्धान्तिक विशेषता यह है कि ये शिक्षा के क्षेत्र में बालक की स्वतन्त्रता पर बल देते हैं। बाल के समुचित विकास के लिये स्वतन्त्रता अनिवार्य है। बालक को अपनी रुचि, योग्यता एवं इच्छा के अनुसार विकसित होने के लिये सुविधा प्रदान करनी चाहिए। शारीरिक दण्ड, भय, बाध्यता एवं चिन्ता आदि से बालक का विकास स्वाभाविक नहीं रह पाता। अतः प्रकृतिवाद ने इन सब का विरोध किया है।
2. पुस्तकीय शिक्षा का विरोध-प्रकृतिवादी शिक्षा मान्यताओं में पुस्तकों का विरोध किया गया है तथा वास्तविक शिक्षा के लिये पुस्तकों को अनावश्यक माना गया है। पुस्तकीय ज्ञान व्यावहारिक नहीं होता। बच्चों को व्यावहारिक रूप से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, यह अनुभव, निरीक्षण एवं स्वयं करके सीखने से ही प्राप्त हो सकता है |
3. शिक्षा बालक केन्द्रित होनी चाहिए-शिक्षा एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न पक्ष सम्मिलित हैं, जैसे कि शिक्षक, छात्र तथा पाठ्यक्रम। प्रकृतिवाद की मान्यता है कि शिक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्त्व बालक का ही होना चाहिए अस्तु शिक्षा बाल केन्द्रित होनी चाहिए, अर्थात् यह कहा जा सकता है कि शिक्षा बालक के लिये है न कि बालक शिक्षा के लिये। बालक पर समाज के अन्य वयस्क पुरुषों के विचार थोपे नहीं जाने चाहिए। शिक्षा का स्वरूप बालक की क्षमता, रुचि एवं स्वभाव के अनुसार होना चाहिए। शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम तथा शिक्षा के उद्देश्यों आदि का निर्धारण बालक के हितों के अनुसार होना चाहिए ।
4. प्रकृति का अनुसरण अनिवार्य है-प्रकृतिवादी सिद्धान्तों में सर्वाधिक महत्त्व इस सूत्र का है- प्रकृति का अनुसरण का करना। यह महा-सूत्र प्रसिद्ध प्रकृतिवादी शिक्षाशास्त्री कॉमेनियम ने प्रदान किया था। इस मान्यता के अनुसार बालक का स्वाभाविक विकास केवल प्राकृतिक वातावरण में ही हो सकता है। कृत्रिम वातावरण में विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं चल सकती। वास्तव में स्वभाव से बालक अच्छा ही होता है। उसे तो कृत्रिम सामाजिक वातावरण ही भ्रष्ट कर देता है।
प्रश्न b (vii) नालन्दा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक विशेषताओं का प्राचीन सन्दर्भ में वर्णन कीजिए।
उत्तर-
नालन्दा विश्वविद्यालय में न केवल भारत के कोने-कोने से अपितु चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया, मध्य एशिया आदि देशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। ह्वी-ली यहाँ के विद्यार्थियों की संख्या दस हजार बताता है। ज्ञात होता है कि यहाँ अध्ययन-अध्यापन का स्तर अत्यन्त उच्चकोटि का था । प्रवेश के लिए एक कठिन परीक्षा ली जाती थी जिसमें दस में दो या तीन विद्यार्थी ही मुश्किल से सफल हो पाते थे। यहाँ के स्नातकों का बड़ा सम्मान था तथा देश में कोई भी उनकी समानता नहीं कर सकता था। इसी कारण यहाँ प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों की अपार भीड़ लगी रहती थी।
यद्यपि नालन्दा महायान बौद्धधर्म की शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था तथापि यहाँ अन्य अनेक विषयों की शिक्षा भी समुचित रूप से प्रदान की जाती थी। पाठ्यक्रम में महायान तथा बौद्धधर्म के अठारह सम्प्रदायों के ग्रन्थों के अतिरिक्त वेद, हेतुविद्या, शब्दविद्या, योगशास्त्र चिकित्सा, तंत्रविद्या, सांख्य दर्शन के ग्रन्थों आदि की शिक्षा व्याख्यानों के माध्यम से दी जाती थी। विभिन्न विषयों के प्रकाण्ड विद्वान् प्रतिदिन सैकड़ों व्याख्यान देते थे जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को उपस्थित होना आवश्यक था। हुएनसांग जिसने स्वयं यहाँ 18 महीने तक रहकर अध्ययन किया लिखता है कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में अत्यन्त उच्चकोटि के विद्वान् निवास करते थे। एक हजार व्यक्ति ऐसे थे जो सूत्रों और शास्त्रों के बीस संग्रहों का अर्थ समझा सकते थे, 500 व्यक्ति ऐसे थे जो 30 संग्रहों को पढ़ा सकते थे, धर्म के आचार्य को लेकर दस ऐसे थे जो 50 संग्रहों की व्याख्या कर सकते थे। इन सभी में शीलभद्र अकेले ऐसे थे जो सभी संग्रहों के ज्ञाता थे। इस प्रकार विभिन्न विद्याओं, विचारों एवं विश्वासों में सामंजस्य स्थापित करना विश्वविद्यालय की प्रमुख विशेषता थी। यहाँ विचारों एवं विश्वासों की स्वतंत्रता तथा सहिष्णुता की भावना विद्यमान थी। हुएनसांग के समय शीलभद्र ही विश्वविद्यालय के कुलपति थे। चीनी यात्री उनके चरित्र तथा विद्वत्ता की काफी प्रशंसा करता है। वे सभी विषयों के प्रकाण्ड पण्डित थे। उसने स्वयं शीलभद्र के चरणों में बैठकर अध्ययन किया था। वह उन्हें ‘सत्य एवं धर्म का भण्डार’ कहता है। यहाँ के अन्य विद्वानों में धर्मपाल (जो शीलभद्र के गुरु तथा उनके पूर्वगामी कुलपति थे), चन्द्रपाल, गुणमति, स्थिरपति, प्रभामित्र, जिनमित्र, ज्ञानचन्द्र आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन सभी की ख्याति दूर-दूर तक फैली हुयी थी। ये सभी विद्वान् मात्र अच्छे शिक्षक ही नहीं थे अपितु विभिन्न ग्रन्थों के रचयिता भी थे। इनकी रचनाओं का समकालीन विश्व में बड़ा सम्मान था। इन प्रसिद्ध आचार्यों के अतिरिक्त नालन्दा में अन्य अनेक विद्वान् भी थे जिन्होंने विद्या के प्रकाश से पूरे देश को आलोकित किया
प्रश्न c (i) बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? अथवा बौद्ध दर्शन की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?
उत्तर-
बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
(1) अनात्मवाद-अनात्म का शाब्दिक अर्थ है ‘आत्मा’ को न स्वीकार करना। परन्तु यह अर्थ उचित नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बौद्ध आत्मा को नहीं मानते। वे मानते हैं और इसे पंचस्कन्थ रूप में मानते हैं, अतः अनात्म का अर्थ ‘न आत्मा’ या अनात्मता नहीं है। इस अनात्मता को बी कुछ लोग ‘नैरात्मवाद’ समझते हैं। परन्तु नैरात्म भी अनात्म नहीं। तथागत के अनात्म का अर्थ उनके प्रयोजन से ही स्पष्ट होगा। तथागत का कहना है कि उनका उपदेश ‘निर्वेद’, निर्माण उपशम अभिज्ञा, सम्बोधि के लिए है। परन्तु इस आदेश के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक ‘अहं भाव’ है जिसका स्वरूप ‘मैं और मेरा’ है। जब तक अहं भाव का नाश नहीं होता निर्वेद या निर्वाण नहीं मिल सकता। यह अहं भाव एक मिथ्या दृष्टि है, एक प्रकार का अज्ञान है
(2) कर्मवाद एवं पुनर्जन्मवाद-गौतम बुद्ध कर्ममार्गी थे तथा उनका विश्वास था कि इस संसार में रहकर मनुष्य जो कर्म करता है-उसका फल उसे अवश्य मिलता है। आत्मा बार-बार अनेक शरीर धारण करती रहती है तथा दुष्कर्मों और सत्कर्मों के अनुसार दण्डित या पुरस्कृत नहीं होती है। सत्कर्म के बिना निर्वाण की प्राप्ति सम्भव नहीं है। मनुष्य चाहे जितने यज्ञ करे या बलि दे, किन्तु सत्कर्म के बिना आवागमन के चक्र से छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता। बुद्ध जी पुनर्जन्मवाद में विश्वास करते थे। उनका विचार था कि आत्मा को निर्मल बनाने के लिये एक जन्म ही यथेष्ट नहीं। बोधिसत्वों के रूप में गौतम बुद्ध के सहस्रों जन्मों का वर्णन प्राप्त होता है, जिनमें धीरे-धीरे उनकी आत्मा की मलिनता दूर हो जाती है तथा अन्त में उन्हें निर्वाण प्राप्त होता है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति बार-बार जन्म लेकर सत्कर्मों के द्वारा निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है।
(3) अनीश्वरवाद-गौतम बुद्ध ने धर्म में दार्शनिक सिद्धान्तों को विशेष महत्त्व दिया। ईश्वर के अस्तित्व के विषय में पूछे जाने पर प्रायः वे मौन रहते थे। एक बार उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देते हुये कहा था कि यदि ईश्वर कहीं है, तो वह भी कर्म के बन्धनों में बँधा हुआ है तथा वह किसी को दण्ड या पुरस्कृत करने में स्वतन्त्र नहीं है।
प्रश्न c (ii) आदर्शवाद की परिभाषा ।
उत्तर- आदर्शवाद के अनुसार जीवन का अन्तिम लक्ष्य आत्मानुभूति होता है। आत्मानुभूति के लिए तीन सनातन मूल्यों सत्यम्, शिवम् एवं सुन्दरम् की प्राप्ति आवश्यक है। नैतिक जीवन के उत्थान के लिए मनुष्य में चार सद्गुणों-संयम, धैर्य, ज्ञान और न्याय का होना आवश्यक है। ये सद्गुण आत्मा के गुण हैं और जो मनुष्य इन्हें जितना अधिक प्राप्त कर लेता है, वह उतना ही अधिक सत्यम्, शिवम् और सुन्दरम् की ओर बढ़ जाता है और आत्मानुभूति करने में सफल होता है। ये नैतिक नियम आध्यात्मिक नियम हैं।
हेंडरसन के अनुसार, “आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, क्योंकि आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक मूल्य, मनुष्य में जीवन के सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण पहलू हैं। एक तत्त्वज्ञानी आदर्शवादी यह विश्वास करता है कि मनुष्य का सीमित मन उस असीमित मन से निकलता है। व्यक्ति और यह संसार दोनों बुद्धि (विचार) की अभिव्यक्ति है और भौतिक संसार की व्याख्या मानसिक संसार के आधार पर की जा सकती है।”
अतः हम कह सकते हैं कि आदर्शवाद सम्भवतः विश्व का सबसे प्राचीन दर्शन है। विश्व के अनेक दार्शनिक एवं शिक्षाशास्त्री आदर्शवादी रहे हैं।
इस दर्शन ने शिक्षा को अत्यन्त प्रभावित किया। पश्चिमी जगत में इसे सुकरात, प्लेटो ने प्रारम्भ किया एवं पूर्व में इसका उदय उपनिषदों से हुआ।
प्रश्न c (iii) उपनिषदों में दिये गये प्रमुख दार्शनिक विचार क्या हैं?
उत्तर- आत्मा-उपनिषदों का ध्यानपूर्वक मनन करने पर हमको यह ज्ञात होता है कि उपनिषदों का प्रमुख एवं प्रतिपाद्य विषय आत्मा है। उनके अनुसार आत्मा हमारी परम सत्ता है और हमारे जीवन का प्रमुख सत्य है। आत्मा ही सर्वव्यापी है और विश्व के सम्पूर्ण पदार्थ इसके अन्तर्गत हैं। आत्मा एक है जो संसार में प्रकृति और मानव में सर्वत्र पाया जाता है। उपनिषदों के अनुसार, आत्मा ही समस्त विश्व का मूल है और साथ ही हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है। संहिता से लेकर आरण्यक तक आत्मा को ब्रह्म से भिन्न बताया है किन्तु उपनिषद में आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है तथा उसी का रूप है, अर्थात् यह आत्मा ही परम ब्रह्म है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार के जितने स्थूल सूक्ष्म पदार्थ वे सब पदार्थ आत्मा के ही रूप हैं। दृष्टा और दृश्य में कोई भेद नहीं है क्योंकि आत्मन् ही सर्वव्यापी है और जगत् के सम्पूर्ण पदार्थ उसी में विलीन हो जाते हैं। यद्यपि आत्मा के स्वरूप का स्पष्ट वर्णन – करना प्रायः असम्भव-सा है, तथापि उपनिषदों में कहा गया है कि यह भूख, प्यास, शोक, मोह, यश तथा मरण से हमारा उद्धार करता है। यह आत्मा पूर्ण तथा अखण्ड है। आत्मा का ज्ञान अन्तःकरण की पवित्रता तथा शुद्धि ही के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा-संसार के सभी पदार्थों का सार है। उपनिषदों में इसको विशेष महत्त्व प्रदान किया गया है। इसका कारण यह है कि इसके समान जगत – में कोई प्रिय वस्तु नहीं है।
ब्रह्म- “ब्रह्मदारण्यक उपनिषद् में यह निरूपित है कि सर्वप्रथम ब्रह्म ज्ञान क्षत्रियों में और बाद में इसे ब्राह्मणों ने ग्रहण किया। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्म’ ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उपनिषदों में ब्रह्म को इन्द्रिय, वाणी, मन आदि सबसे परे माना गया है। सृष्टि के विकास तथा उत्पत्ति का वर्णन अत्यन्त विस्तार के साथ किया गया है जो इस बात का प्रमाण है कि वे दार्शनिक जगत् की सत्यता में विश्वास करते थे। उपनिषद् काल में ऋषि मुनि जीवन और जगत् के प्रति अत्यन्त आशावादी दृष्टिकोण रखते। कहीं-कहीं पर ऐसा भी संकेत मिलता है कि वे जगत् को मिथ्या समझते थे।”
आत्म-साक्षात्कार-उपनिषदों में आत्म-साक्षात्कार के उपायों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कायिक, वाचिक तथा मानसिक संयम करना परमावश्यक है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, सत्यपथ पर चलना, इन्द्रियों का निग्रह करना, किसी की वस्तु का अपहरण न करना, हिंसा से विरत रहना, माता-पिता की सेवा करना, अतिथियों का देवता तुल्य आदर करना आदि ब्रह्म-साक्षात्कार के लिए आवश्यक हैं। वास्तव में ब्रह्म का साक्षात्कार करना ही उपनिषदों का रहस्य है, उपदेश हैं तथा चरम लक्ष्य है।
प्रश्न c (iv) एनी बेसेन्ट का शिक्षा में योगदान।
अथवा
एनी बेसेन्ट का शिक्षा के विषय में दृष्टिकोण बताइए।
उत्तर-एनी बेसेन्ट का शिक्षा में योगदान- एनी बेसेन्ट ऐसी त्यागी महिला थीं जिन्होंने अपना समस्त जीवन मानव-कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने भारत को अपना स्थायी निवास बनाया और शैक्षणिक तथा सामाजिक कल्याण के लिए जीवनपर्यन्त प्रयास किया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान इस प्रकार है-
1. वैदिक साहित्य का प्रसार तथा शिक्षा एवं धर्म में सम्बन्ध स्थापित करना।
2. गीता, महाभारत, उपनिषद् एवं रामायण आदि ग्रन्थों के आधार पर आध्यात्मिक आदर्शों की स्थापना।
3. प्राचीन भारतीय संस्कृति का पालन करना तथा विश्वधर्म को शिक्षा का आधार बनाना।
4. अध्यात्म पर आधारित राष्ट्रीय शिक्षा योजना का निर्माण।
5. अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा पर बल ।
6. पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर देना।
7. बनारस में हिन्दू सेण्ट्रल कॉलेज की स्थापना ।
8. शिक्षा के पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करना।
डॉ. ए. रंगनाथन ने एनी बेसेन्ट के शिक्षा तथा सामाजिक विकास के क्षेत्र में किये गये योगदान के विषय में कहा है- “डॉ. बेसेन्ट सम्पूर्ण राजनीति तथा धर्म, शिक्षा तथा संस्कृति, दर्शन तथा समाजशास्त्र में जीती रहीं। वे अपने समय की महानतम विभूतियों में से थीं। डॉ. बेसेन्ट नर-नारियों के लिए एक अमर उदाहरण हैं।”
प्रश्न c (v) शिक्षा की दृष्टि से समाज की भूमिका की विवेचना कीजिए।
उत्तर- शिक्षा की दृष्टि से समाज की भूमिका की विवेचना कीजिए।
शिक्षा के साधन के रूप में समाज का महत्त्व
(अ) समाज बालक की शिक्षा को प्रारम्भ से ही प्रभावित करता है।
बालक की शिक्षा में परिवार एवं विद्यालय की भाँति समाज का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। वह इसलिए कि परिवार तथा विद्यालय की भाँति समाज भी व्यक्ति के व्यवहार में इस प्रकार परिवर्तन करता है कि वह उस समूह के कार्यों में सक्रिय भाग ले जिसका वह एक सदस्य है। वास्तव में परिवार समाज की एक आधारभूत इकाई है। फलस्वरूप उन्हें एक दूसरे से पृथक् नहीं किया जा सकता। जब हम यह कह सकते हैं कि बालक की शिक्षा को परिवार प्रारम्भ से प्रभावित करता है तो इसका यह भी तात्पर्य होता है कि समुदाय भी बालक की शिक्षा को प्रारम्भ से ही प्रभावित करता है। हाँ, यह अवश्य है कि यह प्रभाव प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होता है।
(ब) बालक के व्यक्तित्व का विकास समाज पर विशेष रूप से निर्भर होता है।
यद्यपि बालक के व्यक्तित्व के विकास पर अनेक बातों का प्रभाव पड़ता है, किन्तु इन सबमें समाज का विशेष स्थान है क्योंकि समाज के अन्तर्गत ही अन्य सभी व्यक्तित्व को प्रभावित करनेवाली बातें रहती हैं और उनके स्वरूप को समाज ही निश्चित करता है। समाज के द्वारा ही अनौपचारिक रूप से व्यक्ति भाषा, धर्म, रीति-रिवाज, कला, नैतिकता इत्यादि की अनेक विशेषताएँ सीखता है। व्यक्ति या बालक की शिक्षा में समुदाय का महत्त्व प्रस्तुत करते हुए विलियम ईगर ने लिखा है, “मानव स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है इसलिये उसने वर्षों के अनुभव से सीख लिया है कि व्यक्तित्व तथा सामूहिक क्रियाओं का समुचित विकास सामुदायिक जीवन द्वारा ही सम्भव है।”
प्रश्न c (vi) तत्त्व मीमांसा के शैक्षिक निहितार्थों को समझाइए ।
उत्तर-तत्त्व मीमांसा ने धर्मों को व्यापक आधार प्रदान किया है और धर्म के माध्यम से साहित्य की नींव मजबूत की है। सभी भाषाओं का साहित्य तत्त्व मीमांसाजनित विश्वासों से प्रभावित हुआ है। हिन्दी काव्य को देखें जिससे हम अच्छी तरह परिचित हैं। हिन्दी का भक्त साहित्य ईश्वर के अस्तित्व, इसकी उपासना और इस सांसारिक माया-मोह से विरक्ति आदि के विचारों से परिपूर्ण है। कबीर,जायसी, सूर, तुलसी और मीरा का काव्य इस बात का प्रमाण है कि तात्त्विक विचारों ने कवियों को प्रेरणा दी है।
तत्त्व मीमांसा ने संगीत, मूर्ति-चित्र और वास्तु आदि कलाओं को सृजन का आधार प्रदान किया है। बड़े-बड़े संगीतज्ञों ने भाव-विभोर होकर संगीत के स्वरों में उस महान तत्त्व के प्रति अपने उद्गार प्रकट किये हैं; जिसका उल्लेख तत्त्वदर्शियों ने किया है। सारा भक्ति संगीत उसी पर आधारित है। संगीत उस तत्त्व की अनुभूति का प्रभावशाली माध्यम है। देवताओं के नाम के संकीर्तन का आधार भी वही परम तत्त्व है। मूर्ति और चित्रकलाएँ उसी परम तत्त्व को विविध रूपों में आकार प्रदान करती हैं। बहुतत्त्ववाद ने चित्रकारों और मूर्तिकारों को प्रेरणा दी कि वे वनस्पतियों, मशु-पक्षियों और स्थूल वस्तुओं के जो अनेक प्रकार की हैं, चित्रों और मूर्तियों के रूप में प्रस्तुत करें। फिर इस अनेकता में उन्हें एकता का बोध हुआ। एक मूर्तिकार जब अनेक प्रकार की मूर्तियाँ या वस्तुएँ बनाता है, तो उसे यह अनुभव होता है कि विभिन्न तथा विविध प्रकार के आकारों की वस्तुएँ एक ही तत्त्व से निर्मित हैं, और वह है मिट्टी, तो सहसा उसे यह निष्कर्ष निकालना पड़ा कि जड़, चेतन में भी एक ही तत्त्व वर्तमान है और उसी के विविध रूप दिखायी देते हैं। वास्तुकला में तत्त्व ज्ञान का आधार इस प्रकार ग्रहण किया कि असीम तत्त्व को एक सीमा में बाँधा, उसकी उपस्थिति मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों की सीमा में दिखाने का प्रयास किया है। इन प्रार्थना स्थलों में जाकर विशेष रूप से इस महान तत्त्व की अनुभूति अच्छी तरह हो सकती है यद्यपि वह सभी जगह वर्तमान और व्याप्त है। इन पूजा स्थलों के आकार-प्रकार और ऊँचाई के पीछे भी तात्त्विक चिंतन है। किसी एक बिन्दु पर पहुँचकर समस्त प्रकार के कलाकार तत्त्व ज्ञानी बन जाते हैं।
प्रश्न d (i) लोकतन्त्र में नागरिकता की शिक्षा क्यों आवश्यक है? व्याख्या कीजिए।
उत्तर- किसी भी देश की शासन-प्रणाली उसी स्थिति में सफल होती है जब उसके नागरिकों में उसके प्रति आस्था हो और वे उसके अनुसार व्यवहार करें। वर्तमान में हमारे देश भारत में लोकतन्त्र शासन प्रणाली है, यह तभी सफल हो सकती है जब इस देश के नागरिकों में लोकतन्त्र के प्रति आस्था हो और वे लोकतन्त्रीय जीवन जीएं। जीवन की विधि के रूप में यह एक ऐसी विधि है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का समान महत्त्व होता है, सब एक-दूसरे को समान आदर की दृष्टि से देखते हैं और सबकों अपने विकास की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है परन्तु बिना किसी दूसरे के विकास में बाधक हुए। इस जीवन शैली में वर्ग भेद एवं शोषण का कोई स्थान नहीं होता। लेकिन हमारे देश की स्थिति यह है कि देश के नागरिक वैसे अभी तक अपने जीने की शैली नहीं बना सके हैं। इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है लोकतन्त्रीय दृष्टिकोण की। उसी स्थिति में देश के सभी नागरिक स्वतन्त्रता का सही अर्थों में उपयोग कर सकेंगे, समानता की भावना से जीवने का आनन्द उठा सकेंगे, भ्रातृत्व भावना के साथ एक साथ रह सकेंगे, एक-दूसरे के व्यक्तित्व का आदर कर सकेंगे, एक-दूसरे का सहयोग कर सकेंगे और उनमें सांस्कृतिक एवं धार्मिक सहिष्णुता का विकास होगा, सभी एक-दूसरे के अधिकारों का संरक्षण करेंगे और साथ ही अपने-अपने कर्त्तव्यों का पालन करेंगे। लोकतन्त्र की सफलता, लोकतन्त्रीय दृष्टिकोण और लोकतन्त्रीय व्यवहार पर ही निर्भर करती है।
बच्चों को शिक्षा के द्वारा लोकतान्त्रिक मूल्यों एवं नागरिकता के अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों के प्रति सचेष्ट किया जाना चाहिए। शिक्षा के द्वारा बच्चों में समाज सेवा एवं राष्ट्र सेवा कार्य अनिवार्य होने चाहिए और शारीरिक श्रम को महत्त्व देना चाहिए। लोकतान्त्रिक शिक्षण-अधिगम विधियों के माध्यम से नागरिक कर्त्तव्यों की भावना विद्यार्थियों में दृढ़ करना चाहिए। बच्चों को सिखाना चाहिए कि वे एक- दूसरे की स्वतन्त्रता की रक्षा करने को तत्पर हों तथा एक-दूसरे की स्वतन्त्रता में बाधक न बनें। प्रारम्भिक शैक्षिक स्तर से ही सभी बच्चों को समान समझा जाए तथा उनमें धर्म, जाति, स्थान के
आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। बाल्यावस्था से बच्चों को समाज सेवा एवं राष्ट्र सेवा कार्यों में लगाया जाए। स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय का स्पष्ट ज्ञान, कराया जाए और साथ ही इनकी मूल भावना भी स्पष्ट की जाए।
प्रश्न d (ii) शिक्षा के द्वारा प्रजातान्त्रिक मूल्यों को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है?
उत्तर-शिक्षा समाज की वह सीढ़ी है जिस पर पैर रखकर व्यक्ति अपने संस्कारों को सँवारता है और शिक्षा को दिशा प्रदान करता है। महान् व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य प्रायः समाज के सभी व्यक्तियों द्वारा समान रूप से स्वीकार किया जाता है। शिक्षा, समाज तथा व्यक्ति तीनों मिलकर यह निर्धारित करते हैं कि किन बातों का ध्यान रखकर प्रजातान्त्रिक मूल्यों को प्राप्त किया जा सकता है।
शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसके अन्तर्गत बालक सत्य के आधार पर अहिंसा द्वारा प्रेमपूर्वक जीवन-यापन करना सीखे। शिक्षा से ऐसा मनुष्य बनाना है जो स्वयं स्वेच्छा से शाश्वत् मूल्यों के पालन का प्रयास करे, जिससे व्यक्ति, समाज सभी का कल्याण सम्भव हो। इसके लिए शिक्षा द्वारा व्यक्ति की आत्मा को जागृत करना आवश्यक है। ऐसा होने पर व्यक्ति जिस प्रकार अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति सचेष्ट रहता है, उसी प्रकार वह दूसरों के हितों के संरक्षण के लिए तत्पर हो सकेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो मूल्य बताए गए हैं, उन्हें शिक्षा द्वारा छात्रों के जीवन में उतारा जा सकता है। वे मूल्य हैं-प्रजातन्त्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, सहिष्णुता, व्यक्ति की गरिमा, विचार, अभिव्यक्ति आदि। ईमानदारी, उपकार, विनम्रता, अहंकार, निस्वार्थता, समभाव, मन-वचन- कर्म की एकता के गुणों का शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में ध्रुवीकरण करके उसमें प्रजातान्त्रिक मूल्यों के विकास में सहायता मिलेगी। इन्हीं मूल्यों को छात्रों को अपने जीवन में उतारना है। बालक को मूल्यपरक शिक्षा देनी चाहिए। वर्तमान समय में मूल्यों के स्पष्टीकरण हेतु मात्र उपदेश ही पर्याप्त साधन माना जाता है। इसमें अनुभूति, चिन्तन तथा क्रियान्वित नहीं है। शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति यह समझे कि वह स्वयं क्या है? उसके प्रजातान्त्रिक कर्त्तव्य क्या हैं? उसे जीवन में किसे प्राथमिकता देनी है? निष्ठाओं का टकराव क्यों होता है? तभी वह अच्छे प्रजातान्त्रिक मूल्यों का विकास कर सकता है।
प्रश्न d (iii) सभ्यता और संस्कृति में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
अथवा
संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है?
उत्तर- इन दोनों शब्दों के भेद को नीचे की तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है-
सभ्यता
1. यह वह वस्तु है जो हमारे पास है।
2. भोजन, परिधान, मोटर, महल तथा अन्य
पार्थिव या भौतिक पदार्थ सभ्यता के उपकरण हैं।
3. हमारी सभ्यता वह है कि जिसका हम उपयोग करते हैं।
4. सभ्यता मनुष्य की कतिपय क्रियाओं से उत्पन्न होने वाली उपयोगी वस्तुओं का नाम है जो साधन के रूप में प्रयुक्त होती हैं।
5. वह बाह्य व्यवस्था तथा साधनों को निरूपित करती है।
संस्कृति
1. यह वह गुण है जो हम में व्याप्त है।
2. परन्तु भोजन करने तथा वस्त्र पहनने की कला, मोटर चलाने और महल बनाने का कौशल संस्कृति है।
3. हमारी संस्कृति वह है जो हम हैं।
4. संस्कृति में मनुष्य की वे क्रियाएँ व्यापार और अभिव्यक्तियाँ निहित हैं जिन्हें वह साध्य के रूप में देखता है।
5. यह हमारी आन्तरिक प्रकृति को व्यक्त करती है
प्रश्न d (iv) भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक कर्त्तव्यों की चर्चा कीजिए ।
उत्तर-
मूल कर्त्तव्य
मूल संविधान में मौलिक कर्त्तव्यों की व्यवस्था नहीं की गयी थी, किन्तु संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा संविधान में 10 मूल कर्त्तव्यों को समाहित कर लिया गया है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक मूल कर्त्तव्य और जोड़ा गया है जिससे अब संविधान में 11 मूल कर्त्तव्य हो गये हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 (क) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह-
(1) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
(2) स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें;
(3) भारत की संप्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;
(4) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
(5) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं;
(6) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे; (7) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;
(8) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें; (9) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
(10) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करै, जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले; और
(11) यदि माता-पिता या संरक्षक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।
प्रश्न d (v) बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ का उल्लेख कीजिए।
उत्तर- बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ
महात्मा बुद्ध एवं उनके शिष्यों-अनुयायियों ने संसार के लोगों को दुःखों से मुक्ति का सन्देश, उपदेश और शिक्षा दी। जो भी शिक्षा दी उस पर मनन-चिन्तन किया तथा विभिन्न सिद्धान्त प्रतिपादित किये। ये सिद्धान्त बौद्ध दर्शन के नाम से पुकारे गये। इन्हीं सिद्धान्तों को शिक्षा-ज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त करके तत्सम्बन्धी विचार निकर्ष निकाले गये जिन्हें बौद्ध शिक्षा दर्शन कहा गया। बौद्ध शिक्षा दर्शन प्रत्यक्षवादी कहा जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य मालुक्यपुत्र को कहा था कि सिद्धान्तों के विवेचन से दुःखी मानवता का दुःख दूर नहीं किया जा सकता, बल्कि दुःखों को दूर करने का प्रयास होना चाहिए, दुःख मुक्ति के मार्ग निकालना चाहिए। यही सिद्धान्त उपदेश रूप में बौद्ध दर्शन बने और उनका व्यावहारिक रूप बौद्ध शिक्षा दर्शन कहा जा सकता है।
प्रश्न d (vi) प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए?
उत्तर- प्रकृतिवाद और शिक्षा के उद्देश्य
प्रकृतिवादियों ने शिक्षा के कई उद्देश्य बताये हैं। यहाँ पर हम उन्हें संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे-
1. जीवन संघर्ष के लिए तैयारी – प्रकृतिवादियों के अनुसार प्रत्येक जीव में जीने की इच्छा होती है। इसी प्रकार मनुष्य में भी जीने की इच्छा होती है। वह अपने जीवन की रक्षा के लिए अपने वातावरण से संघर्ष करता है। डारविन ने इस सम्बन्ध में व्यापक सिद्धान्त निकाला था जिसे ‘जीवन के लिए संघर्ष कहा गया। इसके अनुसार जीव जीवन के लिए संघर्ष होता है और जो समर्थ होता है वही जीवित रहता है। प्रकृतिवादी भी चाहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य बालक को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना होना चाहिए
2. वातावरण के अनुकूल बनाना- प्रकृतिवादियों के अनुसार, बालक को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वह अपने को वातावरण के अनुकूल बना सके। इसके लिए बालक को शारीरिक और मानसिक रूप में स्वस्थ होना चाहिए। लेमार्क ने डारविन के सिद्धान्त को समर्थन करते हुए अपना सिद्धान्त निकाला था। उनके अनुसार, जीव को संसार में जीवित रहने के लिए अपने को वातावरण के अनुकूल बनाना चाहिए। इससे वह अपनी रक्षा में सफल होता है।
3. आत्म-संरक्षण और आत्म-सन्तोष प्राप्त करना- प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य आत्म- संरक्षण और आत्म-सन्तोष प्राप्त करना बताते हैं। उनके अनुसार, ‘आत्म-सन्तोष’ मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है। इसी से मनुष्य का वर्तमान और भविष्य सुख से व्यतीत होता है। हरर्बट स्पेन्सर के अनुसार, व्यक्ति के लिए आत्म-संरक्षण भी आवश्यक है। आत्म-संरक्षण से वह अपने आपको सुरक्षित मानता है। इसके लिए बालक की मूल प्रवृत्तियों और स्वाभाविक आवेगों का विकास करना चाहिए।’
”
4. व्यक्ति का स्वतन्त्र विकास करना- प्रकृतिवादी शिक्षा द्वारा व्यक्ति का स्वतन्त्र विकास करना चाहते हैं। उनके अनुसार, सही शिक्षा वही है जिसके द्वारा बालक की वैयक्तिकता का विकास किया जा सके। बालक की मूल प्रवृत्तियों, रुचियों और रुझानों का विकास किया जाना चाहिए। इससे उसकी वैयक्तिकता का विकास हो सकेगा।
प्रश्न e (i) रसेल के शैक्षिक योगदानों की विवेचना कीजिए।
उत्तर- शिक्षा के क्षेत्र में रसेल का योगदान शिक्षा के क्षेत्र में रसेल के योगदान का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है-
(1 ) लक्ष्य – शिक्षा का लक्ष्य रचनात्मक व्यक्तियों का निर्माण है जो कि एक रचनात्मक समाज की स्थापना करें। रचनात्मक समाज जनतन्त्रीय होता है। शिक्षा के बिना कोई भी प्रगति सम्भव नहीं है अस्तु, अन्य अमरीकन शिक्षाशास्त्रियों के साथ रसेल शिक्षा की जनतन्त्रीय पद्धति का समर्थन करते हैं। उन्होंने अमरीकी शिक्षा व्यवस्था को सर्वोत्तम ठहराया। शिक्षा का लक्ष्य बालक का इस तरह से विकास करना है कि उसकी रचनात्मक प्रवृत्तियाँ अभिव्यक्त हो। इस प्रक्रिया में शिक्षार्थी के बल, साहस, संवेदनशीलता और बद्धि का विकास करना चाहिये। शिक्षित व्यक्तियों में मस्तिष्क की उदारता होनी चाहिये। निरीक्षण, धैर्य, उद्यमशीलता और ज्ञान की सम्भावना में आस्था प्रत्येक शिक्षार्थी के लिये आवश्यक है। चरित्र और व्यक्तित्व के विकास में इन चार गुणों का महत्त्वपूर्ण योगदान है।.
(2) शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त – बालक की शिक्षा छः वर्ष की आयु से आरम्भ होनी चाहिए। इस स्तर पर शिक्षा का लक्ष्य जिज्ञासा को सन्तुष्ट करना और बालक की प्राकृतिक शक्तियों का विकास करना है। शिक्षार्थी के लिए सबसे अधिक आवश्यक लक्षण जिज्ञासा, पूर्वाग्रह से मुक्त होना, ज्ञान की सम्भावनाओं में आस्था, दृढ़ता, तीव्र, स्थायी और संकल्पमय अवधान, धैर्य, विचारों, शब्दों और कार्य में यथार्थवादी दृष्टिकोण है। शिक्षा को शिक्षार्थी के विकास की अवस्था के अनुरूप रूचिकर होना चाहिए। शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करना चाहिए।
प्रश्न e (ii) आर्थिक विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।
उत्तर- आर्थिक विकास का अर्थ
मायर एवं बाल्डविन के अनुसार, “आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आर्थिक व्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है।” इस परिभाषा में तीन शब्द- ‘प्रक्रिया’, ‘वास्तविक राष्ट्रीय आय’ तथा ‘दीर्घकाल’ महत्त्वपूर्ण हैं। इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-
(अ) प्रक्रिया- यहाँ प्रक्रिया का अभिप्राय अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न अवयवों में होनेवाले परिवर्तन से है। ये परिवर्तन विभिन्न तत्त्वों से प्रभावित होते हैं। इन परिवर्तनों का सम्बन्ध साधनों की पूर्ति तथा उनकी माँग में होनेवाले परिवर्तनों से है। साधनों की पूर्ति में परिवर्तन के अन्तर्गत जनसंख्या में वृद्धि, पूँजी संग्रह, अतिरिक्त साधनों की खोज, उत्पादन की नवीन विधियों का प्रयोग तथा अन्य संस्थागत परिवर्तन सम्मिलित हैं। पूर्ति पक्ष के अवयवों में परिवर्तन के साथ-ही-साथ माँग के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। माँग के स्वरूप में आय-स्तर तथा उसके वितरण के स्वरूप में परिवर्तन, उपभोक्ताओं की वरीयता में परिवर्तन आदि परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार आर्थिक विकास के फलस्वरूप माँग एवं पूर्ति के स्वरूप में परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों की सीमा आर्थिक विकास की गति तथा समय पर निर्भर करती है।
(ब) वास्तविक राष्ट्रीय आय इसका अभिप्राय देश में उत्पादित अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल योग के समायोजित मूल्य से है। किसी देश का आर्थिक विकास उस समय होता है जब उस देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है.
(स) दीर्घकाल- आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि शुद्ध राष्ट्रीय आय में उत्तरोत्तर वृद्धि हो । किसी एक वर्ष में अनुकूल परिस्थितियों के कारण हुई वृद्धि को आर्थिक विकास का सूचक नहीं माना जाता है वरन् दस या बीस वर्ष की अवधि में हुए परिवर्तनों पर विचार किया जाता है। इस प्रकार आर्थिक विकास का सम्बन्ध अल्पकालीन परिवर्तनों से न होकर दीर्घकालीन परिवर्तनों से है।
प्रश्न e (iii) शैक्षिक नियोजन का उद्देश्य ।
उत्तर- शैक्षिक नियोजन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
1. शैक्षिक नियोजन के कारण शिक्षा से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार गतिशील होता है।
2. शैक्षिक नियोजन से शिक्षा-संस्थाओं को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सुविधा होती है।
3. शिक्षा-नियोजन के कारण शिक्षा के विविध पक्षों का गुणात्मक विकास होता है जिससे उपलब्धि का स्तर उच्च हो जाता है।
4. शिक्षा में लगे हुए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का उपयुक्त उपयोग शैक्षिक नियोजन के कारण सम्भव हो पाता है।
5. शिक्षा में निवेश का प्रतिफल एक लम्बे समय के बाद दिखाई पड़ता है। इस कारण शैक्षिक नियोजन का महत्त्व अधिक बढ़ जाता है।
6. शैक्षिक नियोजन के कारण आवश्यकताओं का पता लगाने और प्राथमिकताओं को निश्चित करने में सुविधा होती है।
7. शैक्षिक नियोजन के कारण उत्पादन में परिमाणात्मक वृद्धि होती है और भौतिक समृद्धि सुनिश्चित होती है।
8. शैक्षिक नियोजन लोकतंत्रीय सिद्धान्तों पर आधारित होता है इसलिए इसमें सहयोग का सिद्धान्त लागू होता है जिसके कारण इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों, अध्यापकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों का सहयोग प्राप्त होता है।
9. शैक्षिक नियोजन के कारण सम्पूर्ण शिक्षा-प्रक्रिया में संचालन, संगठन और समन्वय का कार्य निरन्तर चलता रहता है।
प्रश्न e (iv) समुदाय की शैक्षिक भूमिका को लिखिए।
उत्तर- समुदाय और शिक्षा
परिवार के पश्चात् समुदाय में बालक की शिक्षा होती हैं। समुदाय में बालक को अपने मित्रों के मध्य रहना पड़ता है। वे मित्र उसके लिये समाज का निर्माण करते हैं और जिस प्रकार का उसका समाज होगा, वैसी ही आदतें तथा व्यवहार बालक में हो जायेंगे। विलियम ईमर के अनुसार- “मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, इसलिये उसने वर्षों से सीख लिया है कि व्यक्तित्व और सामूहिक क्रियाओं का विकास समुदाय द्वारा ही सर्वोत्तम रूप में किया जा सकता है।”
समुदाय, बालक को इस प्रकार शिक्षा देता है-
1. सामाजिक वातावरण का निर्माण करके-समुदाय एक स्थानीय समूह होता है, वह स्थानीय वातावरण का निर्माण करता है। यह वातावरण यदि सांस्कृतिक एवं सौम्य है तो वैसा ही प्रभाव बालक के सामाजिक-सांस्कृतिक विकास पर पड़ेगा। समुदाय वस्तुतः अपने अन्तःवासियों के चरित्र भावना, संवेगों का पूरा-पूरा प्रतिनिधित्व करता है। अतः इन्हीं भावनाओं, संवेगों एवं चरित्र का आरोपण बालकों पर भी उसी प्रकार का होता है जैसे समाज के अन्य सदस्यों पर। वातावरण-निर्माण की प्रतिक्रिया उसकी विशेषता होती है।
2. सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करके-समुदाय में आचार-विचार, व्यवहार की अभिव्यक्ति, समय-समय पर आयोजित उत्सवों तथा समारोहों से होती है। इन उत्सवों में समुदाय की आन्तरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति हुआ करती है। अभिव्यक्ति का यह ढंग ही उस सांस्कृतिक वातावरण की रचना करता है जिससे बालक सहज रूप से कार्य करता है। सांस्कृतिक वातावरण से बालक के व्यवहार में परिष्कार होता है और वह समुदाय की सांस्कृतिक परम्परा का निर्वाह करने में अपनी शक्ति लगा देता है।
3. शिक्षा के ऊपर नियन्त्रण करके- समुदाय की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था होती है। समुदाय की आवश्यकता की पूर्ति करने वाली शिक्षा ही समुदाय को उन्नत बनाती है। समुदाय अपनी आवश्यकतानुसार शिक्षा की व्यवस्था करता है और उस पर अपनी आवश्यकता के अनुकूल नियन्त्रण भी करता है तो वह उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता। यदि समुदाय शिक्षा पर नियन्त्रण नहीं करता तो समुदाय के नेता अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करते हैं और समुदाय की भावी पीढ़ी के लिये शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करते हैं।
4. विद्यालय नियन्त्रण करके-हावर्थ का कहना है-“स्कूल समाज के चरित्र में परिष्कार करने का साधन है। सामाजिक विकास की दिशा में यह परिष्कार उनके आदर्श एवं विचारों पर निर्भर रहता है जो विद्यालय का संचालन करते हैं।” अतः स्पष्ट है कि समुदाय विद्यालय को अपने हाथ में लेकर ही वांछित दिशा में प्रगति कर सकता है। समुदाय का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह विद्यालयों का संचालन करने के लिये योग्य व्यक्तियों को नियन्त्रण हेतु नियुक्त करें। इसके अभाव में विद्यालयों में अराजकता आ जाती है।
प्रश्न e (v) प्रजातान्त्रिक समाज में शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए।
उत्तर- लोकतन्त्र और शिक्षा के उद्देश्य
एक सफल लोकतान्त्रिक समाज में शिक्षा का प्रमुख्य उद्देश्य उचित नागरिक का निर्माण करना है। उचित नागरिक वह है, जिसमें निम्नलिखित विशेषताएँ निहित हों-
(1) अपने अधिकारों तथा कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक,
(2) स्वयं अन्य लोगों के प्रति उत्तरदायित्व निभाने की क्षमता,
(3) देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याओं को समझने की योग्यता,
(4) समाज की प्रथाओं तथा अन्धविश्वासों में स्वतन्त्रता,
(5) आर्थिक कुशलता,
(6) चिन्तन, तर्क तथा निर्णय करने की क्षमता,
(7) रुचियों का व्यापक विकास,
(8) अवकाश के समय का सदुपयोग करने की योग्यता,
(9) प्रेम, सहानुभूति, दया, परोपकार, विश्व बन्धुत्व, राष्ट्र-प्रेम इत्यादि सामाजिक गुणों से सम्पन्न तथा
(10) समाज कल्याण के लिए तत्पर रहना।
माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भारतीय जनतन्त्र के लिए निम्न तीन उद्देश्य निर्धारित किए हैं-
(1) चरित्र का प्रशिक्षण जो कि शिक्षार्थी को इस योग्य बना दे कि वह रचनात्मक रूप से विकसित होता हुआ सामाजिक व्यवस्था में नागरिक के कर्त्तव्य का पालन कर सके,
(2) उनकी व्यावहारिक एवं व्यावसायिक कुशलता में विकास हो, जिससे कि वे देश की आर्थिक स्थिति सुधारने में अपना सहयोग प्रदान कर सके और
(3) उनकी साहित्यिक, कलात्मक एवं सांस्कृतिक रुचियों का विकास हो जो कि उनके आत्मदर्शन के लिए सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं, जिनके बिना एक राष्ट्र की सक्रिय संस्कृति का विकास करना सम्भव नहीं है।
प्रश्न e (vi) वेदान्त दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए।
उत्तर-वेदान्त दर्शन के अनुसार, मनुष्य जीवन का अन्तिम उद्देश्य मुक्ति है और इस मुक्ति के लिए ज्ञान मार्ग का समर्थन किया गया है। शिक्षा के सम्बन्ध में वेदान्त दर्शन में उपनिषदीय ज्ञान का समर्थन किया गया है जिसमें कहा गया है कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। वेदान्त दर्शन में मानव जीवन के दो पक्ष माने गए हैं-
(1) अपरा (व्यावहारिक) और (2) परा (आध्यात्मिक)।
शिक्षा के द्वारा इसमें मानव के दोनों पक्षों का विकास करने पर बल दिया जाता है, लेकिन इन दोनों पक्षों का विकास मुक्ति के उद्देश्यों को सामने रखकर किया जाना चाहिए। व्यावहारिक पक्ष में मनुष्य के शारीरिक, मानसिक एवं चारित्रिक विकास के साथ-साथ उसके वर्ण-कर्म की शिक्षा को सम्मिलित किया है और आध्यात्मिक पक्ष के लिए ज्ञान को आवश्यक माना गया है तथा ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधन चतुष्टय के पालन को आवश्यक बताया है। क्योंकि साधन चतुष्टय का पालन करने के लिए मानव का शरीर और मन स्वस्थ होना चाहिए। वेदान्त दर्शन के अनुसार शिक्षा के इन उद्देश्यों को हम भाषा में स्थूल से सूक्ष्म के क्रम में निम्नलिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं-
साध्य उद्देश्य-मुक्ति ।
साधन उद्देश्य-
(1) शारीरिक विकास एवं शरीर शुद्धि,
(2) मानसिक एवं बौद्धिक विकास,
(3) नैतिक एवं चारित्रिक विकास,
(4) वर्णानुसार कर्म (व्यवसाय) की शिक्षा,
(5) इन्द्रिय निग्रह एवं चित्त शुद्धि,
(6) आध्यात्मिक विकास।
वेदान्त दर्शन के अनुसार शिक्षा की पाठ्यचर्या में मनुष्य के अपरा और परा दोनों पक्षों से सम्बन्धित ज्ञान एवं क्रियाओं का समावेश होना चाहिए। साथ ही पाठ्यचर्या में व्यावहारिक ज्ञान तथा व्यावहारिक क्रियाओं का समावेश किया है और आध्यात्मिक जीवन के लिए परमार्थिक विषय एवं परमार्थिक क्रियाओं का समावेश किया है। वेदान्त दर्शन के अनुसार मानव जीवन का अन्तिम उद्देश्य भेद दृष्टि की समाप्ति और अभेद दृष्टि की प्राप्ति होती है। इसे भी मुक्ति कहा है। इसके अनुसार, आत्मानुशासन अनुशासन की उच्चतम सीमा है, हमें इसी को प्राप्त करना चाहिए।
प्रश्न e (vii) शिक्षा में दर्शन की क्या आवश्यकता है? स्पष्ट करें।
अथवा
शिक्षा में दर्शन की उपादेयता।
अथवा
दर्शन एवं शिक्षा के सम्बन्ध का एक सटीक उदाहरण दीजिए।
उत्तर- दर्शन जीवन के उस लक्ष्य को निर्धारित करता है जिसे हम शिक्षा कहते हैं। स्पेंसर के शब्दों में-“वास्तविक शिक्षा का नियमन दर्शन ही करता है। दर्शनशास्त्र शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। यही कारण है कि विश्व के महान् दार्शनिक महान् शिक्षाशास्त्री भी हुए हैं। प्लेटो, सुकरात, लॉक, फ्रोबेल, कमेनियस, गाँधी, विनोबा, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन आदि इस मत की पुष्टि के प्रमाण हैं।” एडम्स के अनुसार, “शिक्षा, दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, दर्शन, शिक्षा के पारस्परिक सम्बन्ध पर प्रकाश डालता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करता है।”
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
(Long Answer Type Questions)
निर्देश 1- प्रश्न संख्या 2 से 9 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। परीक्षार्थियों को प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न क
चयन करते हुए कुल चार प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 15 अं निर्धारित हैं।
(4 x 15 – 60 अंक)
) इकाई-1
प्रश्न 2 (i) “शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ वस्तुतः दार्शनिक ही होती हैं।” इस कथन पर प्रकाश डालिए।
उत्तर – शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ
(1) निरक्षरता की समस्या-समाज या प्रौढ शिक्षा की सबसे प्रथम समस्या है भारत में निरक्षर वयस्कों की संख्या अधिक होना। सन् 2011 ई. की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है जिसमें से 74 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं और बाकी 26 प्रतिशत व्यक्ति अशिक्षा एवं अज्ञानता से ग्रसित हैं। इन अशिक्षित एवं अज्ञानी व्यक्तियों को शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्त कराना बहुत ही जटिल समस्या है जिसका समाधान करना अत्यधिक कठिन है। इस समस्या पर प्रकाश डालते हुए पी. एन. चटर्जी ने लिखा है, “विश्व के निरक्षर वयस्कों की सम्पूर्ण संख्या में आधे से अधिक भारत में निवास करते हैं। उनको ज्ञान के अल्प-प्रकाश में लाने का कार्य अति विशाल है।”
(2) धनाभाव की समस्या-समाज शिक्षा की दूसरी समस्या है भारत के प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिए धन की कमी का होना। सन् 1951 ई. की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 12 वर्ष से अधिक आयु के प्रौढ़ों की संख्या 21.6 करोड़ है। इन वयस्कों को यदि । वर्ष में साक्षर बनाना हो तो 35 लाख से अधिक अध्यापकों एवं प्रौढ़-विद्यालयों की आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए कि प्रौढ़ विद्यालय में न्यूनतम व्यय 250 रुपया वार्षिक हो तो 35 लाख प्रौढ़-विद्यालयों का संचालन करने के लिए 8.75 करोड़ रुपयों की जरूरत होगी। भला इतनी बड़ी धनराशि प्रौढ़ों को साक्षर बनाने में कैसे खर्च की जा सकती है, जबकि भारत की राष्ट्रीय आय केवल इस धनराशि से दुगुनी ही है। इस प्रकार समाज शिक्षा के प्रसार के लिए धन की जटिल समस्या है।
(3) अध्यापकों के अभाव की समस्या-समाज शिक्षा की तीसरी समस्या है इसके लिए उपयुक्त अध्यापकों का अभाव होना। जिन अध्यापकों को प्रौढ़-विद्यालयों में नियुक्त किया जाता है, वे प्रायः प्राथमिक विद्यालयों के हुआ करते हैं, जिनमें प्रौढ़ों को शिक्षा प्रदान करने की योग्यता का सर्वथा अभाव होता है। न तो उन्हें प्रौढ़ मनोविज्ञान का ज्ञान होता है और न ही वे उनके लिए उपयुक्त शिक्षण-विधियों और उनके प्रयोग करने की योग्यता रखते हैं। ऐसी स्थिति में भला इन शिक्षकों से प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की कैसे आशा की जा सकती है। उपयुक्त शिक्षकों के अभाव की समस्या की अपेक्षा अध्यापकों का कम संख्या में उपलब्ध होना अधिक जटिल समस्या है। ग्रामों में जहाँ प्रौढ़- निरक्षरों का भण्डार है, जीवन के लिए आवश्यक सुविधाओं के अभाव में ग्रामों में स्थित प्रौढ़ विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए तैयार नहीं होते हैं। इन विद्यालयों में अध्यापिकाओं का तो और भी अभाव रहता है। इस प्रकार अध्यापकों के अभाव में समाज शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होना असम्भव हो गया है।
(4) समाज के उत्तरदायित्व की समस्या-समाज शिक्षा की चतुर्थ समस्या है-समाज शिक्षा का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, शिक्षा विभागों, जिला परिषदों और सार्वजनिक शिक्षा संस्थाओं में से किस पर हो ? केन्द्रीय सरकार ने यह उत्तरदायित्व राज्य सरकार को दिया है और स्वयं को इस महत्वपूर्ण कार्य के भार से मुक्त करने का प्रयास किया है। किन्तु सरकारें धनाभाव एवं अन्य समस्याओं के कारण इस भार को ठीक से वहन नहीं कर पा रही हैं। अतः समाज शिक्षा का प्रसार खटाई में पड़ गया है। यदि केन्द्रीय सरकार इस प्रकार समाज शिक्षा की उपेक्षा करती रही तो समाज शिक्षा की कल्पना को साकार रूप देना सम्भव नहीं है।
(5) पाठ्यक्रम निर्धारण की समस्या-समाज शिक्षा की पाँचवीं समस्या है-पाठ्यक्रम के निर्धारण में कठिनाइयों का होना । प्रमुख कठिनाइयाँ इस प्रकार हैं-
(अ) बहुत दिनों से समाज-शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा है किन्तु अब तक इस बात पर मतैक्य नहीं हो सका है कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम सबसे उपयोगी होगा? वयस्कों की अभिरुचियाँ आवश्यकताएँ एवं दृष्टिकोण बालकों से भिन्न होने के कारण उनके लिए बालकों के लिए प्रयुक्त पाठ्यक्रम का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रौढ़ों में शिक्षा सम्बन्धी व्यक्तिगत विभिन्नता की समस्या है। कुछ प्रौढ़ निरक्षर हैं, कुछ अशिक्षित हैं और नवसाक्षर हैं। इन सभी के लिए पृथक्-पृथक् पाठ्यक्रम की आवश्यकता है।
(ब) पाठ्यक्रम निर्धारण सम्बन्धी दूसरी कठिनाई यह है कि यदि हम वास्तव में प्रौढ़ों के रहन- सहन का स्तर ऊँचा करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जो उन्हें बौद्धिक ज्ञान के साथ-साथ किसी न किसी कला या कौशल में प्रशिक्षित या दक्ष बना सके। इस प्रकार के पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी तीसरी कठिनाई यह है कि प्रौढ़ों में सभी आयु के पुरुष एवं स्त्रियाँ हैं। मोटे रूप में इन्हें
तीन आयु श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है-
(i) 12 से 17 वर्ष के प्रौढ़, (ii) 19 से 35 वर्ष तक के प्रौढ़ एवं (iii) 35 वर्ष से अधिक आयु के प्रौढ़। इन तीनों श्रेणियों की अभिरुचियों, आवश्यकताओं, बौद्धिक स्तरों एवं दृष्टिकोणों में अन्तर होता है। अतः सबके लिए समान पाठ्यक्रम निर्धारित करना एक जटिल समस्या है।
(6) शिक्षण-पद्धति के निर्धारण की समस्या-समाज शिक्षा की छठी समस्या है-
प्रौढ़ों के लिए उपयुक्त शिक्षण-पद्धति का निर्धारण करने में कठिनाइयों का होना। हम देखते हैं कि बच्चों में जीवन एवं संसार के प्रति किसी विशिष्ट दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण सभी बच्चों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षण पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है। किन्तु प्रौढ़ों का जीवन एवं संसार के प्रति दृष्टिकोण एक समान नहीं होता है। उन्हें अधिक सामाजिक स्वतन्त्रता के उपयोग का अवसर मिलने के कारण उनमें अहम् की भावना का पर्याप्त रूप से विकास हो जाता है। उनमें कुछ ऐसी आदतों, नियमों एवं सिद्धान्तों का विकास हो जाता है, जिनके विरुद्ध वे न तो स्वयं कार्य करना चाहते हैं और न दूसरों को ऐसा कोई कार्य करने का अवसर देना चाहते हैं। इन सभी परिस्थितियों के कारण प्रौढ़ों के लिए उपयोगी एवं प्रभावशाली शिक्षण पद्धति, निर्धारित करना अति दुष्कर है। यदि सभी प्रौढ़ों के लिए एक पद्धति का प्रयोग किया जाता है तो यह निश्चय है कि उन्हें वह अरुचिकर प्रतीत होगी और उसकी अहम् की भावना स्वतन्त्रता, आदतों, नियमों एवं सिद्धान्तों को ठेस पहुँचेगी, जिसके परिणामस्वरूप उसका असफल हो जाना अवश्यम्भावी है। इन्हीं कठिनाइयों के कारण सामाजिक शिक्षा के लिए अभी तक किसी एक पद्धति को निश्चित नहीं किया जा सकता।
(7) उपयुक्त साहित्य की समस्या-समाज शिक्षा की सातवीं समस्या है इसके लिए उपयुक्त साहित्य के तैयार करने एवं जुटाने की आवश्यकता । प्रौढ़ विद्यालयों में मुख्यतः प्रौढ़ों को लिखना- पढ़ना एवं गणित की शिक्षा प्रदान की जाती है जो उन्हें भविष्य में शिक्षित बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रायः देखा जाता है कि प्रौढ़ विद्यालय की शिक्षा के उपरान्त नवसाक्षर शिक्षा ग्रहण करने का कार्य समाप्त कर देते हैं जिसके परिणामस्वरूप वे पुनः निरक्षर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में नवसाक्षरों के लिए प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद ऐसे साहित्य की आवश्यकता है जो उनमें सामाजिक भावना, आलोचनात्मक शक्ति एवं वस्तुओं को परखने की क्षमता के विकास में योग दे ताकि, “वे कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं निकृष्ट के बीच, ज्ञान के क्षेत्र में सच एवं झूठ के बीच एवं आचरण के क्षेत्र में भले और बुरे के बीच में अन्तर ला सकें।”
(8) शिक्षा के साधनों की समस्या-समाज शिक्षा की आठवीं समस्या है-इसके लिए साधनों के चयन में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता। “समाज शिक्षा के साधनों का अभिप्राय है-वे समूह या संस्थाएँ जो समाज शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से सम्पर्क रखती हैं, उन्हें ज्ञान प्रदान करती हैं एवं उनकी आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करती हैं।” इन साधनों के चयन में इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि प्रौढ़ को ज्ञान प्राप्त करने के प्रति आकर्षित करें। किन्तु ऐसे साधनों का चुनाव करने के लिए अत्यधिक विवेक और अनुभव की आवश्यकता है। यह कार्य केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा हो सकता है जो प्रौढ़ मनोविज्ञान में दक्ष हो ।
प्रश्न 2 (iii) उपनिषदीय दर्शन का मूल्यांकन कीजिए तथा इस दर्शन में निहित शिक्षा पर प्रकाश डालिए।
अथवा
उपनिषदीय शिक्षा व्यवस्था का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव पर निबन्ध लिखिए।
उत्तर – उपनिषद् दर्शन का मूल्यांकन
उपनिषदों में यह वर्णन किया गया है कि अपने आत्म-स्वरूप का साक्षात्कार करके जीव ‘एकेन विज्ञानेन सर्व विज्ञातं भवति’ इस उपनिषद्-वाक्य के अनुसार सभी वस्तुओं के ज्ञान प्राप्त करके स्वयं
• अनुभव कर लेता है कि यह सब ब्रह्म-स्वरूप है। अतः संसार की सभी वस्तुओं का अस्तित्व एवं विनाश जिस सत्ता के कारण होता है उसका ज्ञान मोक्ष की प्रगति में आवश्यक है। इसी कारण सभी उपनिषदों में परम सत्ता की खोज के लिए एक निरन्तर प्रयास दिखलाई पड़ता है।
यदि शिक्षा दर्शन के रूप में देखा जाए तो उपनिषदें दार्शनिक चिन्तन के भण्डार हैं और उनके दार्शनिक विचारधाराओं के स्रोत हैं। षड् दर्शनोंयाय वैशेषिक, सांख्य-योग, वेदान्त और मीमांसा का विकास इन्हीं के आधार पर हुआ है। यद्यपि उपनषिदों में शिक्षा-विषय पर स्वतन्त्र रूप से विचार नहीं किया गया है, फिर भी शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों के सम्बन्ध में उपयुक्त प्रकाश डाला गया है। इसके साथ ही शिक्षक, शिक्षार्थी, अनुशासन व्यवस्था, विद्यालय आदि के विषय में उपनिषद् काल में पर्याप्त सामग्री मिलती है।
आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है। तैत्तिरीयोपनिषद् में उसे पंचकोषीय प्राणी कहा गया है। उपनिषदों में मनुष्य के अन्तःकरण-मन, अहंकार और बुद्धि की विशद विवेचना की गई है। इससे सीखने के स्वरूप और क्रिया का स्पष्ट ज्ञान होता है। उपनिषदों में शिक्षण की जिन विधियों (प्रश्नोत्तर, प्रतिगमन, कथा, व्याख्या और विचार-विमर्श एवं तर्क) का प्रयोग किया गया है, वे सभी आज शिक्षण की युक्तियों के रूप में प्रयोग की जाती हैं। सीखने वाला श्रवण (अध्ययन) के बाद यदि मनन (चिन्तन) और निदिध्यासन (नित्य अभ्यास) करें तो निःसन्देह सीखना स्थायी होगा। आज के शिक्षक इससे लाभ उठा सकते हैं।
स्पष्ट है कि यदि भारतीय दर्शन के अन्तर्गत उपनिषदीय-चिन्तन को देखा जाए तो वह आधुनिक युग की शिक्षा के लिए एक महत्त्वपूर्ण चिन्तन है। आधुनिक युग विज्ञान का युग है जिसमें जीवात्मा को मन की शान्ति के लिए प्रयास करना पड़ता है, पाश्चात्य सभ्यता के अन्धानुकरण के कारण जीव का मन अस्थिर हो भटक रहा है। उपनिषदीय चिन्ताओं में आत्मानुभूति पर विशेष बल देकर मनुष्य के मन की शान्ति की बात कही गई है। विभिन्न मूल्यों का ह्रास न हो। इसके लिए स्व-शिक्षा स्व-नियन्त्रण पर बल दिया गया है। इस प्रकार आज की शिक्षा को उचित दिशा देने के लिए उपनिषदीय दर्शन आज भी शिक्षा में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं, बशर्ते हम मनुष्यों के सर्वांगीण विकास के लिए उस दिशा में प्रयासरत हों।
उपनिषद् दर्शन में शिक्षा का अर्थ –
उपनिषदों के अन्तर्गत शिक्षा के लिए विद्या शब्द का प्रयोग किया गया है और विद्या को अमृत प्राप्ति अर्थात् आत्मानुभूति का साधन माना गया है (विद्या अमृतमश्नुते) उपनिषदों के अनुसार आत्मानाभूति के साधन हैं— ज्ञान, कर्म और योग। इस प्रकार उपनिषदों के अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो हमें ज्ञान, कर्म व योग साधना में प्रशिक्षित करती है, हमें आत्मानुभूति करने योग्य बनाती है।
उपनिषद् दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य
उपनिषद् दर्शन में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्न को बताया गया है-
(1) विद्या से असत्य का नाश होता है और आनन्द की प्राप्ति होती है। आनन्द ब्रह्म या आत्मा का शाश्वत स्वरूप है। आनन्द का प्रथम और निम्नतम लक्ष्य ‘अन्नमय’ है अर्थात् जीवन के भौतिक पक्ष की प्राप्ति आनन्द प्राप्ति का प्रारम्भिक लक्षण है। अतः शिक्षा का प्रथम उद्देश्य भौतिक जीवन की प्राप्ति है।
(2) विद्या स्वस्थ शरीर के निर्माण से सम्बन्धित है। यह भौतिक स्वरूप से उच्चतर होता है। प्राण ही वह शक्ति है जिसके द्वारा वनस्पति तथा प्राणी जगत श्वास लेता है। यही ‘प्राणमय’ स्वरूप है।
(3) उपनिषद् दर्शन में शिक्षा का उद्देश्य बालक का मानसिक विकास करना है। मानव जाति अन्य जातियों से इस कारण उच्च मानी जाती है क्योंकि उसमें मनस होता है जिसके द्वारा वह विचार कर सकती है। यही आनन्द का तीसरा रूप ‘मनोमय’ है। शिक्षा का चतुर्थ उद्देश्य है बालक का सत्य-असत्य तथा अच्छाई-बुराई में अन्तर करना सिखाया जाए। इसी को ‘विज्ञानमय’ कोष कहा गया है। शिक्षा का पंचम उद्देश्य आत्मानुभूति है। यह आत्मा या आनन्द का सर्वोच्च स्थान है। इस स्थिति में ज्ञाता, ज्ञेय तथा ज्ञान के बीच समस्त भेद समाप्त हो जाते हैं। यह आत्मा का अन्तिम स्वरूप ‘आनन्दमय’ कोष है।
प्रश्न 2 (iii) शिक्षा तथा दर्शन में परस्पर सम्बन्ध है, एक का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि एक में परिवर्तन होता है तो दूसरे में भी कैसे परिवर्तन हो जाता है?
अथवा
शिक्षा और दर्शन के परस्पर सम्बन्धों की समीक्षा कीजिए।
अथवा
शिक्षा और दर्शन की अन्योन्याश्रितता स्पष्ट कीजिए।
अथवा
शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है।” इस उक्ति की सतर्कतापूर्वक व्याख्या कीजिए।
उत्तर – शिक्षा और दर्शन का सम्बन्ध
डॉ0 राधाकृष्णन का कथन है, “दर्शन यथार्थता के स्वरूप का तार्किक ज्ञान है।” इसी कारण कहा जाता है कि शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ सम्बन्ध है। शिक्षा की प्रक्रिया व्यक्ति को अपने जीवन में पूर्ण बनाने का प्रयास करती है। व्यक्ति को पूर्ण बनाने तथा उसके विकास के लिए अनुभव आवश्यक होता है। दर्शन अनुभव प्राप्त करने में विशेष रूप से सहायता प्रदान करता है। स्पष्ट है कि शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ सम्बन्ध है। बिना दर्शन की सहायता शिक्षा को पूर्णतः नहीं मिल सकती।
‘शिक्षा दर्शन’ दर्शन की एक शाखा है। शिक्षा दर्शन ऐसे प्रश्नों से सम्बन्धित है-जैसे शिक्षक क्या है ? शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए? आदि। शिक्षा दर्शन से सम्बन्धित अनेक समस्याओं पर गम्भीरता से विचार करता है और उनका समाधान भी करता है। शिक्षा दर्शन के उद्देश्य के विषय में कनिंघम ने इस प्रकार लिखा है- “शिक्षा दर्शन अनेक दार्शनिक विचारधाराओं द्वारा निकाले गये सिद्धान्तों के प्रयोग के रूप में इन विचारधाराओं से भिन्न समस्याओं की खोज के लिए निर्देशन लेता है-” निम्नलिखित पंक्तियों में हम यह स्पष्ट करेंगे कि दर्शन किस प्रकार शिक्षा को प्रभावित करता है और शिक्षा किस प्रकार दर्शन को प्रभावित करती है-
1. दर्शन शिक्षा का पूरक है-दर्शन शिक्षा का पूरक है। इसका मुख्य कारण यह है कि शिक्षण कला दर्शन के अभाव में पूर्णता प्राप्त करने में असमर्थ रहती है। जर्मन दार्शनिक फिक्टे के अनुसार, “दर्शन के अभाव में शिक्षा की कलापूर्ण स्पष्टता प्राप्त नहीं कर सकती।”
2. दर्शन शिक्षा का आधार है-शिक्षा का आधार दर्शन है। जेण्टाइल के अनुसार, “बिना दर्शन की सहायता से शिक्षा प्रक्रिया सही मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती।”
3. दर्शन शिक्षा की अमूल्य सहायता करता है-दर्शन शिक्षा की अमूल्य सहायता करता है। बटलर के शब्दों में- “दर्शन शिक्षा के प्रयोगों के लिए एक पथ-प्रदर्शक है, शिक्षा अनुसन्धान के क्षेत्र के रूप में दार्शनिक निर्णय हेतु निश्चित सामग्री को आधार के रूप में प्रदान करती है।”
4. दर्शन शिक्षा का सिद्धान्त है-दर्शन शिक्षा का सिद्धान्त है। ड्यूवी के अनुसार, “अपने सामान्यतम रूप में दर्शन शिक्षा सिद्धान्त है।”
5. दर्शन विश्व की प्राचीनतम विद्या है-ई० वी० शर्क के अनुसार, “दर्शन विश्व की प्राचीनतम विद्या है। इसका वास्तविक अर्थ है-विज्ञान अथवा व्यवस्थित प्रयत्न जो सैकड़ों वर्षों के एकत्रित साक्ष्यों पर आधारित है।”
6. शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है-दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों को निश्चित करता है जबकि शिक्षा उन्हें प्राप्त करने के साधनों को निश्चित करती है। शिक्षा के अभाव में कोई सिद्धान्त व्यावहारिक रूप नहीं ले सकता है। व्यक्ति के विकास के लिए अनुभव आवश्यक होता है। दर्शन अनुभव प्राप्त करने में विशेष सहायक होता है। इस तथ्य को सर जॉन एडम्स ने अपने शब्दों में इस प्रकार स्पष्ट किया है- “शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। यह दार्शनिक विश्वास का सक्रिय पक्ष जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने का व्यावहारिक साधन है।”
हरबर्ट ने दर्शन और शिक्षा का सम्बन्ध बताते हुए लिखा है, “शिक्षा को छुट्टी मनाने का अवसर ही कहाँ है, जब तक कि दर्शन की गुत्थियाँ सदैव के लिए न सुलझ जायँ ।’
उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि दर्शन और शिक्षा आपस में घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं। समाज की आवश्यकताओं के अनुसार दार्शनिक विचारधाराएँ उत्पन्न होती हैं और उसी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य तथा प्रणाली निश्चित की जाती है।
रॉस ने दर्शन और शिक्षा का सम्बन्ध बताते हुए लिखा है, “दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू के समान हैं। एक में दूसरा निहित है। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा क्रियात्मक पक्ष।” शिक्षक शिक्षा के उद्देश्यों तथा आदर्शों का बालकों में प्रसार करता है। इसी कारण वह शिक्षा के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान रखता है। शिक्षक अपनी दार्शनिक विचारधारा के अनुकूल अपना आदर्श प्रस्तुत करता है। आदर्शों एवं उद्देश्यों को निश्चित करने के लिए दार्शनिक विचारधारा अनिवार्य है। इसी कारण अध्यापकों को दार्शनिक विचारधाराओं से बालकों को प्रेरित तथा प्रभावित कर आगे बढ़ाना होता है। यदि आदर्शों को शिक्षा से पृथक् कर दिया जाय तो शिक्षा अर्थहीन हो जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक के पद का मापदण्ड भी दार्शनिक विचारधाराओं से बनता है।
अतः शिक्षा और दर्शन का एक-दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध है। शिक्षा और दर्शन एक-दूसरे पर निर्भर है। यहाँ पर हम दर्शन और शिक्षा की पारम्परिक निर्भरता की पुष्टि में कुछ शिक्षाविदों के कथन प्रस्तुत करेंगे-
ड्यूवी- “दर्शन अपने सामान्यतया रूप में शिक्षा सिद्धान्त है। ”
जेण्टाइल – “दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती।” फिक्टे- “शिक्षा का कार्य दर्शनशास्त्र की सहायता के बिना पूर्णतया तथा स्पष्टता को प्राप्त नहीं “कर सकता।”
स्पेन्सर- “वास्तविक शिक्षा का संचालन एक वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है।”
हम रॉस के कथन से पूर्णतया सहमत हैं कि “शिक्षा सम्बन्धी समस्त प्रश्न अन्ततः दर्शन से सम्बन्धित हैं।” इस सम्बन्ध में हम शिक्षा और दर्शन का सम्बन्ध स्पष्ट कर चुके हैं। वास्तव में शिक्षा का आधार दर्शन है। दर्शन की सहायता के अभाव में शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती ।
जो विद्वान् यह कहते हैं कि ‘शिक्षा को दार्शनिक विचारों से मुक्त कर देना चाहिए’ उनके विचार अत्यन्त संकीर्ण हैं। जेण्टाइल ने इन विचारों का खण्डन किया है। वह कहता है कि “जो व्यक्ति इस बात में विश्वास रखते हैं कि दर्शनविहीन होने पर भी शिक्षण प्रक्रिया उत्तम रीति से चल रही है वे शिक्षा के अर्थों को पूर्णरूपेण समझने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं।”
हम इस कथन से सहमत हैं कि “सभी शैक्षिक समस्याएँ अन्य में दर्शन की ही समस्याएँ होती हैं।” इस कथन से स्पष्ट होता है कि शिक्षा के सभी अंगों-शिक्षा के उद्देश्यों पर दर्शन का प्रभाव पड़ता है। दार्शनिक विचारधाराओं के परिवर्तन के साथ-साथ शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, पाठ्यविधि आदि में भी परिवर्तन होता रहता है।
इस प्रश्न के उत्तर में इस तथ्य की व्याख्या से कि दर्शन और शिक्षा का घनिष्ठ सम्बन्ध है, यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षक के लिए एक शिक्षा दर्शन की क्यों आवश्यकता होती है। प्लेटो, स्पेन्सर, लॉक, डीवी, महात्मा गाँधी, टैगोर, विवेकानन्द और राधाकृष्णन महान् दार्शनिक होने के साथ-साथ महान् शिक्षाशास्त्री भी थे। स्पेन्सर का कथन है-“वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है।” प्रत्येक अध्यापक को दर्शन का ज्ञान होना आवश्यक है। इसका कारण यह है कि शिक्षा और दर्शन में अटूट सम्बन्ध है। फिक्टे के अनुसार, “दर्शन के अभाव में शिक्षा की कला पूर्ण स्पष्टता को प्राप्त नहीं कर सकती है,” ड्यूवी अध्यापक के लिए दर्शन का ज्ञान अनिवार्य समझता है। उसके अनुसार, “दर्शन अपने सामान्य रूप से शिक्षा सिद्धान्त ही है।’
प्रश्न 3 (i) बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ बताइए।
अथवा
बौद्ध दर्शन के शैक्षिक अभिप्रायों का उल्लेख कीजिए तथा आधुनिक भारतीय शिक्षा हेतु उनकी सार्थकता का परीक्षण कीजिए।
अथवा
मूल्यों के शिक्षण के सन्दर्भ में बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ की विवेचना कीजिए।
उत्तर – बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ
महात्मा बुद्ध एवं उनके शिष्यों-अनुयायियों ने संसार के लोगों को दुःखों से मुक्ति का सन्देश, उपदेश, शिक्षा दी। जो भी शिक्षा दी उस पर मनन-चिन्तन किया तथा विभिन्न सिद्धान्त प्रतिपादित किये। ये सिद्धान्त बौद्ध दर्शन के नाम से पुकारे गये। इन्हीं सिद्धान्तों को शिक्षा – ज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त करके तत्सम्बन्धी विचार निकर्ष निकाले गये जिन्हें बौद्ध शिक्षा दर्शन कहा गया। बौद्ध शिक्षा दर्शन प्रत्यक्षवादी कहा जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य मालुक्यपुत्र को कहा था कि सिद्धान्तों के विवेचन से दुःखी मानवता का दुःख दूर नहीं किया जा सकता, बल्कि दुःखों को दूर करने का प्रयास होना चाहिए, दुःख मुक्ति के मार्ग निकालना चाहिए। यही सिद्धान्त उपदेश रूप में बौद्ध दर्शन बने और उनका व्यावहारिक रूप बौद्ध शिक्षा दर्शन कहा जा सकता है।
बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा का अर्थ –
महात्मा बुद्ध ने अपने युवा जीवन में तीन दृश्य देखे- वृद्ध की दुर्दशा, मृत व्यक्ति के लिए विलाप, संन्यासी की स्थिति। इनसे प्रभावित होकर वह ‘सत्य ज्ञान’ की खोज में निकले। महात्मा बुद्ध का विचार था कि ‘मुझमें भी श्रद्धा है, वीर्य है, स्मृति और प्रज्ञा है, मैं स्वयं धर्म का साक्षात्कार कर सकता हूँ।’ यह आत्मबोध या आत्मज्ञान ही वास्तव में शिक्षा है, इसीलिए महात्मा बुद्ध को बोधिसत्व कहा जाता है।
बोध से क्या तात्पर्य है? इस ओर भी देखना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने मानव जीवन के चार आर्य सत्य बताये हैं-दुःख, दुःख समुदय, दुःख निरोध और दुःख निरोधगामी प्रतिपदा। इस संसार में दुःख ही दुःख है। समस्त संसार जब आग में जल रहा है तब उसमें आनन्द का अवसर कहा? अन्धकार (अज्ञान) से व्यक्ति देख नहीं पाता है (धम्मपद)। अतः अज्ञान और उससे प्राप्त दुःखों को दूर करने का मार्ग जानना ही बोध है अथवा शिक्षा है। अतः बौद्ध दर्शन के अनुसार जीवन में दुःख है और शिक्षा इन दुःखों को दूर करने का मार्ग बताती है। शिक्षा दुःखों का ज्ञान है और दुःखों को दूर करने का अष्टांग प्रदान करती है। जब यह बोध या अनुभूति और प्रयत्न होता है तो वही शिक्षा हो जाती है। अतः शिक्षा व्यावहारिक एवं आध्यात्मिक जीवन में आर्य सत्य (ज्ञान) देने वाली और सद्मार्ग की ओर ले जाने वाली क्रिया है।
महात्मा बुद्ध ने ‘भग्गानं अट्ठांग को सेट्ठी’ अर्थात् अष्टांग मार्ग को सभी मार्गों में श्रेष्ठ कहा है। इस मार्ग पर चलने के लिए शील, समाधि और प्रज्ञा प्राप्त करना जरूरी है। शील पापों, अकर्मों, तृष्णाओं का निरोध हैं, समाधि कुशल चित्त की एकाग्रता और प्रज्ञा अविद्या का नाश है। सम्यक् वाक्, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति, सम्यक् समाधि, समाधि में तथा सम्यक् दृष्टि और सम्यक् संकल्प प्रज्ञा में अन्तर्भूत पाये जाते हैं। इस प्रकार शिक्षा अष्टांग मार्ग का अनुशीलन है जिससे व्यक्ति अर्हत्व की प्राप्ति करता है। अस्तु, शिक्षा अर्हत्व की प्राप्ति का साधन है, उसकी कठिन प्रक्रिया है।
आधुनिक भारतीय शिक्षा की सार्थकता
जिस अष्टांग मार्ग का प्रतिपादन और अनुमोदन महात्मा बुद्ध ने किया है और जैसी शिक्षा उन्होंने दी उसके आधार पर हम शिक्षा के अग्रलिखित आठ कार्य भी निश्चित कर सकते हैं जो आगे दिये जा रहे हैं-
1. सम्यक् दृष्टि के आधार पर अविद्या, अज्ञान, मिथ्या दृष्टि दूर करना तथा वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को पहचानने की क्षमता प्रदान करना। इससे दुःख, दुःख का कारण, दुःख के परिणाम दूर होते हैं।
2. सम्यक् संकल्प के आधार पर राग-द्वेष- तृष्णारहित, अहिंसा, त्याग, दया से पूर्ण जीवन व्यतीत करने का निश्चय करना। इससे व्यक्ति में पवित्र जीवन का विचार दृढ़ होता है, अभ्यास होता है।
3. सम्यक् वाचा के अनुसार पर अप्रिय, मिथ्या, अशुभ, अप्रिय, असंयमित, निन्दनीय वाणी का प्रयोग न करना, जिससे दूसरों को दुःख या कष्ट हो। इसमें भाषा प्रयोग पर नियन्त्रण होता है।
4. सम्यक् कर्मान्त के आधार पर अहिंसा, अस्तेय, सत्य, संयम, शीलता, भद्रता जैसे गुणों का विकास करना जो तदनुकूल व्यवहार-कर्म के लिए अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। शुद्धाचरण के लिए यह
आवश्यक कहा जाता है।
5. सम्यक् आजीव के आधार पर उचित साधनों एवं उपायों से जीविका प्राप्ति करना और अनुचित मार्ग, साधन एवं उपाय का अनुसरण न करके जीवन निर्वाह करना। इससे शुद्ध वृत्ति व अध्यवसाय के लिए प्राणी प्रयत्न करता है और धन के लोभ का संवरण करता है
6. सम्यक् व्यायाम के आधार पर सद् प्रयास या पुरुषार्थ का पालन करना, अकुशल धर्म का त्याग करना, कुशल धर्मों का उपार्जन करना, पुराने बुरे भाव-विचारों से दूर रखना, नये बुरे विचार- भाव न आने देना, मन में शुभ धारणा बनाये रखना।
7. सम्यक् स्मृति के आधार पर अच्छे उपदेशों, ज्ञान, धर्म को बार-बार स्मरण करना, जागरूक रहना और सावधान रहना जिससे निर्वाण प्राप्त होता है।
8. सम्यक् समाधि के आधार पर चित्त को एकाग्र करना तथा क्रोध, आलस्य, उद्धतता, पश्चाताप, सन्देश आदि से विगत होना, सांसारिक लोभ से अडिग रहना, दुःख-सुख में पूर्ण शान्त रहना ।
शिक्षा के ये कार्य व्यक्ति को पूर्ण शिक्षित-सभ्य बनाते हैं। इन गुणों से युक्त व्यक्ति मनसा, वाचा, कर्मणा से अनुशासित होता है। अनुशासित होने से ही व्यक्ति अपना सम्यक् विकास करने में समर्थ होता है। इस प्रकार शिक्षा का कार्य व्यक्ति का सम्पूर्ण विकास बौद्ध दर्शन के अनुसार कहा जा सकता है।
बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य
बौद्ध शिक्षा का कार्य व्यक्ति का मनसा, वाचा, कर्मणा विकास करना कहा जा सकता है, अतएव शिक्षा के उद्देश्य भी तद्नुकूल निर्धारित किये जा सकते हैं जो निम्नलिखित कहे जा सकते हैं-
1. सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास- बौद्ध शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य सम्यक् विकास कहा जा सकता है। व्यक्ति के तीन पक्ष हैं-संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक। ये तीनों पक्ष सम्यक् दृष्टि, सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि के अष्टांग मार्ग में मिलते हैं। इन मार्गों में वैयक्तिक एवं सामाजिक दोनों पक्ष शामिल पाये जाते हैं। ऐसी दशा में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य समन्वित एवं सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। ज्ञान, भाव और क्रिया सभी का विकास बौद्ध शिक्षा का लक्ष्य है।
2. नैतिक एवं आचरणिक विकास- बौद्ध धर्म एवं दर्शन दोनों में नैतिक एवं शुद्ध आचरण पर जोर दिया गया है। उचित कर्म नैतिकता की मुख्य कसौटी है जो व्यक्ति राष्ट्र या समुदाय के सम्बन्ध में सही है। सामाजिक कल्याण औचित्य के अभ्यास या उचित कर्म के अनुपालन पर ही निर्भर करता है। “बौद्ध धर्म-दर्शन के अनुसार उचित ज्ञान, उचित प्रयोजन और उचित वाणी के परिणामस्वरूप ही उचित कर्म या निष्काम कर्म होता है।” यह उपदेश स्वरूप बौद्ध शिक्षा है। अतः बौद्ध शिक्षा का दूसरा उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक एवं आचरणिक विकास करना कहा जाता है। बुद्ध मुख्यतया एक धार्मिक सुधारक तथा आचार के शिक्षक थे, इसलिए उनका ‘आचार मार्ग’ का सूत्र था-
सव्व पापस्य अकरणं कुसलस्य उपसम्पदा ।
सचित्तपरियोदपनं एतं बुननं सासनं । (धम्म पद 14/5 )
3. सांस्कृतिक विकास- बौद्ध धर्म के प्रचार से भारतीय संस्कृति का भी प्रचार हुआ। योगी अरविन्द ने तो यहाँ तक कहा है कि संसार में भगवान बुद्ध के समान क्रियाशील पुरुष आज तक उत्पन्न नहीं हुआ
है। तत्कालीन धर्म के क्रियाकाण्डों का उन्होंने खण्डन किया और नव धर्म शिक्षा को सामने रखा। पूजा-पाठ, यज्ञ-योग, जादू-टोना, पशुबलि आदि का विरोध किया गया जिससे इनके शुद्ध रूप बौद्ध धर्म के पतन के बाद पुनः शुरू किये गये। वेद, शास्त्र, उपनिषद् आदि की आलोचना ने जहाँ बौद्ध संस्कृति का विकास किया वहीं प्राचीन भारतीय संस्कृति (हिन्दू संस्कृति) का पुनरुत्थान भी किया। अब स्पष्ट है कि बौद्ध शिक्षा का एक उद्देश्य सांस्कृतिक विकास भी था।
4. निर्वाण की प्राप्ति-बौद्ध शिक्षा का एक उद्देश्य है। निर्वाण की प्राप्ति । निर्वाण का तात्पर्य ‘अनन्त शान्ति’ है जिससे तृष्णा, काम, भोग, जरा-मरण के क्लेश-दुःख की शान्ति हो जाती है तथा अनन्त सुख-आनन्द की अनुभूति होती है। इस प्रकार बौद्ध शिक्षा में सांख्य और वेदान्त की मुक्ति की धारणा का मेल पाया जाता है। “हीनयानी निर्वाण सांख्य की मुक्ति के समान है और महायानी निर्वाण वेदान्त की मुक्ति का प्रतीक है।” अतएव निर्वाण या दुःख का नाश और सुख की प्राप्ति बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य कहा जाता है।
5. सामाजिक विकास- बौद्ध धर्म सामाजिक आचार-विचार की शिक्षा देता है। अतः बौद्ध शिक्षा का एक उद्देश्य लोगों में सामाजिक योग्यता एवं कुशलता का विकास करना था। बौद्ध भिक्षु स्वयं समाज में जाकर दीक्षा देते थे, देश-विदेश में भ्रमण भी करते थे। इससे उनमें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय भावना का भी विकास होता था। बौद्ध शिक्षा इस प्रकार व्यापक परिप्रेक्ष्य में दी जाती थी और यह व्यापक दृष्टिकोण सामाजिक विकास के उद्देश्य से उत्पन्न होता था। ‘शील’ या उचित जीवन ‘आत्मगत विशुद्धता’ है और मुक्ति प्राप्ति के लिए आवश्यक गुण है जो व्यवसाय और कार्य के आदर्श सम्पादन करने वाले समाज के सदस्य में होता है। बौद्ध शिक्षा का एक उद्देश्य इसीलिए सामाजिक भावना का विकास व्यापकतम परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है। सामाजिक विकास में जनतान्त्रिक जीवन एवं दृष्टिकोण का भी विकास अन्तर्निहित कहा जाता है।
प्रश्न 3 (ii) शिक्षा दर्शन के विभिन्न अंगों की विवेचना कीजिए।
अथवा
दर्शन को परिभाषित कीजिए। इसके प्रमुख उपायों का वर्णन कीजिए।
अथवा
शैक्षिक दर्शन को परिभाषित कीजिए। ज्ञान मीमांसा एवं मूल्य मीमांसा के शैक्षिक महत्त्व को प्रतिपादित कीजिए।
अथवा
शिक्षा में तत्वमीमांसा की भूमिका का वर्णन करें।
उत्तर – दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा
दर्शन और अंग्रेजी भाषा की फिलॉसफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है- ‘फिलॉस’ तथा ‘सोफिया’। फिलॉस का प्रेम तथा सोफिया का अर्थ है – ज्ञान। अन्तः दर्शन शब्द का अर्थ हुआ
‘ज्ञान से प्रेम’ ।
दर्शन की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए सेलर्स ने लिखा है-
“दर्शन एक ऐसा अनवरत प्रयास है जिसके द्वारा मनुष्य संसार तथा अपनी प्रकृति के सम्बन्ध में क्रमबद्ध ज्ञान द्वारा एक सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त करने की चेष्टा करता है।”
राधाकृष्णन के अनुसार, “दर्शन वास्तविकता की प्रकृति का तार्किक अध्ययन है।”
प्लेटो के अनुसार दार्शनिक की परिभाषा इस प्रकार है-“वह जिसे प्रत्येक करार के ज्ञान में रुचि है और जो सीखने के लिए जिज्ञासु है और ज्ञान से कभी भी संतुष्ट नहीं होता, वास्तव में दार्शनिक कहा जा सकता है।”
दर्शन के प्रमुख विभाग
दर्शन के प्रमुख रूप से तीन भाग हैं जो निम्न प्रकार हैं-
(1) तत्त्व मीमांसा-तत्त्व मीमांसा के तीन विभाग हैं-
(i) प्रकृति-दर्शन,
(ii) आत्म-दर्शन तथा
(iii) ईश्वर दर्शन।
(2) ज्ञान मीमांसा – ज्ञान मीमांसा में ज्ञान सम्बन्धी अध्ययन किया जाता है।
(3) मूल्य मीमांसा-मूल्य मीमांसा में व्यक्ति के धार्मिक मूल्यों का अध्ययन किया जाता है।
तत्त्व मीमांसा तथा शिक्षा दर्शन
सृष्टि क्या हैं? इस सम्बन्ध में व्यक्ति की जानने की ललक होती है या सत्य क्या है? इसको व्यक्ति जानना चाहता है यह समाधान तत्त्व मीमांसा में होते हैं। ऐसे प्रश्नों के समाधान एवं सर्वसम्मत भी नहीं है और न उनको प्रमाणित ही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यथार्थ का अनुभव कराने में जो उसका प्रमुख और व्यावहारिक पक्ष है शिक्षा अपने को असमर्थ-सा पाती है। ऐसी स्थिति में शिक्षा के सामने अनेक विकल्प उठ खड़े होते हैं-
(i) तत्त्व मीमांसा के क्षेत्र में उत्पन्न विवादों के चक्कर में छूटने का एक विकल्प यह है कि शिक्षाविद मिलकर एक सर्वसम्मत शैक्षिक तत्त्व ज्ञान को निश्चित करें। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यवहार प्रधान है। अतः मनुष्य, उसकी प्रकृति, उसकी आवश्यकताओं, उसके सामाजिक और आर्थिक जीवन पर देश और काल के सन्दर्भ में तात्त्विक विचार करके शिक्षा का स्वतन्त्र तत्त्व ज्ञान स्थिर करने की आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षाविद् को विभिन्न शाखाओं से मदद लेनी होगी, विशेष रूप से विज्ञान और मनोविज्ञान से ।
शिक्षा के व्यावहारिक पक्ष को ही लें तो मतैक्य नहीं मिलेगा। अब से ढाई हजार साल पहले अरस्तू ने यह कहा था कि क्या पढ़ना चाहिए-सद्गुण या उत्तम जीवन-इस बारे में एकमत नहीं रहा। यह भी स्पष्ट नहीं कि शिक्षा का क्षेत्र ज्ञान है अथवा नैतिक गुण। वर्तमान शिक्षा प्रणाली भ्रांतिपूर्ण है। कोई नहीं कह सकता है कि ठीक सिद्धान्त क्या है, जिस पर शिक्षा को चलना चाहिए। क्या जीवनोपयोगी ज्ञान या सद्गुण या उच्चज्ञान शिक्षा का उद्देश्य हो ? इन तीनों उद्देश्यों के समर्थक पाये जाते हैं। शिक्षा के साधनों के बारे में एकमत नहीं है। अरस्तू के समय से लेकर अब तक यही स्थिति बनी हुई है। एक कठिनाई और आ खड़ी हुई है। प्रजातन्त्र के उदय से विचार भिन्नता को ज्यादा महत्त्व मिला है। साथ ही राजनीति और अर्थशास्त्र को मानव जीवन में अधिक महत्त्व प्राप्त हो गया है और अध्यात्मवाद का पक्ष कमजोर पड़ता जा रहा है। इसलिए शिक्षा का काम अधिक कठिन होता जा रहा है और उसके तात्त्विक पक्ष पर गम्भीर रूप से विचार करने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता से स्वतन्त्र शिक्षा-दर्शन का विकास हो रहा है। पाश्चात्य शिक्षा जगत में तो ऐसा हो ही रहा है। भारत में अति प्राचीन काल से शिक्षा तत्त्व मीमांसा से जुड़ी रही है। अब आवश्यकता इस बात की है कि नयी परिस्थितियों में भारतीय शिक्षा-दर्शन का विकास किया जाए। यह शिक्षा-दर्शन न केवल उद्देश्यों का वरन् पाठ्यक्रम, शिक्षण-विधियों और शिक्षा व्यवस्था तथा मूल रूप से छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाए।
(ii) उपर्युक्त विवरण में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि तात्त्विक मीमांसा के धरातल को छोड़ना शिक्षा के लिए न तो सम्भव ही है और न खतरों से खाली। साथ ही संसार की यथार्थता और ‘संसार की असारता’ के दो परस्पर विरोधी मतों से बने दो अलग-अलग खेमों में से किसी एक खेमे में जाकर बैठना भी शिक्षक के लिए तर्कसंगत नहीं है। उदाहरण के लिए शिक्षा (मान लें) संसार की असारता पर विश्वास करने वालों के मत को स्वीकार करके एक ऐसी व्यवस्था बनाने में लग जायें जिसमें सभी छात्र दार्शनिक वैरागी शासक बन जायें तो संसार की बड़ी दुर्गति होगी। सारे के सारे छात्र इस संसार को माया और भ्रमजाल मानकर जीवन की यथार्थता से मुँह मोड़ कर जंग में जा बैठें तथा कर्महीन बनकर समाधिस्थ हो जायें तो देश का क्या होगा ? समाज कैसे चलेगा? कृषि, उद्योग-धंधे, व्यापार और दुनियादारी ठप्प हो जाएगी। हमारे देश में इस प्रकार की विचारधारा से जहाँ दर्शन, धर्म कला और साहित्य की प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो गईं। वहीं संसार के प्रति वैराग्य होने से देश को आक्रमणकारियों का शिकार होकर महान कष्ट भोगना पड़ा। दूसरी ओर संसार में सार है, यही यथार्थ है-इस मत को सभी स्वीकार करें अपनी व्यवस्था बना लें तो दूसरे प्रकार के छात्र बनेंगे। उनमें हर प्रकार की वासना और योगेच्छा पैदा होगी। दुराचार और आसुरी प्रवृत्तियाँ बढ़ेंगी क्योंकि सांसारिक ऐश्वर्य की वृद्धि से मदांध होकर वे विवेक खो बैठेंगे। यह सब कुछ हम भारत को वर्तमान शिक्षा पद्धति के परिणामों के रूप में देख रहे हैं तब क्या किया जाए?
वास्तव में शिक्षा के लिए किसी एक तात्त्विक विचारधारा से सम्पूर्ण रूप से जुड़ जाना उपयुक्त न होगा। शिक्षा तत्त्व मीमांसा से एक दूसरे प्रकार से लाभ उठा सकती है। इससे दूसरा विकल्प बनता है। वह यह है कि शिक्षाशास्त्री तत्त्व मीमांसा के क्षेत्र में उत्पन्न सभी मतों और वाद-बिन्दुओं का बारीकी से अध्ययन करें। फिर यह देखें कि उनमें कहाँ तक संगति और कहाँ तक असंगति है। यह वर्णनात्मक एवं मूल्यांकन प्रधान ढंग है जो शिक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं उनकी व्यावसायिक तैयारी करने के कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार की दार्शनिक एवं तात्त्विक विचारधाराओं के अध्ययन को सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि शिक्षक इन सबका मूल्यांकन करके विभिन्न तात्त्विक मतों से वे बिन्दु छाँटकर निकल सकें, जो देश-काल और व्यक्ति के सन्दर्भ में सार्थक हो। ऐसा करने से अधिकांश अध्यापक – शिक्षक न तो अवगत हैं और न ही वे जानकार भी इस तरफ ध्यान देते हैं।
(iii) शिक्षा का प्रमुख दायित्व यह है कि वह छात्रों को इस संसार में सफलतापूर्वक और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करे। परन्तु इस दायित्व को पूरा करना तभी सम्भव होगा जब वह पहले निश्चय हो कि संसार की वास्तविकता, उसका यथार्थ क्या है। इस बिन्दु पर आते ही मतभेद उठ खड़े होते हैं। एक तत्त्वज्ञानी यह कहता है कि संसार अनुसार है, माया और भ्रम है, तो दूसरा कहता है यह संसार वास्तविक है, क्योंकि यह अनुभवगत है तो पहले मत को मान लें, तो शिक्षा व्यवस्था का प्रारूप एक प्रकार का होगा और दूसरे का मान लें तो उसका प्रारूप पहले से सर्वथा भिन्न होगा। ऐसी दशा में शिक्षाकर्मी किंकर्त्तव्यविमूढ़ होकर उस नाव के समान बनकर रह जायेगा जो लहरों के थपेड़ों में दिशाहीन होकर चक्कर काटती रहती है तब तो क्या यह विकल्प चुनना उपयुक्त न होगा कि शिक्षा तत्त्व मीमांसा के चक्कर से छुटकारा पा ले। अच्छा यही होगा कि वह तत्त्व मीमांसा को नकारे परन्तु इस विकल्प को चुनना आसान नहीं है क्योंकि तत्त्व मीमांसा को नकारने की बात करना एक अन्य प्रकार के तात्त्विक विवाद को जन्म देना है।
ज्ञान मीमांसा तथा शिक्षा दर्शन
ज्ञान मीमांसा और शिक्षा के तत्त्व निम्न प्रकार हैं-
(i) ज्ञान और छात्र प्रकृति- शिक्षण प्रक्रिया में छात्र ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है। अतः शिक्षा का केन्द्रीय बिन्दु छात्र है। छात्र एक मनुष्य और सजीव प्राणी है। अतः उसकी प्रकृति की जानकारी प्राप्त करना शिक्षक के लिए आवश्यक है। मानव प्रकृति की जानकारी एक ओर तत्त्व मीमांसा से और दूसरी ओर आधुनिक मनोविज्ञान से प्राप्त होती है।
तत्त्व मीमांसा के अन्तर्गत सत्य के विषय में कहा गया है कि कुछ लोग सत्य को चेतन मानते हैं और विश्वास करते हैं कि वह चेतन एक पारलौकिक तत्त्व है और समस्त जगत्-जीव उसी से उत्पन्न मनुष्य अन्दर भी उसी तत्त्व का एक अंश विद्यमान है। इसे ‘आत्मा’ कहा गया है। ज्ञान का अधिकारी यही आत्मा है। ज्ञान प्राप्ति में शरीर का कोई महत्त्व नहीं है। शिक्षा की दृष्टि से इस विचार का महत्त्व यह है कि छात्र के भीतर वर्तमान आत्मतत्त्व को जानने और पहचानने की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि आत्मतत्त्व ही अनुभवकर्त्ता है, वही ग्रहण करता है। शरीर की ज्ञानेन्द्रियों से जो अनुभव प्राप्त होते हैं, उन्हें भोगने वाला वही है। सोते समय मनुष्य स्वप्न देखता है। उस समय ज्ञानेन्द्रियाँ निष्क्रिय रहती हैं, परन्तु उस समय देखने वाला, गंध लेने वाला और सुनने वाला यही आत्मा है। इसका अर्थ है कि छात्र के भीतर वर्तमान आत्मा का विकास करना, उसको विकारों से मुक्त करना शिक्षा का मूल दायित्व है। इसमें संदेह नहीं कि यह आत्मतत्त्व शिक्षा से प्रभावित होता है। इसीलिए प्राचीन धार्मिक शिक्षा में छात्रों को एक विशेष प्रकार के अनुशासन में रहना पड़ता था।
मानव प्रकृति का एक अन्य पहलू सामाजिकता है। कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक पशु है। वह जंगली पशुओं से भिन्न इसलिए है कि वह अपने समान अन्य पशुओं के बीच रहना पसन्द करता है। सच तो यह है कि समाज में रहने से ही उसमें मानवीय गुण जैसे-त्याग, सेवा, सहयोग और भाईचारा आदि उत्पन्न हुए। उसकी अनेक खोजें और आविष्कार समाज के कारण सम्भव हुए। भेड़ियों की माँद में पले मानव बालक यह सिद्ध करते हैं कि समाज से अलग रहने के कारण वे पशु बन गये। समाज में रहने के कारण मनुष्य को भाषा, साहित्य, संस्कृति और सभ्यता का वरदान मिला।
मनोवैज्ञानिकों का एक वर्ग बताता है कि सामाजिकता मनुष्य की आदि प्रवृत्ति है, बच्चा पैदा होते ही सामाजिक बन जाता है। वास्तव में स्नेह और सुरक्षा पाने के लिए उसका सामाजिक होना अनिवार्य है। मनुष्य के भीतर वर्तमान प्रकृति प्रदत्त संवेग या भावनाएँ जैसे-स्नेह, भय, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष सामाजिकता के आधार हैं, उसकी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएँ जैसे-शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आदि तभी पूरी होती हैं, जब वह समाज का सहारा ले । अस्तु, मनुष्य की सामाजिकता की उपेक्षा शिक्षा नहीं कर सकती। प्राचीनकाल की शिक्षा का भी एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य यह था कि मनुष्य दूसरों के लिए जीना मरना सीखे और वर्तमान शिक्षा भी छात्रों के समाजीकरण पर बल देती है। जब हम राष्ट्रीय एवं भावनात्मक एकता की बात करते हैं अथवा छात्रों में विश्वबंधुत्व की भावना पैदा करने की बात करते हैं, तो हमें छात्रों की सामाजिक वृत्ति के विकास की सुदृढ़ बनानी होगी। पाठ्यक्रम में ऐसे विषय जैसे-नागरिकशास्त्र, सामाजिक ज्ञान, भारतीय संस्कृति का परिचय, राष्ट्रीय सेवा आदि शामिल करना होगा ताकि छात्र अतिव्यक्तिवादी न बन जाये। व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अलग महत्त्व है। छात्रों के व्यक्तित्व को दबाया नहीं जाना चाहिए परन्तु यह ध्यान रखना होगा कि वे निपट विद्रोही और उच्छृंखल न बन जायें। उनके भीतर वर्तमान प्रतिभा समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो। छात्र अपनी क्षमताओं का विकास अपने लिए नहीं प्रत्युत् अपने चारों ओर वर्तमान समाज के लिए करें।
(ii) ज्ञान और अध्यापक-कुछ ज्ञान-मीमांसकों का मत है कि ज्ञान मनुष्य के मन में वर्तमान है, यह केवल सुषुप्तावस्था में पड़ा रहता है। ईश्वरीय प्रेरणा से वह स्फुरित होता है। इस दृष्टि से ईश्वर ही ज्ञानदाता है। यदि ऐसा न होता, तो हर व्यक्ति अपने प्रयासमात्र से ज्ञानी बन जाता। बहुत से ऐसे साधु-सन्त, विचारक और ज्ञानी हो गये हैं जिनके मन में ज्ञान उत्पन्न हुआ और इसके लिए वे ईश्वर की कृपा को साधन मानते हैं। यदि ऐसा विचार सत्य है, तो शिक्षा और शिक्षक का कोई महत्त्व नहीं रह जाता। परन्तु व्यावहारिक दुनिया में तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी अदृष्ट शक्ति के भरोसे बैठे रहना एक मूर्खता ही होगी। साधारणजन तो अज्ञान के अन्धकार में डूबे रहेंगे क्योंकि भगवान की कृपा तो कुछ ही लोगों पर होगी।
कुछ ज्ञान-मीमांसक यह मानते हैं कि ज्ञान मनुष्य के मन में पहले से वर्तमान है परन्तु उसे सक्रिय बनाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु मनुष्य ही है परन्तु उसे लोग ब्रह्म या ईश्वर की प्रतिकृति मानते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की कृपा चाहिए। वे कहते हैं कि बिना ‘गुरु’ के ज्ञान सम्भव नहीं। इस मत के अनुसार शिक्षा और शिक्षक का बड़ा महत्त्व है परन्तु आधुनिक शिक्षक ‘गुरु’ नहीं है। गुरु को विशेष प्रकार से परिभाषित किया गया है। सरल अर्थों में गुरु को तत्त्वज्ञानी होना चाहिए जिसने अपने तप (कष्ट सहन) से सत्य का दर्शन किया हो और जो दयावान हो, परोपकारी हो । ऐसा गुरु दुर्लभ होता है। प्राचीन धार्मिक शिक्षा में ऐसे ही गुरु का महत्त्व था। शिक्षा केवल कुछ लोगों • को दी जाती थी या कुछ लोग जो साधनसम्पन्न होते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। इनके लिए ‘गुरु’ तलाश करके सुलभ कराये जाते थे। आज स्थिति बदल चुकी है। प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में बिना किसी भेदभाव के सभी को शिक्षा देने और वह भी अनिवार्य और मुफ्त देने का प्रावधान है। ऐसी दशा में इतनी संख्या में ‘गुरु’ कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। अब गुरु का स्थान ‘शिक्षक’ या ‘अध्यापक’ ने लिया है और ‘शिक्षा’ ‘ब्रह्म ज्ञान’ से भिन्न है जिसे पाने के लिए नचिकेता और सत्यकाम भटकते रहे थे।
ज्ञान मीमांसकों का एक वर्ग यह भी कहता है कि छात्र स्वयं ज्ञान प्राप्त करता है। जो ज्ञान वह अपने निजी प्रयास से अर्जित करता है, वही सच्चा ज्ञान है। इस विचार ने शिक्षा पर व्यापक प्रभाव डाला है। बाल केन्द्रित शिक्षा के आन्दोलन का जन्म इसी विचार से हुआ। अध्यापक एक ऐसे सूत्रधार के समान है जो नाटक के मंच की व्यवस्था करता है और अभिनेताओं को निर्देशन देता है, परन्तु स्वयं पर्दे के पीछे रहता है। इसका उद्देश्य छात्रों को स्वयं सीखने में सहायता देना है। इस स्थिति में अध्यापक केवल सीखने की प्रक्रिया में निर्देश देता है। यहाँ भी स्पष्ट है कि छात्रों को ज्ञान देने में अध्यापक का महत्त्व किसी न किसी रूप में बना हुआ है। मनोविज्ञान की खोजों से और विज्ञान के आविष्कारों से अध्यापकों के महत्त्व में अत्यधिक बदलाव आने की आशंका उत्पन्न हो गयी है। इसका एक उदाहरण अभिक्रमित शिक्षण और शिक्षण-यन्त्र है जिनके द्वारा छात्र अध्यापक से नहीं, पहले से बनाये गये कार्यक्रम और यन्त्रों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसी जमाने में शिक्षा की कल्पना अध्यापक के अभाव में की ही नहीं जा सकती थी। आज तो अध्यापक निरर्थक बना जा रहा है। एजूकेशनल टेक्नालॉजी का यह परिणाम है। दूरस्थ शिक्षा और आकाशीय विश्वविद्यालय इस दिशा में शिक्षा को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इनके परिणाम जिनके कारण ‘अध्यापक’ का पद ही समाप्त हो जाये, अभी देखना बाकी है। अध्यापक के ‘व्यक्तित्व’ को क्या मशीनें प्राप्त कर लेंगी? इसका निर्णय भविष्य करेगा। इतना तो सच है कि कागज पर बने शिक्षण कार्यक्रम और मशीनें छात्र के साथ रागात्मक सम्बन्ध और अंतःक्रिया नहीं पैदा कर सकते। ‘कम्प्यूटर’ एक मानवीय भावों से सम्पन्न अध्यापक का स्थान नहीं ले सकता।
मूल्य मीमांसा और शिक्षा
अन्तर्वर्ती मूल्य या परवर्ती मूल्य-मूल्यों के दो प्रकार हैं-अन्तर्वर्ती (इन्ट्रिन्जिक) और परवर्ती (एक्सट्रिन्जिक)। कुछ लोगों ने प्रथम को स्वतः मान मूल्य और दूसरे को उपकरणीय मूल्य कहा है। प्रथम प्रकार के मूल्य वे हैं जिनका अपने आप में महत्त्व है (जिन्हें हम किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन नहीं बनाते वरन् जिन्हें प्राप्त करना ही मानव-जीवन का उद्देश्य है। इस प्रकार के मूल्यों की श्रेणी में सत्य, शिव, सुन्दर, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे मूल्य रखे जा सकते हैं। दूसरे प्रकार के मूल्य, परवर्ती या उपकरणीय मूल्य वे हैं, जिनको हम किसी महान् उद्देश्य की प्राप्ति के साधन या निमित्त रूप में अपनाते हैं, जैसे-श्रम, ईमानदारी, निष्ठा आदि)।
शिक्षा का मुख्य सरोकार अन्तर्वर्ती मूल्यों से है क्योंकि उनकी प्राप्ति मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। यदि शिक्षा का उद्देश्य जीवन की तैयारी है, तो वह अन्तर्वर्ती या स्वतः मान मूल्य शिक्षा के उद्देश्य बन जाते हैं या शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने में सहायक हैं। शिक्षा के उद्देश्य जैसे- ‘ज्ञानार्जन’, ‘सर्वांगीण जीवन’ (स्पेंसर), ‘सत्य की खोज’ (प्लेटो) आदि स्वतः मान मूल्यों की आधार- शिला पर खड़े किये गये हैं। यह मूल्य सूक्ष्म से अधिक सम्बन्ध रखते हैं। अस्तु, शिक्षक का ध्यान भौतिक वस्तुओं की ओर कम रहेगा। वह चाहेगा कि उसके छात्र सूक्ष्म विचारों की समस्या और मूल तत्त्व को ग्रहण करें। उनके अध्ययन की सामग्री बौद्धिक विषय ही होंगे। जैसे-गणित, भाषा, साहित्य, धर्म और दर्शन। सम्भवतः प्राचीन काल से लेकर अब तक इन विषयों का प्राधान्य इसलिए रहा है कि इनके द्वारा सूक्ष्म तत्त्व को ग्रहण करने में सहायता मिलती है। स्वतः मान मूल्यों की शिक्षण विधियों में चिन्तन और तर्क को ज्यादा महत्त्व मिला है।
अब प्रश्न यह है कि क्या कोई ऐसे उपाय भी अपनाये जा सकते हैं जिनसे छात्रों को इन स्वतः मान अन्तर्वर्ती मूल्यों को व्यवहार में लाकर अनुभव कराया जा सके। केवलं व्याख्या या सिद्धान्त की शिक्षा कारगर नहीं हो सकती। मूल्यों को पहले अध्यापक के और बाद में छात्र के व्यवहार में उतर कर अनुभवजन्य बनना चाहिए। उदाहरण के लिए ‘सत्य’ क्या है? इसे समझाने के बजाय उन्हें सत्य की शोध और खोज करने का व्यवहार सिखाया जाये, ‘सुन्दरं’ का अनुभव छात्रों को उत्तम मनोभावों, जैसे-स्नेह, सहानुभूति और करुणा के माध्यम से कराया जा सकता है, ‘शिवं’ का अनुभव एक ऐसी जीवन-शैली के द्वारा कराया जा सकता है, जिसमें परस्पर सहयोग, परहित चिंतन और सेवा प्रधान हो। ऐसे सूक्ष्म मूल्यों की जड़ें मन में जमाने के लिए यह आवश्यक होगा कि विद्यालय का सम्पूर्ण वातावरण सुनियोजित ढंग से तैयार किया जाये।
प्रश्न 4 (i) शंकराचार्य का दार्शनिक चिन्तन में योगदान का वर्णन कीजिए।
अथवा
शंकराचार्य के वेदान्त दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। इस दर्शन में निहित शिक्षा पर प्रकाश डालिए।
उत्तर – शंकराचार्य का दार्शनिक चिन्तन
शंकराचार्य ने वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया था। उन्होंने मुख्य उपनिषदों-ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर और नृसिंहतापनीय के भाष्यों में ब्रह्म को मूल तत्व के रूप में प्रतिष्ठित किया
है और वादरायण व्यास कृत ब्रह्मसूत्र के भाष्य में अद्वैत वेदान्त का प्रतिपादन किया है। यहाँ उनके दार्शनिक चिन्तन की तत्व मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा प्रस्तुत है।
शंकराचार्य के अद्वैत वेदान्त दर्शन की तत्त्व मीमांसा
शंकर ने इस ब्रह्माण्ड के मूल में केवल ब्रह्म की सत्ता स्वीकार की है जिनका ब्रह्म अनादि, अनन्त
ने और निराकार है। यही ब्रह्म इस ब्रह्माण्ड का कर्त्ता और उपादान कारक है। यही शंकर का अद्वैत है। शंकर के अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्म अपनी इच्छा से अपने अन्दर माया शाक्त का निर्माण करता है और फिर इस माया शक्ति के द्वारा इस नाना वस्तु जगत का निर्माण करता है। जगत् के कर्त्ता के रूप में यह ब्रह्म साकार ब्रह्म अथवा ईश्वर के नाम से विभूषित होता है। आत्मा को शंकर ब्रह्म का अंश मानते हैं और चूँकि ब्रह्म अपने में पूर्ण, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञाता है इसलिए शंकर की सम्मति में आत्मा भी अपने में पूर्ण, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञाता है। जीव के विषय में शंकर का मत है कि शरीर तथा इन्द्रिय समूह के अध्यक्ष और कर्मफल का भोक्ता आत्मा ही जीव है। यही जीव सूक्ष्म शरीर के साथ एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है। जगत् को शंकर नाशवान् एवं असत्य मानते हैं। उनकी दृष्टि से इस जगत् एवं उसमें मानव जीवन की केवल व्यावहारिक सत्ता ही है। पदार्थ की अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, पदार्थ तो विचार शक्ति के तेजी से चक्कर काटने से उत्पन्न भंवर जाल हैं। जिस प्रकार पानी में भंवर का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता उसी प्रकार पदार्थों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। शंकर का यह मत भारतीय प्रत्ययवाद और प्लेटो के विचारवाद से बड़ा मेल खाता है।
शंकराचार्य के अद्वैत वेदान्त दर्शन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा
शंकर ने ज्ञान को दो भागों में बाँटा है-अपरा (लौकिक अथवा व्यावहारिक) तथा पेरा (आध्यात्मिक)। इस वस्तु जगत एवं मनु जीवन के विभिन्न पक्षों के ज्ञान को उन्होंने अपरा ज्ञान कहा है। उनकी दृष्टि से इस ज्ञान की केवल व्यावहारिक उपयोगिता है, इससे मनुष्य अपने जीवन के अन्तिम उद्देश्य ‘मुक्ति’ की प्राप्ति नहीं कर सकता। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् एवं गीता की तत्त्व मीमांसा को वे परा ज्ञान मानते थे। उनकी दृष्टि से यही सच्चा ज्ञान है, इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इन दोनों प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शंकर ने श्रवण, मनन और निदिध्यासन की विधि का समर्थन किया है परन्तु परा ज्ञान के लिए वे श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन के साथ साधन चतुष्टय को आवश्यक मानते थे। उनकी दृष्टि से बिना साधन चतुष्टय (नित्य-अनित्य वस्तु विवेक, भोग विरक्त, शमदमादि संयम और ममुक्षकत्व) के परा ज्ञान नहीं हो सकता।
शंकराचार्य के अद्वैत वेदान्त दर्शन की मूल्य एवं आचार मीमांसा
शंकर ने मनुष्य जीवन को दो रूपों में विभाजित किया है-एक अपरा (व्यावहारिक) और दूसरा परा (आध्यात्मिक)। व्यावहारिक दृष्टि से उन्होंने मनुष्यों को अपने वर्ण-कर्म को निष्ठा एवं ईमानदारी से करने की सलाह दी है। इनका विश्वास है कि जो मनुष्य अपने वर्ण-कर्म को जितनी निष्ठा एवं ईमानदारी से करेगा वह व्यावहारिक दृष्टि से उतना ही सफल होगा।
शंकर के अनुसार मनुष्य जीवन का अन्तिम उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना है। मुक्ति के शंकर ने दो रूप स्वीकार किये हैं-एक जीवन मुक्ति और दूसरी विदेह मुक्ति। उनके मत से किसी भी प्रकार की मुक्ति के लिए ज्ञान मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए शंकर ने श्रवण, मनन और निदिध्यासन पर बल दिया है और इस सबके लिए साधन चतुष्टय को आवश्यक माना है। मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक को इन सबका पालन करना चाहिए।
भारत में शिक्षा पर स्वतन्त्र रूप से विचार करना आधुनिक युग की देन है। इससे पूर्व के विचारक मनुष्य के जीवन पर समग्र रूप से विचार करते थे। शंकर ने भी शिक्षा पर स्वतन्त्र रूप से विचार नहीं किया है। परन्तु उनकी तत्व मीमांसा से शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा से ज्ञान के स्वरूप एवं ज्ञान प्राप्त करने की विधियों और मूल्य एवं आचार मीमांसा से शिक्षा द्वारा मनुष्य के व्यवहार में किए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी होती है
शंकर के अनुसार मनुष्य जीवन का अन्तिम उद्देश्य मुक्ति है और इस मुक्ति के लिए उन्होंने ज्ञान मार्ग का समर्थन किया है। उनकी दृष्टि से जब मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है कि ब्रह्म सत्य है और शेष सब असत्य है तभी वह सांसारिक माया मोह से मुक्त होता है, भेद दृष्टि से मुक्त होता है और सब में स्वयं को और स्वयं में सबको देखता है, और इस ज्ञान की प्राप्ति होती है शिक्षा से । शिक्षा के विषय में उन्होंने उपनिषदीय विचार का समर्थन किया है। उनकी दृष्टि से शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए (सा विद्या या विमुक्त्ये) ।
प्रश्न 4 (ii) महात्मा गाँधी की शैक्षिक विचारधाराओं की विवेचना कीजिए।
अथवा
शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य तथा शिक्षण विधि सम्बन्धी विचारों पर प्रकाश डालते हुए गाँधीजी के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन कीजिए।
अथवा
गाँधीजी के शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए।
अथवा
महात्मा गाँधी के शैक्षिक विचारों की विवेचना करें एवं इसकी समसामयिक प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए।
अथवा
महात्मा गाँधी के शिक्षा में योगदान पर प्रकाश डालें।
उत्तर —
गाँधीजी के शैक्षिक विचार –
गाँधीजी अपने समय में दी जाने वाली शिक्षा-प्रणाली से असन्तुष्ट थे और उनके विचार में ब्रिटिश काल की शिक्षा सैद्धान्तिक, अव्यावहारिक, परीक्षा पास करके नौकरी करने की क्षमता देने वाली, शिक्षित बेकारी बढ़ाने वाली थी। ऐसी शिक्षा मानवीय, सामाजिक, राजनैतिक एवं नागरिक गुणों का विकास नहीं करती थी। देश की ‘गरीबी हटाओ’ में इसका कोई योगदान न था। विदेशी भाषा, विदेशी संस्कृति और सभ्यता की दासता में भारतवासी जकड़े हुए थे। इन सबको दूर करने के लिए गाँधीजी ने नये ढंग से शिक्षा के बारे में सोचा।
(i) शिक्षा का अभिप्राय-
शिक्षा का अर्थ गाँधीजी ने केवल लिखने-पढ़ने या सरलता से नहीं लिया है। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि शिक्षा का आरम्भ और अन्त साक्षरता से नहीं है। यह तो पुरुष और स्त्रियों को शिक्षित करने का एक साधन है। गाँधीजी कहते हैं कि “शिक्षा से मेरा अभिप्राय है- बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के गुणों का सर्वोत्तम ढंग से चतुर्दिक बाह्य प्रकाशन।” गाँधीजी ने बताया है कि “सच्ची शिक्षा वह है जो बालकों की आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं को उनके भीतर से बाहर निकाले और उत्तेजित करे।” शिक्षा से मनुष्य का शरीर, मन और आत्मा का मेल उचित और समरूप ढंग से होता है जिससे मनुष्य पूर्ण बनता है।
(ii) प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी विचार-
प्रौढ़ शिक्षा का साधारण अर्थ उन वयस्क लोगों की शिक्षा से होता है जिन्हें बचपन में कोई भी शिक्षा न मिली अथवा कुछ ही शिक्षा मिली और अब वे अशिक्षित माने जाते हैं। परन्तु गाँधीजी ने इसके बारे में कुछ भिन्न विचार बताया है-“मैं प्रौढ़ शिक्षा को उस साधारण अर्थ में जैसा हम लोग समझते हैं, नहीं लूँगा बल्कि वह तो अभिभावकों की शिक्षा होगी जिससे वे अभिभावक अपने बच्चों के निर्माण में पर्याप्त उत्तरदायित्व निभा सकें।” इसका मतलब है कि प्रौढ़ शिक्षा राष्ट्र के अच्छे नागरिकों की शिक्षा है। स्वतन्त्र भारत में तभी तो इसके अन्तर्गत ज्ञान, स्वास्थ्य, अर्थ, संस्कृति और सामाजिकता के विकास का प्रोग्राम रखा गया। गाँधीजी ने प्रौढ़ शिक्षा को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जागृति का साधन माना। चरित्र, धर्म, राज्य, व्यापार, सेवा सभी के विकास के लिए प्रौढ़ शिक्षा एक प्रमुख साधन है। गाँधीजी ने इसके पाठ्यक्रम को व्यापक बनाया और इसमें उद्योग, कौशल, व्यापक, नैतिकता, पारिवारिक शिक्षा, राष्ट्रीय एकीकरण सब कुछ रखा गया है।
(iii) स्त्री शिक्षा सम्बन्धी विचार-
प्रौढ़ शिक्षा के समान ही गाँधीजी अपने देश की स्त्री शिक्षा पर भी दुखी थे। गाँधीजी ने स्त्री को पुरुष के समान बताया तथा शिक्षा की सभी सुविधाओं को देने के लिए जोर दिया। यह अवश्य है कि गाँधीजी सीता, दमयन्ती, द्रौपदी, गार्गी, मैत्रेयी, अपाला आदि प्राचीन आदर्शों के समान आज की स्त्रियों को भी बनाना चाहते थे। इसलिए आधुनिक भाषा, साहित्य, कला, संगीत, श्रृंगार, वासना, उत्तेजक जीवन से दूर रखना चाहते थे। उन्हें वे घर-गृहस्थी की शिक्षा, समाज सेवा, स्वास्थ्य, सफाई, निरीक्षण, राष्ट्र सेवा, वीरता, साहस के कार्यों की शिक्षा देने के पक्ष में थे। शिक्षा का कार्य भी स्त्रियाँ करें जिससे वे समाज की अग्रदूतियाँ बनें। समाज सुधार करने में उन्हें ऐसी देवियाँ बना दी जायँ कि वे संसार को हिला देवें। स्पष्ट है कि नवीन, समाज एवं वातावरण के अनुकूल मर्यादित ढंग से स्त्री शिक्षा की व्यवस्था हो ।
(iv) शिक्षा के उद्देश्य-
गाँधीजी ने शिक्षा के उद्देश्य को दो प्रकार का माना है- (क) तात्कालिक उद्देश्य और (ख) अन्तिम उद्देश्य ।
(क) तात्कालिक उद्देश्य-
(1 ) चारित्रिक विकास का उद्देश्य-गाँधीजी ने इसे प्रमुख उद्देश्य बताया है और कहा है कि बिना चरित्र के शिक्षा बेकार है। उनके शब्दों में, “सभी ज्ञान का लक्ष्य चरित्र निर्माण होना चाहिए।” अन्यत्र भी उन्होंने कहा है कि “विद्यार्थियों को अपने भीतर खोजना चाहिए और अपने निजी चरित्र की रक्षा करना चाहिए क्योंकि बिना चरित्र के शिक्षा किस काम की और बिना प्रारम्भिक व्यक्तिगत पवित्रता के चरित्र किस काम का होता है।” चरित्र निर्माण के लिए छात्रों को अपने साहस, बल, सद्गुण, परार्थता, सहयोग, प्रेम, सेवा, श्रद्धा को विकसित करना चाहिए।
(2) धनोपार्जन का उद्देश्य-शिक्षा और जीविकोपार्जन एक साथ चले परन्तु धनोपार्जन केवल जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हो, पूँजीवादी भावना से न हो। इसीलिए इन्होंने जोर दिया था कि शिक्षा बेरोजगारी से एक प्रकार की सुरक्षा होना चाहिए। शिक्षा के द्वारा आत्मनिर्भरता का गुण छात्रों एवं व्यक्तियों में विकसित किया जाय तभी सर्वोदय होना सम्भव है।
( 3 ) संस्कृति के विकास का उद्देश्य-गाँधीजी के विचार से संस्कृति जीवन का आधार है। इन्होंने कहा है कि मैं शिक्षा के सांस्कृतिक पक्ष को उसके साहित्यिक पक्ष से अधिक महत्त्वपूर्ण समझता हूँ। संस्कृति शिक्षा का आधार और विशेष अंग है जिसे बालिकाओं व बालक को प्राप्त करना चाहिए। संस्कृति बाह्य एवं आन्तरिक दोनों प्रकार की हो। बाह्य रूप में रहन-सहन के तौर-तरीके हैं और आन्तरिक रूप में उच्च एवं सद्भावनाएँ, निष्ठाएँ आदि हैं |
(4) स्वभाव की पूर्णता का उद्देश्य-मानव स्वभाव दो ढंग से दिखायी देता है-व्यक्तित्व ढंग से, सामाजिक ढंग से। अतएव गाँधीजी के विचार से शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के व्यक्तित्व एवं सामाजिक स्वभाव की पूर्णता लाना होना चाहिए। ऐसी स्थिति में उन्होंने मनुष्य के हाथ, हृदय और मस्तिष्क का विकास एवं प्रयोग का रखा। सामाजिक स्वभाव में नागरिक के उत्तरदायित्व को रखा। मानव स्वभाव को पूर्ण बनाना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए।
(5) स्वतन्त्र विकास एवं मुक्ति का उद्देश्य- यह उद्देश्य भौतिक एवं आध्यात्मिक अर्थों में लिया जाता है। भौतिक अर्थ में आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक समस्याओं से मुक्त करना शिक्षा का उद्देश्य होता है और आध्यात्मिक अर्थ में ज्ञानार्जन, धर्म, सत्यनिष्ठा, आत्मा की पवित्रता प्रदान करना शिक्षा का उद्देश्य होता है।
(ख) अन्तिम उद्देश्य –
अन्तिम उद्देश्य का सम्बन्ध जीवन के अन्तिम एवं उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति में होता है। नीचे लिखे अन्तिम उद्देश्य हैं-
(1) सत्य और ईश्वर की प्राप्ति का उद्देश्य-गाँधीजी लिखते हैं कि इस जगत में चाहे ईश्वर कहिए या सत्य कहिए, उसके सिवाय दूसरा कुछ निश्चित नहीं है। गाँधीजी के लिए इस प्रकार ईश्वर सत्य है और सत्य ईश्वर है। अतएव जीवन का यह सर्वोच्च उद्देश्य है और शिक्षा जीवन का एक अभिन्न अंग है। अतएव शिक्षा का भी उद्देश्य सर्वोच्च ईश्वर और सत्य की प्राप्ति होना चाहिए।
(2) सर्वोदय का उद्देश्य-गाँधीजी पर भारतीय दर्शन-वेदान्त दर्शन का भी प्रभाव पड़ा था जिसके अनुसार व्यक्ति की भलाई में सभी की भलाई निहित होती है। यही तो सर्वोदय भावना है जिससे सभी सुखी, निरोग और निर्भर होकर आगे बढ़ते हैं। डॉ0 एस0 एम0 पटेल ने लिखा है कि “गाँधीजी के दर्शन का सार यह है कि वैयक्तिकता का विकास सामाजिक वातावरण में ही हो सकता है।” शिक्षा का उद्देश्य यदि सर्वोदय हो तभी समाज के वातावरण में वैयक्तिकता का विकास होता है
( 3 ) दासता से मुक्ति का उद्देश्य- हमारे ब्रिटिश शासकों ने हमें जिस तरह प्रशिक्षित किया, उसका परिणाम दासता या दास बुद्धि रहा। गाँधीजी ने शिक्षा के द्वारा इस दासता से मुक्ति प्रदान करने को सोचा। उन्होंने सबसे पहले नौकर अभिवृत्ति को दूर करने के लिये जोर दिया। आज अपने देश में इंजीनियरों को स्वयं उद्योग साहस का प्रशिक्षण देकर दास बद्धि से मुक्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। यह शिक्षा का एक अन्तिम लक्ष्य गाँधीजी के विचारानुसार मिलता है जहाँ उन्होंने शिक्षा को सुरक्षा का अस्त्र बनाया था।
(v) शिक्षा का पाठ्यक्रम-गाँधीजी ने विदेशों में प्रचलित पाठ्यक्रम की ओर ध्यान दिया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि ब्रिटिशकालीन भारतीय शिक्षा का पाठ्यक्रम सैद्धान्तिक, संकीर्ण, एकांगी, दूषित एवं जीवन से दूर था। अतएव उन्होंने पाठ्यक्रम का व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन की आवश्यकता, क्रियाशीलता, उपयोगिता पर आधारित करने को कहा और इस दृष्टि से हस्तकार्यों को प्रमुख एवं केन्द्रीय विषय बनाया। पाठ्यक्रम के निर्माण में मनोवैज्ञानिक आधार को भी अपनाया और बालकों की रुचियों एवं योग्यताओं के अनुसार हस्तकौशल के चुनाव पर जोर दिया। इसके लिए विविध हस्तकौशलों का समावेश पाठ्यक्रम में किए जाने का विचार उन्होंने रखा।
(vi) शिक्षा विधियाँ- पाठ्यक्रम के अनुकूल गाँधीजी ने शिक्षा विधियों को भी बताया है। पाठ्यक्रम में क्रियाशीलता को उन्होंने प्रमुखता प्रदान की। निम्न विधियों के प्रयोग के लिए उनके संकेत मिलते हैं-
(1) क्रिया विधि-
हस्तकौशल चूँकि केन्द्रीय विषय बनाया गया इसलिए क्रिया विधि भी केन्द्रीय विधि बन गयी। हस्तकौशल, शारीरिक शिक्षा आचरण की शिक्षा के लिए व्यावहारिक ढंग से काम करना आवश्यक है। अस्तु क्रियाविधि सबसे महत्त्वपूर्ण विधि हुई। इस सम्बन्ध में गाँधीजी ने लिखा है, “मेरा विश्वास है कि मस्तिष्क की शिक्षा शारीरिक अंगों-हाथ, पैर, आँख, नाक, कान आदि के उचित अभ्यास और प्रशिक्षण से प्राप्त की जा सकती है।”
(2) प्रयोग, प्रदर्शन, निरीक्षण विधि-
क्रिया विधि के समान ही यह विधि भी होती है। प्रयोग विज्ञान शिक्षा के लिए एक मात्र विधि है। प्रदर्शन एवं निरीक्षण गुण प्रयोग के ही अंग हैं। अतएव इन तीनों को मिलाकर शिक्षा दी जाय। ऐसा गाँधीजी का कहना था ।
(3) अनुकरण विधि-
बच्चों को पहले कार्य करके दिखाया जाता है फिर वे अनुकरण करते हैं। अध्यापक-प्रदर्शन का अनुकरण बच्चे करते हैं, इस विधि के लिये भी गाँधीजी का संकेत मिलता है।
(4) सहकारी विधि-
व्यावहारिक कामों को अध्यापक एवं विद्यार्थी या विद्यार्थी एवं विद्यार्थी मिल-जुल कर करते हैं, इसीलिये गाँधीजी का कहना था कि शिक्षा सहकारी ढंग से दी जाय। इससे बहुत से गुणों का विकास भी होता है
(5) सह-सम्बन्ध की विधि-
हस्तकौशल को केन्द्र मानकर शिक्षा देने के पक्ष में गाँधीजी हैं। इसके लिये सह-सम्बन्ध की विधि को प्रयोग करने के लिये वह कहते हैं। हस्तकौशल का ज्ञान देते समय गणित, भाषा, इतिहास सभी कुछ सिखाया जाय।
( 6 ) मौखिक विधि-
हस्तकौशल करते समय बहुत से प्रासंगिक बातों को मौखिक ही बताया जा सकता है। जैसे सूत कातने के समय सूत की बात, रुई की कहानी, उत्पादन आदि जिनका सम्बन्ध विभिन्न विषयों से होता है। व्याख्यान, तर्क, विवेचन, प्रश्नोत्तर आदि प्रविधियों से यह कार्य पूरा किया जा सकता है।
(7) संगीत विधि- प्रार्थना के समय, ड्रिल के समय, कीर्तन भजन के समय इस विधि का प्रयोग होता है। अतएव यह भी एक महत्त्वपूर्ण विधि है।
(8) चिन्तन-मनन की विधि-गाँधीजी ने कहा है कि “चिन्तन-मनन की विधि से ही बालक केवल एक स्वस्थ शरीर का ही विकास नहीं करेगा बल्कि एक स्वस्थ और शक्तिशाली मस्तिष्क का भी।”
(vii) शिक्षक, शिक्षार्थी तथा शिक्षालय सम्बन्धी विचार-गाँधीजी ने इनके बारे में आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाया है। शिक्षक के बारे में उन्होंने कहा है कि वे अपने आचरण को शुद्ध रखें और जिस बात की शिक्षा दें उसको अपने जीवन में स्वयं अपनावें। इसका कारण बताते हुए उन्होंने लिखा है कि “मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है कि छात्र भाषणों और पुस्तकों की अपेक्षा शिक्षक के चरित्र, आचरण एवं व्यक्तित्व से अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं।” अतएव शिक्षक का प्रथम गुण अपना चरित्र उत्तम रखना है। उसे अपने विषय का ज्ञान पूरा-पूरा होना चाहिए। उसे विशेष रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। उसका उत्तरदायित्व महान होता है और वह अपनी योग्यता, गुण, चरित्र, व्यक्तित्व से छात्रों में प्रतिभा एवं क्षमता उत्पन्न करे, उन्हें योग्य बनावे। उसे ईमानदारी से, अहिंसा एवं सत्यता से अपना कर्त्तव्य पूरा करना चाहिए। सजगता एवं सजीवता अध्यापक में अवश्य हो अन्यथा उसके छात्र भी निर्जीव मशीन बनेंगे। शिक्षक चिन्तनशील, उचितवान एवं क्रियावान होना चाहिए। त्याग एवं तपस्या का सीधा-सादा जीवन अध्यापक बितावे। केवल कक्षा में ही नहीं बल्कि कक्षा के बाहर भी वह छात्रों का ध्यान रखे, जैसे माता-पिता-अभिभावक रखते हैं। ऐसी स्थिति के बारे में गाँधीजी के विचार हैं, “शिक्षक का कार्य क्षेत्र केवल कक्षा में नहीं बल्कि उसके बाहर भी होता है। मुझे दुःख है कि शिक्षक आजकल वेतनभोगी कर्मचारी के समान केवल कक्षा में पढ़ाने तक ही में अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझते हैं। कक्षा के बाहर वे छात्र के प्रति अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं समझते हैं। इससे छात्रों की बड़ी हानि होती है। उनके चरित्र तथा व्यक्तित्व के विकास में पूरी सहायता नहीं मिलती है।” इन शब्दों में गाँधीजी के अनुसार शिक्षक को बालक के चरित्र और व्यक्तित्व, ज्ञान एवं प्रतिभा, बुद्धि और कौशल के विकास के लिये पूर्णरूपेण जिम्मेदार माना गया है।
शिक्षालय के लिये गाँधीजी ने प्राचीन आश्रम के आदर्श रखे हैं। उनके विचार से शिक्षालय प्रकृति के सुन्दर, सुरम्य और शान्त स्थल पर हों जहाँ का वातावरण आत्मा, मन और हृदय के विकास के लिये स्वयमेव अभिप्रेरणा प्रदान करे। शिक्षालय शिक्षार्थी के चरित्र निर्माण, विकास एवं कार्य पूरा करने का महान साधन होना चाहिए। शिक्षालय में शिक्षा एवं शिक्षण का संगठन ऐसा रहे कि वह शिक्षार्थी को स्वावलम्बी बनावे। शिक्षालय समुदाय के केन्द्र बनें और समुदाय की सम्पत्ति समझे जावें जिन्हें सभी लोग सुरक्षित रखें। शिक्षालय समुदाय की संस्कृति प्रदान करें और समुदाय के जीवन के लिये शिक्षार्थी को तैयार करावें जिसके आधार पर शिक्षार्थी समुदाय का पुनर्निर्माण करने में समर्थ होवें। शिक्षालय को गाँधीजी ने व्यक्तिकता के स्वतन्त्र विकास, आत्मानुभूति और अनुशासन का साधन माना है।
(viii) अनुशासन सम्बन्धी विचार-गाँधीजी स्वतन्त्र, अनुशासन के विश्नासी थे। इस सम्बन्ध में वे दण्ड के विरोधी थे और दमनवादी सिद्धान्त को नहीं मानते थे। स्वतन्त्र अनुशासन के लिये अच्छा वातावरण होना चाहिए, साथ में स्वेच्छा से कार्य करना चाहिए। अनुशासन की भावना अपने भीतर होनी चाहिए। यह दो तरीके से होता है-एक तो आत्म-नियंत्रण, आत्म-संयम या ब्रह्मचर्य से और दूसरे मिल- जुलकर रहने और काम करने से। गाँधीजी का अनुशासन सम्बन्धी विचार प्राचीन आधार पर होते हुए नये ढंग का था जिस पर भारतीय एवं ईसाई दर्शन एवं धर्म की छाप भी मिलती है।
प्रश्न 4 (iii) रसेल के शिक्षा-सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए।
अथवा
बरट्रेन्ड रसेल के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन कीजिए।
रसेल के शिक्षा-सिद्धान्त
रसेल द्वारा शिक्षा के क्रान्तिकारी सिद्धान्त प्रस्तुत किए गए। उन्होंने पाठशालाओं की दीवारों के बीच नन्हें-नन्हें बच्चों की आत्मा को पुकारते हुए पाया। उनकी छटपटाती जीवन्तता कुंठित होती हुई स्वतंत्रता को देखकर उसका संवेदनशील हृदय रो पड़ा। रसेल ने यह भी स्पष्ट रूप से अनुभव किया कि कुछ साधन-सम्पन्न एवं धनी परिवारों के बच्चे ही शिक्षा पाते हैं, अनेकों एवं ज्यादातर दीन- साधनहीन परिवारों के बच्चे शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर पाते। उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से देखा कि शिक्षा अनुपयोगी एवं रूढ़िवादी है। शिक्षण के क्षेत्र में उन्होंने यह दृश्य देखा कि गलत अनुशासन से शिक्षा ) जकड़ी हुई है। विद्यालयों में बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किए जा रहे हैं। उन पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। विद्यालयों में प्रेम तथा ममता की हमेशा कमी रही है। बच्चों के अंदर विद्यमान सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को कोई महत्त्व नहीं दिया जा रहा है।
रसेल इस डरावनी परिस्थिति को देखकर बहुत ही बेचैन हो उठा। वह तो घोर मानवतावादी था और इसलिए संसार के सभी मनुष्य की मंगल कामना करता था। अतएव रसेल ने अपना शिक्षा सिद्धान्त निम्नवत् तरीके से निश्चित किया-
–
(1) स्व एवं सहयोगी अनुशासन-शिक्षा का स्वरूप ऐसा हो कि उसमें बच्चे सहयोगी वातावरण में अपना विकास कर सकें। इस तरह के वातावरण में हों तो स्व एवं सहयोगी अनुशासन का विकास संभव हो सकता है। यह अनुशासन खेल के मैदान का होना चाहिए। इसमें दबाव एवं डर प्र की कमी हमेशा रहेगी। इसमें बच्चों को स्वतंत्र विकास का भी मौका मिलेगा।
(2) शिक्षा सार्वभौम तथा सबके लिए समान सुविधा की हो-महान् मानवतावादी एवं संवेदनशील रसेल ने देखा कि संसार की कुछ साधन-सम्पन्न तथा अमीर परिवारों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा तो है, लेकिन ज्यादातर परिवार के बच्चे साधन तथा धन की कमी के कारण शिक्षा से वंचित हैं। इस तरह की शिक्षा-व्यवस्था से किसी का भला नहीं होने वाला है। इससे संसार अ में शान्ति और व्यवस्था नहीं आ सकती। सभी मानवता के विकास की शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा का उ द्वार बिना किसी तरह के भेदभाव के सभी के लिए खुला रहना चाहिए। यहाँ यह बात याद रखने के योग्य है कि सभी के लिए शिक्षा से यह तात्पर्य नहीं कि बच्चों की वैयक्तिक रुचि, प्रवृत्ति एवं प्रतिभा को विकसित करने का मौका न दिया जाए। दस दिशा में शिक्षा को भरसक प्रयत्नशील जागरूक रहना है।
(3) शिक्षा उपयोगी हो-शिक्षा का उपयोगी तथा व्यावहारिक होना ही उसका सामान्य महत्त्व है। जो शिक्षा उपयोगी नहीं, वह सामान्य जीवन में महत्त्वपूर्ण नहीं होती। आज भारत में यह एक सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि वर्तमान शिक्षा उपयोगी नहीं है और इसका फल होता है कि इस शिक्षा को पाकर निकलनेवाले सामान्य युवक-युवतियाँ बेकारी के अंधकार में भटकते रहते हैं। इसलिए रसेल का यह विचार ठीक ही है कि सामान्य शिक्षा का जीवनोपयोगी होना बहुत जरूरी है।
(4) विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा के लिए विशिष्ट व्यवस्था-शिक्षा की सुविधा जहाँ सबके लिए हो, वहाँ मेधावी एवं प्रतिभासम्पन्न बच्चों के लिए विज्ञान एवं तकनीक को विशेष शिक्षा की सुविधा हो। इससे वैज्ञानिकों व तकनीकी ज्ञान की उन्नति हो सकेगी
(5) बच्चों के अन्दर उपस्थित सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को जगाया जाए – यह मनोविज्ञान द्वारा सिद्ध हो चुका है कि बच्चों में सीखने की, काम करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है। अतः सच्ची शिक्षा वही है, जो उनके अंदर निहित स्वाभाविक प्रवृत्ति को जंगाए और विकास की ओर अग्रसर करे। यह भी देखा जाता है कि बच्चे स्वतः ही चलने तथा बोलने को उद्यत होते हैं। यह उनके अंदर निहित क्रियात्मक शक्ति का ही परिचायक है। इसे जगाने, विकसित करने के लिए छड़ी और डरावनी वस्तु का सहारा नहीं लिया जा सकता है।
(6) शिक्षा मानवीय तत्त्वों से पूर्ण-रसेल ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षा का सिर्फ उपयोगी होना ही सब कुछ नहीं है। उसमें मानवीय तत्त्वों का समावेश होना भी जरूरी है। बिना मानवीय तत्त्व के मात्र उपयोगी शिक्षा बन्धुत्व, प्रेम, सद्भावना, परोपकार-भावना कहाँ प्राप्त कर सकेगी ?
(7) चरित्र की शिक्षा-वर्तमान समय में चरित्र की शिक्षा भी अनिवार्य है। बच्चों में साहस रचनात्मक भाव, सत्यप्रियता, सद्भावना प्रेम, क्रीड़ाप्रियता एवं सहानुभूति जैसे-गुणों का विकास किया जाए।
(8) स्वस्थ एवं साहसी बच्चों का निर्माण- रसेल के शिक्षा के सिद्धान्त का मुख्य मंत्र है- स्वस्थ एवं साहसी मानव का निर्माण। जिस शिक्षा में डरपोक व अस्वस्थ मनुष्य का निर्माण होता है, वह शिक्षा किसी भी अर्थ में शिक्षा नहीं हो सकती। उसमें जन्म से ही बच्चों के समुचित लालन व पोषण को बहुत महत्त्व प्रदान किया है। ऐसा देखने में आया है कि माता के डरपोक होने से बच्चों में भी भय का समावेश अनजाने में ही हो जाता है। इसलिए माता-पिता के निडर होने की भी जरूरत है। यह तभी हो सकता है जब उनका भी शिक्षण हो। विद्यालय का वातावरण भी होना जरूरी है।
(9) यौन-शिक्षा का समावेश-रसेल ने स्पष्ट रूप से माना है कि आज के मनुष्य में ज्यादातर मानसिक तनाव व ग्रंथियाँ उपयुक्त यौन-शिक्षा की कमी से है। इसलिए आधुनिक शिक्षा में उपयुक्त एवं उपयोगी यौन-शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।
प्रश्न 5. (i) रसेल की शिक्षा पद्धति का प्रयोजन स्पष्ट कीजिए।
उत्तर –
रसेल की शिक्षा पद्धति का प्रयोजन
रसेल ने शिक्षा पर विचार करते हुए उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। रसेल के अनुसार बिना उद्देश्य के शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं है। वास्तव में शिक्षा के उद्देश्य देश, काल एवं सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित होते हैं। जीवन्त शिक्षा वही है, जिसके उद्देश्य जीवन के अनुरूप व उसकी इच्छाओं-आवश्यकताओं को पूरा कर सकने में सक्षम हैं। शिक्षा के उद्देश्य एकल नहीं होने चाहिए। वे तो सर्वांगीण दृष्टिकोण के अनरूप निर्मित होते हैं। वास्तव में शिक्षा उद्देश्य प्रबुद्ध, सुविकसित, संवेदनशील, जीवन्त, साहसी तथा प्रगतिशील मानव का निर्माण करना है। यहाँ रसेल द्वारा निर्धारित शिक्षा के उद्देश्य को निम्नलिखित बिन्दुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है-
(1) साहस का समावेश-साहस एक नैसर्गिक गुण है। जिस मानव में साहस नहीं, वह कीड़े- मकोड़े से भी बदतर है। अनावश्यक डर की अनुपस्थिति ही तो वास्तविक साहस है। साहस के बिना प्रगति, निर्माण व अन्वेषण संभव नहीं है। साहस की कमी से मनुष्य का जीवन नीरस व दुःखमय हो जाता है। उसका जीना भी बेकार है। माताओं में साहस की कमी बच्चों पर भी बुरा प्रभाव डालता है। साहस के बल पर मानव एवरेस्ट, अंतरिक्ष व चाँद पर विजय प्राप्त कर सका है। साहस के बल पर अमेरिका की खोज हो सकी। इस तरह मानव जीवन को सार्थकता प्रदान करने तथा ज्ञान-विज्ञान की प्रगति के लिए साहस एक अमूल्य कुंजी है। अतः शिक्षा का एक महान उद्देश्य बच्चों में साहस का समावेश करना है।
(2) ओजस्विता का विकास-शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ओजस्विता का अधिक महत्त्व है। जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य सुन्दर एवं बुलन्द होता है, उसमें उत्साह, प्राणवत्ता व प्रसन्नता भरपूर मात्रा में होती है। वास्तव में सुन्दर स्वास्थ्य ही तो ओजस्विता की आधारशिला है जहाँ स्वास्थ्य है, वहीं ओजस्विता के द्वारा आनन्द एवं प्रसन्नता में बढ़ोत्तरी होती है व दुख एवं वेदना का नाश होता है। ओजस्विता के कारण मानव अपने परिवेश व जीवन में रुचि लेता है इसकी कमी में वह उदासीन तथा उत्साहहीन हो जाता है। विश्व में रुचि भी वह तभी लेता है जब उसमें ओजस्विता होती है। जिस तरह स्वस्थ एवं जीवन्त मोर मस्त और खुश रहता है तथा किसी का परवाह नहीं करता, उसी तरह स्वस्थ तथा ओजस्वी मानव भी प्रतियोगिता एवं अनावश्यक चिंताओं से आजाद होता है। अतः यह स्पष्ट है कि शिक्षा का परम उद्देश्य है बच्चों में सुन्दर तथा ओजस्विता एवं प्राणवत्ता का उन्मुक्त विकास।
(3) बुद्धि का विकास-
बुद्धि के बल ही मानव ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, दर्शन, कला, सभ्यता एवं संस्कृति के क्षेत्र में प्रगति कर सका है।
सच तो यह है कि बुद्धि को गति देनेवाली शक्ति है, जिज्ञासा नये ज्ञान-विज्ञान की जानकारी एवं नये तथ्यों की खोज-पिपासा ही जिज्ञासा है। जिज्ञासा की कमी में बुद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः बच्चों में जिज्ञासा की भावना को जागृत करना व उसका विकास करना बुद्धि का विकास करना शिक्षा का परम उद्देश्य है।
(4) संवेदनशीलता का प्रस्फुटन-संवेदनशील मनुष्य में पाया जाने वाला एक विशिष्ट गुण है। जिस व्यक्ति में यह गुण नहीं है, वह पशु के समान है। वास्तव में यह हमेशा मानवीय गुण है। पशु में यह गुण नहीं होता। इसका सम्बन्ध हृदय से ज्यादा होता है। संवेदनशीलता का सम्बन्ध हमारे संवेगों से है यह मौलिक रूप से संवेगात्मक है। शुरू में सुखपूर्वक व्यवहार तक इसका क्षेत्र सीमित होता है। लेकिन परिपक्वता तथा आयवृद्धि के साथ इसका स्वरूप सहानुभूति सा हो जाता है। वास्तव में संवेदनशीलता साहस को दृढ़ व वस्तुनिष्ठ बनाता है। अतः बच्चों में संवेदनशीलता का प्रस्फुटन शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है।
(5) उपयुक्त एवं आवश्यक यौन-शिक्षा-वर्तमान समय में यौन-शिक्षा के अभाव में युवकों को अनेक प्रकार के मानसिक रोग व तनाव हो रहे हैं। यौन-शिक्षा के द्वारा उन्हें बहुत कुछ अंशों में दूर किया जा सकता है। वास्तव में, यौन-भावना स्वाभाविक है। इसे दबाकर हम यौन एवं तज्जनित अपराधों को ही जन्म देते हैं। इसलिए आवश्यक एवं उपयुक्त यौन-शिक्षा देना भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए।
(6) वैयक्तिक भिन्नता एवं प्रतिभा का समादर-बच्चों की शिक्षा वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित होना चाहिए। उनकी रुचि, प्रवृत्ति व प्रतिभा के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था हो। शिक्षा का परम उद्देश्य है कि वैयक्तिक प्रतिभा का समादर एवं विकास किया जाए।
(7) विज्ञान कला का शिक्षण देना- आज के प्रगतिशील वैज्ञानिक युग में विज्ञान का शिक्षण जरूरी ही नहीं अनिवार्य भी है। इसके बिना आधुनिक युग की कठिन समस्याओं को समझना भी संभव नहीं है। कला का शिक्षण भी मनुष्य के सांस्कृतिक विकास के लिए जरूरी है।
(8) महिलाओं तथा पुरुषों को व्यावसायिक शिक्षण प्रदान करना-सामान्य जीवन- यापन व कतिपय मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता पैदा करने के लिए बच्चे-बच्चियों को व्यावसायिक शिक्षण देना भी बहुत जरूरी है। अतः रसेल ने व्यावसायिक शिक्षण को भी शिक्षा का उद्देश्य रखा है।
–
(9) विश्व बन्धुत्व की भावना का विकास-युद्ध और वैमनस्य से तार-तार संसार की आज सबसे बड़ी जरूरत है मानवीय सद्भावना। अतः विश्वशान्ति समृद्धि एवं प्रगति के लिए विश्वबंधुत्व की शिक्षा बहुत जरूरी है।
प्रश्न 5 (ii) डॉ. एनी बेसेंट के शैक्षिक चिन्तन की संक्षिप्त विवेचना कीजिए।
अथवा
एनी बेसेंट के द्वारा दिये गये शिक्षा के पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए।
अथवा
एनी बेसेंट के शिक्षा का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर —
डॉ. एनी बेसेंट का शैक्षिक चिन्तन
डॉ. एनी बेसेंट बहुमुखी प्रतिभा की महिला थी। इंग्लैण्ड से भारत आने के बाद इन्होंने भारतीयों के सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक उत्थान के लिए अथक परिश्रम किया। ये जानती थीं कि भारतीयों के सामाजिक पिछड़ेपन, आर्थिक विपन्नता, धार्मिक कूपमंडूकता और राजनैतिक दासता, इन सबका मूल कारण शिक्षा का अभाव है। ये भारत की तत्कालीन अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली से असन्तुष्ट थीं। इन्होंने सर्वप्रथम भारतीयों के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास पर बल दिया। साथ ही शिक्षा का प्रकाश जन-जन तक पहुँचाने पर बल दिया बच्चे, युवक, वृद्ध, सभी की शिक्षा की व्यवस्था पर बल दिया, पिछड़ों की शिक्षा पर बल दिया और स्त्रियों की शिक्षा पर बल दिया। इन्होंने इस बीच शिक्षा के विषय में जो कुछ भी सोचा-विचारा और किया वह सब भारतीय सन्दर्भ में हो। इन्होंने भारत के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना भी तैयार की थी। इनके शैक्षिक विचार किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय शिक्षा के निर्माण में सहायक हो सकते हैं। यहाँ इनके शैक्षिक विचारों का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत है।
शिक्षा का सम्प्रत्यय
एनी बेसेंट के अनुसार बच्चों को विद्यालयों में कुछ तथ्य रटवाकर परीक्षा में उत्तीर्ण करवाना भर शिक्षा नहीं है, शिक्षा द्वारा तो उनका शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक एवं आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। ये शिक्षा को विकास की एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करती थीं जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं और शक्ति को विकसित किया जाता है। इनके अपने शब्दों में- की
-मनुष्य जन्मजात क्षमताओं और शक्ति को विकसित करना ही शिक्षा है।
शिक्षा के उद्देश्य
एनी बेसेंट शिक्षा को मनुष्य के सर्वांगीण विकास का साधन मानती थीं। ये मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक, दोनों प्रकार के विकास पर समान बल देती थीं। इनके द्वारा निश्चित शिक्षा के उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध किया जा सकता है-
1. शारीरिक विकास-
एनी बेसेंट के अनुसार मनुष्य की सबसे पहली आवश्यकता है-स्वास्थ्य और सुन्दरता। इन्होंने स्पष्ट किया कि मनुष्य के शारीरिक विकास के साथ उसमें प्राकृतिक सौन्दर्य की वृद्धि स्वाभाविक रूप से होती है। अतः शिक्षा द्वारा बच्चों का शारीरिक विकास किया जाना चाहिए।
2. मानसिक एवं बौद्धिक विकास-
मानसिक विकास में एनी बेसेंट का तात्पर्य बच्चों की मानसिक शक्तियों-स्मृति, तर्क, विवेक तथा निर्णय के विकास से था और बौद्धिक विकास से इनका तात्पर्य बच्चों को भाषा एवं विभिन्न विषयों के ज्ञान कराने से था। ये बच्चों की मानसिक शक्तियों के विकास एवं उन्हें विभिन्न विषयों के ज्ञान कराने पर समान बल देती थीं।
3. संवेगात्मक एवं चारित्रिक विकास-
एनी बेसेंट ने स्पष्ट किया कि मनुष्य आचरण करता है अपने संवेगों के आधार पर करता है अतः प्रारम्भ से ही उसके संवेगों को समाज के आदर्शोनुकूल प्रशिक्षित करना चाहिए। इनकी दृष्टि से इसी स्थिति में बच्चे नैतिक आचरण की ओर प्रवृत्त होते हैं, उनमें आत्मबल का विकास होता है और वे चरित्रवान बनते हैं। एनी बेसेंट के यह शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए।
4. सामाजिक विकास-
एनी बेसेंट के शब्दों में- “शिक्षा का परम कर्त्तव्य है कि वह मनुष्यों को उच्च कोटि का सामाजिक प्राणी बनाए, उनमें एक-दूसरे के प्रति प्रेम, सहानुभूति और सहयोग की भावना विकसित करे। इसे ही दूसरे शब्दों में सामाजिक विकास कहते हैं।”
5. आर्थिक विकास-
एनी बेसेंट ने भारत की असली तस्वीर देखी थी, दीन-हीनों की हड्डियों से झाँकती गरीबी देखी थी। ये जानती थीं कि बिना आर्थिक विकास के गरीबी दूर नहीं की जा सकती, जीवन स्तर ऊँचा नहीं उठाया जा सकता। अतः इन्होंने शिक्षा द्वारा बच्चों को उपयोगी कला-कौशल, उद्योग एवं व्यवसायों की शिक्षा देने पर बल दिया। इसे शिक्षा जगत् में आर्थिक विकास का उद्देश्य, व्यावसायिक उद्देश्य और रोटी का उद्देश्य, अनेक नामों से अभिव्यक्त किया जाता है।
6. राष्ट्रीय चेतना की जागृति-
राष्ट्रीय चेतना से एनी बेसेंट का अर्थ था अपनी जाति, संस्कृति एवं धर्म के प्रति गर्व की भावना और अपने देश के प्रति प्रेम एवं समर्पण की भावना । इन्होंने देखा कि उस समय भारतवासियों में इस भावना की बड़ी कमी थी। इन्होंने इस बात पर बहुत बल दिया कि शिक्षा द्वारा बच्चों को अपनी सभ्यता एवं संस्कृति की श्रेष्ठता से अवगत कराया जाए, उनमें उसके प्रति गौरव की भावना का विकास किया जाए और साथ ही उनमें राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्र समर्पण की भावना का विकास किया जाए।
7. धार्मिक एवं आध्यात्मिक विकास-
एनी बेसेंट का धर्म के प्रति दृष्टिकोण बहुत उदार था. ये संसार के सभी धर्मों का आदर करती थीं परन्तु धार्मिक अन्धविश्वासों की ये बड़ी विरोधी थीं। ये मनुष्यों को मानव धर्म की शिक्षा देने पर बल देती थीं और उन्हें धार्मिक अन्धविश्वासों से मुक्त करना चाहती थीं। इनका विश्वास था कि सच्चे मानव धर्म से ही मनुष्य का भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास किया जा सकता है। इनके अनुसार कोई भी शिक्षा जो मनुष्य को अपने चरम लक्ष्य (अध्यात्म) की प्राप्ति में सहायक नहीं होती, एक अधूरी शिक्षा है।
शिक्षा की पाठ्यचर्या
एनी बेसेंट ने शिक्षा की पाठ्यचर्या को दो आधारों पर विकसित किया है-एक शिक्षा के उद्देश्य और दूसरा शिक्षा के स्तर। शिक्षा के स्तरों को इन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार पर निश्चित किया था। यहाँ इनके द्वारा विकसित विभिन्न स्तरों की पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रस्तुत है-
1. शिशु स्तर (2.5 वर्ष से 5 वर्ष की आयु तक)-
एनी बेसेंट शिशु मनोविज्ञान से परिचित थीं। ये जानती थीं कि इस आयु स्तर पर शिशुओं का शारीरिक विकास तेजी से होता है, उनकी इन्द्रियाँ प्रशिक्षित होती हैं और उनके व्यक्तित्व निर्माण की नींव रखी जाती है। इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य और शिशुओं के मनोविज्ञान की दृष्टि से इस स्तर पर मौखिक भाषा के विकास पर सर्वाधिक बल दिया, साथ ही गणना, संगीत और खेल-कूद की क्रियाओं को स्थान दिया। इन्होंने इस स्तर पर शिशुओं को ऐसा पर्यावरण प्रदान करने पर बल दिया जिसमें वे सत्य, प्रेम, सहानुभूति और सहयोग का सच्चा पाठ पढ़ें, ये उनके व्यक्तित्व के अंग हों।
2. प्राइमरी स्तर (5 वर्ष से 7 वर्ष की आयु तक)-
एनी बेसेंट पूर्व बाल्यकाल मनोविज्ञान से भी परिचित थीं। ये जानती थीं कि इस काल में बच्चों का मानसिक विकास तेजी से होता है इसलिए इस स्तर की पाठ्यचर्या में इन्होंने पढ़ने-लिखने एवं गणित और साथ ही धार्मिक कहानियों, खेल-कूद, सफाई और सामाजिक सेवा कार्यों को स्थान दिया।
3. लोअर सेकेण्ड्री स्तर (7 वर्ष से 10 वर्ष की आयु तक)-
मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इस काल में बच्चों का मानसिक एवं संवेगात्मक विकास तेजी से होता हैं। इस दृष्टि से एनी बेसेंट ने इस स्तर की पाठ्यचर्या में मातृभाषा के साथ संस्कृत, पालि, अरबी तथा फारसी भाषाओं, इतिहास तथा भूगोल और गणित विषयों के अध्ययन, प्रकृति अध्ययन एवं हस्तकौशल शिक्षा को स्थान दिया। इन्होंने इस स्तर पर धार्मिक कहानियों के माध्यम से धर्म की शिक्षा देने की बात भी कहीं। खेल-कूद एवं व्यायाम की क्रियाएँ इस स्तर पर भी चालू रहेंगी।
4. अपर सेकेण्ड्री स्तर (10 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक )-
एनी बेसेंट ने स्पष्ट किया कि इस आयु स्तर पर बच्चों का शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है और उनके संवेग स्थिर होने शुरू होते हैं, अतः इस स्तर पर लोअर सेकेण्ड्री स्तर के सभी विषयों-मातृभाषा, संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी, इतिहास, भूगोल, गणित और सभी क्रियाओं-प्रकृति अध्ययन, हस्त कार्य, खेल-कूद और व्यायाम को स्थान दिया जाए और इनके साथ-साथ अंग्रेजी भाषा एवं विज्ञान विषयों और प्रारम्भिक चिकित्सा एवं समाजसेवा क्रियाओं को स्थान दिया जाए।
5. हाई स्कूल स्तर (14 से 16 वर्ष की आयु तक )-
हाईस्कूल शिक्षा को एनी बेसेंट ने छह वर्गों में विभाजित किया और छहों के लिए अलग-अलग पाठ्यचर्या निश्चित की है-
(1) सामान्य हाई स्कूल (साहित्यिक)- मातृभाषा, संस्कृत, पालि, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, भारतीय इतिहास, ब्रिटेन का इतिहास तथा भूगोल ।
(2) सामान्य हाई स्कूल-वैज्ञानिक-मातृभाषा, संस्कृत, पालि, अरबी या फारसी, अंग्रेजी, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, बीजगणित तथा रेखागणित।
(3) सामान्य हाई स्कूल प्रशिक्षण-मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, विद्यालय व्यवस्था, शारीरिक शिक्षा, शिक्षण अभ्यास, प्रकृति विज्ञान तथा गृह विज्ञान ।
(4) वाणिज्य हाई स्कूल-देशी भाषाएँ, विदेशी भाषाएं, व्यावहारिक पत्र व्यवहार, हिसाब- किताब, व्यापारिक कानून, टंकण, शीघ्र लिपि, व्यापारिक इतिहास तथा व्यापारिक भूगोल।
(5) तकनीकी हाई स्कूल-मातृभाषा, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, व्यावसायिक इतिहास, आरम्भिक इंजीनियरिंग, यंत्र विद्या तथा विद्युत ज्ञान ।
(6) कृषि हाई स्कूल-संस्कृत, पालि, अरबी या फारसी, ग्रामीण इतिहास, भूगोल, गणित, हिसाब-किताब, भूमि की नाप-तौल, कृषि सम्बन्धी रासायनिक एवं भौतिक विज्ञान, कृषि सम्बन्धी यन्त्र ज्ञान, प्रकृति अध्ययन, बागवानी, हाईजीन तथा प्रारम्भिक इंजीनियरिंग ।
6. उच्च स्तर (16 वर्ष से 21 वर्ष की आयु तक )-
इस स्तर को इन्होंने दो स्तरों में विभाजित किया है- स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर और दोनों के लिए पाठ्यक्रम की सीमा निश्चित की है-
(1) स्नातक स्तर (16 वर्ष से 19 वर्ष की आयु तक)- इस स्तर को इन्होंने साहित्यिक, वाणिज्य, वैज्ञानिक, तकनीकी और कृषि आदि वर्गों में विभाजित किया और इस बात पर बल दिया कि इस स्तर की पाठ्यचर्या केवल सैद्धान्तिक न हो अपितु व्यावहारिक भी हो। उसे पूरा करने के बाद स्नातक अपनी संस्कृति से परिचित हों और वास्तविक जीवन में सफल हों।
(2) स्नातकोत्तर स्तर (19 वर्ष से 21 वर्ष की आयु तक )-
इन दो वर्षों में किसी स्नातक को वर्ग विशेष के क्षेत्र विशेष में विशेष योग्यता प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाए। इस स्तर पर यह ध्यान रखा जाए कि यथा ज्ञान एवं कौशल का व्यावहारिक जीवन में उपयोग हो।
इकाई – III
प्रश्न 6 (i) सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा के योगदान को बताइए।
अथवा
‘सामाजिक परिवर्तन’ में शिक्षा की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
अथवा
सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समझाइए तथा इसमें शिक्षा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालिए।
अथवा
सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारणों का भारतीय सन्दर्भ में उल्लेख कीजिए। सामाजिक परिवर्तन की क्या विशेषताएँ हैं? शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन के सम्बन्धों की व्याख्या कीजिए। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा के महत्व पर चर्चा कीजिए।
सामाजिक परिवर्तन
संसार की समस्त वस्तुएँ, विचार, सभ्यता, संस्कृति आदि परिवर्तनशील हैं। समाज जो परिवर्तनशील है। जब सामाजिक व्यवस्था प्रक्रिया या सामाजिक संरचना में स्पष्ट रूप से कोई अन्तर दृष्टिगोचर होत है तब हम उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, “सामाजिक संरचना अथवा सामाजिक सम्बन्धों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं।’
जेन्सन ने सामाजिक परिवर्तनों को लोगों के कार्य तथा विचार करने की पद्धतियों में रूपान्तरण कहकर परिभाषित किया है। डॉसन एवं गेटिस के अनुसार, “सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है क्योंकि समस्त संस्कृति अपनी उत्पत्ति, अर्थ एवं प्रयोग में सामाजिक हैं।’
इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में कुछ बातें होती हैं जो निम्नलिखित हैं-
(1) सामाजिक परिवर्तन का सम्बन्ध किसी व्यक्ति या समूह-विशेष के जीवन में होने वाले परिवर्तनों से नहीं है। सामाजिक परिवर्तन वास्तव में सामुदायिक परिवर्तन से सम्बन्धित है।
(2) सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है।
(3) सामाजिक परिवर्तन की गति असमान होती है।
(4) सामाजिक परिवर्तन की गति समय से प्रभावित होती है।
(5) सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी कठिन है।
सामाजिक परिवर्तनों में शिक्षा का योगदान
शिक्षा सामाजिक मूल्यों तथा उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होती है। अतः समाज के उद्देश्यों के अनुसार ही शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। समाज का मतलब है उस समाज से जो समाज का बदला हुआ नवीन रूप है। इस बदले हुए रूप के अनुरूप ही शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित होते हैं। कभी-कभी ऐसी स्थिति भी सामने आती है जबकि शिक्षा के उद्देश्यों का समाज के उद्देश्यों के साथ मेल नहीं खाता। लेकिन समाज शिक्षा को अपने अनुरूप बना ही लेता है। ऐसी स्थितियाँ भी आती हैं जबकि सामाजिक परिवर्तन तेजी के साथ हो जाता है और शिक्षा अपने अन्दर परिवर्तन नहीं ला पाती।
उदाहरण के लिए, यदि कोई समाज सैनिक शक्ति की दृढ़ता में विश्वास करता है तो उसकी शिक्षा में ‘सैनिक शिक्षा’ को महत्त्व दिया जाता है। यदि समाज लोकतन्त्र में विश्वास करता है तो शिक्षा में उन तत्त्वों का समावेश किया जाना आवश्यक हो जाता है जिनसे कि जनतान्त्रिक विचारधारा को बल मिल सके।
विद्यालय शिक्षा प्रदान करने का केन्द्र होता है। शिक्षा पर यानी विद्यालय व्यवस्था के ऊपर सामाजिक व्यवस्था का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अत । विद्यालय का प्रबन्ध सामाजिक व्यवस्थाओं पर निर्भर कहा जा सकता है। सामाजिक व्यवस्था के भी कुछ उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों की पूर्ति शिक्षा के द्वारा विद्यालय ही करते हैं |
विद्यालय पर उस देश की राष्ट्रीय नीति का प्रभाव पड़ता है। आज संसार के सभी अविकसित देशों में औद्योगिक शिक्षा का प्रचार बड़ी तेजी से हो रहा है। इसलिए विज्ञान और तकनीकी शिक्षा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। देश में औद्योगिक तथा तकनीकी शिक्षा विद्यालयों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है।
तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा का यह परिणाम अनेक देशों में साफ-साफ दिखायी दे रहा है कि वे देश आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। उनको कोई भी चीज़ अन्य देशों से नहीं माँगनी पड़ रही है। इस आत्मनिर्भरता और शिक्षा के परिणामस्वरूप सभी देशों के समाज में काफी परिवर्तन आ गया है।
हर कोई समाज आगे बढ़ना चाहता है, यानी परिवर्तन चाहता है। परिवर्तन या उन्नति होगी कैसे? सभी जानते हैं कि शिक्षा के द्वारा शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल भेजती है। विद्यालय भी उसी ढंग की शिक्षा का प्रबन्ध करता है जो शिक्षा लोग चाहते हैं।
जिस समाज में शिक्षा की ठीक व्यवस्था नहीं होती उस समाज की उन्नति करने वाले लोगों की कमी हो जाती है। इसका प्रभाव उस समाज के परिवर्तन पर बहुत ही बुरा पड़ता है। इससे यह स्पष्ट है कि शिक्षा का प्रभाव समाज पर अवश्य पड़ता है। जिस देश में शिक्षा नहीं है उस देश के लोग संसार के सभी देशों से पिछड़ जाते हैं।
उक्त कथन से स्पष्ट है कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का विशेष हाथ होता है। अन्य शब्दों में, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन से प्रभावित न हो तो वह उस समाज का कोई कल्याण नहीं कर सकती।
सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक
सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण निम्न प्रकार है-
1. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास-
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास से सामाजिक परिवर्तन को तीव्र गति प्राप्त होती है। यह सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली कारक है। नए मशीनी आविष्कारों से जीवन-शैली में अन्तर आता है। आज संचार प्रणाली में आई क्रान्ति ने नवीन युग का सूत्रपात किया है। कम्प्यूटर, मोबाइल फोन, इन्टरनेट आदि की खोजों ने भौगोलिक दूरी को कम कर दिया है, इसने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के सम्बन्धों को प्रभावित किया है। विश्व, भूमण्डलीकरण की ओर प्रवृत्ति है, विश्व स्तर पर सहयोगी कार्यक्रमों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। भूमण्डलीय समस्याओं जैसे प्रदूषण, भूकम्प, पोलियो, समुद्री तूफान आदि के निदान हेतु समस्त विश्व प्रयासरत हैं। अनेक जन स्वास्थ्य, कार्यक्रम विश्व स्तर पर चलाए जा रहे हैं। आतंकवादी अमानवीय कृत्यों का विकराल रूप आज समस्त विश्व के लिए चुनौती बना है। सभी देश मिलकर इसका समाधान खोजने में प्रयासरत् हैं। इस प्रकार तकनीकी प्रगति ने ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ के चिरकालीन भारतीय आदर्श को वास्तविक रूप दिया है, जो शिक्षा द्वारा ही सम्भव हुआ है।
–
2. विचारधाराएँ-
जनमत में परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन आता है। प्राचीन काल से अब तक सभी देशों में राजनैतिक, सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं, उन सबका मूल कारण उनकी विचारधाराओं में परिवर्तन ही रहा है। कई देशों, जैसे- रूस, जर्मनी, फ्रांस आदि का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जनमत के शक्तिशाली होने पर उनका शासन-तन्त्र भी बदला है। जनमत के निर्माण में शिक्षा एक प्रभावी भूमिका निभाती है। विभिन्न विचारधाराओं, जैसे समाजवाद, पूँजीवाद, मार्क्सवाद आदि का प्रचार उनके नेताओं द्वारा शिक्षा के माध्यम से ही किया जाता है, यद्यपि इस प्रचार में विद्यालयों की अपेक्षा शिक्षा के अनौपचारिक साधनों का प्रभाव अधिक पड़ता है। आज भी संचार के साधन समाज पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। पश्चिमी संस्कृति की ओर युवाओं का बढ़ता रुझान, परम्परागत नैतिक आदर्शों एवं मूल्यों की उपेक्षा, भौतिकता के प्रति लगाव आदि वैचारिक परिवर्तन को इंगित करते हैं। शिक्षा के द्वारा पश्चिमीकरण की इस प्रक्रिया में उचित-अनुचित, उपयोगी अनुपयोगी की समझ प्रदान करके सामाजिक नियन्त्रण किया जाता है तथा इस अन्धानुकरण को रोककर विचारधाराओं की सही शिक्षा प्रदान करने का कार्य शिक्षा द्वारा सम्पन्न किया जाता है।
3. समाजीकरण की प्रक्रिया-
व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। वह जिस समाज में जन्म लेता है और अपना जीवन-निर्वाह करता है उसके विचारों, विश्वासों, मान्यताओं, परम्पराओं और रूढ़ियों का उस पर प्रभाव पड़ता है। अपने परिवार, पड़ोस, समूह, विद्यालय और समाज के अन्य व्यक्तियों के सम्पर्क में आकर वह जीने का ढंग सीखता है, उनसे सामंजस्य स्थापित करता है और उनकी संस्कृति को आत्मसात् करता है, यही उसका समाजीकरण कहलाता है। जब व्यक्ति को अपने समाज से लगाव होता है, वह उसकी क्रियाओं में भागीदारी करता है, समाज के सुख-दुःख उसके सुख-दुःख बन जाते हैं और समाज पर विपत्ति आने पर वह अपने सुखों की परवाह न करके दूसरों का दुःख दूर करने का प्रयास करता है तब उसके यह समस्त कार्य ‘हम की भावना’ से प्रेरित होते हैं और हम उसे समाजीकृत मनुष्य कहकर पुकारते हैं। समाजीकृत स्त्रियों एवं पुरुषों के प्रयासों से सामाजिक परिवर्तन आता है। सामाजिक परिवर्तनों में समाज के महान् व्यक्तियों की निःस्वार्थता, उच्च मनोबल और पवित्र आत्मा की झलक होती है। शिक्षा द्वारा व्यक्तियों का समाजीकरण किया जाता है और उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति का रोपण करके उन्नत चरित्र का गठन किया जाता है।
4. सांस्कृतिक कारक-
मानव द्वारा निर्मित समस्त परिवेश उसकी संस्कृति कहलाता है, इसमें अभौतिक एवं भौतिक दोनों प्रकार की चीजें सम्मिलित होती हैं। भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तीव्र गति से होता है जबकि अभौतिक संस्कृति धीमी गति से परिवर्तित होती है। दोनों ही प्रकार के परिवर्तन हमारी जीवन-शैली, जीवन-स्तर, विचारधारा और हमारे सामाजिक सम्बन्धों पर प्रभाव डालते हैं इनसे सम्पूर्ण समाज में परिवर्तन आता है। शिक्षा हमारी संस्कृति के निर्माण की आधारशिला है। शिक्षा द्वारा होने वाली वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी उन्नति द्वारा हम भौतिक विकास करते हैं तथा वैचारिक उन्नति से अपने आदर्शों, मूल्यों और परम्पराओं को नवीन रूप देते हैं। इस प्रकार शिक्षा सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है जो सामाजिक परिवर्तन लाता है।
5. प्राकृतिक कारक-
मानव-जीवन प्रकृति पर निर्भर करता है। वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा मनुष्य ने प्रकृति पर नियन्त्रण प्राप्त करके उसे अपने उपयोग में लाने का प्रयास किया है, किन्तु प्राकृतिक शक्तियाँ इतनी सशक्त हैं कि मनुष्य को उनके सामने अपनी हार स्वीकार करनी पड़ती है। ज्वालामुखी के फटने, बाड़ आने, भूकम्प आने, सूखा पड़ने, अतिवृष्टि होने आदि आदि खगोलीय आपदाओं से हमारी जीवन-शैली पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे सामाजिक सम्बन्धों में भी परिवर्तन आता है। शिक्षा द्वारा, इन विपत्तियों के समय सावधानी बरतने पर सकारात्मक कदम उठाने की समझ उत्पन्न की जाती है।
प्राकृतिक कारक हमारे जीवन की समृद्धि के भी आधार हैं, जैसे – कोयले और धातु आदि की खानों तथा तेल और गैस के कुओं की खोज से जीवन समृद्ध होता है, जिससे सामाजिक परिवर्तन अनुकूल दिशा में होता है। शिक्षा द्वारा नवीन प्राकृतिक सम्पदा को मानव कल्याण हेतु प्रयोग करने का ज्ञान प्राप्त होता है।
6. जैविकीय कारक-
विश्व में असंख्य जनसंख्या है, जिसकी अनेक प्रजातियाँ हैं। इन प्रजातियों के मिलने से और सम्बन्ध स्थापित करने से सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन आता है। जनसंख्या के बढ़ने- घटने तथा स्त्री-पुरुष अनुपात में परिवर्तन आने से पारिवारिक संरचना, आर्थिक क्षमता और जीवन-शैली प्रभावित होती है। विपरीत दिशा में होने वाले परिवर्तनों को शिक्षा द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री माल्थस के अनुसार यदि समाज जनसंख्या विस्फोट को समय से पूर्व नियन्त्रित नहीं कर पायेगा तब प्राकृतिक विप्लव की स्थिति उत्पन्न होगी, जो विनाश का कारण सिद्ध होगी। माल्थस की उक्त चेतावनी ने विश्व को सचेत किया है। विभिन्न देशों की सरकारें और स्वयं-सेवी संगठन दोनों ही जन-शिक्षा द्वारा जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण के प्रयास कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों द्वारा किए जा रहे शिक्षा-प्रसार कार्यक्रमों में जनसंख्या शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया गया है।
7. मनोवैज्ञानिक कारक-
मानवीय प्रवृत्ति परिवर्तनशील है, वह नवीन को स्वीकार करने और पुरातन को छोड़ने की ओर संचालित होती है। व्यक्ति सदैव नवीन वस्तुओं की खोज में लगा होता है, यह नवीन वस्तुएँ भौतिक अथवा अभौतिक हो सकती हैं। विदेशी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव को देखकर हम व्यक्ति की इस मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का अनुमान लगा सकते हैं। किन्तु प्रत्येक नवीन वस्तु लाभकारी नहीं होती, इसलिए नवीनता को स्वीकार करने में कुछ सावधानियाँ आवश्यक हैं। इस बात की समझ शिक्षा प्रदान करती है कि किस नवीन वस्तु को ग्रहण किया जाए और किस पुरातन वस्तु को संरक्षित किया जाए।
प्रश्न 6 (ii) भारत में राष्ट्रीय एकता से क्या तात्पर्य है? इसे दूर करने में शिक्षा कैसे सहायक बन सकती है?
अथवा
राष्ट्रीय एकता की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय एकता भावना के विकास में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय एकता के अर्थ को स्पष्ट करें एवं भारतीय सन्दर्भ में शिक्षा की विवेचना करें।
अथवा
राष्ट्रीय एकता का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु शिक्षक और विद्यालय की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
उत्तर –
राष्ट्रीय एकता अथवा राष्ट्रीयता का अर्थ एवं परिभाषा
राष्ट्रीय एकता राष्ट्रीयता का पर्याय है, राष्ट्रीयता का अर्थ किसी राष्ट्र के नागरिकों की एकता की भावना से होता है। यह भावना किसी भी राष्ट्र के विकास के लिये आवश्यक है। राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना ही राष्ट्रीय एकता अथवा राष्ट्रीयता है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा राष्ट्रीय एकता की व्याख्या विभिन्न प्रकार की गयी है, जो निम्न प्रकार है-
राष्ट्रीय एकता सम्मेलन की रिपोर्ट (1961) के अनुसार, “राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के हृदयों में एकता, संगठन, सन्निकटता की भावना, सामान्य नागरिकता की भावना और राष्ट्र के प्रति शक्ति की भावना का विकास किया जाता है।
”
बूबेकर के मतानुसार, “राष्ट्रीयता साधारण रूप में, देश-प्रेम की अपेक्षा देश भक्ति के अधिक व्यापक क्षेत्र की ओर संकेत करती है। राष्ट्रीयता में स्थान के सम्बन्ध के साथ-साथ जाति, भाषा, इतिहास, संस्कृति और परम्पराओं के सम्बन्ध भी प्रदर्शित होते हैं।”
इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम राष्ट्रीयता के अर्थ को स्पष्ट कर सकते हैं। राष्ट्रीयता की भावना में देश-प्रेम के तत्त्व निहित होते हैं जो देश के नागरिकों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करते हैं। सच्ची राष्ट्रीयता वही है जिसमें व्यक्ति देशहित, राष्ट्रहित के लिए सभी कुछ त्याग देने के लिए तत्पर रहता है।
राष्ट्रीय एकता में शिक्षा की भूमिका
शिक्षा संस्थाओं तथा राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति का सबसे प्रमुख साधन है। इसकी उपयोगिता राष्ट्रीय एकता समिति ने भी स्वीकार की थी। वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम किये जा सकते हैं-
1. राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली-
देश में राष्ट्रीय एकता लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक ही शिक्षा प्रणाली होनी चाहिये। वर्तमान शिक्षा 10+2+3 को यदि अच्छी प्रकार से सारे देश में लागू करने का प्रयास किया जाये तो यह राष्ट्रीय एकता लाने में सहायता दे सकती है। हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रणाली बनाने पर बल दिया है। प्रान्तीय सरकार और केन्द्रीय सरकार मिलकर एक ऐसा कार्यक्रम तैयार करें कि सभी बच्चे एक हीं राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली अपनाएँ। शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्रकार के भेदभावों को मिटा देना चाहिये। शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाकर राष्ट्र सेवा, त्रिभाषी फार्मूला इत्यादि को अनिवार्य बना देना चाहिये।
2. शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन-
आज हमने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक उद्देश्य रखे हुए हैं परन्तु वास्तविकता यह है कि हमारी शिक्षा परीक्षा प्रधान है। उसमें बच्चों के स्वास्थ्य, आचरण, भावनाओं इत्यादि को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट हों और उनके माध्यम से छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना भरने का प्रयास किया जाये।
3. दैनिक सामूहिक सभा कार्यक्रम-
सभी विद्यालयों का कार्यक्रम 15 मिनट की दैनिक सामूहिक सभा से आरम्भ होना चाहिये। इसमें राष्ट्रगान, नैतिक शिक्षा आदि की बातें बच्चों को बताई जानी चाहिये। समय-समय पर राष्ट्रीय एकता पर भाषण दिये जाने चाहियें। बच्चों व अपनी राष्ट्र भाषा, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करने के बारे में बताना चाहिये।
4. शिक्षा विधियों में सुधार-
शिक्षण विधियों में भी पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। शिक्षण विधियों का सम्बन्ध परोक्ष रूप में अध्यापक के छात्रों के साथ व्यवहार से होता है। अतः शिक्षण की उन विधियों का चुनाव करना चाहिये जिनमें अध्यापक सभी बच्चों की समान रूप से सहायता कर सके और सभी बच्चों को अपनी योग्यतानुसार विकसित होने के समान अवसर प्राप्त हों।
5. राष्ट्रीय नेताओं के जन्म दिवस मनाना-
विद्यालयों में राष्ट्रीय नेताओं के जन्म दिवस मनाकर भी बच्चों में राष्ट्रीय एकता की भावना भरी जा सकती है। इनके जन्म दिवस मनाते हुए हम बच्चों को नेताओं द्वारा राष्ट्रीय एकता के लिये किये गये कार्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं और उन्हें भी इन राष्ट्रीय नेताओं के पदचिह्नों पर चलने के लिये प्रेरित किया जाना चाहिये
6. राष्ट्रीय पर्वों के मनाना –
विद्यालय में राष्ट्रीय पर्वों 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर धूमधाम से मनाकर भी बच्चों में राष्ट्रीय एकता की भावना भरने का प्रयास किया जाना चाहिये।
7. भ्रमण – अध्यापक एवं छात्रों में राष्ट्रीय एकता लाने के लिये देश के विभिन्न भागों, विशेषकर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक और राष्ट्रीय महत्त्व के स्थानों का भ्रमण करने के अवसर दिये जाने. चाहिये। इससे उन्हें अपने देश की विशालता और राष्ट्र की भिन्न-भिन्न संस्कृतियों का ज्ञान होगा और उनमें एकता की भावना का विकास होगा।
अध्यापक बच्चों के लिए आदर्श है, इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि अध्यापक स्वयं राष्ट्रीयता की भावना से पूर्ण हो। उसको राष्ट्रप्रेमी होना चाहिये। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रभाषा के प्रति उनमें श्रद्धापूर्ण सम्मान होना चाहिये। यदि अध्यापक राष्ट्रध्वज के नीचे खड़ा होकर पहले अपने आपको भारत राष्ट्र का नागरिक समझता है तो बच्चे भी उनका अनुसरण करेंगे। समाज सेवा तथा राष्ट्र सेवा अध्यापक का धर्म होना चाहिये और इस भावना को प्रदर्शन उन्हें विद्यालयों में अपने कार्य को पूरा करके बताना चाहिये। अध्यापक को सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार रखना चाहिये। अध्यापक को अपने नैतिक प्रवचनों में इस बात पर बल देना चाहिये कि जाति धर्म सम्प्रदाय और किसी भी अन्य से ऊँचा राष्ट्र होता है। शिक्षा के क्षेत्र में ऊपर लिखित कार्यक्रमों को सही दिशा तभी दी जा सकती है जब अध्यापक स्वयं राष्ट्रीयता का प्रतीक बनकर सामने आए।
8. राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों का आदान-प्रदान-
राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों का एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में आदान-प्रदान होना चाहिये। एक प्रान्त के बच्चों को दूसरे प्रान्तों में अध्ययन करने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये, जिससे अन्तर्सास्कृतिक एवं अन्तर्प्रान्तीय भावना का विकास होगा तथा यह राष्ट्रीय एकता के विकास में भी सहायक होगा।
9. राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों का आदान-प्रदान –
माध्यमिक स्तर पर अध्यापकों तथा विश्वविद्यालय स्तर प्राध्यापकों का राष्ट्रीय स्तर पर आदान-प्रदान होना चाहिये। जब भिन्न-भिन्न भाषा, जाति, धर्म और सम्प्रदाय के अध्यापक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जायेंगे तो इनके माध्यम से भिन्न- भिन्न संस्कृतियों का तालमेल होगा, इनका यह तालमेल बच्चों में सांस्कृतिक भावना का विकास करेगा और यह राष्ट्रीय एकता के विकास में भी सहायक होगा तथा पूरा देश एकता के सूत्र में बँधेगा।
10. राष्ट्रभाषा हिन्दी का विकास-
राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी भाषा के विकास के लिए प्रयास किए जाने चाहिये। यद्यपि हमारे देश में संविधान के अनुसार 15 भाषाओं की मान्यता है लेकिन हमने हिन्दी को राष्ट्र भाषा का स्थान दे रखा है। अतः राष्ट्र भाषा के विकास के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि राष्ट्र भाषा हमें एकता के सूत्र में बाँधती हैं
11. पाठ्य-पुस्तकों में सुधार –
पाठ्य-पुस्तकों का पुनः अवलोकन किया जाना चाहिये और उनमें से ऐसी सामग्री निकाल दी जानी चाहिए जो राष्ट्रीय एकता में बाधक हो। इन पुस्तकों में राष्ट्रीय एकता में सहायक होने वाली सामग्री का समावेश होना चाहिये। इसके लिए देश की विभिन्न सभ्यता एवं संस्कृति से सम्बन्धित विषय सामग्री का चुनाव करना चाहिये।
12. धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा-
राष्ट्रीय एवं भावात्मक शिक्षा के लिए धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा का होना बड़ा आवश्यक है। धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा द्वारा चरित्र का निर्माण होता है। सभी व्यक्ति एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग जो संकीर्ण भावनाओं के नहीं होते उनमें भावात्मक एकता आ जाती है।
13. रेडियो तथा टेलीविजनों का प्रयोग-
रेडियो तथा टेलीवीजन पर ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जायें जो राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायक हो। हमारे देश में ऐसे प्रयास किए भी जाते हैं। रेडियो तथा टेलीवीजन पर विभिन्न भाषाओं के पाठ तथा विभिन्न भाषाओं, धर्मों, सभ्यता एवं संस्कृति से सम्बन्धित कथा, नाटक गीत और कविताएँ आदि प्रसारित होते रहते हैं। इससे बच्चों को पूरे देश की झाँकी देखने में सहायता मिलती है।
14. पैन फ्रैण्ड्स तथा उपहार-
कई बार समय या धन के अभाव के कारण भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के विद्यार्थी प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित नहीं कर सकते परन्तु उनमें पत्रों द्वारा मित्रता स्थापित हो सकती है। कुछ पत्रिकाएँ भी इसमें योगदान दे सकती हैं। ये पत्रिकाएँ ऐसे विद्यार्थियों के पते और रुचि आदि का विवरण दे सकती हैं जो पत्र मित्रता स्थापित करना चाहते हैं। इन पत्रों में वे अपने क्षेत्रों के पक्षों की महत्त्वपूर्ण जानकारी अपने मित्रों को दे सकते हैं। कभी-कभी कोई छोटी-मोटी सौगात भेज कर अपने क्षेत्र की कला की जानकारी दे सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय एकता में बहुत बढ़ावा मिल सकता है
15. पुस्तकालय –
पाठशाला के पुस्तकालयों में अधिक और ठीक प्रकार की पुस्तकें होनी चाहिये। पुस्तकालय में ऐसी पुस्तकें होनी चाहिये जिनको पढ़ने से भावात्मक एकता को प्रोत्साहन मिले न कि दूसरे धर्मों, जातियों तथा क्षेत्रों के प्रति घृणा के भाव आएँ ।
प्रश्न 7 (i) शिक्षा में प्रकृतिवाद क्या है? शिक्षा सिद्धान्त में इसका योगदान क्या है?
प्रकृतिवाद का अभिप्राय और परिभाषा
दार्शनिकों के अनुसार प्रकृतिवाद वह विचारधारा है, जिसमें विचारों की तुलना में व्यक्ति को प्रधानता दी गई। प्रकृतिवाद आत्मा-परमात्मा जैसी अलौकिक बातों में विश्वास नहीं करता। प्रकृतिवाद में आध्यात्मिक विचारों का कोई महत्त्व नहीं है। हर वस्तु का जन्म प्रकृति से होता है और उसका अन्त भी प्रकृति में ही होता है। प्रकृति ही सम्पूर्ण जगत् की नियन्ता है। प्रकृति से परे या प्रकृति के बाद कुछ नहीं है। यों कहा जाए कि प्रकृति ही नियम भी है और वही नियन्ता भी, प्रकृति ही साधन है और वही साध्य भी, प्रकृति ही आदि और प्रकृति ही अन्त भी । प्रकृतिवाद प्रकृति को ही मनुष्य का धर्म एवं सामाजिक आधार मानता है।
विभिन्न विद्वानों ने प्रकृतिवाद को इस प्रकार परिभाषित किया है-
जायस के शब्दों में, “प्रकृतिवाद एक ऐसा दार्शनिक तन्त्र है। जिसमें प्रभुत्व विशेषता के रूप में आध्यात्मिक, अन्त ज्ञानात्मक एवं पदार्थ जगत् से परे की अनुभूतियों को बहिष्कृत किया जाता है।”
पैरी के अनुसार, “प्रकृतिवाद, विज्ञान नहीं है, वरन् विज्ञान के बारे में दावा है। अधिक स्पष्ट रूप में यह इस बात पर दावा है कि वैज्ञानिक ज्ञान अन्तिम है, जिसमें विज्ञान से बाहर या दार्शनिक ज्ञान का कोई स्थान नहीं है।”
जेम्स बार्डे के अनुसार, “प्रकृतिवाद वह सिद्धान्त है, जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक् करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है।’
थॉमस और लैंग के शब्दों में, “प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है, और यह विश्वास करता है कि अन्तिम वास्तविकता-भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं।”
प्रकृतिवाद का दार्शनिक आधार
प्रकृतिवादी दार्शनिकों का मानना है कि इस सृष्टि की रचना परमाणुओं के संयोग से हुईं है। इसके अनुसार जो कुछ हम देखते हैं, वह परमाणुओं के संयोग का फल है। प्रकृतिवादियों के अनुसार मनुष्य-इन्द्रियों एवं विभिन्न शक्तियों का समन्वित रूप है। इसमें आत्मा नामक चेतन तत्त्व नहीं है। सम्पूर्ण सृष्टि में नियम विद्यमान है। सब कार्य नियमानुसार होते हैं। इसलिए मनुष्य भी नियमाधीन है। और उसमें स्वतन्त्र इच्छा जैसी कोई शक्ति नहीं है। ये नियम प्रकृति के स्वयं नियम हैं। प्रकृति के नियम, शाश्वत एवं अपरिवर्तनीय हैं। इसमें प्रयोजन नाम की वस्तु के लिए कोई स्थान नहीं है। इसमें परिवर्तन किसी प्रयोजन से नहीं होते हैं, वरन् कार्य-कारण सम्बन्ध के आधार पर अपने आप स्वयं हो जाते हैं।
इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डार्विन ने विकास सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि प्रारम्भ में साधारण जातियों का निर्माण हुआ, उसके बाद साधारण जातियों से पौधे, पौधों से निम्न वर्ग के जीव-जन्तु निम्न वर्ग के जीव-जन्तुओं से पशु और पशु से मानव का निर्माण हुआ है। उनकी यह विचारधारा जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवाद कही जाती है। आत्मा-परमात्मा के विषय में सभी प्रकृतिवादी एकमत हैं। आत्मा को तो ये एक क्रियाशील तत्त्व के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन परमात्मा जैसी किसी अवधारणा को नहीं मानते। इन विचारकों के अनुसार प्रकृति भी अन्तिम सत्य है
•
प्रकृतिवादी दार्शनिक प्रकृति की अवधारणा में उन रचनाओं को शामिल करते हैं, जो प्रकृति ने इस सृष्टि में उत्पन्न की है। जिसमें मानव का कोई योगदान नहीं है। जैसे— पृथ्वी, समुद्र, पहाड़, नदियाँ, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, तारे, बादल, वर्षा, वनस्पति और जीव-जन्तु, परन्तु दार्शनिक दृष्टि से प्रकृति संसार का वह मूल तत्त्व है, जो पहले से था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। इसमें वे क्रियाएँ भी निहित हैं, जो निश्चित नियमों के अनुसार होती हैं, जैसे पहले होती थीं वैसे आज भी होती हैं और वैसे ही भविष्य में होती रहेंगी। उदाहरण के लिए, बर्फ और वाष्प, ये प्राकृतिक पदार्थ हैं, इनकी रचना समान तत्त्वों (हाइड्रोजन और ऑक्सीजन) से हुई है। हम जानते हैं कि बर्फ से जल, जल से वाष्प जल और जल से बर्फ, ये सब निश्चित नियमों के अनुसार बनते-बिगड़ते हैं। पदार्थों के मूल तत्त्व और उनके बनने-बिगड़ने के नियमों को ही प्राकृतिक प्रकृति मानता है और इनके ज्ञान को वास्तविक ज्ञान मानता है।
प्रकृतिवादी विद्वानों का स्पष्ट रूप से यह मानना है कि मानव को अपनी प्रकृति के अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए। प्रकृतिवादी मानव को किसी नियम में जकड़ कर रखने के आदी नहीं थे, ये मानव की
के पक्षधर थे। इनका तर्क है कि जिन कार्यों के करने में अनुमुक्तता को मनुष्य सुख उन कार्यों को वह करेगा और जिन कार्यों को करने से उसे दुःख का अनुभव होगा, उन्हें वह अपने आप त्याग देगा।
प्रकृतिवाद के प्रमुख सिद्धान्त
प्रकृतिवाद के मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार हैं-
(1) दिमाग मनुष्य की ताकत और शरीर द्वारा संचालित होने वाली समस्त क्रियाओं का स्रोत है।
(2) नैतिक मूलप्रवृत्ति, जन्मजात अन्तरात्मा, परलोक, वैयक्तिक अमरता, ईश्वर-कृपा, प्रार्थना- शक्ति और इच्छा की स्वतन्त्रता, भ्रम है।
(3) इस सृष्टि का निर्माण वस्तु या तत्त्व से हुआ है। मानव भी वस्तु का ही एक रूप है।
(4) मानव की मूल प्रवृत्ति पशुओं के समान होती है।
(5) विकास की प्रक्रिया में मस्तिष्क एक घटना है। यह उच्चकोटि के जीवों में अधिक विकसित नाड़ी-मण्डल का समूह है।
(6) प्रकृति अन्तिम सत्ता या वास्तविकता है.
(7) इन्द्रियों का अनुभव ही ज्ञान और सत्य का आधार है।
(8) मनुष्य के सांसारिक जीवन की भौतिक दशाएँ विज्ञान की खोजों और मशीनों के आविष्कारों के माध्यम से परिवर्तित कर दी गयी।
(9) वास्तविकता की व्याख्या केवल प्राकृतिक विज्ञानों द्वारा की जा सकती है।
(10) प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है
(11) प्रकृति के नियम अपरिवर्तनीय हैं। अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियम सब घटनाओं को भली प्रकार स्पष्ट करते हैं।
(12) प्रकृतिवाद के अनुसार समाज व्यक्ति के लाभ के लिए है। अतः समाज का स्थान व्यक्ति के बाद आता है।
(13) प्रकृति में धर्म एवं ईश्वर का कोई स्थान नहीं है ।
शिक्षा का प्रयोजन
प्रकृतिवाद व्यक्ति के स्वाभाविक, गुणों की रक्षा करना चाहता है। यह एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें व्यक्ति के स्वाभाविक अधिकार सदैव सुरक्षित रहे। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना है, जिसमें समानता, भ्रातृत्व, सरलता तथा स्वतन्त्रता के स्वाभाविक गुण समाज के सदस्यों में वर्तमान में रहें। इस प्रकार प्रकृतिवाद के शिक्षा उद्देश्य में हमें वैयक्तिकता की झलक देखने को मिलती है। रूसो एक ऐसी शिक्षा-व्यवस्था की कामना करता है, जो कि कृत्रिम समाज की झंझटों तथा अधिकारवाद के बन्धनों से मानव की रक्षा करेगा। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा किसी जो भावी जीवन की तैयारी कर रहे हैं। प्रत्युत शिक्षा स्वयं जीवन है। शिक्षा कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है, बाहर से बालक पर लादी जाएगी, वरन् शिक्षा तो स्वयं बालक के विकास की एक प्रक्रिया है। शिक्षा का प्रधान उद्देश्य एक ऐसे स्वाभाविक राज्य की स्थापना करना है, जिसमें व्यक्ति के स्वाभाविक अधिकारों की रक्षा होती है, जिसमें साधारण जनता की स्वाभाविक रुचियों का प्राधान्य रहता है, जहाँ व्यक्ति की स्वाभाविक इच्छाओं और रुचियों का अवदमन नहीं किया जाता और जहाँ कृत्रिम समाज के कृत्रिम कलाओं और विज्ञान को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है।
प्रश्न 7 (ii) अवसरों में समानता से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक अवसरों में समानता की संक्षिप्त विवेचना कीजिए।
अथवा
भारत में शिक्षा के अवसरों की विषमताओं का वर्णन कीजिए तथा इन विषमताओं को दूर करने के लिए संवैधानिक प्रावधान की संक्षिप्त विवेचना कीजिए।
अवसरों की समानता
इस ‘यू.एन. डिक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स’ (U.N. Declaration of Human Rights) ने धारा 1 एवं धारा 2 के अन्तर्गत मानवीय अधिकारों तथा समानता के अवसरों को स्वीकार किया है।
धारा 1-“सभी व्यक्ति जन्म से स्वतन्त्र हैं, अतः वे सम्मानजनक तथा समान अधिकारों के हकदार हैं। वे सभी तर्क एवं चेतना से अभिपूरित हैं तथा उन्हें परस्पर एक-दूसरे के प्रति भाई-चारे की भावना के साथ कार्य करना चाहिए।”
धारा 2-“प्रत्येक व्यक्ति इस घोषणा में उद्धृत मूल अधिकारों तथा स्वतन्त्रता का हकदार है। अतः उन्हें जाति, भाषा, धर्म, रंग, लिंग, राजनीतिक मतों द्वारा पृथक्-पृथक् नहीं किया जा सकता है।”
उपरोक्त विश्वव्यापी आन्दोलन से भारतीय संविधान भी प्रभावित है। संविधान के क्रियान्वयन के साथ ही 1950 में भारत में सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा की घोषणा कर दी गयी है। इन्हीं समानताओं को लक्ष्य मानकर शिक्षा को राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रगति का समुन्नत मार्ग माना गया है। इसकी अबाध प्रगति के लिए सुव्यवस्थित, सुनिश्चित, समान अवसरों को जुटाया गया है।
शैक्षिक अवसरों की समानता
‘समानता’ शब्द से तात्पर्य उन समान परिस्थितियों से है, जिनमें सभी व्यक्तियों को विकास के समान अवसर प्राप्त हो सकें और सामाजिक भेदभाव का अन्त हो सके तथा सामाजिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति भी सम्भव हो सके। प्रसिद्ध राजनीतिविद् प्रो. लास्की ने लिखा है-“समानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाये अथवा सभी को समान वेतन दिया। जाये। यदि एक पत्थर ढोने वाले का वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ या वैज्ञानिक के समान कर दिया जाये, तो इससे समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जायेगा। अतः समानता का अर्थ यह है कि विशेष अधिकार वाला वर्ग न रहे और सबको उन्नति के समान अवसर मिलें।”
शैक्षिक अवसरों की समानता का तात्पर्य सभी के लिए एक समान शिक्षा नहीं है, बल्कि प्रत्येक बालक की शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, नैतिक परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना है
धर्म इसका तात्पर्य राज्य द्वारा व्यक्तियों की शिक्षा के सन्दर्भ में जाति, रूप, रंग, प्रान्तीयता एवं भाषा, आदि के मध्य भेदभाव न करने से भी है।
शिक्षा के क्षेत्र में ‘समानता’ की अवधारणा को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किये गये हैं-
(1) एक निश्चित अवधि तथा भेदभावरहित निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था ।
(2) माध्यमिक स्तर पर विभिन्नीकृत पाठ्यक्रम व्यवस्था ।
(3) उच्च स्तर पर सभी के लिए अपेक्षित शैक्षिक उन्नति की व्यवस्था, ताकि वे उचित योगदान देने में सक्षम हो सकें
भारत में शिक्षा के अवसरों की विषमताएँ
“शिक्षा की चुनौती : नीति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य के बिन्दु 7.1″ में शिक्षा अवसरों की विषमताओं की जटिलताओं का निम्नलिखित रूप में उल्लेख किया गया है-
1. ग्रामीण और नगरीय विभिन्नता-
“बुद्धि, नैतिक, न्याय और घनिष्ठता की दृष्टि से शिक्षा की व्यवस्था में बहुत अधिक असमानता है। यद्यपि जनसंख्या का तीन-चौथाई भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, फिर भी उन्हें शिक्षा के लिए बहुत कम संसाधन प्राप्त हो रहे हैं। समृद्ध लोग शहरों में निजी रूप से चलायी जाने वाली अच्छी शिक्षण संस्थाओं का लाभ लेते हैं तथा ये ही व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं में आन्तरिक स्थानों के बहुत बड़े हिस्से पर अधिकार कर लेते हैं, जबकि ग्रामीण स्कूलों की अपेक्षाकृत दयनीय दशा के कारण ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है।
2. लिंग और जाति पर आधारित विषमता-
इसी प्रपत्र के बिन्दु 7.2 में लिंग पर आधारित असमानता तथा जातिगत असमानता के बिन्दुओं की विवेचना निम्नलिखित रूप में की गई है- “लड़कियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों ने पिछले देशक के दौरान उल्लेखनीय प्रगति की है। इसके उपरान्त भी वे शैक्षिक उपलब्धि के अन्तिम सोपान पर हैं। बालिकाएँ दो घर-गृहस्थी के कार्यों में अपनी दत्तचिन्तता तथा सामाजिक कुरीतियों की शिकार होती हैं, जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चे ऐसी अयोग्यताओं, जो स्थानों के आरक्षण से नहीं दूर की जा सकती हैं, के कारण उन्नति नहीं कर सकते। इनमें से अधिकांशतः पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी होने के कारण बाल्यकाल के कुपोषण, सामाजिक अकेलेपन की भावना, कार्य करने की खराब आदतें तथा अपनी बौद्धिक क्षमताओं के प्रति आत्मविश्वास के अभाव के कारण समुचित विकास नहीं कर सकते। वे अपने को सामान्य धारा के छात्रों से सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। इन मनोवैज्ञानिक दबावों के कुप्रभाव को समाप्त करने के लिए तथा उनकी योग्यताओं में बढ़ोत्तरी करने हेतु एवं समाज की प्रमुख धारा में उन्हें समन्वित करने के लिए विशेष कार्यक्रम की आवश्यकता है।”
3. डॉ. त्यागी एवं पाठक का मत-इन्होंने इन शैक्षिक विषमताओं का उल्लेख क्रमबद्ध ढंग से निम्नलिखित रूप में किया है-
(1) जिन स्थानों पर प्राथमिक, माध्यमिक या कॉलेज की शिक्षा देने वाली संस्थाएँ नहीं हैं, वहाँ के बच्चों को वैसा अवसर नहीं मिल पाता, जैसा उन बच्चों को मिल पाता है, जिनकी बस्तियों में ये संस्थाएँ उपलब्ध हैं।
शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य नोट्स
(102) Perspectives in Psychology of Teaching, Learning and Development
(102) shikshan adhigam evan vikaas ke manovigyaan ka pariprekshy
| विषय | शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य नोट्स |
| कोड | 102 |
| विश्वविद्यालय | महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बी.एड प्रथम सेमेस्टर |
| सेमेस्टर | प्रथम सेमेस्टर |
| lnfo | यहा से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बी.एड प्रथम सेमेस्टर के पेपर 102 शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य नोट्स को जल्द ही शामील किया जायेगा | |
लिंग विद्यालय एवं समाज नोट्स
(103) GENDER SCHOOL AND SOCIETY
(103) Ling vidyaalay evan samaaj
| विषय | (१०३) लिंग विद्यालय एवं समाज नोट्स , |
| विश्वविद्यालय | महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बी.एड प्रथम सेमेस्टर |
| सेमेस्टर | प्रथम सेमेस्टर |
| lnfo | यहा से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बी.एड प्रथम सेमेस्टर के पेपर लिंग विद्यालय एवं समाज नोट्स को जल्द ही शामील किया जायेगा | |
शिक्षा में क्रियात्मक अनुसन्धान नोट्स
(104) ACTION RESURCH IN EDUCATION
(104) shiksha mein kriyaatmak anusandhaan
| विषय | शिक्षा में क्रियात्मक अनुसन्धान नोट्स |
| कोड | 104 |
| विश्वविद्यालय | महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बी.एड प्रथम सेमेस्टर |
| सेमेस्टर | प्रथम सेमेस्टर |
| lnfo | यहा से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बी.एड प्रथम सेमेस्टर के पेपर 104 शिक्षा में क्रियात्मक अनुसन्धान नोट्स को जल्द ही शामील किया जायेगा | |
shiksha ka samaajashaastreey evan daarshanik aadhaaragat pariprekshy ,
shikshan adhigam evan vikaas ke manovigyaan ka pariprekshy ,
ling vidyaalay evan samaaj ,
shiksha mein kriyaatmak anusandhaan ,
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith B.Ed 1st Semester Notes