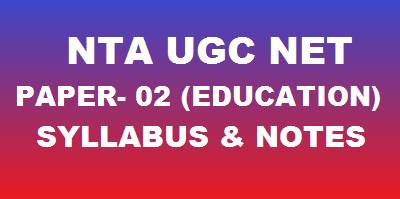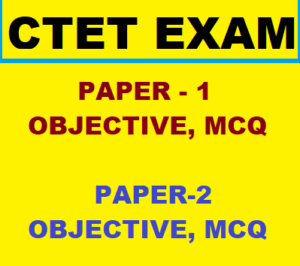NTA UGC NET EDUCATION SYLLABUS
| TOPIC | NTA UGC NET PAPER-2 EDUCATION SYLLABUS |
| SUBJECT CODE | 09 (EDUCATION) |
| SHORT INFO | VVI NOTES.IN के इस पेज में NTA UGC NET PAPER -02 EDUCATION में TEN (10) यूनिट है जिसका नाम निचे दिया गया है | 10 यूनिट के सिलेबस दिया जा रहा है | जिसे आप अध्ययन कर NTA UGC NET EDUCATIONका परीक्षा पास कर सकते है | |
UGC NET PAPER-2 EDUCATION EXAM PAITURN
NTA UGC NET शिक्षा (EDUCATION) के परीक्षा में 150 प्रश्न होंगे| यह परीक्षा 300 अंकों की होगी , जो 3 घंटे में हल किए जाएंगे। इस परीक्षा में 2 पेपर होंगे जिनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
| यूजीसी नेट पेपर -२ शिक्षा परीक्षा पैटर्न | |
| कुल मार्क | पेपर 1 – 100, पेपर 2- 200 |
| प्रश्नों के प्रकार | बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) |
| पत्रों की संख्या | यूजीसी नेट पेपर I – सामान्य , यूजीसी नेट पेपर-II – विषय संबंधित शिक्षा |
| प्रश्नों की संख्या | पेपर 1 – 50, पेपर 2- 100 यानि 150 |
| समय अवधि | 3 घंटे |
| नकारात्मक अंकन | नहीं. |
UGC NET PAPER २ EDUCATION SYLLABUS
| UGC NET PAPER -02 EDUCATION में दस यूनिट है | जिसका नाम निचे लिखा गया है | ये दस यूनिट के सिलेबस के अनुसार इसका उतर भी दिया जायेगा | |
- ईकाई 1 शैक्षिक अध्ययन
- इकाई 2 शिक्षा का इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र
- ईकाई 3 शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया
- ईकाई 4 अध्यापक शिक्षा
- ईकाई 5 पाठ्यचर्या अध्ययन
- ईकाई 6 शिक्षा में शोध
- ईकाई 7 शिक्षणशास्त्र, प्रौढशिक्षा विज्ञान तथा मूल्यांकन
- ईकाई 8 शिक्षा में/के लिए प्रौद्योगिकी
- ईकाई 9 शैक्षिक प्रबंधन, प्रशासन एवं नेतृत्व
- ईकाई 10 समोवशी शिक्षा
| NTA UGC NET/JRF NEWS – NOTES – PDF के लिए ग्रुप को ज्वाइन करे | |
| व्हाट एप ग्रुप |  |
| टेलीग्राम लिंक |  |
NTA UGC NET/JRF UNIT 1 SYLLABUS IN HINDI
ईकाई 1. शैक्षिक अध्ययन
(a) विद्या के विशेष सन्दर्भ में भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं (सांख्य, योग, वेदांत, बौद्ध, जैन) का योगदान, दयानंद दर्शन; तथा शैक्षणिक लक्ष्यों और ज्ञानार्जन की विधियों के प्रति इस्लामी परंपराएं ।
(b) पाश्चात्य विचारधाराओं (आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, व्यावहारिकतावाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद) का योगदान तथा सूचना, ज्ञान और प्रज्ञान के विशेष सन्दर्भ में शिक्षा में उनका योगदान ।
(c) ‘शिक्षा का समाजशास्त्र’ के प्रति विभिन्न उपागम (प्रतीकात्मक परस्परक्रिया, संरचनात्मक प्रकार्यवाद तथा संरचनात्मक प्रकार्यवाद तथा संघर्ष सिद्धांत)। सामाजिक संस्थाओं की संकल्पना, सामाजिक आंदोलनों के सिद्धांत (सापेक्ष वंचन, संसाधन जुटाना, राजनीतिक प्रक्रिया सिद्धांत तथा नव सामाजिक आंदोलन सिद्धांत)।
(d) समाजीकरण तथा शिक्षा-शिक्षा और संस्कृति; सामाजिक परिवर्तन के लिए शैक्षिक विचार के विकास में विचारकों (स्वामी विवेकानंद, रवीन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरोबिंदो, जे. कृष्णामूर्ति, पावलो फ्रेरे, वोल्स्टनक्राफ्ट, नेल नौडिंग्स तथा सावित्रीबाई फुले) का योगदान, भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित राष्ट्रीय मूल्य-शिक्षा के विशेष संदर्भ में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्या, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समानता, स्वाधीनता ।
NTA UGC NET/JRF UNIT 2 SYLLABUS IN HINDI
ईकाई 2 शिक्षा का इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र
(a) अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में समितियों और आयोगों का योगदान- माध्यमिक शिक्षा आयोग (1953), कोठारी शिक्षा आयोग (1964-66), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986, 1992), राष्ट्रीय शिक्षक आयोग (1999), राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005), राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2007), यशपाल समिति रिपोर्ट (2009), अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2009), न्यायमूर्ति वर्मा समिति रिपोर्ट (2012)।
(b) नीतियों और शिक्षा के बीच संबंध, शिक्षा नीति और राष्ट्रीय विकास के बीच संपर्क कड़ी, शिक्षा नीति तथा नीति निरूपण प्रक्रिया के निर्धारक तत्व : वर्तमान स्थिति का विश्लेषण, नीति विकल्पों का सृजन, नीति विकल्पों का मूल्यांकन, नीतिगत निर्णयन, नीति कार्यान्वयन की योजना बनाना, नीति के प्रभाव का आकलन तथा अनुवर्ती नीति-चक्र ।
(c) शिक्षा के अर्थशास्त्र की संकल्पना : शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण बनाम लागत प्रभावी विश्लेषण, उच्च शिक्षा को आर्थिक प्रतिफल-संकेतन सिद्धांत बनाम मानव पूंजी सिद्धांत, शैक्षिक वित्त-व्यवस्था की अवधारणा, सूक्ष्म एवं स्थूल स्तर पर शैक्षिक वित्त-व्यवस्था, बजट निर्माण की संकल्पना ।
(d) राजनीति और शिक्षा के बीच संबंध, शिक्षा की राजनीति संबंधी दृष्टिकोण-उदारवादी, रूढ़िवादी तथा समालोचनात्मक, राजनीति को समझने के उपागम – (व्यवहारवाद), प्रणाली विश्लेषण का सिद्धांत तथा तर्कसंगत विकल्प का सिद्धांत), राजनीतिक विकास का राजनीतिक समाजीकरण के लिए शिक्षा ।
NTA UGC NET/JRF UNIT 3 SYLLABUS IN HINDI
ईकाई 3. शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया
.
(a) वृद्धि तथा विकास : संकल्पना तथा प्रिंसिपुल्स, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं तथा संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, व्यक्तित्व :परिभाषाएं तथा सिद्धांत (फ्रायड, कार्ल रोजर्स, गोर्डन ऑलपोर्ट, मैक्स बर्थिमर, कुर्त कोफ्का), मानसिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वच्छता।
(b) बुद्धि के प्रति उपागम-ऐकिक से बहुलित तक : सामाजिक बुद्धि की संकल्पनाएं, बहुल-बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, स्टर्नवर्ग गार्डनर द्वारा प्रवर्तित बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि का निर्धारण, समस्या समाधान की संकल्पनाएं, समालोचनात्मक चिंतन, अधिसंज्ञान तथा सर्जनात्मकता ।
(c) अधिगम (ज्ञानार्जन) के नियम (प्रिंसिपुल्स) तथा सिद्धांत (थिअरिज) : अधिगम के व्यवहारपरक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, सामाजिक सक्षमता, सामाजिक संज्ञान की संकल्पना, सामाजिक संबंध तथा समाजीकरण के लक्ष्यों की समझ ।
(d) मार्गदर्शन तथा परामर्शन: प्रकृति, प्रिंसिपुल्स तथा आवश्यकता, मार्गदर्शन के प्रकार (शैक्षणिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत, स्वास्थ्य तथा सामाजिक और निदेशात्मक, गैर-निदेशात्मक एवं ), परामर्शन के प्रति उपागम-संज्ञानात्मक-व्यवहारवादी (एल्बर्ट एलिस-आर. ई.बी.टी.) और मानवतावादी, व्यक्ति-केंद्रित परामर्शन (कार्ल रोजर्स) परामर्शन के सिद्धांत (व्यवहारवादी, तर्क संगत, संवेगात्मक तथा यथार्थ)
NTA UGC NET/JRF UNIT 4 SYLLABUS IN HINDI
ईकाई 4. अध्यापक शिक्षा
(a) अध्यापक शिक्षा का अर्थ, प्रकृति तथा विषय-क्षेत्र; अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रकार, एन सी ई आर टी तथा एन सी टी ई के पाठ्यचर्या प्रलेखों में प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या की संरचना तथा इससे संबंधित दूरदृष्टि, सेवा- पूर्व अध्यापक शिक्षा के घटकों का संगठन संव्यवहारपरक उपागम ( आधारित पाठ्यक्रमों
के लिए) प्रतिपादक, सहयोगात्मक तथा अनुभवजन्य अधिगम ।
(b) शुल्मैन, डेंग तथा ल्यूक तथा हेबरमैन के दृष्टिकोण से अध्यापक शिक्षा के ज्ञानाधार को समझना, मननात्मक अध्यापन का अभिप्राय तथा मननात्मक शिक्षा के माडल्स : व्यवहारवादी, सक्षमता-आधारित तथा पूछताछ उन्मुख अध्यापक शिक्षा मॉडल्स ।
(c) सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की संकल्पना, आवश्यकता, उद्देश्य तथा विषय-क्षेत्र, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा का संगठन और इसकी विधियों की रीतियां, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर सेवकालीन अध्यापक शिक्षा की एजेंसियां और संस्थान (एस एस ए आर एम एस ए एस सी ई आर टी एन सी ई आर टी, एन सी टी ए तथा यू जी सी), सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की योजना बनाने से संबंधित विचारणीय प्राथमिक बिंदु (उद्देश्य, समयावधि, संसाधन तथा बजट) ।
(d) व्यवसाय तथा व्यवसायीकरण की संकल्पना, एक व्यवसाय के रूप में अध्यापन, अध्यापकों की व्यावसायिक आचार नीति, अध्यापक विकास को प्रभावित करने वाले वैयक्तिक तथा प्रसंगाश्रित कारक, आई सी टी एकीकरण, अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए गुणवत्ता प्रवर्धन, अध्यापक शिक्षा में नवप्रवर्तन ।
ईकाई 5. पाठ्यचर्या अध्ययन
(a) पाठ्यचर्या की संकल्पना तथा सिद्धांत, पाठ्यचर्या विकास की कार्यनीति, पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया की अवस्थाएं, नियोजन की आधारशिला – दार्शनिक आधार (राष्ट्रीय, लोकतंत्रीय) समाजशास्त्रीय आधार (सामाजिक-सांस्कृतिक पुनर्निर्माण), मनोवैज्ञानिक आधार (अध्येता की आवश्यकताएं तथा अभिरुचियां, बेंचमार्किंग तथा राष्ट्र-स्तरीय सांविधिक निकायों की भूमिका-पाठ्यचर्या विकास में यू.जी.सी. एन सी टी ई तथा विश्वविद्यालय की भूमिका)
(b) पाठ्यचर्या अभिकल्प के मॉडल : परंपरागत तथा समकालीन मॉडल (शैक्षिक/विषय-आधारित मॉडल, सक्षमता आधारित मॉडल, सामाजिक कार्य/क्रियाकलाप मॉडल (सामाजिक पुनर्निर्माण), वैयक्तिक आवश्यकताएं तथा अभिरूचि मॉडल, परिणाम आधारित एकीकृत मॉडल, हस्तक्षेप मॉडल, सी आई पीपी मॉडल (कांटेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस, प्रोडक्ट मॉडल)
(c) अनुदेशात्मक प्रणाली, अनुदेशात्मक मीडिया, पाठ्यचर्या संव्यवहार को बढ़ाने में अनुदेशात्मक तकनीकें तथा सामग्री, पाठ्यचर्या मूल्यांकन के उपागम : पाठ्यचर्या तथा अनुदेश के प्रति उपागम (शैक्षिक तथा सक्षमता आधारित उपागम), पाठ्यचर्या मूल्यांकन के मॉडल्स : टाइलर का मॉडल, स्टेक का मॉडल, स्क्रीवेन का मॉडल, किर्कपैट्रिक का मॉडल ।
(d) पाठ्यचर्या परिवर्तन का अर्थ और इसके प्रकार, पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, पाठ्यचर्या परिवर्तन के प्रति उपागम, पाठ्यचर्या परिवर्तन तथा परिष्कार में विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा शैक्षणिक प्रशासकों की भूमिका, पाठ्यचर्या शोध का विषय क्षेत्र तथा पाठ्यचर्या अध्ययनों में शोध के प्रकार ।
NTA UGC NET/JRF UNIT 6 SYLLABUS IN HINDI
ईकाई 6. शिक्षा में शोध
(a) शैक्षिक शोध का अर्थ तथा विषय-क्षेत्र, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ तथा चरण, वैज्ञानिक पद्धति के अभिलक्षण (अनुकरणीयता, परिशुद्धता, मिथ्यापनीयता तथा मितव्ययिता), वैज्ञानिक पद्धति के प्रकार ( गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक तथा वर्णनात्मक), एक वैज्ञानिक कार्यकलाप के रूप में शोध के लक्ष्य : समस्या समाधान, सिद्धांत निर्माण तथा भविष्य कथन, शोध के प्रकार (मौलिक, अनुप्रयुक्त, क्रियाशील), शैक्षिक शोध के प्रति उपागम (मात्रात्मक तथा गुणात्मक), शैक्षिक शोध में अभिकल्प ( (वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक तथा ऐतिहासिक) ।
(b) चर: अवधारणा, कंस्ट्रक्ट्स तथा चर, चरों के प्रकार (अनाश्रित, आश्रित, बाह्य, मध्यवर्ती तथा मॉडरेटर), प्राक्कल्पना- अवधारणा, स्रोत, प्रकार (शोध, निर्देशात्मक, गैर-निर्देशात्मक, निराकरणीय, प्राक्कल्पना निर्माण, प्राक्कल्पना के अभिलक्षण, नमूना चयन की तकनीकें (प्रायिकता तथा गैर-प्रायकिता नमूना चयन) शोध के उपकरण – उपकरण की विधि मान्यता, विश्वसनीयता तथा मानकीकरण, उपकरणों के प्रकार (कोटि-निर्धारण पैमाना, ( अभिवृत्ति निर्धारण पैमाना, प्रश्नावली, अभिक्षमता परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण, इंवेंटरी), शोध की तकनीकें (प्रेक्षण, साक्षात्कार तथा प्रक्षेपी तकनीकें ) ।
(c) मापन पैमाने के प्रकार (नॉमिनल, क्रमसूचक, अंतराल और अनुपात) मात्रात्मक डाटा विश्लेषण-वर्णनात्मक डाटा विश्लेषण (केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन, परिवर्तिता, विश्वासाश्रित सीमाएं तथा डाटा की रेखाचित्रात्मक प्रस्तुतिकरण) प्राक्कल्पना का परीक्षण (प्रकार I तथा प्रकार II की त्रुटियां), सार्थकता के स्तर, सांख्यिकीय जांच की शक्ति तथा इसके प्रभाव का आकार, प्राचलिक तकनीकें, गैर-प्राचलिक तकनीकें, प्राचलिक तकनीकों के प्रयोग के लिए संतुष्ट करने वाली स्थितियां, आनुमानिक डाटा विश्लेषण, सांख्यिकीय तकनीकों के उपयोग और विवेचन : सहसाहचर्य, टी-परीक्षण, जेड-परीक्षण, ए एन ओवी ए (अनोवा), काई-वर्ग (समान प्रायिकता तथा सामान्य प्रायिकता प्राक्कल्पना)। गुणात्मक डाटा विश्लेषण – डाटा न्यूनन तथा वर्गीकरण, वैश्लेषिक प्रवर्तन और कंस्टेंट कंपेरिजन, त्रिभुजन की अवधारणा ।
(d) गुणात्मक शोध अभिकल्प : ग्राउंडेड थियरी अभिकल्प (प्रकार, अभिलक्षण, अभिकल्प, जी टी रिसर्च संचालित करने में निहित चरण, जी टी सबलताएं और दुर्बलताएं) – विरणात्मक (नैरेटिव) शोध अभिकल्प (अर्थ तथा प्रमुख अभिलक्षण, विवरणात्मक शोध अभिकल्प के संचालन में निहित चरण), केस अध्ययन अभिकल्प के घटक, अर्थ, अभिलक्षण, केस अध्ययन अभिकल्प के प्रकार, केस अध्ययन शोध के संचालन में निहित चरण, सबलताएं और दुर्बलताएं), नृजाति वर्णन (अर्थ, अभिलक्षण, निहित पूर्वधारणाएं, नृजाति वर्णन शोध संचालन में निहित चरण, नृजाति पर ब्योरा -लेखन, सबलताएं तथा दुर्बलताएं) मिश्रित पद्धति अभिकल्प : अभिलक्षण, मिश्रित पद्धति अभिकल्प के प्रकार (विभुजन, व्याख्यात्मक तथा गवेषणात्मक अभिकल्प), मिश्रित पद्धति अभिकल्प के संचालन में निहित चरण, मिश्रित पद्धति की सबलताएं और दुर्बलताएं ।
NTA UGC NET/JRF UNIT 7 SYLLABUS IN HINDI
ईकाई 7. शिक्षणशास्त्र, प्रौढशिक्षा विज्ञान तथा मूल्यांकन
(a) शिक्षणशास्त्र, शिक्षणशास्त्र संबंधी विश्लेषण- संकल्पनाएं तथा चरण, आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र, अर्थ, आवश्यकता तथा अध्यापक शिक्षा में इसका निहितार्थ, शिक्षण का संगठन : स्मृति स्तर (हार्बर्टियन मॉडल), समझ स्तर ( मोरिसन टीचिंग मॉडल), परावर्ती स्तर (बिगे तथा हंट टीचिंग मॉडल ) शिक्षा में प्रौढशिक्षा विज्ञान की संकल्पना : अर्थ, नियम (प्रिंसपुल्स), स्व-निर्देशित अधिगम की सक्षमता, प्रौढशिक्षा का सिद्धांत (माक्लय नोल्ज), शिक्षार्थी स्वायत्तता का गत्यात्मक मॉडल ।
(b) मूल्यांकन – अर्थ, प्रकृति, दृष्टिकोण (अधिगम के लिए मूल्यांकन) अधिगम के लिए मूल्यांकन तथा अधिगम का मूल्यांकन, मूल्यांकन के प्रकार (पदस्थापन, प्रारंभिक, निदानात्मक, योगात्मक) उद्देश्यों और परिणामों के बीच संबंध, अधिगम के संज्ञानात्मक (एंडरसन तथा क्रैथवोहल), भावात्मक (क्रैथवोहूल) तथा साइकोमोटर (आर एच दवे) क्षेत्रों का मूल्यांकन ।
(c) शिक्षा के शिक्षणशास्त्र में मूल्यांकन : प्रतिपुष्टि युक्तियां : अर्थ, प्रकार, मानदंड, प्रतिपुष्टि की युक्ति के रूप में मार्गदर्शन : पोर्टफोलियो का विश्लेषण, रिफलेक्टिव, जर्नल, रूब्रिक्स का प्रयोग कर फील्ड एंगेज्मेंट, सक्षमता आधारित मूल्यांकन, अध्यापक निर्मित आई सी टी संसाधनों का मूल्यांकन ।
(d) प्रौढ़ शिक्षा का मूल्यांकन-अंतःक्रिया-विश्लेषण : फ्लैंडर का अंतः क्रिया विश्लेषण, गैलोवे की अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति (कक्षांतर्गत घटनाओं की रिकॉर्डिंग, अंतःक्रिया मैट्रिक्स का निर्माण और व्याख्या), अध्यापक मूल्यांकन के मानदंड ( उत्पाद, प्रक्रिया तथा पूर्वान मानदंड), स्व तथा समकक्ष मूल्यांकन के लिए रूब्रिक्स (अर्थ, निर्माण के चरण)
NTA UGC NET/JRF UNIT 8 SYLLABUS IN HINDI
ईकाई 8. शिक्षा में/के लिए प्रौद्योगिकी
(a) एक विषयानुशासन के रूप में शैक्षिक प्रौद्योगिकी (ईटी) की संकल्पना : (सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) तथा अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी, औपचारिक, गैर-औपचारिक (मुक्त तथा दूर-शिक्षा), अनौपचारिक, तथा समावेशी शिक्षा पद्धति में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक तथा रचनावादी सिद्धांतों का विहंगावलोकन और अनुदेशात्मक अभिकल्पों में उनका निहितार्थ (स्किनर, पियागे, आजूबेल, ब्रुनर, विगोत्सकी) अधिगम सिद्धांतों तथा अनुदेशात्मक कार्यनीति के बीच संबंध ( वृहद् तथा लघु एवं औपचारिक तथा गैर-औपचारिक समूहों के लिए)
(b) अनुदेशात्मक अभिकल्प के प्रति सिस्टम्स उपागम, अनुदेशात्मक अभिकल्प को विकसित करने के मॉडल (ए डी डी आई ई, ए एस एस यू आर ई, डिक तथा केयरी मॉडल मैंसन का) गैग्रे द्वारा प्रतिपादित ‘नाइन इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन’ तथा ‘फाईव
ईज ऑफ कंस्ट्रक्टीविज्म’, रचनावादी अनुदेशात्मक अभिकल्प के नौ तत्व, शिक्षा में कंप्यूटर का अनुप्रयोग सी ए आई सी, सी ए एल सी बी टी सी एम एल, कंसेप्ट, ओ डी एल एम तैयार करने की प्रक्रिया, ई-लर्निंग की अवधारणा, ई-लर्निंग के प्रति उपागम (ऑफलाइन, ऑनलाइन, सहकालिक, असहकालिक, मिश्रित अधिगम, मोबाइल अधिगम) ।
(c) ई-लर्निंग में उभरती प्रवृत्तियां : सामाजिक अधिगम (अवधारणा, अधिगम के लिए वेब 2.0 के साधनों का उपयोग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, चैट्स, वीडियो कान्फ्रेंसिंग, डिस्कशन फोरम), ओपेन एजुकेशन रिसोर्सेज (क्रियेटिव कॉमन, मैसिव ओपेन ऑनलाइन कोर्सेज; अवधारणा तथा अनुप्रयोग), ई-इंक्लुजन : ई-इंक्लुजन की अवधारणा ई-लर्निंग में सहायक – प्रौद्योगिकी का उपयोगकर्ता संतुष्टि और शुद्ध लाभ (डी एंड एम आई एस सक्सेस मॉडल, 2003) ई-शिक्षार्थियों तथा ई-अध्यापक-अध्यापन तथा शोध के लिए आचारनीतिक मुद्दे ।
(d) मूल्यांकन, प्रशासन तथा शोध में आई सी टी का प्रयोग : ई-पोर्टफोलियोज, शोध के लिए आई सी टी – ऑनलाइन रिपोजिटरीज तथा ऑनलाइन पुस्तकालय, ऑनलाइन तथा ऑफलाइन मूल्यांकन टूल्स (ऑनलाइन सर्वेक्षण टूल्स तथा टेस्ट जेनरेटर्स) – अवधारणा तथा विकास ।
NTA UGC NET/JRF UNIT 9 SYLLABUS IN HINDI
ईकाई 9. शैक्षिक प्रबंधन, प्रशासन एवं नेतृत्व
(a) शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन-अर्थ, सिद्धांत, कार्य तथा महत्व, संस्थानिक निर्माण, पोस्डकार्ब (पी ओ एस डी सी ओ आर बी), सी पी एम, पर्ट (पी इ आर टी), प्रबंधन – एक प्रणाली के रूप में, स्वोट (एस डब्ल्यू ओ टी) एनालिसिस, टेलरवाद, एक प्रक्रिया के रूप में प्रशासन, अधिकारी तंत्र के रूप में प्रशासन, प्रशासन के प्रति मानव संबंध उपागम, संगठनात्मक अनुपालन, संगठनात्मक विकास, संगठनात्मक वातावरण ।
(b) शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व : अर्थ तथा प्रकृति, नेतृत्व के प्रति उपागम : विशिष्टता, परिवर्तनकारी, कार्य संपादन परक, मूल्य आधारित, सांस्कृतिक, मनो-गत्यात्मक और करिश्माई नेतृत्व के मॉडल (ब्लेक तथा मुटन्स का प्रबंधकीय ग्रिड, फिडलर का कंटींजेंसी मॉडल, त्रि-आयामी मॉडल, हर्सी तथा ब्लेंचर्ड का मॉडल, लीटर-मेंबर एक्सचेंज थियरी) ।
(c) गुणवत्ता की अवधारणा तथा शिक्षा में गुणवत्ता : भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, गुणवत्ता का क्रम विकास : निरीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, गुणवत्ता आश्वासन, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन (टी क्यू एम), सिक्स सिग्मा, गुणवत्ता गुरु, वाल्टर सेवार्ट, एडवर्ड डेमिंग, सी के प्रहलाद ।
(d) परिवर्तन प्रबंधन : अर्थ, नियोजित परिवर्तन की आवश्यकता, परिवर्तन का त्रि-चरण मॉडल (अनफ्रीजिंग, मूविंग, रीफ्रीजिंग), परिवर्तन का जापानी मॉडल : जस्ट-इन-टाइम, पोकायोक, गुणवत्ता की लागत मूल्यांकन लागत, विफलता की लागत तथा निवार्य लागत, लागत लाभ विश्लेषण, लागत प्रभाविता एवं पहल, (राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद् (एन ए ए सी), कार्य निष्पादन संकेतक, भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यू सी आई), उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन एजेंसियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क (आई एम क्यू ए ए एच ई) ।
NTA UGC NET/JRF UNIT 10 SYLLABUS IN HINDI
ईकाई 10. समावेशी शिक्षा
(a) समावेशी शिक्षा : अवधारणा, सिद्धांत, विषय-क्षेत्र तथा लक्षित समूह (विविधतापूर्ण शिक्षार्थी; हाशिए पर स्थित समूह, अन्यथा सक्षम शिक्षार्थी), समावेशी शिक्षा के दर्शन का उद्विकास : विशेष, एकीकृत, समावेशी शिक्षा, विधिक प्रावधान : नीतियां एवं अधिनियम, (राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), प्रोग्राम ऑफ एक्शन (1992) निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, (1995) निःशक्तता पर राष्ट्रीय नीति (2006), राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (2005), आसमान शिक्षार्थियों के लिए रियायतें तथा सुविधाएं (शैक्षिक तथा आर्थिक), भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम (1992), सर्व शिक्षा अभियान एस एस ए के अंतर्गत समावेशी शिक्षा, एन सी आर पी डी (यूनाइटेड नेशंस कंवेंशन ऑन दी राइट्स ऑफ परसंस विद डिस्एबिलिटीज) तथा इसका निहितार्थ ।
(b) दोषग्रस्तता (इपेयरमेंट), दिव्यांगता (डिसएबिलिटी) तथा अपंगता (हैंडीकैप) की अवधारणा, आई सी एफ मॉडल के आधार पर दिव्यांगताओं का वर्गीकरण, विद्यालय की तैयारी, तथा समावेशन के मॉडल्स, असमान अध्येताओं का बाहुल्य, इनके प्रकार, अभिलक्षण तथा इनकी शैक्षिक आवश्यकताएं, बौद्धिक, शारीरिक तथा बहुल दिव्यांगता, दिव्यांगता के कारण तथा निवारण, समावेश हेतु असमान शिक्षार्थियों की पहचान, शैक्षिक मूल्यांकन की विधियां, तकनीक तथा उपकरण ।
(c) समावेशी कक्षाओं का नियोजन और प्रबंधन : आधारित संरचना, मानव संसाधन तथा अनुदेशात्मक व्यवहार, असमान शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यचर्या तथा पाठ्यचर्या अनुकूलन, असमान शिक्षार्थियों के लिए सहायक तथा अनुकूली प्रौद्योगिकीः उत्पाद (सहायक-साधन तथा उपकरण) तथा प्रक्रिया (व्यक्तिकृत शिक्षा योजना, उपचारात्मक शिक्षण), माता-पिता तथा पेशेवरों की भागीदारी, माता-पिता, समकक्ष व्यक्तियों, पेशेवरों, अध्यापकों, विद्यालय की भूमिका ।
(d) समावेशी शिक्षा में बाधाकारक तथा सुकारक तत्व : अभिवृत्ति, सामाजिक तथा शैक्षिक, भारत में समावेशी शिक्षा की समसामयिक स्थिति तथा आचारनीतिक मुद्दे, भारत में समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में शोध प्रवृत्तियां ।